| Sunday, 04 March 2012 16:20 |
कविता के दावे हमारे बड़े कवियों की कुछ उक्तियां याद की जा सकती हैं। अज्ञेय ने लिखा है कि 'मैं सच लिखता हूं, लिखकर सब झूठा करता जाता हूं' और मुक्तिबोध मानते थे कि 'साहित्य से बहुत अधिक की उम्मीद करना मूर्खता होगी।' श्रीकांत वर्मा ने पूरी आक्रामकता से कहा था कि 'मूर्खों, देश को खोकर ही मैंने प्राप्त की थी कविता।'
नए शब्द |
Sunday, March 4, 2012
बनारस में लोकसंपदा
बनारस में लोकसंपदा
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

 अशोक वाजपेयी
अशोक वाजपेयी 

































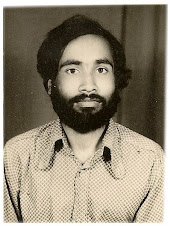

No comments:
Post a Comment