मंदिरों में जाएं, घंटा बजाएं और नक्सलाइट कहलाने से बचें!
मंदिरों में जाएं, घंटा बजाएं और नक्सलाइट कहलाने से बचें!

♦ उदय शंकर

जय भीम कॉमरेड का पोस्टर

विलास घोगरे

शीतल, कबीर कला मंच
मैं. जय भीम कॉमरेड देखने बहुत उम्मीद के साथ नहीं गया था। मैं आनंद की लगभग सारी फिल्मों से गहरे रूप से परिचित हूं और फिल्म का नाम इस परिचय के ऊपर एक झटके सा ही देता रहा था। झटके का एक मुख्य कारण जो मैं अनुभूत कर रहा था, वह यह कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जब मार्क्सवादी खेमे में एक खास तरह की निराशा देखने को मिल रही है और ऐसे दौर से आनंद भी अछूते रहेंगे इसकी उम्मीद तो थी लेकिन फिल्म के नाम से यह उम्मीद भी डगमगाने लगी थी। खैर, धन्यवाद अपने एक करीबी का, जिसके लगभग दबाव के कारण मैं इस फिल्म का साक्षी बन पाया। 'जय भीम कॉमरेड' आनंद के मित्र और प्रख्यात क्रांतिकारी-दलित गायक विलास घोगरे को एक रचनात्मक श्रद्धांजलि भी है। विलास घोगरे को मैंने पहली बार आनंद की ही फिल्म बॉम्बे: हमारा शहर में 'एक कथा सुनो रे लोगो… एक व्यथा सुनो रे लोगों… हम मजदूर की करुण कहानी, आओ करीब से जानो!!' गाते हुए देखा-सुना था। आनंद इस फिल्म (जय भीम कॉमरेड) में एक ऐसे ही फिल्म निर्देशक के रूप में सामने आते हैं, जो गरीब की 'करुण' कथा को करीब से जानने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। इसके पहले कि उनकी सारी फिल्में एक तरह से 'राजनीतिक' हैं। 'जय भीम कॉमरेड' शायद आनंद की पहली फिल्म है, जिसमें राजनीति तो है ही लेकिन इसके अलावा वे सांस्कृतिक और सामाजिक कथाओं-व्यथाओं को भी प्रमुखता से सामने लेकर आये हैं। विलास के उपर्युक्त चर्चित गीत के शब्दों को ध्यान से देखें, तो 'गरीब की करुण कथा' कोई सपाट पद नहीं है। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू को भी देखने का एक प्रबल आग्रह है। सिने-संसार में 'जय भीम कॉमरेड' अपने तईं इसी प्रबल आग्रह की पूर्ति करता है।
16 जनवरी, 1997 को लोकप्रिय ट्रेड यूनियन एवं कम्युनिस्ट नेता दत्ता सामंत की हत्या होती है और इसी के साथ मिल-मजदूरों के संगठन-संघर्ष का एक इतिहास खत्म होता है। बाल ठाकरे की मराठा-मान की राजनीति इस समय अपने चरम पर जाती है। 1 जुलाई, 1997 को बांबे के रमाबाई कालोनी में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान का विरोध दर्ज करा रहे दलितों पर पुलिसिया दमन होता है और उसमें दसियों प्रदर्शनकारी पुलिस की गोली से मारे जाते हैं और इसी घटना के बाद कवि विलास घोगरे आत्महत्या करके अपना प्रतिकार दर्ज करते हैं। इस 'विडंबनात्मक' आत्महत्या ने ही आनंद को इस फिल्म के लिए उकसाया है। 'विडंबना' कहने का तात्पर्य मेरा इससे है कि जो कवि जीवन भर मार्क्सवाद का अनुयायी बनकर जीवन का करुण गीत गाता रहा और अंत समय में खुद एक करुण कहानी बन गया, लेकिन विडंबना का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आत्महत्या करते समय विलास ने अपने सिर पर लाल झंडा नहीं बल्कि नीला रिबन लपेट रखा था। विचारधारा का यह सांकेतिक स्थानापन्न लगभग संदेश और सीख की तरह प्रेषित होता है। संदेश उनके लिए जो गरीबी की करुण कहानी जीते हैं और सीख उनके लिए जो सर्वहारा के हितैषी तो हैं लेकिन भारतीय सर्वहारा की सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्थितियों के बजाय वर्ग-संघर्ष के आर्थिक आधारों पर ही टिके रहे।
फिल्म का पहला भाग रमाबाई कालोनी की घटनाओं और दलित-अंबेडकरवादी राजनीति के चरम फैलाव को अपने आपमें समेटता है। किसी भी तरह की अस्मितावादी राजनीति की मजबूती और अपने समाज पर उसकी पकड़ को जानने के लिए उनके सांस्कृतिक उत्सव एक उम्दा औजार के रूप में काम करते हैं। अकारण नहीं है कि आनंद ने इस औजार का भरपूर इस्तेमाल किया है और फिल्म को रोचक, नाटकीय तथा संगीतमय बनाने में इस औजार का काफी योगदान है। नहीं तो इस तरह के विषयों पर documentary बनाना एक तरह का दस्तावेजी शगल मात्र रह जाता है। Documentary सिनेमा का एक मनोरंजन-प्रद रूप भी होता है और आनंद इसका भरपूर ख्याल रखते हैं। महाराष्ट्र में दलित-आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका पैमाना वहां के उत्सवों में, मसलन अंबेडकर-जयंती, महापरिनिर्वाण-दिवस आदि के दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बनाया जा सकता है। इन कार्यकर्मों को देख कर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह संस्कृति और इसी से जुड़ा उत्सव-मनोरंजन उनके विचारों और जीवन से ज्यादा अलग नहीं हैं। एक बड़े दलित नेता फिल्म में कहते हैं कि यहां दो तरह के अंबेडकरवादी हैं, एक जो अंबेडकर के भक्त हैं और दूसरे जो अंबेडकर के अनुयायी हैं। अंबेडकर अनुयायीपसंद हैं, न कि भक्ताहंकारी। लेकिन, मुझे लगता है कि किसी भी विचारधारा की सांस्कृतिक जड़ को मजबूत करने में, उसे एक 'जातीय' रूप देने में, 'भक्तों' की सबसे बड़ी भूमिका होती है और महाराष्ट्र के भीतर दलित-आंदोलन की मजबूती में, उसकी सांस्कृतिक जड़ों को गहरे तक जमाने में भक्तों की भूमिका से इनकार करना असंभव होगा। 'भक्त' आचरण और वाणी में फर्क नहीं करता है। लेकिन अनुयायी और भक्त के अनुपात में खाई खतरनाक साबित होती है। अंबेदकरवादियों में भक्तों की संख्या अनुयायियों के अनुपात में पहाड़ हो गयी है और मार्क्सवादियों में भक्त इक्का-दुक्का ही हुए होंगे।
भाजपा और शिवसेना के मोर्चेबंदी वाली सरकार के समय रमाबाई कालोनी में पुलिसिया दमन हुआ था। मनोहर जोशी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका मानना था कि ये अंबेडकर का नाम लेने वाले कोई अंबेडकरवादी नहीं हैं बल्कि नक्सलाइट हैं। पांच साल बाद सत्ता में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस आती है और उसका भी व्यवहार कोई अलग नहीं था। खैरलांजी की जाति-उत्पीड़न और यौन-हिंसा की घटना कांग्रेसी शासन-काल में ही घटित होती है। तब के अंबेडकरवादी नेताओं के भीतर भारतीय राजनीति के इन दो दक्षिणपंथी पालों को लेकर कोई गलतफहमी नहीं थी, इसलिए किसी भी तरह की खुशफहमी का सवाल ही नहीं उठता है। फिल्म का पहला भाग एक तरह से विलास भोगरे की पीढ़ी के अंबेडकरवादियों के क्रांतिकारी व्यवहारों को सामने लाता है। दलित आंदोलन का जो क्रांतिकारी पक्ष है, मसलन छुआछूत विरोधी आंदोलन, धार्मिक अंधविश्वास का नकार और उसके रचनात्मक प्रतिकार के साथ ही साथ अंबेडकर के विचारों को सांस्कृतिक-व्यवहार के धरातल पर अमल में ले आना आदि, उसको बहुत ही उम्दा ढंग से पर्दे पर ले आना आनंद की सफलता है। महाराष्ट्र के दलित-आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने बड़े पैमाने पर जन-गायकों और सांस्कृतिक टोलियों को सामने आने का मौका दिया, जो कि मार्क्सवादियों के अलावा कहीं और नहीं दिखता था और मार्क्सवाद में यह परंपरा इतनी कमजोर हुई कि इप्टा की सौवीं जयंती के अवसर पर उसको इतिहास की एक गौरवशाली थाती के बतौर ही याद कर पा रहे हैं। फिल्म का यह भाग आज के किसी भी 'पेशेवर' दलित चिंतक के लिए उत्साहजनक साबित होता है। साथ ही साथ मार्क्सवादियों को बगलें झांकने को मजबूर करता है। लेकिन फिल्म के एक दर्शक के नाते यह भाग मुझे कहीं से भी विचार के स्तर पर पेशेवर होने का मौका नहीं देता है। क्योंकि, प्रथमतया मैं फिल्म देखने गया था और मैं उससे संतुष्ट था। 'पेशेवर' विचारकों की तरह न हताश और न ही अति उत्साहित। बस संतुष्ट। बेशक, आनंद का कैमरा और संपादन-दृष्टि का योगदान तो इसमें है ही, साथ ही साथ नुआन्सेस लिए गुदगुदाते व्यंग्यबाण और अंधविश्वास से लबरेज हिंदू धर्मं के रीतिरिवाजों को फिर से जिलाने या तेज करने की संगठित कोशिशों और उसमें 'सबसे तेज' बन रहे मीडिया के योगदानों को हास्य से हास्यास्पद बना देने की कला आनंद के अलावा कहां है, मैं नहीं जानता।
फिल्म का दूसरा भाग पेशेवर विचारकों के लिए पलटमार का काम करता है। इसमें अंबेडकर के विचारों से किनाराकशी और निज-हित साधन हेतु दलित नेताओं के पतनशील व्यवहारों को केंद्रित किया गया है। कैसे वे अपनी जड़ों से कटते चले गये और वोट-बैंक की राजनीति में social engineering करते हुए निजी हितों को ही समुदाय का हित बता कर थोपने लगे। बहुजन से सर्वजन की राजनीति में स्थानापन्न इसी social engineering का उदहारण है। रमाबाई कालोनी में हत्या-कांड मचाने वाली भाजपा-शिवसेना कैसे उसी कालोनी में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम करने में सफल हो जाती है। अंबेडकरवादी युवाओं को एक समय आकर्षित करने वाली, मनुवाद और ब्राह्मणवाद को ठेंगे पर रखने वाली पार्टी RPI भाजपा-शिवसेना के साथ गठजोड़ में कैसे चली जाती है। कैसे दलित पैंथर के संस्थापकों में विचलन आता है आदि-आदि।
अंबेडकरवादी नेता या पार्टी भले दलाल हो गये हों, लेकिन अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के विचार दलित युवकों को अभी भी आंदोलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन युवाओं को संगठित होना है और ऐसे ही युवाओं का एक सांस्कृतिक संगठन है कबीर कला मंच। कबीर कला मंच विलास भोगरे के बाद वाली पीढ़ी के दलित युवकों का सांस्कृतिक संगठन है। यह संगठन न तो कॉर्पोरेट और न ही एनजीओ पोषित है। इसे किसी पार्टी का सांस्कृतिक मंच भी नहीं कह सकते हैं। यह सांस्कृतिक संगठन 'जय भीम कॉमरेड' के दूसरे भाग का बड़ा हिस्सा बनता है। दलित युवकों और युवतियों का यह मंच अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के विचारों को अपने गीतिनाट्यों में पिरोकर उसे गांवों में, मोहल्लों में प्रदर्शित करता है। आज जहां दलित विचारकों का एक तबका इंग्लिश देवी के मंदिर के निर्माण की बात करते-करते औपनिवेशिक भूत को और आज के अमेरिकी साम्राज्यवादी विस्तार को न्यायोचित ठहरा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के भीतर अंबेडकरवादी दलित युवकों-युवतियों का 'कबीर कला मंच' अपने नाटकों और गीतों के जरिये पश्चिम की सांस्कृतिक गुलामी को अपने कटाक्ष का विषय बना रहा है, बाजारवादी व्यवस्था और संस्कृति को नकारने की हिम्मत को रचनात्मक तेवर दे रहा है। 'जय भीम कॉमरेड' कॉमरेड इस नोट के साथ खत्म होती है कि अभी सात महीने पहले कबीर कला मंच को भूमिगत होना पड़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने उस पर माओवादी और नक्सलाइट होने का लेबल चस्पां कर दिया है। गीत, कविता, ढोल, ढपली और मंजीरा स्टेट के लिए शस्त्र बन गया है। आप भले कभी बंदूक छुए भी न हों लेकिन अगर आपकी ढपली पुलिस की गोली से तेज चलेगी तो आप नक्सलाइट हों जाएंगे। इसीलिए अगर नक्सलाइट कहलाने से बचना है तो मंदिर में जाएं और घंटा बजाएं, सुबह शाम आरती में शामिल हों और लड्डू खाएं।
फिल्म इस अंतर्दृष्टिपरक 'संदेश' के साथ खत्म होती है कि भारतीय मार्क्सवादी, भारतीय सर्वहारा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू को revisit करें। अंबेडकर के विचारों के क्रांतिकारी पहलुओं को समाहित करें। 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओ की विचारधारा' नामक पद भारतीय राजनीति में संभव है, तो इसमें अंबेडकर की विचारधारा को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है! लब्बोलुआब यह है कि दोनों धाराओं की 'आत्मालोचना' भी है यह फिल्म। हम जैसों के लिए फिल्म का यह 'प्रस्ताव' उत्साहजनक है और 'पेशेवरों' के लिए निराशाजनक। स्क्रीनिंग के बाद संवाद वाले सत्र में कुछ 'पेशेवर' फिल्म पर निराशाजनक समाप्ति का आरोप लगाते पाये गये। फिल्म में मार्क्सवादी राजनीति को बहुत विस्तार से नहीं देखा गया है और इससे जुड़ी आलोचनाएं क्रांतिकारी-दलित युवा संस्कृतिकर्मियों के द्वारा ही सामने आती हैं। अंत में यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि अंबेडकरवाद के व्यावहारिक धरातल की सांस्कृतिक भव्यता और राजनीतिक विपन्नता के द्वंद्व को इतनी सूक्ष्मता से कोई सामने लाया हो, मुझे पता नहीं, कम से कम सिने-संसार में तो कोई नहीं। उम्मीद करूंगा कि वे कभी इतने ही विस्तार से मार्क्सवादियों की बौद्धिक भव्यता और सांस्कृतिक विपन्नता को भी अपने आयोजन में शामिल करेंगे। इतनी भव्य योजना को पर्दे पर लाने के लिए आनंद पटबर्द्धन के लिए एक ही अभिवादन – जय भीम कॉमरेड।
…
 (उदय शंकर। वर्ष 2007 में जेएनयू से हिंदी में एमए और अब भी जेएनयू से ही पीएचडी के लिए शोधरत। तीन खंडों में आलोचक सुरेंद्र चौधरी के रचना संचयन का संपादन। सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ाव। छात्र राजनीति में भी सक्रिय। उनसे udayshankar151@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
(उदय शंकर। वर्ष 2007 में जेएनयू से हिंदी में एमए और अब भी जेएनयू से ही पीएचडी के लिए शोधरत। तीन खंडों में आलोचक सुरेंद्र चौधरी के रचना संचयन का संपादन। सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़ाव। छात्र राजनीति में भी सक्रिय। उनसे udayshankar151@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)







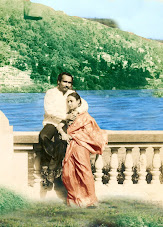












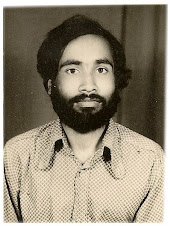

No comments:
Post a Comment