अरविंद मोहन
जनसत्ता 19 मार्च, 2012: उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय दलों की राजनीति पर गहरे सवाल उठाए हैं। पंजाब की तो नहीं, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी कुछ चतुष्कोणीय की जगह दो दलीय रूप लेती लग रही है और इस राज्य में कथित राष्ट्रीय दलों की भूमिका हाशिये की ही दिखती है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने स्वयं अपनी-अपनी पार्टी की चुनावी कमान अपने हाथ में रखी और अपना सारा जोर लगा कर देख लिया। राष्ट्रीय मीडिया भी क्षेत्रीय दलों की कम परवाह करता है। पर सबकी तैयारियां धरी रह गर्इं और बसपा गिरते-गिरते भी कांग्रेस और भाजपा से तिगुनी ताकत दिखा गई। वह लगभग तीन चौथाई स्थानों पर मुख्य मुकाबले में रही, जबकि कांग्रेस और भाजपा उत्तर प्रदेश में एक चौथाई सीटों पर भी सीधी लड़ाई में नहीं आ सकीं।
पर इसी से यह हिसाब लगाना भी आसान हो गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में यह स्थिति क्यों आई है। यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछले पचीस-तीस वर्षों से धीरे-धीरे यह स्थिति बन गई है कि आधे से ज्यादा राज्यों में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का अधिक दखल नहीं रह गया है। आम चुनाव में भी राष्ट्रीय दलों द्वारा जीती जाने वाली सीटों का अनुपात घटता गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत दिनों के बाद स्थिति थोड़ी-सी बदली थी और कांग्रेस के हक में बदली थी, सो कांग्रेसी बहुत उत्साहित थे और राजनीतिक पंडित भी क्षेत्रीय दलों वाली राजनीति का अंत देखने लगे थे।
जाहिर तौर पर ये सारे लोग अब कुछ मायूस होंगे। कांग्रेस की पिछले आम चुनाव की सफलता को कम करके आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अस्मिता की राजनीति की जगह सुशासन के सवाल पर चुनाव मैदान में उतरी थी और पहले से बेहतर प्रदर्शन करके आई थी। राजनीतिक पंडित इसे कांग्रेस प्रणाली की वापसी या कांगेस का चौथा जीवन मानते थे- बिल्ली के सात जनम की तरह।
अपने पहले जनम में तो कांग्रेस की भूमिका और दर्शन क्या थे यह बताने की जरूरत नहीं है। मुल्क जो भी है या इसका जो भी स्वरूप उभरा है वह उसी कांग्रेस ने, उसके नेता गांधी ने तैयार किया है।
आजादी के बाद की नेहरूयुगीन कांग्रेस को, उसकी कार्य प्रणाली को राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी कांग्रेस प्रणाली का नाम देते हैं। वे इस कांग्रेस के दर्शन की ज्यादा चर्चा नहीं करते, पर मानते हैं कि तब की कांग्रेस समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समूह को अपने अंदर जगह देने का प्रयास करती थी। एक इंद्रधनुषी छतरी जैसा सामाजिक गठजोड़ भी इसके पक्ष में दिखता रहा। हालांकि तभी मध्य जातियों और कई क्षेत्रों के लोगों का कांग्रेस से अलगाव प्रकट होने लगा था। पंजाब, तमिलनाडु, ओड़िशा और पूर्वोत्तर में कांग्रेस से अलग राह पर चलने की शुरुआत हो चुकी थी, पर नेहरू जी यह दिखाने का प्रयास जरूर करते रहे कि उनको सभी की परवाह है।
कांग्रेस प्रणाली ने राजीव गांधी की अगुआई में एक जबर्दस्त वापसी की- नेहरू युग का रिकार्ड भी तोड़ दिया और संसद में 413 सीटें लेकर आई। पर इस बार इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर का मामला था, देश के टूटने का डर था, यह अलग बात है कि वह वास्तविक भय था या बस उसका माहौल बना दिया गया था, और इन सबसे बढ़ कर प्रबंधकीय कौशल का कमाल भी जुड़ा हुआ था।
पर इस दौर का अंत और जल्दी हुआ- वही प्रबंधकीय कौशल के लोग बोफर्स घोटाले के आरोपों में फंस गए और वे घोटाले में सचमुच उनका कोई हाथ रहा हो या नहीं, इतना तो हर कोई जान गया कि उनकी मामले की तह तक जाने में कोई रुचि नहीं थी- उलटे वे आरोपों पर परदा डालने की कोशिश करते ही नजर आए।
इस घटना ने सौ साल की पार्टी की जड़ें खोद दीं और उसके बाद की कांग्रेस कभी भी अपनी पुरानी रंगत में नहीं लौट सकी। राजीव युग में ही दक्षिण के सारे राज्यों और हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर ने अलग राह पकड़ ली थी।
मंडल और मंदिर जैसी दो बड़ी राजनीतिक परियोजनाओं ने मुल्क की सियासत बदलने के साथ-साथ हर राज्य की राजनीतिक लड़ाई को एकदम अलग कर दिया, जिसमें अगर कथित राष्ट्रीय पार्टियां रहीं भी तो क्षेत्रीय दलों वाले तेवर और मजबूत स्थानीय नेता के बल पर- केंद्र से नेता थोपे जाने के दौर का अंत हो गया। कई राज्यों में तो कांग्रेस मैदान से बाहर ही हो गई।
नब्बे के दशक की सबसे प्रभावी परिघटना राज्य-स्तरीय राजनीतिक शक्तियों का उदय था और कई अर्थों में राष्ट्रीय राजनीति का मतलब राज्यों की राजनीति का कुल योगफल रह गया। गठबंधन मजबूरी नहीं धर्म हो गया। पर इस दौरान दुनिया के स्तर पर उभरी परिघटना यानी भूमंडलीकरण ने चुपके से मंडल और मंदिर को काटा या उनसे गलबहियां कर ली। इन दोनों धाराओं के अगुआ लोगों को इसमें कोई हर्ज नहीं लगा, उन्होंने इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई या इससे जुड़ने में उन्हें लाभ ज्यादा दिखा। भाजपा को स्वदेशी को छोड़ कर खुद को उदारीकरण का सच्चा हितैषी बताने में कोई संकोच नहीं हुआ। यही नहीं, सत्ता के लिए राम मंदिर, धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता की मांग को दफनाने में उसे कोई हिचक नहीं हुई। भाजपा सरकार ने स्वदेशी का नाम लेने वाले संघ परिवार के संगठनों को किनारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जैसे मडल के मंडल के धुरंधरों को कांग्रेस या भाजपा का दरबारी बनने और पेप्सी-वायदा कारोबार लाने वाला कहलाने में कोई झिझक नहीं हुई। नब्बे के बाद से लगातार सत्ता में बने रहे इन पिछड़ा नेताओं ने एक भी मामले में उदारीकरण का विरोध करने का रिकार्ड नहीं बनाया है। दूसरी तरफ तर्कवाद पर आधारित द्रविड़ आंदोलन केवल सत्ता की मलाई काटने और सत्ता के दुरुपयोग के रिकार्ड बनाने लगा।
मंडल-मंदिर और इन सब पर भारी बाजारवाद ने सारी राजनीति में ऐसा घोर-मट्ठा कर दिया है कि मुद्दों की, सिद्धांतों की, संगठन और विचारों की बात करना मूर्खता का काम लगने लगा है। कौन किस दल में है, किसे कहां से महंगी राजनीति करने-चुनाव लड़ने का खर्च आ रहा है, किस नेता का खर्च कौन उठा रहा है, कितने अपराधी संसद और विधानमंडलों में हैं इसका कोई हिसाब नहीं है या चुनाव आयोग और एडीआर जैसे स्वयंसेवी संगठन हिसाब लगाते भी हैं तो सारी चिंताएं कागजी होकर रह जाती हैं।
हर चुनाव में अपराधियों और करोड़पतियों का जीतना एक सूचना भर नहीं है। लेकिन एनजीओ संस्कृति में रचे-बसे लोग इस मुद्दे पर तथ्य सार्वजनिक जानकारी में लाने से अधिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनकी सीमा जाहिर हो जाती है। जब से चुनाव आयोग ज्यादा प्रभावी होने का दावा कर रहा है तब से चीजों का और बिगड़ना बताता है कि आयोग की भी सीमा को दर्शाता है।
राजनीति की असल बीमारी इस कवायद से दूर नहीं होगी। लेकिन दिखावटी राजनीति चल जा रही है। स्वदेशी वाली भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा लगाती है। दंगाइयों का बचाव करने वाले नरेंद्र मोदी विकास पुरुष बन जाते हैं। अगड़ों को खुलेआम जूते मारने की वकालत करने वाली नेता ब्राह्मण-बनिया सम्मेलन से सर्वसमाज की नेता बन जाती हैं। विकास की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ही सबसे तेज स्लर में पहचान की राजनीति का राग अलापने लगती है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की राजनीति न करने वालों का जमा-जमाया खेमा उखड़ जाता है।
पर सारा कुछ नकारात्मक ही नहीं हुआ है। आज क्षेत्रवाद का मतलब अलगाववाद नहीं रह गया है तो क्षेत्रीय नेता के केंद्रीय मंत्री बनने का मतलब अयोग्यता को बढ़ाने की मजबूरी नहीं है। मनमोहन सिंह भले गठबंधन की मजबूरी का रोना रोएं, पर सही कार्यसूची और खुली चर्चा में सहयोगियों से बात करके शासन चलाने का काम भी होने लगा है। करुणानिधि और प्रकाश सिंह बादल को केंद्र में आना चाहे न सुहाए, पर रामदॉस, रामविलास पासवान जैसे क्षेत्रीय नेताओं को दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी करना अच्छा लगता है। अभी तक कथित राष्ट्रीय पार्टियों के सहारे ही गठबंधन बनते थे, अब नीतीश कुमार या मुलायम सिंह की अगुआई में नया गठबंधन बनने की अटकलें शुरू हो गई हैं।
यह जरूर है कि अब भी हमारी शासन व्यवस्था केंद्र की तरफ झुकी हुई है और बहुत सारे मामलों में केंद्र अपनी मनमर्जी चलाता रहा है। उन विषयों में भी जो समवर्ती सूची में आते हैं या जिनमें राज्यों की भूमिका कहीं अधिक मानी जाती है। इसलिए केंद्र को यह भय सताता है कि क्षेत्रीय नेता आए और राज्यों का जोर बढ़ा तो जाने क्या हो जाएगा। यह पिंजड़े में रहने वाले पंछी जैसा मामला है।
दूसरी ओर, क्षेत्रीय नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि बड़ी राजनीति की तैयारी उनकी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक-दो मुद््दों या अपने फौरी सियासी गुणा-भाग से मतलब रहता है। शिबू सोरेन केंद्र में मंत्री बन कर भी झरखंडी ही रहते हैं और ममता बनर्जी बंगाल की रेलमंत्री थीं या भारत की, यह भेद मुश्किल हो गया था। विषयों का घालमेल भी है। आंतरिक सुरक्षा के मामलों में केंद्र की चिंता वाजिब लगती है, जबकि राज्य अपने अधिकारों और संघीय ढांचे की दुहाई दे रहे हैं।
नए चुनाव के बाद नई राजनीति हो। क्योंकि राष्ट्रीय दल पूरे मुल्क की आकांक्षाओं को समेट नहीं पा रहे हैं। बेहतर होगा कि अब तक की गठबंधन राजनीति के अनुभव को ध्यान में रख कर साफ संवाद और स्पष्ट घोषित साझा कार्यक्रम को आधार बना कर नए गठबंधन की राजनीति शुरू की जाए। मुलायम हों या ममता, नीतीश हों या जयललिता, सबको इसी दिशा में सोचना चाहिए। |







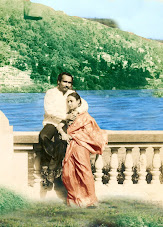












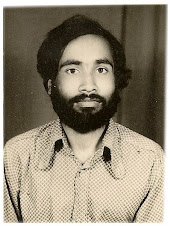

No comments:
Post a Comment