प्रेमचंद एक अनुभव
प्रेमचंद एक अनुभव
दयानंद पांडेय
 जिस बरस प्रेमचंद जन्मशती मनाई जा रही थी यानी 1980 में, जनवादी लेखक संघ ने प्रेमचंद के जन्म-स्थान लमही में त्रिदिवसीय प्रेमचंद मेला लगाया था। मैं भी गया था। बड़ी तड़क भड़क तो नहीं थी मेले में – मेला गंवईं भी नहीं था। मेला था कुछ जनवादी लेखक और रंगकर्मी बंधुओं का। मेले में गोष्ठियां हुईं, गोष्ठियों में फ़तवेबाज़ी हुई। फ़तवेबाज़ी में कई खुश हुए और कई नाराज। गांव के लोग यानि लमही के 'लाला जी लोग' यह सब ताकते रहे थे दूर-दूर से। और सी.आई.डी. वाले चोरी छिपे अपनी रिपोर्ट लिखते रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगभग कटे कटे से यह सब देख रहे थे। हैरानी कई बातों को ले कर हो रही थी:
जिस बरस प्रेमचंद जन्मशती मनाई जा रही थी यानी 1980 में, जनवादी लेखक संघ ने प्रेमचंद के जन्म-स्थान लमही में त्रिदिवसीय प्रेमचंद मेला लगाया था। मैं भी गया था। बड़ी तड़क भड़क तो नहीं थी मेले में – मेला गंवईं भी नहीं था। मेला था कुछ जनवादी लेखक और रंगकर्मी बंधुओं का। मेले में गोष्ठियां हुईं, गोष्ठियों में फ़तवेबाज़ी हुई। फ़तवेबाज़ी में कई खुश हुए और कई नाराज। गांव के लोग यानि लमही के 'लाला जी लोग' यह सब ताकते रहे थे दूर-दूर से। और सी.आई.डी. वाले चोरी छिपे अपनी रिपोर्ट लिखते रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगभग कटे कटे से यह सब देख रहे थे। हैरानी कई बातों को ले कर हो रही थी:
- कि प्रेमचंद मेले में सी.आई.डी. वालों की दिलचस्पी क्यों है?
- कि इस मेले में इस तरह की फ़तवेबाज़ी की ज़रुरत क्या है?
- कि लमही के लाला लोग प्रेमचंद मेले में हिस्सेदार क्यों नहीं हैं?
- कि यह प्रेमचंद मेला है या कुछ शहरियों का पिकनिक?
जो भी हो इन सवालों का जवाब बहुत मुश्किल नहीं था – सब के पास था। लेकिन इन सारी बातों को जबान पर ला कर कोई भी मजा बदमजा नहीं करना चाहता था। हां मजा।
इस मेले में हिंदुस्तान के लगभग हर कोने; कस्बों से महानगर तक के महिला पुरुष, युवक युवतियां आए थे। लगभग तीन साढ़े तीन सौ लोग रहे होंगे, जिन में बहुत मजे हुए लोग भी थे और एकदम नए भी। इन में बहुत सारे कस्बाई ऐसे थे – जो 'महानगर' को नहीं देखे थे। बहुत से 'महानगरीय' ऐसे थे जो 'गांव' नहीं देखे थे। और मजा यह कि दोनों 'महानगर' और 'गांव' फ़िल्मों में देखे हुए थे। और उसी आधार पर अपना- अपना आकलन बिठा रहे थे। तो गांव के लोग महानगर न देख – महानगरियों को 'घूरते' रहे…बड़े निरापद भाव से । सहज और सरल हो कर या कहिए इस का पन दिखा कर। और महानगरीय लोग लमही में अपना वह 'फ़िल्मी गांव' ढूंढ रहे थे। जो ढूंढे नहीं मिला था – उन्हें। तो भी लमही में भारी बागीचा था। मंदिर और तालाब समेत सारी गवंई चीज़ें उपलब्ध थीं। एक वाकिया बताऊं।
'सांझ का समय था। जून का उमस भरा महीना। हवा एकदम बंद थी। कुछ महानगरीय लड़कियां, जिन्हें गोष्ठियों में मजा नहीं आ रहा था, गांव घूमने का इरादा बना बैठीं। हम भी उन के साथ थे। एक किसी गरीब घर में वे ताबड़ तोड़ घुसीं। उस घर की बेटियां और बहुएं चिहुंक कर परदे में हो गईं। घर की 'बूढ़ा' ने घूंघट काढ़े भरसक खातिरदारी की। वह बिना बोले बेना (हाथ पंखा) के जुगाड़ में थीं, और यह 'देवियां' अपने अपने कपड़ों की शिकन सवांरते क्रीज़ उभारते बोल रही थी, 'हाय क्या तो अभी ठंडी हवा चल रही…आ हा…!' और 'बूढ़ा' ने कहा, 'हां बचवा!' इस बेतहाशा गरमी में भी इन 'देवियों' को 'ठंडी ठंडी हवा' इस लिए लग रही थी 'वह गांव में थीं…।' वैसे तो लमही के इन तीन दिनों के किस्से बहुत हैं। फिर कभी अलग से बयान करुंगा। यों लमही में मैं व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों से मिला। प्रेमचंद के बारे में उन से जानना चाहा। अधिकांश प्रेमचंद को इतना ही जानते थे कि वे एक लेखक थे। उन्हें इस बात पर गर्व था बस। या फिर वे अपने वंशज के रूप में अपने परदादा, दादा, काका, भइया के रूप में ही जानते थे – इस का भी उन्हें गर्व था। और कुछ बुजुर्गों के पास सिर्फ़ उन्हें देखने भर की एक धुंधली सी याद थी और कुछ नहीं। सच तो यह है कि एक आम हिंदुस्तानी की तरह उन्हें भी अपनी सामान्य जिंदगी से फुर्सत नहीं मिलती कि वह कुछ 'इस तरह' का सोचें – उन के अपने ही महाभारत से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। चाहे वह नई पीढ़ी हो या बीच की या बूढ़ी पीढ़ी। सब का अपना अपना रोना है।
लमही गांव की अन्य जातियों में लोग प्रेमचंद के बारे में यही जानते हैं कि वह लाला थे, मनसिधुवा थे। बड़े बढ़िया आदमी थे… बस। उन की नई पीढ़ी जो सिर्फ़ 'साक्षर' है, प्रेमचंद नाम भी नहीं जानती। बहुत कुरेदने पर गांव में उन की मूर्ति याद दिलाने पर उन का कहना था कि – 'अरे हां, उन का त जानी ले..'.का जान ल?' पूछने पर वह चुप ही रहे।
प्रेमचंद की यह स्थिति लमही ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। क्यों कि प्रेमचंद सरकारी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उपेक्षित हैं – यहां तक कि साहित्यिक तौर पर भी।
कहने को तो प्रेमचंद को मैं ने भी तब जाना जब पांचवीं या छठवीं में पढ़ता था। 'पंच परमेश्वर' और 'ईदगाह' के मार्फ़त। वैसे ईमानदारी की बात यह है – प्रेमचंद को मैं तब न जानता था। एक सामान्य पाठ्यक्रम की दृष्टि से उन्हें पढ़ा था। पढ़ाया ही ऐसे गया। तब साहित्य में मेरी दिलचस्पी भी न थी। दिलचस्पी तो दूर साहित्य क्या बला है से अनभिज्ञ, साहित्य शब्द से ही गोल था।
हां तो मैं कह रहा था कि प्रेमचंद को मैं ने जाना – 'पंच परमेश्वर' और 'ईदगाह' के मार्फ़त। वो भी इम्तहान के लिहाज़ से। और हम हमारे सहपाठी प्रेमचंद को कम हामिद ईदगाह का मेला, दादी, हामिद के समवयस्कों को अधिक जानते महसूसते थे। बल्कि जब वह कहानी पढ़ी थी, उस साल दशहरे के मेले में जाते वक्त हर दोस्त हामिद जैसा उत्साह बल्कि अतिरिक्त उत्साह जता रहा था। लेकिन हामिद जैसी संवेदना हम में न थी, इसे भला कैसे नकार सकता हूं। बल्कि इस के पूर्व 'पंच परमेश्वर' पढ़ कर लगता था कि अरे, यह तो हमारे गांव की कहानी है। हमारे बाबू जी(चाचा) की एक छोटी बिटिया थी – मंजू। 'पंच परमेश्वर' के चाव में हम उसे 'जुम्मन जुम्मन' कहने लगे। कहने क्या चिढ़ाने लगे। बात यहां तक बढ़ी कि बड़की माई (चाची) से डांट खानी पड़ी। बड़की माई ने कहा, 'का ई मुसुरमाने क बिटिया है…कि जुम्मन जुम्मन कह ल…।' लेकिन आदत नहीं गई…और सीधे जुम्मन जुम्मन न कह कर मंजू मंजू इस लहजे में कहते कि वह जुम्मन बन जाए मतलब कि वह चिढ़े भी और हम डांट भी न खाएं…। लेकिन डांट खाने से बढ़ कर नौबत कनेठी और तमाचा खाने की भी आ गई। तब मैं ने बड़की माई को पलट कर जवाब दिया था, 'हम उसे मुसलमान कहां बनाते हैं? हम तो उस के नाम 'मंजू' का उलटा भर कर करते हैं – और वह जुम्मन हो जाए तो हम क्या करें – आपने नाम ही ऐसा रखा है – नहीं अच्छा लगता तो – नाम ही बदल डालिए!' तब इतनी समझदारी न थी न ही इतनी हिम्मत कि बड़की माई से कहता कि, 'मुसलमान भी हाड़ मांस का होता है – और हमारे ही जैसा। बस नाम में ही फ़र्क होता है…'।
बहरहाल यह किस्सा कई दिनों तक चला। बड़ी घटनाएं घटी। अब हम किशोर हो रहे थे। 'गुल्ली डंडा' और 'दो बैलों की कथा' तक आ पहुंचे थे। और अपने को एक अजीब दुनिया में पा रहे थे। 'गुल्ली डंडा' खूब छक कर खेलते कोई 'बड़ा' मना करता तो पलट कर पूछते कि, किताब में भी कभी कुछ गलत लिखा होता है…। जवाब मिलता, 'नहीं तो!' और तब हम अपनी अकल के मुताबिक 'बघारते' हुए बताते कि हमारी हिंदी की किताब में पढ़िए, गुल्ली डंडा…!' और वह चुप हो जाते। अपने बैलों में हीरा मोती की ही छाप ढ़ूंढता…नाद…कनहौद…सब कुछ वैसा ही। लेकिन प्रेमचंद कौन बला हैं – हम तब भी नहीं ही जानते थे। हम जानते थे सिर्फ़ उन कहांनियों को; जिन में हम अपनी चेतना, अपना आस-पास देखते महसूसते। लेकिन यह तो महसूस होने ही लगा था कि यह बात हर कहानी में नहीं मिलती – और भूख बढ़ती गई, ऐसी कहानियों को पढ़ने की। फिर जानकार लोगों ने कहा, प्रेमचंद की कहानियां खरीद कर पढ़ो…। अभी खरीदने की जुगत लगा ही रहा था कि गरमियों की छुट्टी में एक दोस्त से 'निर्मला' पढ़ने को मिली। 'मंसाराम, तोता राम…बतौर शैलेष जैदी,…सामान्य पाठक के लिए निर्मला में 'आह' और 'वाह' की पर्याप्त सामग्री है…।' तो साहब हम भी निर्मला के 'आह' और 'वाह' से मुक्त न हो सके। और यहीं से लत पड़ी उपन्यासों को पढ़ने की।
इस बहाव में आ कर बहुत सारे सड़ियल उपन्यास अधिक, पोख्ता उपन्यास कम पढ़े – ये ससुरे पल्ले ही नहीं पड़ते थे और उपलब्ध भी नहीं होते थे आसानी से। खैर इस उपन्यास पढ़ने की लत ने भारी नुकसान दिया। ग्यारहवी में फेल हुआ। फेल कैसे न होता – पाठ्यक्रम की किताबों के नीचें जो एक किताब हुआ करती थी – वह चाहे क्लास हो या घर। बिना पढ़े चैन ही नहीं आता था। हर वक्त गुलशन नंदा, कर्नल रंजीत वगैरह ही दिमाग में छाए रहते। यहां यह बता दू कि प्रेमचंद का रंग दिमाग से उतर चुका था…बुजुर्गों की राय में दीवाना हो चला था। समझदारी के किले तोड़ता – दीवानगी की हद तोड़ रहा था। बहरहाल फेल हुआ तो क्या – गरमी की छुट्टी तो हुई ही। और हर साल की तरह गया गांव, छुट्टी बिताने। अम्मा ने कहा, मौसी के वहां ज़रा हो आओ। मौसी के यहां गया। वहां मौसी के एक देवर थे। पॉकेट बुकों का एक भारी खजाना रख रखा था। मैं गया दो दिनों के लिए था लौटा दस दिन बाद। वह भी बड़े बेमन से। तो भी कुछ पॉकेट बुक्स मांग लाया था। पढ़ता रहता । अम्मा खुश रहतीं कि बेटा फेल हुआ – इस को महसूस कर रहा है और खूब पढ़ रहा है। उसे क्या पता कि मैं कोर्स नहीं पॉकेट बुक्स पढ़ रहा हूं, यानि फिर फेल होने की तैयारी…बहरहाल अम्मा अम्मा थी और मैं मैं।
गांव में एक हिंदी से एम.ए. चाचा जी थे। बेकार चल रहे थे उन दिनों। अब एक डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हो गए हैं। लेकिन भारतेंदु को 'भारतेंदू जी' ही कहते हैं – और साहित्य की कोई बात हो तो खैनी रगड़ते हुए वह भारतेंदू जी पर ही ला पटकते हैं… इतना कि हम लड़के उन्हें 'भारतेंदू जी' ही नाम से नवाजने लगे। बहरहाल तब उन्हें चाचा कहता था। उमर में काफी बड़े थे पिता जी से कुछ ही बरस छोटे। लिहाज़ ज़बरदस्त ढंग से करना पड़ता था। उन दिनों मुझे ट्रांजिस्टर से फ़िल्मी गानों के सुनने का शौक भी जोर मारने लगा था। गांव में अपने घर ट्रांजिस्टर उपलब्ध न था। सो दुपहरिया में गाने सुनने अपने एक हमजोली दोस्त के पास जाता था। इत्तफाक ही था कि एम.ए. चाचा का वह भतीजा लगता था। भतीजा तो मैं भी लगता था लेकिन ज़रा दूर का। वह सगा था। बहरहाल 'फिल्मी गाना सुनने जाता था लेकिन हमेशा तो गाने नहीं आते थे ट्रांजिस्टर पर। सो बकिया वक्त काटने के लिहाज़ से वहीं पॉकेट बुक्स साथ होते थे। एक दिन मैं पढ़ ही रहा था कि – शायद गुरुदत्त थे कि वही एम.ए. चाचा आ पड़े। मेरे पास पॉकेट बुक देख कर खिल उठे। बोले, 'का रे दयवा…बड़ी नीक किताब लेल बाड़े, देखीं त…' सकुचाते लजाते वह पॉकेट बुक उन्हें थमा मैं फुर्र हो गया। और चोरी पकड़ी गई…सोच सोच कर दिल धक-धक करने लगा। दूसरी सुबह एम.ए. चाचा हाजिर। वह किताब हाथ में लिए आते दिखे…मैं मरा जा रहा था। आते ही मुझे गुहराने लगे अपनी ही शैली में, 'दयवा रे…!' मैं नहीं आया छोटे भाई को भेज दिया। लेकिन उन्हों ने मुझे बुलाया। बड़े स्नेह के साथ वह पॉकेट बुक वापस दी और दुलराते हुए पूछा, 'औरो किताब धइले बाटे..'। मैं गदगद हो उठा था उन के स्नेह से। दौड़ा-दौड़ा घर में गया तीन चार पॉकेट बुक्स ला कर उन्हें थमा दी। फिर तो यह सिलसिला निकल पड़ा – वह मुझ से पॉकेट बुक्स लाते – मैं उन से। अम्मा और खुश हुई कि '…' बहरहाल यह सिलसिला शुरू हुए कुछ ही दिन हुए होंगे कि पिता जी आए। मैं शरमाया-शरमाया सा आंख चुराए रहने लगा – फेल जो हो गया था…। तिस पर आग में घी भी पड़ गया…। हमारे एम.ए. चाचा ने बताया कि आप का लड़का खराब हो रहा है, उपन्यास पढ़ने लगा है…। और शाम मेरी शामत हाजिर थी। वो डांट पिलाई गई कि मत पूछिए। बहरहाल, तफ्तीश के दौरान पाया गया कि मैं यह सारी किताबें मौसी के वहां से लाया हूं, पहले भी मौसी बदनाम थीं। मैं जाता था – वह भेंट में पर्याप्त पैसे देती थीं – और मैं उसे सिनेमा में उड़ाता था – क्लास छोड़-छोड़ कर…। वैसे भी मौसी बड़ी प्रिय थीं मुझे, अब भी उतनी ही प्रिय हैं। खैर, पूछा गया, मैं मौसी के यहां फिर क्यों गया था। मैं ने कोई चारा न देख बताया, अम्मा ने भेजा था। अम्मा की भी खबर ली गई। और फ़ैसला हुआ कि मौसी क्या किसी भी रिश्तेदार के यहां आना जाना बिलकुल बंद। सारी पॉकेट बुकें जब्त। जुलाई करीब थी, किसी तरह काटा। स्कूल खुला। शहर आ गया। फिर कोर्स में जुट गया। लोगों ने कहा साइंस तुम्हारे बस की नहीं, छोड़ दो। साइंस छोड़ दी। कला विषय ले लिए। अब वक्त ही वक्त होता – मन नहीं मानता – फिर उपन्यासों की ओर आया। पिता जी ने कहा, 'पढ़ना ही है तो ज़रा ढंग की किताबें पढ़ो – क्या उपन्यासों के चक्कर में पड़े रहते हो – वो भी जासूसी फासूसी।' पिता जी के एक मित्र थे। उन्हों ने 'सत्यार्थ प्रकाश' दी। सच, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। एक दिन घूमते-घामते एक बुक स्टाल पर गया – 'प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां' देखीं मन में आया खरीद लूं। किताब एक रुपया की थी। जेब में चवन्नी भी न थी। मन मार कर रह गया। पिता जी से इस मद में पैसे मांगते भी डर लगता था। कि मुहल्ले की एक लड़की जो उमर में मुझ से काफी बड़ी थी के पास वही किताब देखी। मैं ने कहा, 'दीदी इसे मुझे भी पढ़ने को दे दीजिए न!' दीदी पिघल गईं और यह कहते हुए कि, 'गायब नहीं करना, न फाड़ना, जल्दी ही वापस कर देना…।' जाहिर है दीदी मुझे कोरा नादान समझ रही थीं। मैं तब नेकर पहनता ज़रुर था लेकिन क्या क्या खुराफातें सोचा करता था- कोई भी भला क्या जाने…।
मुझे आब भी याद है – वह बरसाती दिन। और दिन भर में ही सारी कहानियां पढ़ गया था। पूस की रात, कफन, मिस पद्मा, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, बड़े घर की बेटी, गृहदाह आदि…और मैंने अब प्रेमचंद की रचनाएं, किताबें ढूंढ ढूंढ कर पढ़नी शुरू कर दी। सच बताऊं – और लेखक रुमानी तौर पर जितना उड़ाते थे – प्रेमचंद नहीं उड़ा पाते थे – हमारे किशोर दिमाग को। प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी एक अजीब टूटन और घुटन सी होने लगती। लेकिन तभी लगा कि यह ईदगाह से गुल्ली डंडा की यात्रा में मैं भी शामिल…। कफन, पूस की रात, सदगति से पूरा पूरा तो नहीं कहीं कहीं साक्षात्कार ज़रूर हो जाता था – अपने गांव की चमरौटी में। खास कर अपने गांव की चौहद्दी में प्रेमचंद के पात्रों को मैं भरा-पुरा पाने लगा था, चाहे वह रंगभूमि के हों – गबन या गोदान के।
रुढ़ियों, शोषकों के जबड़े में फंसे प्रेमचंद के पात्रों को देख कर अजीब सी उत्तेजना मन में समा जाती। जब कि उन रुमानी जासूसी उपन्यासों के चरित्र देखना, महसूसना तो दूर, सोचने में भी कहीं नज़र नहीं आते…। कोफ्त होने लगती। मैं पछताने लगा कि उफ्फ इतना सारा वक्त मैं ने इन बेहूदी किताबों पर क्यों जाया किया? अब मैं बी.ए. में पढ़ने लगा था। हिंदी, अंगरेजी, संस्कृत लिए थे। इस लिए साहित्य चाहे वह किसी तरह का हो – पढ़ने की मनाही न थी। भीतर ही भीतर यह समझा जाने लगा कि लड़का 'समझदार' होने लगा है…लेकिन आलमारी की तलाशी कभी कभार हो ही जाती कि 'लड़का, क्या पढ़ रहा है और बार बार जबानी तौर पर भी ताकीद की जाती, 'कोर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो पछताओगे…।' सचमुच मैं कोर्स पर ध्यान कम बेस क्या नहीं ही दे पाता था – जी उचट गया था। कुछ 'कामरेड' दोस्त मिल गए थे, उन्हों ने पूरी तौर पर कनविंस कर रखा था कि यह शिक्षा प्रणाली घटिया है, सो यह अकादमिक पढ़ाई करना भी घटियापन के सिवा कुछ नहीं। और मैं भी बाकायदा जब तब 'यह सब' लोगों को सुनाने लगा था! लोग सुनते – ऊबते और उकता कर खिसक लेते। मैं किला फतह समझता। नतीज़ा यही निकला कि फिर फेल हुआ। कई मोड़ों पर । टूटते जुड़ते तमाम लेखकों से गुज़रा फिर प्रेमचंद की ओर आ पलटा। [ इस बीच थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने लगा था। कब कैसे यह दूसरी बात है।] प्रेमचंद मुझे अपनी दीवानगी, असफलता, संघर्ष हर कहीं अपने साथ मिलते। यह वह घड़ी थी जब मैं प्रेमचंद को सिर्फ ऊपर ही ऊपर जानता था। गोरखपुर में रहता था। और यह भी नहीं जानता था कि प्रेमचंद यहां कभी बचपन के अनमोल क्षण और प्रौढ़ता के जुझारूपन से गुज़रे हैं। बाले मियां के मैदान रोज जाता, खेलने-घूमने। रावत पाठशाला, तुर्कमानपुर, नार्मल स्कूल, घंटाघर और रेती के पास से भी कभी कभार ज़रूर गुज़रता। कभी पैदल, कभी साइकिल से। लेकिन बेखबर कि प्रेमचंद का यहां से कभी कोई वास्ता रहा होगा। साहित्यिकों में विश्वविद्यालय में कभी कोई चर्चा भी न करता – इन सारी बातों की – और प्रेमचंद की रचनाएं छोड़ उन के बारे में फिलहाल गंभीरता से, कुछ पढ़ने को न मिला था – तो क्या मैं सपना देखता कि प्रेमचंद गोरखपुर में… ।'
खैर, 31 जुलाई को नार्मल स्कूल के कुछ छात्रों ने एक गोष्ठी रखी – मुझे भी बुलाया गया…फिर मालूम हुआ कि अरे, प्रेमचंद और गोरखपुर…हद है …मैं बड़ा अभिभूत हुआ। और सचमुच पहली बार प्रेमचंद से बड़ी आत्मीयता महसूस हुई। हद दरजे की आत्मीयता। नार्मल स्कूल, रेती चौक, बाले मियां का मैदान मेरे लिए अब पहले जैसा निर्जीव नहीं रह गया था। कह सकते हैं – ये जगहें मेरे लिए मक्का मदीना सी बन गईं। फिर प्रेमचंद और गोरखपुर के मुत्तलिक मैं ने जानकारी लेनी शुरू कर दी – बड़े उत्साह से इस काम में लगा रहा। गोरखपुर में हर जगह प्रेमचंद को ढूंढता फिरने लगा…। लेकिन मुक्कमल तौर पर प्रेमचंद मुझे नहीं मिले। गोरखपुर वालों ने प्रेमचंद को भुलाया ही नहीं गायब कर रखा था। और मैं था कि बेचैन था।* प्रेमचंद मेरे अजीज बन चले थे। तरह तरह की कल्पनाएं करता…। आकार पर आकार गढ़ता – उसी राप्ती किनारे जहां गांधी जी से प्रभावित हो कर प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ स्वराज आंदोलन में हिस्सा लेने का निश्चय किया था। लेकिन मेरे दिमाग में प्रेमचंद की एक अनगढ़ सी तस्वीर उगती मिटती, मिटती उगती। और यह क्रम चलता टूटता कि प्रेमचंद से मैं चिढ़ने लगा। क्यों कि जो आदर्श, जो सूत्र उन से सीखे थे – वे व्यावहारिक स्तर पर देखने में तो बड़े 'साबूत', 'एक्टिव' लगते। लेकिन 'करने' के स्तर पर 'तोड़' डालते थे। इस बीच प्रेमचंद की व्यक्तिगत ज़िंदगी के पन्ने भी पढ़ने को मिलने लगे। जो ढेर सारी अनैतिक बाते उन के बारे में बताती ही नहीं पुष्ट भी करती थीं। उन के साहित्य के बारे में भी अजब गजब बातें सुनने पढ़ने को मिलने लगीं। लेकिन स्थिति यह थी कि लाख चाहने पर भी अंतर्मन प्रेमचंद को गरियाने न देता। कि तभी लगा अरे, प्रेम-चंद – प्रेमचंद ही हैं। प्रेमचंद को कई कोनों से जान लेने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर अपने को पाया, निहायत व्यक्तिगत स्तर पर कि : प्रेमचंद न होते तो मैं जिंदा न होता – कभी का मर गया होता। हर मोड़ पर। वही मोड़ जो 'किशोर' था तब तोड़ते थे, आज 'युवा' हूं तब भी 'तोड़ते' हैं – आगे भी 'तोड़ेंगे'। लेकिन यह जानता हूं – कि इस टूटने से मैं बचूंगा, इस टूटने से लड़ूंगा, इस 'टूटने' को मैं तोड़ूंगा। यहां यह बता दूं कि प्रेमचंद के कई पात्रों को जब तब स्थितियों के मुताबिक हमेशा ही अपने भीतर बाहर, जीता महसूसता रहा हूं। चाहे वह पात्र छोटा से छोटा हो – नायक, खलनायक हो यहां तक कि संवेदना के स्तर पर महिला पात्रों को भी जीता रहा हूं – अपने ढंग से। न सही पूरा पूरा उन का जुझारुपन मुझे बहुत भाता रहा है। खास कर इन स्थितियों में:
तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल
मछली बच कर जाय कहां जब जल ही सारा जाल।
माधव मधुकर उन दिनों एक कविता गोदान पर पढते थे। उन्हों ने प्रेमचंद के गोदान पर एक छोटी सी कविता में आज की स्थितियों को बड़ी खूबी से उभारा है।
होरी की गाय
अभी तक घर नहीं आई
बैंकर खन्ना
अब भी नेता है
देशी पहनता
और विदेशी पीता है।
स्थितियां चाहें लाख बदल गई हों, देश काल और संदर्भ बदल गए हों – हमारे बुजुर्ग अब भी होरी की स्थितियों विसंगतियों में ही नहीं वरन दस गुणी विपरीत स्थितियों और चौतरफा विसंगतियों को झेल रहे हैं। ऐसे में हम गोबर गांव छोड़ शहर और शहर आ कर, 'जब भी पांव जले धूप में/ घर ही याद आए।' को कसमसा-कसमसा कर गुनगुनाते हुए ज़िंदगी बनाम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गलाजतों का किला तोड़ने में लगे हुए हैं। तोड़ते हुए खुद टूट रहे हैं। हां लेकिन टूटे नहीं हैं – टूटेंगे भी नहीं. टूटेगी तो यह व्यवस्था – यही हम जैसे तमाम 'गोबरों' की तमन्ना है। और इस तमन्ना को हम गोबर हासिल कर के रहेंगे। हो सकता है इस क्रम में कुछ होरी गोबर पीढ़ी दर पीढ़ी और जुड़े – कहीं और तेज़ धारदार और मज़बूत हौसलों के साथ।
[१९८२ में भावना प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित प्रेमचंद व्यक्तित्व और रचनादृष्टि, से साभार]
* उस समय एक रपट लिखी थी, हाजिर है :
जहां प्रेमचंद ने रंगभूमि की रचना की
जब बनारस में लमही तथा प्रदेश एवं देश के अन्य स्थानों पर हिंदी और उर्दू के यथार्थवादी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई, अपने शहर गोरखपुर ने भी बड़े हल्के फुल्के ढंग से उन्हें याद कर लिया।
बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन इसी नगर के बुलाकीपुर और तुर्कमानपुर मुहल्लों की सीलन भरी कोठरियों में बीता। इसी शहर में उन्हों ने नौकरी छोड़ कर सामाजिक कार्यकर्ता बन देश सेवा का व्रत लिया तथा इसी शहर में नार्मल स्कूल के उस विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्हों ने 'रंगभूमि', 'ईदगाह', 'पंचपरमेश्वर' तथा ऐसी ढेर सारी रचनाएं रचीं।
मुंशी प्रेमचंद के पिता उन दिनों यहां गोरखपुर डाकखाने में डाक मुंशी थे। जब वे बुलाकीपुर के उस कच्चे सीलन भरे मकान में रह कर कक्षा छ: सात की पढ़ाई कर रहे थे। कहा जाता है कि उसी कोठरी में उन की प्रिय बहन ने इलाज की कमी और भूख की तड़पन के बीच दम तोड़ दिया था। संभवत: उर्दू बाज़ार के उस तंबाकू वाले को हम आप नहीं जान सकते, बल्कि पहचान भी नहीं सकते, परंतु मुंशी प्रेमचंद उसे कभी नहीं भूले। क्यों कि बचपन में स्कूल जाते समय उस की दुकान पर चोरी-चोरी उन्हों ने 'गुड़गुड़ी' का स्वाद लिया था और बाद में नार्मल स्कूल में सहायक मास्टर एवं उपविद्यालय निरीक्षक बनने पर वे नियमित रूप से तंबाकू खरीदने उर्दू बा्ज़ार जाते और घंटों गुड़गुड़ी की 'चुस्की' लेते थे। उन के एक प्रसिद्ध उपन्यास में गली गली घूम कर खादी के लट्ठे बेचने की बात आप ने पढ़ी होगी किंतु गोरखपुर की गलियों ने मुंशी प्रेमचंद को कंधों पर खादी के गट्ठर लादे देखा है।
विद्यालय निरीक्षक जैसी नौकरी, प्रतिष्ठा आदि को लात मार कर उन्हों ने देश सेवी भाई महावीर प्रसाद पोद्दार 'भाई जी' की प्रेरणा से बीस आने रोज पर खादी के लट्ठे ले कर फेरी लगाने की नौकरी स्वीकार की और जन सेवा में लगे। अच्छा हुआ कि शहर के कुछ बुद्धिजीवी आज गंदगी और बदबू से घिरे, मुंशी प्रेमचंद पार्क (नार्मल स्कूल) में पहुंचे और उस महान साहित्यकार की चिर उपेक्षित अंचल प्रतिमा को माल्यार्पण कर श्रद्धाजंलि अर्पण से फर्ज अदायगी कर ली, वह भी तब जब नार्मल स्कूल के प्राधानाचार्य एवं कुछ छात्रों ने उन्हें ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया। हमने भी उस महान साहित्यकार को याद तो कर लिया पर उन की एकमात्र यादगार प्रेमचंद पार्क एवं उन की मूर्ति के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों कि इसी शहर में कुछ लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा की आंखें निकाल कर उन्हें अंधा कर दिया। वे कोठरियां अब ध्वस्त होने ही वाली हैं, जिनमें रह कर प्रेमचंद ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी थीं। वह पार्क उजड़ गया है जिसे प्रेमचंद पार्क की संज्ञा दी जाती है। उस वटवृक्ष के चबूतरे की ईंटें गायब हो गई हैं, जहां उन्हों ने ढेरों रचनाएं रची थीं। अब ऐसे शहर, जिसने मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति को नहीं बख्शा, जहां के विश्वविद्यालय को मुंशी प्रेमचंद से चिढ़ है, सामाजिक संस्थाएं जो मात्र फर्ज पूरा करती हैं, में रह कर कौन जाए उस अंधी मूर्ति का दर्शन करने।
[सारिका, १९७८ में प्रकाशित]
सरोकारनामा

दयानंद पांडेय ,लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. अपनी कहानियों और उपन्यासों के मार्फ़त लगातार चर्चा में रहने वाले दयानंद पांडेय का जन्म 30 जनवरी, 1958 को गोरखपुर ज़िले के एक गांव बैदौली में हुआ। हिंदी में एम.ए. करने के पहले ही से वह पत्रकारिता में आ गए। 33 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। उन के उपन्यास और कहानियों आदि की कोई डेढ़ दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। लोक कवि अब गाते नही पर प्रेमचंद सम्मान तथा कहानी संग्रह 'एक जीनियस की विवादास्पद मौत' पर यशपाल सम्मान। बांसगांव की मुनमुन, वे जो हारे हुए, हारमोनियम के हजार टुकड़े, लोक कवि अब गाते नहीं, अपने-अपने युद्ध, दरकते दरवाज़े, जाने-अनजाने पुल (उपन्यास), प्रतिनिधि कहानियां, बर्फ में फंसी मछली, सुमि का स्पेस, एक जीनियस की विवादास्पद मौत, सुंदर लड़कियों वाला शहर, बड़की दी का यक्ष प्रश्न, संवाद (कहानी संग्रह), हमन इश्क मस्ताना बहुतेरे (संस्मरण), सूरज का शिकारी (बच्चों की कहानियां), प्रेमचंद व्यक्तित्व और रचना दृष्टि (संपादित) तथा सुनील गावस्कर की प्रसिद्ध किताब 'माई आइडल्स' का हिंदी अनुवाद 'मेरे प्रिय खिलाड़ी' नाम से प्रकाशित। उनका ब्लाग है- सरोकारनामा





































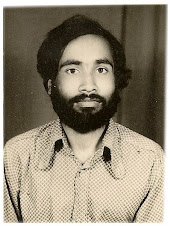

No comments:
Post a Comment