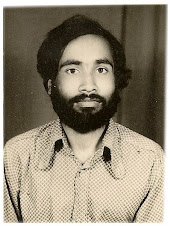दिनेशपुर आये हुए पूरे चार साल हो गए।कोलकाता से दिल्ली होकर 21 अक्टूबर 2017 को अपने गांव बसंतीपुर स्थायी तौर पर वापस आ गया।
घर लौटना चाहता था। लेकिन घर से एक बार निकल जाने के बाद घर वापस लौटना उतना आसान भी नहीं होता। हम कोलकाता में 27 साल बीता चुके थे। सोदपुर में हर कोई जानता था।उस समाज में एकाकार हो गए थे।
रिफ्यूजी कालोनी की तराई की ज़िंदगी से अलग कोलकाता में मुख्यधारा के बंगाली समाज,बांग्ला भाषा और संस्कृति के भूगोल से लौटकर फिर विस्थापित होना भारत विभाजन की त्रासदी को नए सिरे से जीने के बराबर था।हमारे लोग इसीतरह अनचाहे बंगाल के इतिहास भूगोल से बाहर हो गए थे 1947 में।
पिताजी तो 1947 से पहले से तेभागा आंदोलन की वजह से कोलकाता में ही थे।चाचा और ताउजी कोलकाता पुलिस में थे।
सिर्फ दादी और ताई जी जैशोर में थीं। तब पिताजी और चाचाजी अविवाहित थे।
रातोंरात पूर्वी बंगाल के लोग भारत में जहां भी थे,शरणार्थी बन गए।कोलकाता और पश्चिम बंगाल,बिहार,असम में जो जहां थे,वहीं खड़े खड़े शरणार्थी बन गए।
जन्मने से पहले हम और हमारी अजन्मी पीढियां शरणार्थी बन गए अपने ही देश में।
यह सिलसिला जारी है।
जारी रहेगा अनन्तकाल।
भारत में जन्म होने के बावजूद पूर्वी बंगाल मूल के सभी बच्चे जन्मजात 1947 के बाद शरणार्थी ही बनते हैं। पश्चिम पंजाब या सिंध या म्यांमार य से आए लोगों के साथ ऐसा नहीं होता।
फिर सचमुच शरणार्थी होने का अहसास अक्टूबर 2017 में हुआ। कोलकाता से वापसी के वक्त।
कोलकाता में 27 साल से नियमित अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी में देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में लिखते छपते रहने के बाद रचनाकर्म का फेसबुक तक सीमित हो जाना सचमुच कायापलट जैसा हो गया।
36 साल तक पेशावर संपादकी करने के बावजूद में हमेशा लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता रहा। सिर्फ संपादकी में कभी सीमाबद्ध नहीं रहा।
छात्र जीवन की घुमक्कड़ी आखिर तक जारी रही। पैर कभी थके नहीं, रुके नहीं।
पिता पुलिनबाबू की तरह मेरे पांवों के नीचे सरसों रहा है। जो चैन से कहीं बैठने नहीं देता। कानों में चीखें गूंजती रहती है। पीडितों के बीच जाकर खड़े होने के सिवाय ज़िंदा रहने का कोई मकसद नज़र ही नहीं आता।
कोलकाता से वापसी पर वह सरसों अब गायब हैं। लेकिन चीखें फिर भी गूंजती हैं।
बंगाल के हर कोने में और देश के हर हिस्से में मेरी जो दौड़ थी,वह तराई में सीमित हो गयी।
दफ्तर से घर और घर से दफ्तर की दिनचर्या हो गयी।
ऐसा कभी था नहीं। सपने मरे भी नहीं,लेकिन सपनों के लिए दौड़ना भी जरूरी है।
जड़ हो जाना जीवन नही है।
सविता जी कोलकाता और पूरे दक्षिण बंगाल में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। उनकी वह ज़िन्दगी वही थम गई।
उनका गीता संगीत खत्म हो गया।
हमारे जीवन के रंग,रंगकर्म का अवसान हो गया।
इतनी कीमतें अदा करने के बाद जो घर लौटा,उसके बाद क्या इतना आसान था यहाँ नये सिरे से सेट होना?
दिनेशपुर और पूरे तराई क्षेत्र में मेरे उठने बैठने की कोई जगह नहीं थी।
अपना गांव सिरे से बदल गया है।
अपने लोग भी बदल गए।
साझा चूल्हा लापता हो गया।
अलगाव और अवसाद में अभिजीत कुमार जैसे रंगकर्मी के अवसान के बाद सोचने को मजबूर हूँ कि मास्टर प्रताप सिंह कैंसर से दम तोड़ने से पहले प्रेरणा अंशु की जिम्मेदारी अगर मुझे देकर नहीं जाते तो मेरी नियति अभिजीत से कितनी अलग होती!
लोग पूछ रहे हैं कि अभिजीत कुमार को क्या हुआ?
जब अपने लोग,अपने साथी किसी को अकेला छोड़ दें और अंतिम दर्शन से पहले खोज खबर न लें,जैसे कि पहाड़ और उत्तराखण्ड का नया दस्तूर,नई संस्कृति, पैसे की संस्कृति हो गयी,तो अलगाव,समझौते,भटकाव और अवसाद में जो होता है,वहीं हुआ। समाज के लिए काम करने वालों की सामाजिक सुरक्षा न हो तो जो होता है,वहीं हुआ।ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है।
न जाने कितनों के साथ ऐसा हो रहा है।
अपने लोगों में लौटकर कोई काम करने की चनौतियाँ कम नहीं हैं। अपने ही लोग खारिज कर दें तो?
जनवरी 2018 तक मैं उन्हीं के भरोसे रहा, जिनके भरोसे में घर लौट आया। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया।
जनवरी में मास्साब से बात हुई।
रूपेश से मुलाकात हुई।
तुरन्त प्रेरणा अंशु की जिम्मेदारी मास्साब ने पहली मुलाकात में ही मुझे दे दी।
फरवरी 2018 का अंक मैंने मास्साब के साथ निकाला। अंक लेट हो गया। मास्साब के निधन के कुछ घण्टे बाद अंक छपकर प्रेस से आया।
सीसी टीवी फुटेज में देखा गया कि मृत्यु शय्या से उठकर मास्साब आधी रात के बाद प्रेरणा अंशु के दफ़्तर में जाकर बैठे और नए अंक की तलाश करते रहे।
अब अंक लेट होता है तो मुझे हमेशा लगता है कि मास्साब नया अंक का इंतज़ार कर रहे होंगे।