| Sunday, 16 June 2013 12:23 |
|
रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की गुरु-शिष्य जोड़ी कुछ-कुछ वैसी ही है जैसी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की थी। गुरु के प्रति शिष्य की अपार भक्ति, लेकिन गुरु की आस्थाओं और विश्वासों के प्रति प्रश्नरहित निष्ठा नहीं। बल्कि कुछ बातों में एकदम विपरीत। रामकृष्ण परमहंस काली, यानी ईश्वर के प्रति भावाकुलता और प्रेम को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। उधर विवेकानंद इसे स्त्रैण समझते थे। रामकृष्ण दूसरों की सेवा करने, दान करने या इस तरह के अन्य कामों को 'अहं' का प्रतीक समझते थे, क्योंकि उनके विचार में करुणा और दया केवल ईश्वर के अधिकार में हैं, मनुष्य के नहीं। शंभु मलिक के बारे में वे कहते हैं कि वह दक्षिणेश्वर आकर दान करने में ही सारा समय लगा देता है और उसे काली के दर्शन करने तक की फुरसत नहीं मिलती। उनकी राय में जरूरत से अधिक सेवाकार्य भगवतप्राप्ति की राह में रोड़ा था। लेकिन विवेकानंद ने दीन-दुखियों की सेवा में ही धर्म के दर्शन किए। विवेकानंद द्वारा प्रचारित धर्म पौरुषमय, भावाकुलता से रहित और व्यावहारिकता पर आधारित धर्म था।
स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह ही स्वामी विवेकानंद भी वेदों को सबसे ऊपर मानते थे। फर्क यह था कि वे वेदों के साथ-साथ उपनिषदों का भी समान महत्त्व स्वीकार करते थे और उन्होंने अपनी व्याख्या सेवेदांत को 'व्यावहारिक वेदांत' में बदल दिया था। लेकिन दोनों स्वामियों की तुलना करें तो जहां विवेकानंद का व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और आधुनिक था, वहीं जाति के सवाल पर दयानंद उनसे अधिक आकर्षक लगते हैं। ज्योतिर्मय शर्मा ने दयानंद का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मुझे किताब पढ़ते हुए उनका स्मरण हो आया।
स्वामी दयानंद के लिए हर वह व्यक्ति आर्य यानी श्रेष्ठ था जो वेदों की सत्ता को सर्वोपरि समझे। आर्य समाज में होने वाले हवन में किसी भी जाति का व्यक्ति भाग ले सकता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद इस मुद्दे पर उलझे हुए नजर आते हैं। अद्वैतवादी होने के कारण उन्हें हरेक प्राणी और वस्तु की एकता में विश्वास है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर उन्हें जाति-व्यवस्था भी अनिवार्य लगती है। वह ब्राह्मण को बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठतर मानते हैं और चाहते हैं कि वे निचली जातियों को अपने स्तर तक उठाने के लिए प्रयास करें। वे उच्च जातियों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लोगों के मन में सदिच्छा जगाने के अलावा और कोई सुझाव नहीं। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति-व्यवस्था, जिसकी जड़ें हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गहराई से जमी हैं, की समाप्ति को विवेकानंद आवश्यक नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि जिस देश में भी वह गए हैं, उसमें किसी न किसी रूप में उन्होंने जाति को देखा है। यहां वे पेशे के अनुसार समूह बनने को जाति से मिला कर देखते हैं और जाति-व्यवस्था की इस बुनियादी मान्यता को नजरअंदाज कर देते हैं कि जाति बदली नहीं जा सकती। चाहे किसी की योग्यता कुछ भी क्यों न हो, निचली जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी ही जाति के लिए निर्धारित काम करने को अभिशप्त है। जाति की यह जकड़न आज भी दूर नहीं हुई है।

 कुलदीप कुमार
कुलदीप कुमार 

































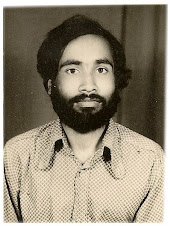

No comments:
Post a Comment