इस संसद में हमारा कौन है?
पलाश विश्वास
 हमारी संसद ने 13 मई, रविवार को अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए। इस तेरह मई को सविता और मेरे विवाह के भी २९ साल पूरे हो गये। जैसे हर भारतीय विवाह वार्षिकी या जन्मदिन मनाने की हालत में नहीं होता, जयादातर को तो तिथियां मालूम नहीं होतीं, उसी तरह संसद का यह साठवां जन्म दिन सत्ता वर्ग का उत्सव बनकर रह गया है। इसमें महज रस्मी औपचारिकता है, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय जनता या भारतवर्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। विडंबना है कि जिस भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर हर भारतवासी जन्मजात गर्व महसूस करता है, देश में संसदीय लोकतंत्र होने के बावजूद उसके ज्यादातर हिस्से की किसी लोकतांत्रिक गतिविधि में हिस्सेदारी नहीं है। लोकतंत्र से बहिष्कृत हैं बहुजन मूलनिवासी बहुसंख्यक जनता, जिसके लिए राष्ट्र लोककल्याणकारी गणराज्य नहीं, बल्कि दमनकारी सैनिक महाशक्ति है, जो उसकी हर आवाज को कुचलने के लिए सदैव तत्पर है। संसद की साठवीं सालगिरह के मौके पर अब भी अनशन पर बैठी हैं लगातार ग्यारह साल से मणिपुर की वास्तविक अग्निकन्या इरोम शर्मिला। कश्मीर से लेकर मणिपुर, समूचे मध्यभारत और पूरी की पूरी आदिवासी दुनिया किसी न किसी रूप में विशेष सैन्य कानून के दायरे में हैं और संसद में उनका कोई नहीं है। और गौर फरमायें, इस संसद में हमारा भी कोई नहीं है। देश में अब ऐसा कोई सासंद नहीं है, जिससे हम अपनी समस्याएं बता सकें और वह संसद में हमारी आवाज बुलंद करते हुए हालात बदल दें। अगर विशिष्ट परिस्थितियां और पहचान न हों तो हम इन सांसदों में से किसी को नहीं जानते और न इनमें से कोई हमारा प्रतिनिधित्व करता है।
हमारी संसद ने 13 मई, रविवार को अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए। इस तेरह मई को सविता और मेरे विवाह के भी २९ साल पूरे हो गये। जैसे हर भारतीय विवाह वार्षिकी या जन्मदिन मनाने की हालत में नहीं होता, जयादातर को तो तिथियां मालूम नहीं होतीं, उसी तरह संसद का यह साठवां जन्म दिन सत्ता वर्ग का उत्सव बनकर रह गया है। इसमें महज रस्मी औपचारिकता है, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय जनता या भारतवर्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। विडंबना है कि जिस भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर हर भारतवासी जन्मजात गर्व महसूस करता है, देश में संसदीय लोकतंत्र होने के बावजूद उसके ज्यादातर हिस्से की किसी लोकतांत्रिक गतिविधि में हिस्सेदारी नहीं है। लोकतंत्र से बहिष्कृत हैं बहुजन मूलनिवासी बहुसंख्यक जनता, जिसके लिए राष्ट्र लोककल्याणकारी गणराज्य नहीं, बल्कि दमनकारी सैनिक महाशक्ति है, जो उसकी हर आवाज को कुचलने के लिए सदैव तत्पर है। संसद की साठवीं सालगिरह के मौके पर अब भी अनशन पर बैठी हैं लगातार ग्यारह साल से मणिपुर की वास्तविक अग्निकन्या इरोम शर्मिला। कश्मीर से लेकर मणिपुर, समूचे मध्यभारत और पूरी की पूरी आदिवासी दुनिया किसी न किसी रूप में विशेष सैन्य कानून के दायरे में हैं और संसद में उनका कोई नहीं है। और गौर फरमायें, इस संसद में हमारा भी कोई नहीं है। देश में अब ऐसा कोई सासंद नहीं है, जिससे हम अपनी समस्याएं बता सकें और वह संसद में हमारी आवाज बुलंद करते हुए हालात बदल दें। अगर विशिष्ट परिस्थितियां और पहचान न हों तो हम इन सांसदों में से किसी को नहीं जानते और न इनमें से कोई हमारा प्रतिनिधित्व करता है।
प्रधानमंत्री ने संसद के 60 साल पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि संसद में बने कानून से देश को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 21 साल से संसद सदस्य हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। क्या ऐसा ही गौरव कश्मीर, मणिपुर, लालगढ़, दंडकारण्य जैसे इलाके के लोग, ग्यारह साल से अनशनरत इरोम शर्मिला, जेल में भयावह उत्पीड़न की शिकार सोनी सोरी, गुजरात और अन्यत्र दंगापीड़ित, जल, जंगल, जमीन, आजीविका, पहचान, आरक्षण, नागरिकता, मातृभाषा, मानवाधिकार नागरिक अधिकार से बेदखल तमाम लोग महसूस करते होंगे? 13 मई 1952 से 13 मई 2012 तक संसद और देश ने अनेक पड़ाव देखे हैं। कई मौके आए, जब लगा कि संसद का होना देश के लिए सबसे जरूरी है, तो कई बार ऎसा भी लगा कि संसद ने देश के साथ न्याय नहीं किया। संसद के पास गिनाने के लिए अनेक उपलब्धियां होंगी, लेकिन उसकी अनेक नाकामियां भी हैं, जो संसदीय व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। क्या हमारे सांसदों को इसकी परवाह है या जिस जनांदोलन की वजह से आज यह संसदीय गणतंत्र है, उस जनांदोलन को खत्म करने और उसके निर्मम सैनिक दमन में संसदीय सहयोग का आप क्या कहेंगे?
मेरा जन्म उत्तराखंड की तराई में बसाये गये एक शरणार्थी बंगाली परिवार में हुआ जबकि मेरी शिक्षा दीक्षा विशुद्ध कुमांयूनी परिवेश में हुआ। मैं बंगाल से उतना जुड़ा नहीं हूं २१ साल से बंगाल में रहते हुए बीतने के बावजूद, जितना कि हिमालय और हिमालयी लोगों से। मैंने पत्रकारिता शुरू की खान मजदूरों और आदिवासी जनता के मध्य। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आंदोलनों से हमारा गहरा नाता रहा है। संक्षिप्त फिल्मी यात्रा के जरिये मेरे संबंध मणिपुर, नगालैंड, असम और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के राज्यों से भी है। ओड़ीशा में मेरा ननिहाल है, जहां कारपोरेट साम्राज्य है। मूलनिवासी अस्मिता आंदोलन की वजह से संपूर्ण दक्षिण भारत और महाराष्ट्र, गुजरात एवम् राजस्थान के गांवों और कस्बों से मेरे निहायत आत्मीय संबंध है। पर मैं इनमें से किसी भी स्थान पर खड़े होकर एक भारतीय की हैसियत से गर्व का अहसास नहीं कर सकता। जनसंख्या स्थानांतरण के लिए ब्राह्मणवादी वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो भारत विभाजन हुआ और जिसकी परिणति आज का संसदीय लोकतंत्र है, उसके शिकार हमारे चंडाल जाति के लोग देश भर में छितरा दिये गये हैं। जिन्हें आज नागरिकता से वंचित करके देशनिकाले का हुक्म सुनाया जा रहा है। हम विभाजन के वक्त हमारे पुरखों को दिये राष्ट्र नेताओं के वायदों को भूल नहीं सकते। भारत के संविधान में वह धारा आज भी जस के तस मौजूद है, जिसमें विभाजन पीड़ितों को पुनर्वास और नागरिकता देने का वायदे किये गये हैं, जिसके लिए मेरे मां बाप जिये मरे। संविधान के फ्रेमवर्क के बाहर नागरिकता संविधान संशोधन कानून सर्वदलीय सहमति से बनी, तो किसे इस संसद में मैं अपना मान लूं?
सम्पूर्ण हिमालय में जो तबाही का आलम है, जिस तरह सैन्य शासन में जीने को मजबूर है कश्मीर और संपूर्ण पूर्वोत्तर, जैसे हमारे उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के बहाने समूचे हिमालय को एटम बम बना दिया गया है, अभी तक जैसे मुज़फ्फरनगर सामूहिक बलात्कार कांड के अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं, ऐसे में एक उत्तराखंडी या एक कुमांयूनी की हैसियत से मैं इस संसदीय व्यवस्था पर कैसे गर्व करूं? राजीव लोचन साह ने नैनीताल समाचार में सही लिखा है कि 18 सालों में धूल की इतनी परतें जम गई हैं कि यह नाम अब सामान्य उत्तराखंडवासी की स्मृति में धुँधलाने लगा है। 1994, जब मुजफ्फरनगर में वह वीभत्स कांड हुआ था, के आसपास पैदा हुई एक पूरी पीढ़ी है जो अब वयस्क होकर वोटर के रूप में राजनीति में भी हिस्सेदारी करने लगी है। उसने अपने माँ-बाप से इस घटना के बारे में सुना भी होगा तो वह फाँस नहीं महसूस की होगी, जो पुराने गठिया वात की तरह हमारी पीढ़ी की स्मृति में लगातार टीसता है। गिरदा तो मरते-मरते तक 'खटीमा मसुरी मुजफ्फर रंगै गे जो…..' गाने का कोई मौका नहीं चूकता था। अब हम जैसे आन्दोलनकारियों के लिये भी 1 या 2 सितम्बर या 2 अक्टूबर को शहीदों को याद करना एक उबाऊ सा कर्मकांड रह गया है, जिसे हम अलसाये ढंग से निपटाते हैं। एक समय था जब हम तमाम लोग यही कहते थे कि यदि मुजफ्फरनगर कांड के अपराधियों को सजा न मिली तो उत्तराखंड राज्य बनने का भी कोई अर्थ नहीं है। मुजफ्फरनगर कांड हमारे भीतर गुस्सा भरता था तो हमें कुछ करने को प्रेरित भी करता था। अब महीनों बीत जाते हैं, मुजफ्फरनगर कांड का जिक्र भी कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। पता नहीं कहीं कोई मुकदमा मुजफ्फरनगर कांड के अपराधियों पर चल भी रहा है या अब सभी खत्म कर दिये गये हैं। ऐसे में यदि उत्तराखंड में कांग्रेस की नवगठित सरकार एक ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट जनरल बना देती है, जिसकी भूमिका उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2003 में मुजफ्फरनगर कांड के प्रमुख आरोपी अनन्त कुमार सिंह को दोषमुक्त किये जाने के मामले में संदिग्ध रही हो तो इस पर ताज्जुब नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन उत्तराखंड के हितैषियों का तब भी यह धर्म बनता है कि आवाज भले ही कमजोर हो गई हो, शरीर से खून निचुड़ गया हो या शक्ति कमजोर पड़ गई हो, ऐसी गलत बातों का यथासंभव विरोध अवश्य करना चाहिये। शायद नई पीढ़ी में कुछ निकल आयें, जिनकी संवेदना जाग्रत हो….शायद फिर उत्तराखंड के नवनिर्माण की कोई लड़ाई शुरू हो…..शायद…
तनिक गौर फरमाये राकेश कुमार मालवीय के लिखे पर! आजादी के बाद से भारत में अब तक साढ़े तीन हजार परियोजनाओं के नाम पर लगभग दस करोड़ लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। लेकिन सरकार को अब होश आया है कि विस्थापितों की जीविका की क्षति, पुनर्वास-पुनस्र्थापन एवं मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है। यानि इतने सालों के अत्याचार, अन्याय पर सरकार खुद अपनी ही मुहर लगाती रही है। तमाम जनसंगठन कई सालों से इस सवाल को उठाते आ रहे थे कि लोगों को उनकी जमीन और आजीविका से बेदखल करने में तो तमाम सरकारें कोई कोताही नहीं बरतती हैं। लेकिन जब बात उनके हकों की, आजीविका की, बेहतर पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की आती है तो वहाँ सरकारों ने कन्नी ही काटी है। प्रशासनिक तंत्र भी कम नहीं है जिसने 'खैरात' की मात्रा जैसी बांटी गई सुविधाओं में भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ा है। इसके कई उदाहरण हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में सैकड़ों सालों पहले बसे बाईस हजार की आबादी वाले हरसूद शहर को एक बंजर जमीन पर बसाया गया। कैसे तवा बांध के विस्थापितों से उनकी ही जमीन पर बनाये गए बांध से उनका मछली पकड़ने का हक भी छीन लिया गया। एक उदाहरण यह भी है कि पहले बरगी बांध से विस्थापित हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का एक झुनझुना पकड़ाया गया। बांध बनने के तीन दशक बाद अब तक भी प्रत्येक विस्थापित परिवार को तो क्या एक परिवार को भी नौकरी नहीं मिल सकी है। लेकिन दुखद तो यह है कि सन् 1894 में बने ऐसे कानून को आजादी के इतने सालों बाद तक भी ढोया गया। इस कानून में बेहतर पुनर्वास और पुनस्र्थापन का सिरे से अभाव था। सरकार अब एक नये कानून का झुनझुना पकड़ाना चाहती है। इस संबंध में देश में कोई राष्ट्रीय कानून नहीं होने से तमाम व्यवस्थाओं ने अपने-अपने कारणों से लोगों से उनकी जमीन छीनने का काम किया है। देश भर में अब तक 18 कानूनों के जरिये भूमि अधिग्रहण किया जाता रहा है।ओडीशा,झारखंड, छत्तीसगढ़ या बंगाल कहीं भी जमान के किसी टुकड़े पर खड़ा होकर हम नहीं कह सकते कि यह संसद हमारी संसद है।वरिष्ठ राजनीतिज्ञ उन दिनों को याद करते हैं, जब संसद की कार्यवाही में व्यवधान नहीं पैदा होते थे और शोरशराबा, नारेबाजी व विद्वेष देखने-सुनने को नहीं मिलते थे।लेकिन इस शोर शराबे और संसदीय नौटंकी की रणनीति तो नीति निर्धारण की प्रक्रिया से जनता का ध्यान हटाना ही होता है। मीडिया की तरह संसद में भी बुनियादी मुद्दो पर गंभीर चर्चा होने के बजाय गैर जरूरी मुद्दों पर फोकस होता है। बेहतरीन सर्वदलीय समन्वय के तहत बिना शोर शाराबा, यहां तक कि बिना बहस, बिना रिकार्डिंग कानून बाजार और वैश्विक पूंजी के मनमुताबिक पास कर लिये जाते हैं। एक से बढ़कर एक जनविरोधी कानून और फैसले लागू हो जाते हैं, जिनमें तथाकथित जनप्रतिनिधियों की सर्हावदलीय सहमति होती है। वाकई हमारे सांसद वहां बैठे होते, तो सरकार के पास कानून बनाने लायक संख्या न होने के बावजूद कैसे संविधान संशोधन कानून तक बिना रोक टोक पास हो जाते हैं और कैसे बाजार तय कर देता है वित्तमंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक?
पहले कांग्रेस और उसके विद्वान ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व इतना प्रबल रहा है और विपक्ष के तमाम गिग्गजों के तार उनसे इतने मजबूती से जुड़े रहे हैं, कि उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर अंबेडकर जैसे लोग किनारे लग गये। विपक्षी नेताओं को भी आखिर चुनाव जीतना होता था। संसदीय बहस के स्तर का सवाल उतना बड़ा नहीं, बल्कि नीति निर्धारण और विधायी कामकाज में पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। तब निःशब्द सहमति और सहयोग से होता था सबकुछ। आज संसदीय कार्यवाही का मुकाबला सूचना महाविस्पोट से भी है। सच को छुपाने के लिए आज के सांसद पहले के सांसदों के मुकाबले में ज्यादा बड़े अभिनेता है, यह तो मानना पड़ेगा।
कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी और संसद में श्रेष्ठ परंपराएं शुरू कीं। विपक्षियों व उनके विचार का आदर करते थे, स्वस्थ बहस को बढ़ावा देते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद की गरिमा बढ़ाते थे। हाजिर जवाब नेता थे। उनमें पंडित नेहरू को भी चुप करा देने का बौद्धिक माद्दा था। प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी (सीपीआई नेता) अपने आप में एक संस्था की तरह थे। संसदीय ज्ञान, परंपरा के विद्वान थे। आज भी उन्हें याद किया जाता है।अटल बिहारी वाजपेयी 29 की उम्र में 1957 में लोकसभा पहुंचे। इस प्रखर वक्ता का पहला भाषण सुनने पंडित नेहरू भी उपस्थित हुए थे।प्रखर समाजवादी, गांधीवादी डॉक्टर राममनोहर लोहिया को प्रखर सांसद के रूप में याद किया जाता है। सरकार को घेरने व राह बताने में वे बेजोड़ थे। मधु दंडवते 20 साल तक सदन में राष्ट्रप्रेम व कामकाज से छाए रहे। संसदीय समझ के दिग्गज की पार्थिव देह भी चिकित्सा जगत के काम आई। समाजवादी नेता मधु लिमये ने संसद में मर्यादाओं को ऊपर उठाया। संसदीय परंपराओं के बेजोड़ विद्वान लिमये सरकार को भी निरूत्तर कर देते थे। लालकृष्ण आडवाणी बहस को प्रारम्भ करने में माहिर रहे हैं। अपनी बात को तरतीब से कहने में कुशल नेताओं में उनकी गिनती होती है। सीपीआई नेता इंद्रजीत गुप्त की बहस लाजवाब होती थी। उनकी बात समझने के लिए लोग कान लगा देते थे और वे किसी को भी छोड़ते नहीं थे। चंद्रशेखर हाथ हिलाते आते थे पर किसी विषय पर बोलने, बहस को पटरी पर लाने, उसमें नई जान डालने में कुशल थे। आज भी उनकी कमी खलती है।लेकिन इस गौरवशाली इतिहास का हश्र यह कि आज देश खुला बाजार है और कारपोरेट, बिल्डर, मापिया राज है!
हालांकि संसद जनता द्वारा चुनी जाती है और वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भारतीय जनता मताधिकार का प्रयोग बखूबी करता है लेकिन हर चुनाव के बाद संसद की जो तस्वीर बनती है, उसमें उसका अपना कोई चेहरा नहीं होता।गरीब इलाकों में सासंद तो दूर राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता तक जाने की तकलीप नहीं उठाते क्योंकि वे लोग उन्हें वह सब कुछ नहीं दे सकते , जो उन्हें बाजार और सत्तावर्ग से हासिल होता है। भारत में साठे छह हजार से ज्यादा जातियां हैं मनुस्मृति व्यवस्था के मुताबिक। गांधी और अंबेडकर के समझौते के मुताबिक अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण हासिल है। संसद में आरक्षित सीटें हैं। पर इन आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन ये बहिष्कृत जातियां या उनके प्रतिनिधि नहीं करते।तमाम दलों के सवर्ण नेता ही चुनते हैं आरक्षित सीटों के उम्मीदवार। अपने अपने हिसाब से। जातियों के दबंग गठजोड़ बनाकर सत्ता में बागेदारी सुनिश्चित करने के लिए। मजबूत जातियों के कामयाब गठबंधन से ही सत्ता हासिल होती है। यहां बदलाव का मतलब है, जातियों और संप्रदायों के समीकरण में बदलाव। जिसमें हमेशा मलाई मजबूत जातियों के हाथ लगती है। कमजोर जातियों को आरक्षण ही नसीब नहीं है, प्रतिनिधित्व की बात रही दूर।उत्तर भारत में हाल के वर्षों में जो सामाजिक उथल पुथल हुआ, उसका फायदा चुनिंदा दंबग जातियों को ही मिला। बाकी बहुसंख्य बहुजन मूलनिवासी जिस अंधेरे में थे , उसी अंधेरे में जीने और मारे जाने को अभिशप्त है।
कहने को कहा जाता है कि साठ साल पहले और आज की संसद में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। उन दिनों एक से बढ़कर एक विद्वान और दिग्गज संसद पहुंचे थे और बहस ऐसी होती थी कि सुनने और देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे लेकिन अब देश की सबसे बड़ी इस पंचायत का नजारा ही बदल गया है।विश्लेषकों और वरिष्ठ सांसदों का भी यही मानना है कि अब वैसे सांसद और वैसी बहस तो कल्पना मात्र रह गई है। यही नहीं व्यापक संवैधानिक मुद्दों के बदले राज्यों और वर्गीय हितों से सम्बंधित मुद्दे अक्सर इसके एजेंडे में आ रहे हैं। हकीकत यह है कि संसद में ब्राह्मणों के एकाधिकार में कुछ दलित व पिछड़ी जातियों के नेताओं की घुसपैठ के अलावा कुछ नहीं बदला है।आज जो घोटाले सामने आ जाते हैं, वह सूचना महाविस्फोट और कारपोरेट घरानों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, कारपोरेट लाबिइंग और बाजार के दबाव के कारण हैं, और वे भी पहले की तरह ही रफा दफा कर दिये जाते हैं। पहले जो महाघोटाले हुए, उसके लिए बोफोर्स प्रकरण का उदाहरण काफी है। विद्वानों की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही विद्वता के साथ बहुसंख्य जनसंख्या के बहिष्कार का कार्यक्रम चला। तब भी भारत सरकार की नीतियां संसद नहीं, देशी पूंजीपति और औद्योगिक घराने किया करते थे और उनहीं के पैसे के दम पर संसद का चेहरा रंगरोगन होता था। रिलायंस समूह के चामत्कारिक उत्थान के पीछे सत्ता का कितना हाथ रहा है, हम अच्छी तरह जानते हैं। हम बार बार कहते रहे हैं कि उदारीकरण और ग्लोबीकरम कोई नई बात नहीं है और न ही विदेशी पूंजी की गुसपैठ कोई नई बाता है। भारतीय संसद की शुरुआत से ही नीति निर्धारण का ऐसा इंतजाम रहा कि अर्थ व्यवस्था से बाहर हो गये ९५ फीसद लोग।
पांच फीसद लोगों को हर मौका, हर राहत, हर सहूलियत , हर विशेषाधिकार से नवाजा जाता रहा। कोई वित्तीय नीति बनी ही नहीं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों और विदेशी कर्ज से चलती रही अर्थव्यवस्था। विदेशी कर्ज इसलिए कि संपन्न लोगों के लिए ईंधन चाहिए था और राष्ट्र की सुरक्षा के बहाने हथियारों के सौदे होने थे।
करों का बोझ हमेशा उन्हीं पर लादा गया, जो यह बोझ उठा ही नहीं सकते। जो कर अदा कर सकते हैं, उन्हें करों में छूट देने के सिलसिले के कारण हर साल वित्तीय घाटा जारी रहा और यह कोई नई बात नहीं है। मंदी की बहुप्रचारित परिणति भी नहीं। करों में छूट और वित्तीय घाटा भारतीय बजट का अहम हिस्सा रहा है।
भुगतान संतुलन का चरमोत्कर्ष तो हमने उदारीकरण से काफी पहले झेला जब अपना रिजर्व सोना तक बेचना पड़ा और अर्थव्यवस्था उबारने के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत सरकार के लिए अपने वित्तमंत्री तैनात करने शुरु कर दिये। नेहरु युग में रक्षा क्षेत्र में आधारभूत उद्योगों में विदेशी पूंजी का बोलबाला रहा। तो हरित क्रांति के नाम पर बड़े बांध, उर्वरक, कीटनाशक , बीज, आदि के बहाने विदेशी पूंजी का अबाध प्रवेश रहा। भोपाल गैस त्रासदी तो उदारीकरण से पहले की घटना है।
गरीबों और दूसरे लोगों को सब्सिडी से वित्तमंत्री की नींद की चर्चा होती है, पर इस सब्सिडी के मुकाबले दस गुणा ज्यादा करों में जो कारपोरेट जगत को छूट दी जाती है, रक्षा सौदों में जो कमीशन खाया जाता है और साठ साल में नीति निर्धारण के एवज में विदेशी बैंकों में जो कालाधन जमा है, उसका क्या?
संसद का नजारा और माहौल अब कितना बदल गया है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहली लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की बड़ी संख्या थी और मार्क्सवादी विपक्ष में थे। आज जबकि कांग्रेस सहयोगी दलों की बैसाखी की सहारे है तो वामपंथियों की जगह दक्षिपंथियों ने ले ली है। वामपंथी आज कमजोर और अकेले पड़ गए हैं।
पहली लोकसभा में अधिकतर प्रशिक्षित वकील थे तो अब कृषि से जुड़े लोगों की तादाद अधिक हो गई है। यही नहीं उम्र के लिहाज से भी इसमें काफी तब्दीलियां आई हैं। 1952 में सिर्फ 20 फीसदी सांसद 56 या उससे अधिक उम्र के थे जबकि 2009 में यह संख्या 43 फीसदी हो गई।
पहली लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, ए. के. गोपालन, सुचेता कृपलानी, जगजीवन राम, सरदार हुकुम सिंह, अशोक मेहता और रफी अहमद किदवई जैसे दिग्गज थे।
उन दिनों बड़ी जीवंत बहस हुआ करती थी। पहली लोकसभा में कुल 677 बैठकें हुईं जो लगभग 3,784 घंटे चलीं। इसका लगभग 48.8 फीसदी समय का उपयोग विधायी कार्यों में किया गया। लेकिन इसके 60 वर्षों के बाद स्थितियां पूरी तरह बदल गई है। अब बिरले ही ऐसे मौके आते हैं जब बहस दमदार हो। आज तो अधिकांश समय हंगामे में जाया हो जाया करता है।
पहली लोकसभा में प्रत्येक वर्ष औसतन 72 विधेयक पारित हुए। 15वीं लोकसभा में यह संख्या घटकर 40 हो गई।
पलाश विश्वास। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी हैं । आजीवन संघर्षरत रहना और दुर्बलतम की आवाज बनना ही पलाश विश्वास का परिचय है। हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी के पॉपुलर ब्लॉगर हैं। "अमेरिका से सावधान "उपन्यास के लेखक। अमर उजाला समेत कई अखबारों से होते हुए अब जनसत्ता कोलकाता में ठिकाना ।





































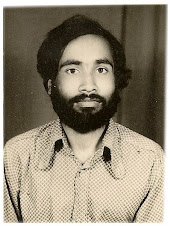

No comments:
Post a Comment