प्रियदर्शन
जनसत्ता 26 जनवरी, 2012 : इसमें शक नहीं कि बीते साठ वर्षों के दौरान अगर किसी एक विचार ने अखिल भारतीय सर्वानुमति बनाई है तो वह गणतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र का विचार है। आज इस देश में कोई भी विचारधारा संसदीय लोकतंत्र के विचार को खारिज करके नहीं चल सकती। उलटे उसे सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र में अपने भरोसे की दुहाई देनी होती है तभी वह बाकी जमातों को स्वीकार्य होती है। दुनिया भर में वामपंथ सर्वहारा की तानाशाही का नारा देकर आया, भारत में उसे बहुमत की लोकशाही का सम्मान करना पड़ा। सिर्फ राज्यों के स्तर पर नहीं, केंद्रीय स्तर पर भी इस देश की वामपंथी ताकतों ने व्यावहारिक राजनीति की जरूरतों को समझते हुए खुद को बदला और संसदीय लोकतंत्र के साथ खड़ी हुर्इं।
ठीक यही बात उन दक्षिणपंथी समूहों के बारे में कही जा सकती है जो कभी इस देश के संविधान को शक की निगाह से देखते थे और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आज गणतंत्र की ताकत के आगे सब सिर झुका रहे हैं। ध्यान से देखें तो मुट््ठी भर नक्सली समूहों ने जरूर इस व्यवस्था को चुनौती दी है, लेकिन नक्सलवाद का व्यापक इतिहास बताता है कि बहुत सारे समूह हथियार का रास्ता और ताकत के बल पर सत्ता परिवर्तन का ख्वाब छोड़ कर मुख्यधारा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। फिलहाल जो समूह इस प्रक्रिया से बाहर हैं, वे भी चुनावी राजनीति को अपने ढंग से प्रभावित करने और अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं।
दरअसल, गणतंत्र की यह अपरिहार्यता ही वह मूल्य है जिसे भारतीय लोकतंत्र ने पिछले साठ वर्षों में सबसे कायदे से सींचा है। इस गणतंत्र के आगे पुरानी सामंती ऐंठ भी सिर झुकाती है और नई उभरती जातिगत अस्मिताएं भी। कायदे से देखें तो इस देश में धर्म और जाति की राजनीति भी संसदीय लोकतंत्र की आड़ में ही हो रही है।
लेकिन क्या संसदीय लोकतंत्र की इस अपरिहार्यता पर, गणतंत्र की इस सर्व-स्वीकार्यता पर हमें खुश होना चाहिए? एक अर्थ में निश्चय ही यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इस बात का खयाल करने पर कहीं और बड़ी मालूम होती है कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ चुनावी प्रणाली तक महदूद नहीं है, उसके कई स्तर हैं और उसमें कई संस्थाएं हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण को रोकती हैं और अंतत: देश को यही इकलौता रास्ता अख्तियार करने को मजबूर करती हैं। वस्तुत: बहुत सारी गैरबराबरी और नाइंसाफी से घिरे इस भारतीय समाज में एक नागरिक एक वोट का कारगर मंत्र वह ताकत है जो सबको बराबरी पर ला बिठाता है और गणतंत्र को सही मायनों में सार्थक करता है।
लेकिन भारतीय गणतंत्र की असली चुनौतियां यहीं से शुरू होती हैं। एक बार जब सबको मालूम हो जाता है कि गणतंत्र की पोशाक पहने बिना इस देश में गुजारा नहीं है तो सारी विचारधाराएं या अविचारधाराएं यही वर्दी सिलवा लेती हैं। पता चलता है कि हमारा गणतंत्र सांप्रदायिक नफरत और असहिष्णुता की राजनीति को भी र्इंधन दे रहा है, जातिगत ऐंठ और जड़ता को कहीं ज्यादा कुरूप राजनीतिक ताकत दे रहा है और कहीं-कहीं क्षेत्रीय उन्माद को भी हवा दे रहा है। जैसे इतना भर नाकाफी हो, पैसे और अपराध के गठजोड़ ने वाकई इस गणतंत्र को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है।
इस मोड़ पर यह बात समझ में आती है कि असल में गणतंत्र की बस पोशाक बची हुई है, आत्मा नहीं। उसकी जगह कहीं जातिगत सड़ांध की ऐंठन हैं, कहीं पूंजी की बेलगाम ताकत और कहीं जुर्म का बेशर्म अट््टहास। पैसे और बाहुबल के इस खेल के आगे वाकई हमारा गणतंत्र बेबस नजर आता है, हमारे राजनीतिक दल इसके आगे घुटने टेकते दिखाई पड़ते हैं।
इस 26 जनवरी पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या वाकई हमारा गणतंत्र सिर्फ पोशाक रह गया है- सिर्फ ऊपर दिखने वाली देह- जिसकी आत्मा चली गई हो? ऐसा बेजान गणतंत्र हमारे किस काम का है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम देख रहे हैं, वह पूरी सच्चाई नहीं है? गणतंत्र में अब भी जान और हरकत बाकी है, अपने समाज की पहचान बाकी है और अपने मुद््दों से आंख मिलाने का साहस बाकी है?
कम से कम एक स्तर पर यह गणतंत्र हमें आश्वस्ति और उम्मीद देता है। पहली बार इस गणतंत्र में उन समुदायों को जुबान मिली है जो बरसों नहीं, सदियों से सताए हुए थे। पहली बार आदिवासियों और दलितों के हक पहचाने जा रहे हैं, पिछड़ों की आकांक्षाओं को समझा जा रहा है, उनकी राजनीतिक नुमाइंदगी सुनिश्चित हो पाई है। पहली बार सत्ता वास्तविक अर्थों में उन लोगों तक पहुंची है जिनके नाम पर यह गणतंत्र चलाया जा रहा है।
मगर इस बहुत बड़ी सच्चाई की अपनी तंग करने वाली दरारें भी हैं। यह बात भी साफ नजर आ रही है कि संसदीय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति ने समाज को कई तरह के खानों में बांट दिया है। पुरानी जातिगत जकड़नें नए राजनीतिक स्वार्थों के साथ मिल कर वैमनस्य के नए ध्रुव बना रही हैं। पुराने सांप्रदायिक टकराव चुनावी राजनीति की बिसात पर नए तरह के अलगाव पैदा कर रहे हैं। एक तार-तार होता समाज है जिसकी अखिल भारतीयता लगातार संदिग्ध हुई जा रही है।
दुर्भाग्य से इस नई बनती राजनीतिक संस्कृति के पास कोई स्मृति नहीं है और इसलिए जाति और धर्म के नाम पर बनने वाली नई गोलबंदियां खतरनाक ढंग से मौकापरस्त भी हैं और भ्रष्ट भी। न पिछड़ों की नुमाइंदगी कर रहे लालू-मुलायम भरोसेमंद दिखाई पड़ते हैं न दलितों का नेतृत्व कर रहीं मायावती के पास एक बेहतर समाज बनाने का सपना दिखता है। सच तो यह है कि निहायत परिणामवादी चुनावी राजनीति से तय हो रहे इनके गणित में किसी बड़े सपने की जगह ही नहीं है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट के समय हुए बवाल से जो बदलाव की क्रांतिकारी संभावना पैदा हुई वह एक नई तरह की यथास्थिति में बदल कर रह गई है और लालू-मुलायम या मायावती फिलहाल नए सामंतों जैसे ही दिख रहे हैं। यह सच है कि फिर भी इनकी मौजूदगी ने राजनीति में पिछड़े-दलित तबकों के लिए उम्मीद और गुंजाइश दोनों पैदा की हैं और समानता और स्वाभिमान का नया भरोसा इनमें पैदा हुआ है। लेकिन यह ऊर्जा जितने बडेÞ पैमानों पर जिन बदलावों के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, उनकी किसी को कल्पना ही नहीं है। शायद इसी का नतीजा है कि सत्ता भले पिछड़े-दलितों के बीच जा रही हो, सत्ता के लाभ उन तबकों तक नहीं पहुंच रहे- उलटे वे लगातार उनसे दूर हुए हैं। इस देश में जो लोग सबसे ज्यादा सताए और उजाडेÞ जा रहे हैं, वे दरअसल वही लोग हैं जिनके नाम पर अस्मितावादी राजनीति परवान चढ़ रही है।
इस प्रक्रिया का एक चिंताजनक पहलू और है। जो कुछ भी संसदीय राजनीति के दायरे से बाहर है, जो कुछ भी चुनावी राजनीति से खुद को अलग रखना चाहता है, उसे अलोकतांत्रिक बताते हम नहीं हिचकते। पिछले दिनों अण्णा हजारे के आंदोलन पर चल रही बहस के दौरान यह बात हमारे नेताओं की तरफ से बार-बार उठाई गई कि टीम अण्णा का आंदोलन लोकतंत्र विरोधी है- बस इसलिए कि वह चुनावी प्रक्रिया से खुद को अलग रख रहा है और संसद के बाहर एक कानून पर बहस कर रहा है।
निश्चय ही अण्णा हजारे के आंदोलन की कई सीमाएं बेहद स्पष्ट हैं और उनकी कई जायज आलोचनाएं भी हैं, लेकिन उनके आंदोलन को लोकतंत्र विरोधी बताना अपने गणतंत्र को एक ऐसी संस्थागत जड़ता या रीतिबद्धता में धकेल देना है जो अंतत: अपने चरित्र में लोक विरोधी है। फिर दुहराने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति इसीलिए आ रही है कि हमने लोकतंत्र को जीवन-दृष्टि की तरह नहीं, बस पोशाक की तरह पहन रखा है।
शायद यही वजह है कि जिस जन को केंद्र बना कर हमारे गणतंत्र की अवधारणा रची गई है, वही इस समूची व्यवस्था में सबसे उपेक्षित है और सबसे ज्यादा हाशिये पर है। इसका एक नतीजा यह भी हुआ है कि हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था जैसे एक नई आर्थिक व्यवस्था की गुलाम बनती जा रही है। चुनावों में जो पैसा लग रहा है, वह किसी शून्य से नहीं आ रहा, वह चंद नेताओं की दलाली से भी नहीं मिल रहा, उसके पीछे अब सुनियोजित ढंग से लगी कॉरपोरेट देसी और विदेशी पूंजी है। इस पूंजी को अपने लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, लाइसेंस चाहिए, दुकानें चाहिए, सिंगल विंडो क्लीयरेंस चाहिए, सौ फीसद निवेश की छूट चाहिए और एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वह अपनी नवसाम्राज्यवादी परियोजना को अंजाम दे सके। जब कोई जनतांत्रिक प्रतिरोध उसकी इस परियोजना के आडेÞ आता है या उसकी रफ्तार मद्धिम करता है तो यह पूंजी इस पूरे गणतंत्र को कोसती है और उस चीन को याद करती है जहां फैसले फटाफट हो रहे हैं।
हमारे गणतंत्र की असली विडंबना यहीं से शुरू होती है। हमारे संविधान ने राजनीतिक और सामाजिक बराबरी की जो प्रस्तावना लिखी है, उसको अमल में लाने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं के समांतर वे आर्थिक प्रक्रियाएं भी जारी हैं जो अपने स्तर पर भयावह गैरबराबरी को बढ़ावा दे रही हैं। बल्कि यह सिर्फ गैरबराबरी का मामला नहीं है, इस देश के सारे संसाधनों पर संपूर्ण कब्जे की भी कोशिश है। यह पुरानी औपनिवेशिकता को नए सिरे से साधना है और यह काम वही वर्ग कर रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में भी सत्ता के हमकदम हुआ करते थे।
सिर्फ इत्तिफाक नहीं है कि हमारा मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान अपरिहार्यत: उस उच्च मध्यवर्गीय संस्कृति से संचालित है जो खुद को वैश्विक या खगोलीकृत बताती है लेकिन मानसिक तौर पर असल में अमेरिका या यूरोप में बसती है। मौजूदा उदारीकरण ने उसे यह मौका दिया है कि वह भारतीय गणतंत्र के भीतर भी अपना एक स्वर्ण विश्व बसा सके। लेकिन इस स्वर्ण विश्व की कीमत वह असली भारत चुका रहा है जो साधनों के लिहाज से अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के बावजूद विपन्न है, क्योंकि उन पर कब्जा इस सत्ता-केंद्रित वर्ग का है।
इस दोहरी प्रक्रिया का ही नतीजा है कि हमारे देश में दो भारत बन गए हैं- एक अमीरों का चमचमाता भारत और दूसरा गरीबों का बजबजाता भारत। गरीबी और अमीरी हमारे देश में पहले से रहीं, लेकिन वह फासला नहीं रहा जो अब मौजूद है- और यह सिर्फ आर्थिक फासला नहीं है, यह पूरी तरह सांस्कृतिक-वैचारिक फासला भी है- जैसे वाकई ये दो भारत दो अलग-अलग देश हों। छब्बीस जनवरी पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि हम इन दो देशों का फासला मिटा कर इन्हें एक कैसे बनाएं। |







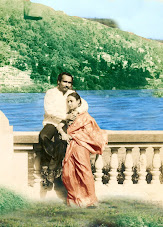












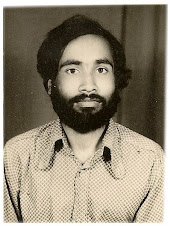

No comments:
Post a Comment