आखिर हम कितना गहरा खोदेंगे: अरुंधति रॉय
Posted by Reyaz-ul-haque on 4/08/2014 08:21:00 PMएक सिलसिला सा पूरा हुआ. अरुंधति रॉय का यह व्याख्यान पढ़ते हुए आप पाएंगे कि चीजें कैसे खुद को दोहरा रही हैं. यह व्याख्यान एक ऐसे समय में दिया गया था जब भाजपा के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार चुनावों में थी, कहा जा रहा था कि भारत का उदय हो चुका है, लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं. लोग सोच रहे थे कि एनडीए के छह सालों के शासन ने तो पीस डाला है, एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए. कांग्रेस जीती भी. लेकिन आज, दस साल के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तो पीस कर रख दिया, भाजपा को मौका दिया जाना चाहिए. हवाओं और लहरों की बड़ी चर्चा है. लेकिन इस व्याख्यान को इस नजर से भी पढ़ा जाना चाहिए, कि क्या भारत में होने वाले लगभग हरेक चुनाव इसी तरह की झूठी उम्मीदें बंधाते हुए नहीं लड़े जाते. हर बार एक दल उम्मीदें तोड़ता है और दूसरे से उम्मीदें बांध ली जाती हैं. अगला चुनाव (या बहुत हुआ तो उससे अगला या उससे अगला) चुनाव आते आते ये दल आपस में भूमिकाएं बदल लेते हैं- और जनता ठगी जाती रहती है. क्या यह कहने का वक्त नहीं आ गया है कि बस बहुत हो चुका? या बास्तांते!
हाल ही में एक नौजवान कश्मीरी दोस्त मुझसे कश्मीर की जिन्दगी के बारे में बात कर रहा था। राजनैतिक भ्रष्टाचार और अवसरवाद के दलदल, सुरक्षा–बलों के बेरहम वहशीपन और हिंसा में डूबे समाज की अधूरी संक्रमणशील सीमाओं के बारे में बता रहा था, जहाँ आतंकवादी, पुलिस, खुफिया अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी और पत्रकार भी एक–दूसरे के रू–ब–रू होते हैं और आहिस्ता–आहिस्ता एक–दूसरे में तब्दील हो जाते हैं। वह अन्तहीन खून–खराबे, लोगों के लगातार 'गायब' होने, फुसफुसाहटों, भय, अनसुलझी अफवाहों के बीच जीने के बारे में और जो सचमुच हो रहा है, जो कश्मीरी जानते हैं कि हो रहा है और जो हम बाकियों को बताया जाता है कि हो रहा है, इसकी आपसी असम्बद्धता के बीच जीने के बारे में बता रहा था। उसने कहा, 'पहले कश्मीर एक धन्धा था, अब वह पागलखाना बन चुका है।'
जितना अधिक मैं उसकी टिप्पणी के बारे में सोचती हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे यह वर्णन पूरे हिन्दुस्तान के लिए उपयुक्त जान पड़ता है। यह मानते हुए कि कश्मीर और – मणिपुर, नगालैण्ड और मिजोरम के – उत्तर-पूर्वी राज्य उस पागलखाने के दो अलग-अलग खण्ड हैं जिनमें इस पागलखाने के ज्यादा खतरनाक वार्ड हैं। लेकिन, हिन्दुस्तान के बीचोबीच भी, जानकारी और सूचना के बीच, जो हम जानते हैं और जो हमें बताया जाता है उसके बीच, जो अज्ञात है और जिसका दावा किया जाता है उसके बीच, जिस पर पर्दा डाला जाता है और जिसका उद्घाटन किया जाता है उसके बीच, तथ्य और अनुमान के बीच, 'वास्तविक' दुनिया और आभासी दुनिया के बीच जो गहरी खाई है, वह ऐसी जगह बन गयी है जहाँ अन्तहीन अटकलों और सम्भावित पागलपन का साम्राज्य फैला हुआ है। एक जहरीला घोल है जिसे हिला–हिला कर खौलाया गया है और सबसे ज्यादा घिनौने, विध्वंसक राजनैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है।
हर बार जब कोई तथाकथित आतंकवादी हमला होता है, सरकार थोड़ी–बहुत या बिना किसी छानबीन के, इसकी जिम्मेवारी किसी के सर पर मढ़ने के लिए दौड़ पड़ती है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी, संसद भवन पर 13 दिसम्बर 2001 का हमला या छत्तीसिंहपुरा (कश्मीर) में मार्च 2000 को तथाकथित आतंकवादियों द्वारा सिखों का जनसंहार इसके कुछ बड़ी–बड़ी मिसालें हैं। (वे तथाकथित आतंकवादी, जिन्हें बाद में सुरक्षा–बलों ने मार गिराया, बाद में निर्दोष साबित हुए। बाद में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि खून के फर्जी नमूने डीएनए जाँच के लिए पेश किये गये थे।[2] इनमें से हर मामले में जो साक्ष्य सामने आये, उनसे बेहद बेचैन कर देने वाले सवाल उभरे और इसलिए मामले को फौरन ताक पर धर दिया गया। गोधरा का मामला लीजिए–जैसे ही घटना घटी, गृहमंत्री ने घोषणा की कि यह आई.एस.आई. का षड्यंत्र है। विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि यह पेट्रोल बम फेंक रहे मुसलमानों की भीड़ का काम था।[3] गम्भीर सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। अटकलों का कोई अन्त नहीं है। हर आदमी जो जी चाहे मानता है, लेकिन घटना का इस्तेमाल संगठित साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए किया जाता है।
11 सितम्बर के हमले की घटना के इर्द–गिर्द बुने गये झूठ और प्रपंच का उपयोग अमरीकी सरकार ने एक नहीं, बल्कि दो देशों पर हमला करने के लिए किया–और ऊपरवाला ही जाने आगे–आगे होता है क्या? भारत सरकार इसी रणनीति का इस्तेमाल करती है–दूसरे देशों के साथ नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ।
पिछले एक दशक के अर्से में पुलिस और सुरक्षा–बलों द्वारा मारे गये लोगों की गिनती हजारों में है। हाल में मुम्बई के कई पुलिसवालों ने प्रेस के सामने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अपने ऊँचे अधिकारियों के 'आदेश' पर उन्होंने कितने 'गैंगस्टरों' का सफाया किया।[4] आन्ध्र प्रदेश में औसतन एक साल में तकरीबन दो सौ 'चरमपन्थियों' की मौत 'मुठभेड़' में होती है।[5] कश्मीर में, जहाँ हालात लगभग जंग जैसे हैं, 1989 के बाद से अनुमानतः 80 हजार लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग गायब हैं।[6] 'गुमशुदा लोगों के अभिभावक संघ' (एपीडीपी) के अनुसार अकेले 2003 में तीन हजार से अधिक लोग मारे गये हैं, जिनमें से 463 फौजी हैं।[7] 'अभिभावक संघ' के अनुसार अक्टूबर 2002 में जब से मुफ्ती मोहम्मद सरकार 'मरहम लगाने' के वादे के साथ सत्ता में आयी, तब से 54 लोगों की हिरासती मौत हुई है।[8] प्रखर राष्ट्रवाद के इस युग में जब तक मारे गये लोगों पर गैंगस्टर, आतंकवादी, राजद्रोही, या चरमपन्थी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, उनके हत्यारे राश्ट्रीय हित के धर्मयोद्धाओं के तौर पर छुट्टा घूम सकते हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। अगर यह सच भी होता (जो कि निश्चय ही नहीं है) कि हर आदमी जो मारा गया है वह सचमुच गैंगस्टर, आतंकवादी, राजद्रोही, या चरमपन्थी था–तो यह बात हमें सिर्फ यही बताती है कि इस समाज के साथ कोई भयंकर गड़बड़ी है जो इतने सारे लोगों को ऐसे हताषा–भरे कदम उठाने पर मजबूर करता है।
भारतीय राज्य–व्यवस्था में लोगों को उत्पीड़ित और आतंकित करने की तरफ जो रुझान है उसे 'आतंकवाद निरोधक अधिनियम' (पोटा) को पारित करके संस्थाबद्ध और संस्थापित कर दिया गया है, जिसे दस राज्यों ने लागू भी कर दिया है। पोटा पर सरसरी निगाह डालने से भी यह पता चल जायेगा कि वह क्रूरतापूर्ण और सर्वव्यापी है। यह ऐसा अनगिनत फंदों वाला और सर्वसमावेशी कानून है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है–विस्फोटकों के जखीरे के साथ पकड़े गये अल–कायदा का कार्यकर्ता भी और नीम के नीचे बाँसुरी बजा रहा कोई आदिवासी भी। पोटा की हुनरमन्दी की खासियत यह है कि सरकार इसे जो बनाना चाहे, यह बन सकता है। जीने के लिए हम उनके मोहताज हैं जो हम पर राज करते हैं। तमिलनाडु में राज्य सरकार इसका इस्तेमाल अपनी आलोचना का दम घोंटने के लिए करती है।[9] झारखण्ड में 3200 लोगों को, जिनमें ज्यादातर गरीब आदिवासी हैं और जिन पर माओवादी होने का आरोप लगाया गया है, पोटा के तहत अपराधी ठहराया गया है।[10] पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस कानून का उपयोग उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो अपनी जमीन और आजीविका के अधिकार के हनन का विरोध करने की जुर्रत करते हैं।[11] गुजरात और मुम्बई में इसे लगभग पूरे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता र्है।[12] गुजरात में, 2002 के राज्य प्रायोजित जनसंहार के बाद, जिसमें अनुमानतः 2000 मुसलमान मारे गये और डेढ़ लाख बेघर कर दिये गये, 287 लोगों पर पोटा लगाया गया, जिनमें 286 मुसलमान और एक सिख है।[13] पोटा में इस बात की छूट दी गयी है कि पुलिस हिरासत में हासिल बयान कानूनी सबूत के तौर पर माने जा सकते हैं। हकीकतन, पोटा निजाम के तहत, पुलिसिया छानबीन की जगह पुलिस यातना ले लेती है। यह ज्यादा त्वरित, ज्यादा सस्ता है और शर्तिया नतीजे पैदा करने वाला है। अब कीजिए बात सरकारी खर्च घटाने की।
मार्च 2004 में, मैं पोटा पर हो रही जनसुनवाई में मौजूद थी।[14] दो दिनों तक लगातार हमने अपने इस अद्भुत लोकतन्त्र में हो रही घटनाओं की लोमहर्षक गवाहियाँ सुनीं। मैं यकीनन कह सकती हूँ कि हमारे पुलिस थानों में सब कुछ होता है–लोगों को पेशाब पीने पर मजबूर करने, उन्हें नंगा करने, जलील करने, बिजली के झटके देनें, सिगरेट के जलते हुए टोटों से जलाये जाने, गुदा में लोहे की छड़ें घुसेड़ने से ले कर पीटने और ठोकरें मार–मार कर जान ले लेने तक।
देश भर में पोटा के आरोपित सैकड़ों लोग, जिनमें कुछ बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कैद करके जमानत के बिना, विशेष पोटा अदालतों में, जो जनता की छानबीन से परे हैं, सुनवाई के इन्तजार में हिरासत में रखे गये हैं। पोटा के तहत धरे गये अधिकतर लोग एक या दो अपराधों के दोषी हैं। या तो वे गरीब हैं–ज्यादातर दलित और आदिवासी। या फिर वे मुसलमान हैं। पोटा आपराधिक कानून की इस माने हुए नियम को उलट देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। पोटा के तहत आपको तब तक जमानत नहीं मिल सकती जब तक आप साबित नहीं कर देते कि आप निर्दोष हैं और वह भी उस अपराध के सिलसिले में जिसका औपचारिक आरोप आप पर नहीं लगाया गया है। सार यह है कि आपको यह साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं भले ही आपको उस अपराध का सान–गुमान भी न हो जो फर्जिया तौर पर आपने किया है। और यह हम सब पर लागू होता है। तकनीकी तौर पर हम एक ऐसा राष्ट्र हैं, अपराधी ठहराये जाने का इन्तजार कर रहा है।
यह मानना भोलापन होगा कि पोटा का 'दुरुपयोग' हो रहा है। इसके विपरीत इसका इस्तेमाल ठीक–ठीक उन्हीं कारणों से किया जा रहा है, जिसके लिए यह बनाया गया था। असल में तो अगर मलिमथ समिति की सिफारिशों को लागू किया जाये तो पोटा जल्दी ही बेकार हो जायेगा। मलिमथ समिति ने सिफारिश की है कि किन्हीं सन्दर्भों में सामान्य आपराधिक कानून को पोटा के प्रावधानों के मुताबिक ढाला जाय।[15] इसके बाद कोई अपराधी नहीं रहेगा, सिर्फ आतंकवादी होंगे, साफ-सुथरा हल है, झंझट बचेगा।
जम्मू–कश्मीर और अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में आज 'सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम' न केवल सेना के अफसरों और कमीशन–प्राप्त जूनियर अधिकारियों को, बल्कि गैर–कमीशन–प्राप्त जूनियर अधिकारियों को भी किसी व्यक्ति पर हथियार रखने या कानून–व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाने के सन्देह में बल–प्रयोग (यहाँ तक कि मार भी डालने) की इजाजत देता है।[16] सन्देह में! किसी भी भारतवासी को इस बारे में कोई भ्रम नहीं हो सकता कि इसका क्या मतलब होता है। सुरक्षा बलों द्वारा यातना, गुमशुदगी, हिरासत में मौत, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएँ दर्ज की गयी हैं, वे आपका खून जमा देने के लिए पर्याप्त हैं। इस सब के बावजूद, अगर हिन्दुस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी और खुद अपने मध्यवर्ग के बीच एक वैध लोकतन्त्र की छवि बनाये रखने में सफल है, तो यह एक जीत ही है।
'सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम' उस अधिनियम का और भी कठोर प्रारूप है, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आन्दोलन से निपटने के लिए 15 अगस्त 1942 को पारित किया था। 1958 में इसे मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू किया गया, जिन्हें 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था। 1965 में पूरा मिजोरम, जो तब असम का हिस्सा था, 'अशांत' घोशित कर दिया गया। 1972 में इस अधिनियम के तहत त्रिपुरा भी आ गया। और 1980 के आते–आते पूरे मणिपुर को 'अशांत' घोषित कर दिया गया।[17] इससे ज्यादा और कौन–से सबूत चाहिए कि दमनकारी कदम उल्टा नतीजा देते हैं और समस्या को सुलझाने के बजाय उलझा देते हैं?
लोगों का उत्पीड़न करने और उनका सफाया कर देने की इस अशोभन उत्सुकता के साथ–साथ भारतीय राज्य–व्यवस्था में उन मामलों की छानबीन करके उन्हें अदालतों तक पहुँचाने न्याय देने की लगभग प्रकट अनिच्छा भी दिखाई देती है, जिनमें भरपूर साक्ष्य मौजूद हैं: 1984 में दिल्ली में तीन हजार सिखों का संहार, 1993 में मुम्बई में और 2002 में गुजरात में मुसलमानों का संहार (आज तक किसी को सजा नहीं), कुछ साल पहले जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रशेखर की हत्या, 12 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के शंकर गुहा नियोगी की हत्या–इसके चन्द उदाहरण हैं।[18] जब पूरी राज्य मशीनरी ही आपके खिलाफ खड़ी हो, तो चश्मदीद गवाहियाँ और ढेर सारे प्रामाणिक सबूत तक नाकाफी हो जाते हैं।
इस बीच, बड़ी पूँजी से निकलने वाले अखबारों में उल्लसित अर्थषास्त्री हमें बताते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। दुकानें सामानों से अटी पड़ी हैं। सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए हें। इस चकाचौंध से बाहर कर्ज में डूबे किसान सैकड़ों की तादाद में आत्म–हत्या कर रहे हैं।[19] देश भर से भुखमरी और कुपोषण की खबरें आ रही हैं, फिर भी सरकार ने अपने गोदामों में 6 करोड़, 30 लाख टन अनाज सड़ने दिया।[20] एक करोड़ 20 लाख टन अनाज निर्यात करके घटायी गयी दरों पर बेचा गया जिन दरों पर भारत सरकार भारत के गरीब लोगों को नहीं देना चाहती थी।[21] सुप्रसिद्ध कृषि अर्थषास्त्री उत्सा पटनायक ने सरकारी आँकड़ों के आधार पर भारत में तकरीबन सौ वर्षों की अन्न उपलब्धता और अन्न की खपत की गणना की है। उन्होंने हिसाब लगाया है कि 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों और 2001 के बीच वार्षिक अन्न उपलब्धता घट कर द्वितीय विश्वयुद्ध के वर्षों से भी कम हो गयी है, जिनमें बंगाल के अकाल वाले वर्ष शामिल हैं, जिसमें 30 लाख लोगों ने भुखमरी से जानें गँवा दी थीं।[22] जैसा कि हम प्रोफेसर अमर्त्य सेन की कृतियों से जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भूख से हुई मौतों को अच्छी नजर से नहीं देखतीं। इस पर 'स्वतंत्र समाचार माध्यमों' में नकारात्मक टीका–टिप्पणी और आलोचना होने लगती है।[23]
लिहाजा, कुपोषण और स्थायी भुखमरी के खतरनाक स्तर आजकल पसन्दीदा आदर्श हैं। तीन साल से कम उम्र के 47 फीसदी हिन्दुस्तानी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 46 फीसदी की विकास रुक गया है।[24] उत्सा पटनायक अपने अध्ययन में बतलाती है कि भारत के लगभग 40 फीसदी ग्रामवासियों की अन्न की खपज उतनी ही है जितनी कि उप–सहारा अफ्रीका के लोगों की खाते हैं।[25] आज ग्रामीण भारत में एक औसत परिवार हर साल 1990 के दशक के आरम्भिक वर्षों की तुलना में 100 किग्रा कम अनाज खाते हैं।[26]
लेकिन भारत के शहरों में, जहाँ कहीं भी आप जायें–दुकान, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जिम्नेजियम, हॉस्पिटल–हर जगह आपके सामने टीवी के पर्दे होंगे, जिनपर चुनावी वादों के पूरे हो चुके दिखेंगे। भारत चमक रहा है, 'फील गुड' कर रहा है। आपको महज किसी की पसलियों पर पुलिसवाले के बूटों की धमक पर अपने कान बन्द करने हैं, महज गन्दगी, झोपड़–पट्टियों, सड़कों पर चीथड़ों में जर्जर टूटे हुए लोगों से अपनी निगाहें हटानी हैं और उन्हें टीवी के किसी दोस्ताना पर्दे पर डालनी हैं, और आप उस दूसरी खूबसूरत दुनिया में दाखिल हो जायेंगे। बॉलीवुड की हरदम ठुमके लगाती, कमर मटकाती, नाचती–गाती दुनिया, तिरंगा फहराते और 'फील गुड' करते, स्थायी रूप से साधन–सम्पन्न और हरदम खुश हिन्दुस्तानियों की दुनिया। दिनों–दिन यह कहना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन–सी दुनिया असली है और कौन–सी दुनिया आभासी। पोटा जैसे कानून टेलीविजन स्विच के मानिन्द हैं। आप इनका प्रयोग गरीब, तंग करने वाले, अवांछित लोगों को पर्दे पर से हटाने के लिए कर सकते हैं।
***
भारत में एक नये तरह का अलगाववादी आन्दोलन चल रहा है। क्या इसे हम 'नव–अलगाववाद' कहें? यह 'पुराने अलगाववाद' का विलोम है। इसमें वे लोग जो वास्तव में एक बिलकुल दूसरी अर्थ–व्यवस्था, बिलकुल दूसरे देश, बिलकुल दूसरे ग्रह के वासी हैं, यह दिखावा करते हैं कि वे इस दुनिया का हिस्सा हैं। यह ऐसा अलगाव है जिसमें लोगों का अपेक्षाकृत छोटा तबका लोगों के एक बड़े समुदाय से सब कुछ– जमीन, नदियाँ, पानी, स्वाधीनता, सुरक्षा, गरिमा, विरोध के अधिकार समेत बुनियादी अधिकार–छीन कर अत्यन्त समृद्ध हो जाता है। यह रेखीय, क्षेत्रीय अलगाव नहीं है, बल्कि ऊपर को उन्मुख अलगाव है। असली ढाँचागत समायोजन जो 'इंडिया शाइनिंग' को, 'भारत उदय' को भारत से अलग कर देता है। यह इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम वाले भारत से अलग कर देता है।
यह ऐसा अलगाव है जिसमें सार्वजनिक तन्त्र, उत्पादक सार्वजनिक सम्पदा, पानी, बिजली, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन–वह सारी सम्पदा जिसे, यह माना जाता है कि, जनता की नुमाइन्दगी करने वाले भारतीय राज्य को धरोहर की तरह सँजो कर रखना चाहिए, वह सम्पदा जिसे दशकों के अर्से में सार्वजनिक धन से निर्मित किया और सुरक्षित रखा गया है–उसे राज्य निजी निगमों को बेच देता है। भारत में 70 प्रतिशत आबादी–70 करोड़ लोग–ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।[27] उनकी आजीविका प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इन्हें उनसे छीन लेना और थोक में निजी कम्पनियों को बेचना बर्बर पैमाने पर बेदखल करने और कंगाल बना देने की शुरुआत है।
इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कुछेक व्यापारिक घरानों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जागीर बनने की ओर बढ़ रहा है। इन कम्पनियों के प्रमुख कार्याधिकारी (सीईओ) इस देश को, इसके तन्त्र और इसके संसाधनों, इसके संचार माध्यमों और पत्रकारों के नियन्ता होंगे। लेकिन जनता के प्रति उनकी देनदारी शून्य होगी। वे पूरी तरह से–कानूनी, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक रूप से–जवाबदेही से बरी होंगे। जो लोग कहते हैं कि भारत में कुछ प्रमुख कार्याधिकारी प्रधानमन्त्री से ज्यादा ताकतवर हैं, वे जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं।
इस सब के आर्थिक आशयों से बिलकुल अलग, भले ही यह वह सब हो जिसका गुण–गान होता है (जो यह नहीं है)–चमत्कारिक, कार्यकुशल, अद्भुत–क्या इसकी राजनीति हमें स्वीकार है? अगर भारतीय राज्य अपनी जिम्मेदारियों को मुट्ठी भर निगमों के यहाँ गिरवी रखने का फैसला करता है तो क्या इसका मतलब यह है कि चुनावी लोकतन्त्र की रंगभूमि पूरी तरह अर्थहीन है? या अब भी इसकी कोई भूमिका रह गयी है?
'मुक्त बाजार' (जो दरअसल मुक्त होने से कोसों दूर है) को राज्य की जरूरत है और बेतरह जरूरत है। गरीब देशों में जैसे–जैसे अमीर और गरीब लोगों के बीच असमानता बढ़ती जाती है, राज्य का काम भी बढ़ता जाता है। अकूत मुनाफा देने वाले 'प्यारे सौदों' की गश्त पर निकली बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकासशील देशों में राज्य मशीनरी की साँठ–गाँठ के बिना इन सौदों को तय नहीं कर सकतीं, न इन परियोजनाओं को चला सकती हैं। आज कॉर्पोरेट भूमण्डलीकरण को गरीब देशों में वफादार, भ्रष्ट, सम्भव हो तो निरंकुश सरकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ की जरूरत है ताकि अलोकप्रिय सुधार लागू किये जा सकें और विद्रोह कुचले जा सकें। इसे कहा जाता है 'निवेश का अच्छा माहौल बनाना।'
जब हम वोट डालते हैं, तब हम चुनते हैं कि राज्य की उत्पीड़नकारी दमनकारी शक्तियाँ हम किस पार्टी के हवाले करना चाहेंगे।
फिलहाल भारत में हमें नव–उदारवादी पूंजीवाद और साम्प्रदायिक नव–फासीवाद की, एक–दूसरी को काटती, खतरनाक धाराओं के बीच से रास्ता बनाना है। जहाँ 'पूँजीवाद' शब्द की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी है, वहीं 'फासीवाद' शब्द का इस्तेमाल अक्सर लोगों को खिझा देता है। हमें अपने आप से पूछना होगा: क्या हम इस शब्द का सटीक प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम परिस्थिति को बढ़ा–बढ़ा कर देख रहे हैं? क्या हमारे रोजमर्रा के अनुभव फासीवाद सरीखे हैं?
जब कोई सरकार कमोबेश खुले–आम ऐसे जनसंहार का समर्थन करती है जिसमें किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के दो हजार लोग बर्बरतापूर्वक मार दिये जाते हैं, तो क्या यह फासीवाद है? जब उस समुदाय की औरतों के साथ सरे–आम बलात्कार होता है और उन्हें जिन्दा जला दिया जाता है, तो क्या यह फासीवाद है? जब सर्वोच्च सत्ता इस बात की गारण्टी करती है कि किसी को इन अपराधों की सजा न मिले, तो क्या यह फासीवाद है? जब डेढ़ लाख लोग अपने घरों से खदेड़ दिये जाते हैं, दड़बों में बन्द कर दिये जाते हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं, तो क्या यह फासीवाद है? जब देश भर में नफरत के शिविर चलाने वाला सांस्कृतिक गिरोह, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, विनिवेशमन्त्री की प्रशंसा और सम्मान का पात्र बन जाता है, तो क्या यह फासीवाद है? जब विरोध करने वाले चित्रकारों, लेखकों, विद्वानों और फिल्म–निर्माताओं को गाली दी जाती है, उन्हें धमकाया जाता है और उनकी कृतियों को जलाया, प्रतिबन्धित और नष्ट किया जाता है, तो क्या यह फासीवाद है?[28] जब सरकार एक फरमान जारी करके स्कूलों की इतिहास की पाठ्य–पुस्तकों में मनमाने परिवर्तन कराती है, तो क्या यह फासीवाद है? जब भीड़ प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अभिलेखागार पर आक्रमण करती है और उसमें आग लगा देती है, जब हर छुटभैया नेता पेशेवर मध्यकालीन इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता होने का दावा करता है, जब कष्ट साध्य विद्वत्ता को आधारहीन लोकप्रिय दावेदारी के बल पर खारिज कर दिया जाता है, तो क्या यह फासीवाद है?[29] जब हत्या, बलात्कार, आगजनी और भीड़ के न्याय को सत्ताधारी पार्टी और उससे दाना–पानी पाने वाले बौद्धिकों का गिरोह सदियों पहले की गयी वास्तविक या झूठी ऐतिहासिक गलतियों का समुचित प्रतिकार कह कर जायज ठहराता है, तो क्या यह फासीवाद है? जब मध्यवर्ग और ऊँचे तबके के लोग एक क्षण को रुक कर च्च–च्च करते हैं और मजे से फिर अपनी जिन्दगी में रम जाते हैं, तो क्या यह फासीवाद है? जब इस सबकी सरपरस्ती करनेवाले प्रधानमन्त्री को राजनीतिज्ञ और भविष्य द्रष्टा कह कर उसकी जय–जयकार की जाती है तब क्या हम भरे–पूरे फासीवाद की बुनियाद नहीं रख रहे होते?
उत्पीड़ित और पराजित लोगों का इतिहास बहुत हद तक अनलिखा रह जाता है–यह सच्चाई सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं पर लागू नहीं होती। अगर ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के राजनैतिक रास्ते पर चलना ही हमारा चुना हुआ रास्ता है तो निश्चय ही भारत के दलितों और आदिवासियों को हत्या, आगजनी और बेलगाम कहर बरपा करने का अधिकार है?
रूस में कहा जाता है कि अतीत अनुमान से परे है। भारत में, स्कूली पाठ्य–पुस्तकों के साथ हुई छेड़–छाड़ के अनुभव से हम जानते हैं कि यह बात कितनी सच है। अब सभी 'छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी' बस यही उम्मीद लगाये रखने की हालत में पहुँचा दिये गये हैं कि बाबरी मस्जिद खुदाई में पुरातत्व–विदों को राम मन्दिर का कोई अवशेष नहीं मिलेगा। अगर यह सच भी हो कि भारत की हर मस्जिद के नीचे कोई–न–कोई मन्दिर है तो फिर मन्दिर के नीचे क्या था? शायद किसी और देवी–देवता का कोई और हिन्दू मन्दिर। शायद कोई बौद्ध स्तूप। बहुत करके कोई आदिवासी समाधि। इतिहास सवर्ण हिन्दूवाद से शुरू नहीं हुआ, हुआ था क्या? कितना गहरे हम खोदेंगे? कितना उलटेंगे–पलटेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ मुसलमान जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इस देश का अटूट अंग है, बाहरी और आक्रमणकारी कहे जाते हैं और क्रूरता से निशाना बनाये जाते हैं, जबकि सरकार विकास अनुदान के लिए ठेकों और कॉर्पोरेट सौदों पर उस हुकूमत के साथ करार करने में व्यस्त है जिसने सदियों तक हमें गुलाम बनाये रखा। 1876 से 1902 के बीच, भयंकर अकालों के दौरान लाखों हिन्दुस्तानी भूख से मर गये, जबकि अंग्रेज सरकार राशन और कच्चे माल का निर्यात करके इंग्लैण्ड भेजती रही। ऐतिहासिक तथ्य मरने वालों की संख्या सवा करोड़ से तीन करोड़ के बीच बताते हैं।[30] बदला लेने की राजनीति में इस संख्या की भी तो कोई जगह होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए क्या? या फिर प्रतिशोध का मजा तभी आता है जब उसके शिकार कमजोर और अशक्त हों और आसानी से निशाना बनाये जा सकते हों?
फासीवाद को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी ही कड़ी मेहनत 'निवेश का बेहतर माहौल बनाने' के लिए करनी पड़ती है। क्या दोनों साथ–साथ बेहतर काम करते हैं? ऐतिहासिक रूप से, कॉर्पोरेशनों को फासीवाद से किसी तरह से गुरेज नहीं रहा है। सीमेन्स, आई.जी. फारबेन, बेयर, आईबीएम और फोर्ड ने नाजियों के साथ व्यापार किया था।[31] हमारे पास भी बिलकुल हाल का उदाहरण सीआईआई (कनफेडेरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, भारतीय उद्योग संघ) का है, जिसने 2002 के गुजरात जनसंहार के बाद राज्य सरकार के आगे घुटने टेक दिये थे।[32] जब तक हमारे बाजार खुले है, एक छोटा–सा घरेलू फासीवाद अच्छे सौदे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा।
यह दिलचस्प है कि जिस समय तत्कालीन वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह भारत के बाजार को नव–उदारवाद के लिए तैयार कर रहे थे, लगभग उसी समय लालकृष्ण आडवानी साम्प्रदायिक उन्माद को हवा देते हुए और हमें नव-फासीवाद के लिए तैयार करते हुए अपनी पहली रथ-यात्रा पर निकले हुए थे।[33] दिसम्बर 1992 में उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तहस–नहस कर दिया। 1993 में महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार ने एनरॉन के साथ बिजली खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर किये। यह भारत में पहली निजी बिजली परियोजना थी। एनरॉन समझौता विध्वसंक साबित होने के बावजूद भारत में निजीकरण के युग की शुरुआत कर गया।[34] अब जब कांग्रेस चारदीवारी पर बैठ कर रिरिया रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके हाथ से मशाल छीन ली है। सरकार के दोनों हाथ मिल कर अभूतपूर्व जुगलबन्दी कर रहे हैं। एक थोक के भाव देश बेचने में व्यस्त है, जबकि दूसरा ध्यान बँटाने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कर्कश, बेसुरा राग अलाप रहा है। पहली प्रक्रिया की भयावह निर्ममता दूसरी प्रक्रिया के पागलपन में सीधे जा मिलती है।
आर्थिक रूप से भी यह जुगलबन्दी एक कारगर नमूना है। मनमाने निजीकरण से पैदा होनेवाले अकूत मुनाफों (और 'इण्डिया शाइनिंग' की कमाई) का एक हिस्सा हिन्दुत्व की विशाल सेना–आर.एस.एस., विहिप, बजरंग दल और बेशुमार दूसरी खैराती संस्थाओं और ट्रस्टों को मदद पहुँचाता है जो स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवाएँ चलाते हैं। देश भर में इन संगठनों की दसियों हजार शाखाएँ फैली हुई हैं। जिस नफरत का उपदेश ये वहाँ देते हैं, वह पूँजीवादी भूमण्डलीकरण के हाथों निरन्तर बेदखली और दरिद्रता का शिकार लोगों की अनियन्त्रित कुण्ठा से मिल कर गरीबों द्वारा गरीबों के विरुद्ध हिंसा को जन्म देती है। यह इतना कारगर पर्दा है जो सत्ता के तन्त्र को सुरक्षित और चुनौतीरहित बनाये रखता है।
बहरहाल, जनता की हताशा को हिंसा में बदल देना ही हमेशा काफी नहीं होता। 'निवेश का अच्छा माहौल' बनाने के लिए राज्य को अक्सर सीधा हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। हाल के वर्षों में, पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर, जिनमें ज्यादातर आदिवासी थे, कई बार गोलियाँ चलायी हैं। झारखण्ड में नगरनार; मध्यप्रदेश में मेंहदी खेड़ा; गुजरात में उमर गाँव; उड़ीसा में रायगढ़ और चिल्का और केरल में मुतंगा में लोग मारे गये हैं। लोग वन भूमि में अतिक्रमण करने के लिए मारे जाते हैं और उस समय भी जब वे बाँधों, खदान खोदने वालों और इस्पात के कारखानों से वनों की रक्षा कर रहे होते हैं। दमन–उत्पीड़न चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जम्बुद्वीप टापू, बंगाल; मैकंज ग्राम, उड़ीसा। पुलिस द्वारा गोली चलाने की लगभग हर घटना में जिन पर गोली चलायी गयी होती है उन्हें फौरन उग्रवादी करार दे दिया जाता है।]35]
***
जब उत्पीड़ित जन उत्पीड़ित होने से इन्कार कर देते हैं तब उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है और उनके साथ वैसा ही सलूक होता है। आतंक के विरुद्ध युद्ध के इस युग में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 181 देशों ने इस साल मतदान किया। अमरीका तक ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। भारत मतदान से बाहर रहा।[36] मानवाधिकार पर चैतरफा हमले के लिए मंच तैयार किया जा रहा है।
इस हालत में, आम लोग एक अधिकाधिक हिंसक होते राज्य के हमलों का मुकाबला कैसे करें?
अहिंसक सिविल नाफरमानी की जगह सिकुड़ गयी है। अनेक वर्षों तक संघर्ष करने के बाद कई जन प्रतिरोध आन्दोलनों की राह बन्द हो गयी है और वे अब ठीक ही महसूस कर रहे हैं कि दिशा बदलने का वक्त आ गया है। वह दिशा क्या होगी, इस पर गहरे मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हथियारबन्द संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचा है। कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़ कर, जमीन की विशाल पट्टियाँ, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के पूरे–पूरे जिले उन लोगों के नियन्त्रण में हैं जो इस विचार के हामी हैं।[37] दूसरों ने अधिकाधिक मात्रा में यह मानना शुरू कर दिया है कि उन्हें चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए–व्यवस्था के भीतर घुस कर अन्दर से उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। (क्या यह कश्मीरी अवाम के सामने मौजूद विकल्पों जैसी नहीं है?) याद रखने की बात यह है कि जहाँ दोनों के तरीके मूल रूप से अलग–अलग हैं, वहीं दोनों एक बात पर सहमत हैं कि अगर इसे मोटे शब्दों में कहें तो अब बहुत हो गया। या बास्ता।
भारत में इस समय ऐसी कोई बहस नहीं हो रही, जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका नतीजा, देश के जीवन को बदल कर रख देगा–चाहे बेहतरी की तरफ बदले, चाहे बदतरी की तरफ। अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण–हरेक के लिए।
हथियारबन्द संघर्ष राज्य की ओर से की गयी हिंसा को बड़े पैमाने पर उकसा देता है। कश्मीर और समूचे पूर्वोत्तर राज्यों को इसने जिस दलदल की ओर धकेल दिया है, उसे हमने देख लिया है। तो हम क्या वहीं करें, जो प्रधानमन्त्री की सलाह है कि हमें करना चाहिए? विरोध छोड़ दें और चुनावी राजनीति के अखाड़े में दाखिल हो जायें? रोड शो में शामिल हो जायें? निरर्थक गाली–गलौज के कर्कश आदान–प्रदान में भाग लें, जिसका एकमात्र उद्देश्य उस मिली–भगत और सम्पूर्ण सहमति पर पर्दा डालना है जो तकरार में जुटे इन लोगों के बीच वैसे पहले से ही लगभग पूरी तरह मौजूद है? हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे–परमाणु बम, बड़े बाँध, बाबरी मस्जिद विवाद और निजीकरण–पर बीज कांग्रेस ने बोये और फिर भाजपा ने उसकी घिनौनी फसल काटने के लिए सत्ता सँभाली।
इसका यह मतलब नहीं है कि संसद का कोई महत्व नहीं है और चुनावों को नजरअन्दाज कर देना चाहिए। अलबत्ता, एक फासीवादी प्रवृत्ति वाली खुल्लम–खुल्ला साम्प्रदायिक पार्टी और एक अवसरवादी साम्प्रदायिक पार्टी के बीच सचमुच अन्तर है। निश्चय ही, जो राजनीति खुले तौर पर गर्व के साथ नफरत का प्रचार करती है, उसमें और काँइयेपन से लोगों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति में सचमुच अन्तर है।
लेकिन यह सही है कि एक की विरासत ने ही हमें दूसरी की भयावहता तक पहुँचाया है। इन दोनों ने मिल कर उस वास्तविक विकल्प को क्षरित कर दिया है जो संसदीय लोकतन्त्र में मिलना चाहिए। चुनावों के गिर्द रचा गया उन्माद और मेले–ठेले का माहौल संचार माध्यमों में केन्द्रीय स्थान इसलिए ले लेता है, क्योंकि हर आदमी पक्के तौर पर जानता है कि जीते चाहे जो कोई, यथास्थिति मूल रूप से कतई नहीं बदलने जा रही है। (संसद में जोरदार बहस–मुबाहसे और आवेग–भरे भाषणों के बाद भी पोटा को हटाने की प्राथमिकता किसी पार्टी के चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं बनी। वे सभी यह जानते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत है, इस रूप में या उस रूप में)।[38] चुनाव के दौरान या विपक्ष में रहते हुए वे जो भी कहें, केन्द्र या राज्य की कोई भी सरकार, कोई भी राजनैतिक दल–दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी या हाशिये का–नव–उदारवाद के अश्वमेध के घोड़े को नहीं पकड़ सका है। 'भीतर' से कोई क्रान्तिकारी बदलाव नहीं आयेगा।
व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानती कि चुनावी अखाड़े में उतरना वैकल्पिक राजनीति का रास्ता है। ऐसा किसी किस्म के मध्यवर्गीय नकचढ़ेपन के कारण नहीं–कि 'राजनीति गन्दी चीज है' या 'सभी नेता भ्रष्ट हैं'–बल्कि इसलिए कि मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ कमजोर जगहों से नहीं, बल्कि मजबूत जगहों से लड़ी जानी चाहिए।
नव–उदारवाद और साम्प्रदायिक फासीवाद के दोहरे हमले का निशाना गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय बन रहे हैं। जैसे–जैसे नव–उदारवाद गरीब और अमीर के बीच, 'इण्डिया शाइनिंग' और भारत के बीच खाई को चौड़ा करता जा रहा है, वैसे–वैसे मुख्यधारा की किसी भी राजनैतिक पार्टी के लिए गरीब और अमीर दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का नाटक करना अधिकाधिक हास्यास्पद होता जा रहा है, क्योंकि एक के हितों का प्रतिनिधित्व दूसरे की कीमत पर किया जा सकता है। सम्पन्न भारतीय के नाते मेरे 'हित' (अगर मैं साधने की सोचूँ तो) आन्ध्र प्रदेश के गरीब किसानों के हितों से मुश्किल से ही मेल खायेंगे।
गरीबों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनैतिक पार्टी गरीब पार्टी होगी। उसके पास धन की बहुत कमी होगी। आजकल बिना धन के चुनाव लड़ना सम्भव नहीं है। कुछेक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ताओं को संसद में भेज देना तो दिलचस्प है, लेकिन राजनैतिक रूप से सार्थक नहीं है। यह प्रक्रिया इस लायक नहीं है कि उसमें अपनी सारी उर्जा खपा दी जाए। व्यक्तिगत करिश्मा, व्यक्तित्व की राजनीति क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सकती।
लेकिन गरीब होना कमजोर होना नहीं हैं। गरीबों की ताकत सरकारी इमारतों या अदालती दरवाजों के भीतर नहीं है। वह तो बाहर, खेतों, पहाड़ों, घाटियों, सड़कों और इस देश के विश्वविद्यालयों के परिसरों में है। वहीं बातचीत करनी चाहिए। वहीं लड़ाई छेड़ी जानी चाहिए।
अभी तो ये जगहें दक्षिणपन्थी हिन्दू राजनीति के हवाले कर दी गयी हैं। उनकी राजनीति के बारे में आपके विचार जो भी हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वे इन जगहों पर मौजूद हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे–जैसे राज्य अपनी जिम्मेवारियों से मुँह मोड़ कर स्वास्थ्य, शिक्षा और आवष्यक सार्वजनिक सेवाओं को आर्थिक संसाधन देना बन्द करता जा रहा है, वैसे–वैसे संघ परिवार के सिपाही उन क्षेत्रों में दाखिल होते गये हैं। घातक प्रचार करती अपनी हजारों शाखाओं के साथ–साथ वे स्कूल, हस्पताल, दवाखाने, एम्बुलेंस सेवाएँ, दुर्घटना राहत निकाय भी संचालित करते हैं। वे शक्तिहीनता के बारे में जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि लोगों, खासकर शक्तिहीन लोगों की न सिर्फ रोजमर्रा की, सीधी–साधी व्यावहारिक जरूरतें होती हैं, बल्कि उनकी भावनात्मक, आध्यात्मिक, मनोरंजनपरक आवश्यकताएँ और इच्छाएँ भी होती हैं। उन्होंने ऐसी घिनौनी कुठाली बनायी है जिसमें गुस्सा, हताशा, रोजमर्रा की जिल्लत– और बेहतर भविष्य के सपने–सब एक साथ पसाये जा सकते हैं और खतरनाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इस बीच, परम्परागत मुख्यधारा का वामपन्थ अब भी 'सत्ता हथियाने' के सपने देख रहा है, लेकिन समय की पुकार को सुनने और कदम उठाने के सिलसिले में अजीब कड़ापन और अनिच्छा प्रदर्शित कर रहा है। वह अपनी ही घेरेबन्दी का शिकार हो गया है और पहुँच से बाहर ऐसे बौद्धिक स्थान में सिमट गया है जहाँ प्राचीन बहसें ऐसी आदिकालीन भाषा में चलायी जा रही हैं, जिसे नाममात्र के लोग ही समझ सकते हैं।
संघ परिवार के हमले के सामने चुनौती का थोड़ा–बहुत आभास पेश करने वाली एकमात्र ताकत वो जमीनी प्रतिरोध आन्दोलन हैं, जो छिटपुट तौर पर पूरे देश में चल रहे हैं और 'विकास' के प्रचलित नमूने के कारण हो रही बेदखली और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश आन्दोलन एक–दूसरे से अलग–थलग हैं और 'विदेशी पैसे पानेवाले एजेण्ट' होने के निरन्तर आरोप के बावजूद, उनके पास पैसे या संसाधन नहीं हैं। वे आग से जूझने वाले महान योद्धा हैं। उनकी पीठ दीवार से सटी हुई है; लेकिन उनके कान धरती की धड़कन सुनते हैं; वे जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। अगर वे इकट्ठा हो जायें, अगर उनकी मदद की जाये, तो वे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनकी लड़ाई को, जब भी वह लड़ी जायेगी, आदर्शवादी लड़ाई होना होगा, कठोर विचारधारात्मक नहीं।
ऐसे समय, जब अवसरवाद की तूती बोल रही है, जब उम्मीद दम तोड़ती लग रही है, जब हर चीज रूखी–सूखी सौदेबाजी हो गयी है, हमें सपने देखने का साहस जुटाना होगा। रोमांस पर फिर से दावेदारी करनी होगी। न्याय में, स्वतन्त्रता में और गरिमा में विश्वास का रोमांस। सबके लिए। हमें एकजुट हो कर लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए हमें समझना होगा कि यह दैत्याकार पुरानी मशीन कैसे काम करती है। कौन कीमत चुकाता है, किसे फायदा होता है।
देश भर में छिटपुट चलने वाले और अलग–अलग मुद्दों की लड़ाई अकेले लड़ने वाले अनेक प्रतिरोध आन्दोलनों ने समझ लिया है कि उनकी किस्म की विशेष हित वाली राजनीति, जिसका कभी समय और जगह थी, अब काफी नहीं है। चूँकि अब वे हाशिये पर आ गये हैं, इसलिए अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति से मुँह मोड़ लिया जाय, यह मुनासिब नहीं होगा। लेकिन यह गम्भीर आत्म–निरीक्षण करने की जरूरत की तरफ इशारा करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग जो लोकतन्त्र को फिर से हासिल करना चाहते हैं, वे अपने चाल–चलन और काम करने के तरीके में समतावादी और जनतान्त्रिक हैं। अगर हमारे संघर्ष को उन आदर्शों पर खरा उतरना है तो हमें उन अन्दरूनी नाइन्साफियों को खत्म करना होगा जो हम दूसरों पर ढाते हैं, महिलाओं पर ढाते हैं, बच्चों पर ढाते हैं। मिसाल के लिए जो साम्प्रदायिकता से लड़ रहे हैं, उन्हें आर्थिक अन्याय पर आँख नहीं बन्द करनी चाहिए। जो लोग बड़े बाँध या विकास की परियोजनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें साम्प्रदायिकता से या अपने क्षेत्र में जातीय दमन से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, भले ही तात्कालिक रूप से उन्हें अपनी फौरी मुहिम में कुछ नुकसान उठाना पड़े। अगर तदबीर के तकाजे और मौकापरस्ती हमारी आस्था के आड़े आ–जा रही है, तब हममें और मुख्यधारा के नेताओं में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। अगर हम न्याय चाहते हैं तो यह न्याय और समानता सबके लिए होनी चाहिए, न कि कुछ खास समुदायों के लोगों के लिए, जिनके पास हितों को ले कर कुछ पूर्वाग्रह है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। हमने अहिंसक प्रतिरोध को 'फील गुड' के राजनैतिक अखाड़े में सिकुड़ जाने दिया है, जिसकी सबसे बड़ी सफलता संचार माध्यमों के लिए फोटो खिंचाने के अवसर हैं और सबसे कम सफलता उपेक्षा है।
हमें प्रतिरोध की रणनीति का मूल्यांकन करके उस पर तुरन्त विचार करना होगा, वास्तविक लड़ाइयाँ छेड़नी होंगी और असली नुकसान पहुँचाना होगा। हमें याद रखना है कि दाण्डी मार्च बेहतरीन राजनैतिक नाटक ही नहीं था, वह ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक आधार में सेंध लगाना था।
हमें राजनीति के अर्थ की पुनर्व्याख्या करनी होगी। 'नागरिक समाज' की पहलकदमियों का 'एनजीओकरण' हमें विपरीत दिशा में ले जा रहा है।[39] वह हमें अराजनैतिक बना रहा है। हमें 'फण्ड' और 'चन्दे' का मोहताज बना रहा है। हमें सिविल नाफरमानी के अर्थ की पुनःकल्पना करनी होगी।
शायद हमें जरूरत है लोकसभा के बाहर एक चुनी हुई छाया–संसद की, जिसके समर्थन और अनुमोदन के बगैर संसद आसानी से नहीं चल सकती। ऐसी संसद जो एक जमींदोज नगाड़ा बजाती रहती है, जो समझ और सूचना में साझेदारी करती है (जो सब मुख्यधारा के समाचार–माध्यमों में उत्तरोत्तर अनुपलब्ध हो रहा है)। निडरता से, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हमें इस मशीन के पुर्जों को बेकार बनाना होगा, जो हमें खाये जा रही है।
हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे बोलने के दौरान भी हिंसा का घेरा कसता जा रहा है। हर हाल में बदलाव तो आना ही है। वह खून से सना हुआ भी हो सकता है या खूबसूरती में नहाया हुआ भी। यह हम पर मुनहसिर है।
2. हिना कौसर आलम और पी.बालू, 'जे एण्ड के (जम्मू एण्ड कश्मीर) फजेज डीएनए सैम्पल्स टू कवर अप किलिंग्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 मार्च 2002।
3. देखें कम्यूनलिज्म कॉम्बैट, 'गोधरा,' और वरदराजन द्वारा सम्पादित 'गुजरात' में ज्योति पुनवाणी, 'द कारनेज ऐट गोधरा।'
4. सोमित सेन, 'शूटिंग टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन एनकाउण्टर कॉप्स,' टाइम्स ऑफ इण्डिया, 23 अगस्त 2003।
5. डब्ल्यू चन्द्रकान्त, क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज ऐक्टिविस्ट्स इन दि ऑफिंग?', द हिन्दू, 4 अक्टूबर 2003, जिसमें लिखा है:
6. जम्मू कश्मीर कोअलिशन फॉर सिविल सोसाइटी के अध्ययन, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू ऐण्ड कश्मीर बीटविन 1900–2006 (श्रीनगर 2006), में अनुमान प्रकट किया गया है कि 1990 और 2004 के बीच जम्मू और कश्मीर में मरने वालों की असली तादाद 70,000 से अधिक थी, जबकि भारत सरकार ने 1990 से 2005 तक सिर्फ 47,000 मृतकों की सूचना दी। देखें, ऐजाज हुसैन, 'मुस्लिम, हिन्दू प्रोटेस्ट्स इन इण्डियन कश्मीर,' एसोसिएट प्रेस, 1 जुलाई 2008; डेविड रोहडे, 'इण्डिया ऐण्ड कश्मीर सेपेरेटिस्ट्स बिगिन टॉक ऑन एंण्डिंग स्ट्राइफ,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 23 जनवरी 2004, पृ.ए8; डोएचे–प्रेस एजेन्तुर, 'थाउजेण्ड्स मिसिंग, अनमार्क्ड ग्रेव्ज टेल कश्मीर स्टोरी,' 7 अक्टूबर 2003।
7. लापता लोगों के माता–पिता के संगठन (एपीडीपी), श्रीनगर की अप्रकाशित रिपोर्ट।
8. देखें एडवर्ड ल्यूस, 'कश्मीरीज न्यू लीडर प्रॉमिसेज ''हीलिंग टच'', फाइनैन्शियल टाइम्स (लन्दन), 28 अक्टूबर 2002, पृ. 12।
9. रं मार्सेलो, ऐण्टी–टेरेरिज्म लॉ बैक्ड बाई इण्डियाज सुप्रीम कोर्ट, फाइनैन्शियल टाइम्स (लन्दन) 17 दिसम्बर 2003, पृ. 2।
10. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), 'ए प्रिलिमिनेरी फैक्ट फाइण्डिंग ऑन पोटा केसेज इन झारखण्ड,' डेल्ही इण्डिया, 2 मई 2003। इण्टरनेट पर उपलब्ध: http://pucl.org/Topics/Law/2003/poto–jharkhand.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
11. 'पीपुल्स ट्रिब्यून हाइलाइट्स मिसयूज ऑफ पोटा', द हिन्दू, 18 मार्च 2004।
12. 'पीपुल्स ट्रिव्यूनल।' 'ह्यूमन राइट्स वॉच आस्क सेन्टर टू रिपील पोटा' द हिन्दू, 18 मार्च 2004 भी देखें।
13. देखें लीना मिश्रा, '240 पोटा केसेज, ऑल अगेंस्ट माइनॉरिटीज,' टाइम्स ऑफ इण्डिया, 15 सितम्बर 2003 और 'पीपुल्स ट्रिब्युनल हाइलाइट्स मिसयूज ऑफ पोटा,' 18 मार्च 2004। टाइम्स ऑफ इण्डिया ने पेश की गयी गवाही की गलत सूचना दी। जैसा कि प्रेस ट्रस्ट का लेख दर्ज करता है, गुजरात में, 'सूची में एकमात्र गश्ैरमुस्लिम एक सिख है, लिवरसिंह तेजसिंह सिकलीगर, जिसका उल्लेख उसमें सूरत के एक वकील हसमुख ललवाला पर जानलेवा हमला करने के लिए हुआ था और जिसने अप्रैल (2003) में सूरत की पुलिस हिरासत में कथित रूप से फाँसी लगा ली थी।' गुजरात पर देखें, रॉय, 'डेमोक्रेसीः हू इज शी ह्वेन शी इज ऐट होम?' (हिंदी में:लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है)।
14. देखें, पीपल्स ट्रिब्युनल ऑन पोटा ऐण्ड अदर सिक्यूरिटी लेजिसलेशन्ज, द टेरर ऑफ पोटा (नई दिल्ली, इण्डिया, 13–14 मार्च 2004)। इण्टरनेट पर उपलब्ध http://www.sabrang.com/pota.pdf (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
15. 'ए प्रो–पुलिस रिपोर्ट,' द हिन्दू, 20 मार्च 2004। ऐमनेस्टी इण्टरनेशनल, 'इण्डियाः रिपोर्ट ऑफ दी मलिमथ कमिटी रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम: सम कमेंट्स,' 19 सितम्बर 2003 (एएसए 20/025/2003)।
16. 'जे एण्ड के (जम्मू एण्ड कश्मीर) पैनल वॉण्ट्स ड्रेकोनियन लॉज विदड्रॉन,' द हिन्दू, 23 मार्च 2003। साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेन्टर (एसएएचआरडीसी), 'आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स ऐक्ट: ए स्टडी इन नैशनल सिक्यूरिटी टिरिनी,' नवम्बर 1995, http://www.hrdc.net/sahrdc/resources/armed_forces.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
17. 'ग्रोथ ऑफ ए डीमन: जेनिसिस ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स ऐक्ट, 1958' और सम्बन्धित दस्तावेज, मणिपुर अपडेट्स। इण्टरनेट पर उपलब्ध है, देखें, http://www.geocities.com/manipurupdate/December_features_1.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
18. देखें, एडवर्ड ल्यूस, 'मास्टर ऑफ ऐम्बिग्विटी,' फाइनैन्शियल टाइम्स (लन्दन), 3–4 अप्रैल 2004, पृ. 16। 31 मार्च 2007 को चन्द्रशेखर प्रसाद की हत्या। देखें, ऐन्ड्रयू नैश, 'ऐन इलेक्शन ऐट जेएनयू,' हिमाल, दिसम्बर 2003।
19. पी. साइनाथ, 'नियो–लिबरल टेरेरिज्म इन इण्डिया: दी लार्जेस्ट वेव ऑफ सुइसाइड्स इन हिस्ट्री,' काउण्टरपंच, फरवरी 2009। इण्टरनेट पर उपलब्धः http://www.counterpunch.org/sainath02122009.html
20. एन.ए. मजूमदार, एलिमिनेट हंगर नाओ, पॉवर्टी लेटर, बिजनेस लाइन, 8 जनवरी 2003।
21. 'फूडग्रेन एक्सपोर्ट मे स्लो डाउन दिस फिष्ष्स्कल (इयर),' इण्डिया बिजनेस इनसाइट, 2 जून 2003, 'इण्डिया–ऐग्रिकल्चर सेक्टर: पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी,' बिजनेस लाइन, 26 जून 2001, रणजीत देवराज, 'फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेन्स्ट ग्लोबलाइजेशन,' इण्टर प्रेस सर्विस, 25 जनवरी 2001।
22. उत्सा पटनायक, 'फॉलिंग पर कैपिटा अवेलिबिलिटी ऑफ फूडग्रेन्स फॉर ह्यूमन कन्जंप्शन इन द रिफॉर्म्स पीरियड इन इण्डिया,' अखबार, (2 अक्टूबर 2001)। इण्टरनेट पर उपलब्धः http://indowindow.virtualstack.com/akhabar/article.php?article=44category=3&issue=12 (29 मार्च 2009 को देखा गया।) पी. साइनाथ, 'हैव टॉर्नाडो, विल ट्रैवल,' द हिन्दू मैग्जीन, 18 अगस्त 2002। सिल्विया नसर, 'प्रोफइल: द कॉन्शेन्स ऑफ द डिस्मल साइन्स,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 9 जनवरी 1994 पृ. 3-8। मारिया मिश्रा, 'हार्ट ऑफ स्मगनेस: अनलाइक बेल्ज्यिम, ब्रिटेन इज स्टील कम्प्लेसेंटली इगनोरिंग द गोरी क्रुऐलिटीज ऑफ इट्स एम्पायर,' द गार्जियन, (लन्दन) 23 जुलाई 2002, पृ. 15। उत्सा पटनायक, 'ऑन मेजरिंग, ''फैमिन'' डेथ्स: डिफ्रेंट क्राइटीरिया फॉर सोशयलिज्म ऐण्ड कैपिटलिज्म,' अखबार, 6 (नवम्बर–दिसम्बर 1999)। इण्टरनेट पर उपलब्धः http://www.indowindow.com/akhabar/article.php?article= 74&category=8&issue=9 (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
23. अमर्त्य सेन, 'डेवेलपमेन्ट ऐज फ्रीडम' (न्यूयॉर्क: अल्फ्रेड ए, नॉफ, 1999)
24. 'द वेस्टेड इण्डिया,' द स्टेट्समैन (इण्डिया), 17 फरवरी 2001। 'चाइल्डब्लेन,' द स्टेट्समैन (इण्डिया), 24 नवम्बर 2001।
25. उत्सा पटनायक, 'द रिपब्लिक ऑफ हंगर ऐण्ड अदर एसेज,' (गुड़गाँव: थ्री एसेज कलेक्टिव, 2007)।
26. प्रफुल्ल बिदवई, 'इण्डिया एडमिट्स सीरियस अग्रेरियन क्राइसिस,' सेण्ट्रल क्रॉनिकल (भोपाल), 9 अप्रैल 2004।
27. रॉय, पॉवर पोलिटिक्स, द्वितीय संस्करण, पृ. 13।
28. उदाहरण के लिए देखें, रणदीप रमेश, 'बांग्लादेशी राइटर गोज इनटू हाइडिंग', द गार्जियन (लन्दन), 27 नवम्बर 2007, पृ. 25, यह देशनिकाला प्राप्त और 2004 से कलकत्ता में रह रही लेखिका तसलीमा नसरीन के बारे में है, रणदीप रमेश, 'बैण्ड आर्टिस्ट मिसेज डेल्हीज फर्स्ट आर्ट शो,' द गार्जियन (लन्दन), 23 अगस्त 2008, पृ. 22। यह निष्कासित चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के बारे में है, और सोमिनी सेनगुप्ता, 'ऐट ए यूनिवर्सिटी इन इण्डिया, न्यू अटैक्स ऑन ऐन ओल्ड स्टाइल: इरोटिक आर्ट,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 19 मई 2007, पृ. B7। यह महाराजा शिवाजीराव विश्वविद्यालय के छात्रों की प्रदर्शनी के बारे में। अरुंधति रॉय, 'तसलीमा नसरीन ऐण्ड ''फ्री स्पीच,''' नई दिल्ली, इण्डिया 13 फरवरी 2008 भी देखें, इण्टरनेट पर उपलब्ध http://www.zmag.org/znet/viewArticle/166646 (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
29. शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने जेम्स डब्ल्यू. लेन की पुस्तक 'शिवाजी: हिन्दू किंग इन इस्लामिक इण्डिया (ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2003) की 'सभी प्रतियों को जलाने का आह्वान' किया। देखें, 'मॉकरी ऑफ द लॉ,' द हिन्दू 3 मई 2007। प्रफुल्ल बिदवई, 'मेक्कार्थी, वेयर आर यू?' फ्रंटलाइन (इण्डिया); 10–23 मई 2003, इसमें विख्यात इतिहासकार रोमिला थापर के खिलाफ चलाये गये अभियान के बारे में लिखा गया है; और अनुपमा कटकम, ''पॉलिटिक्स ऑफ वैण्डलिज्म, फ्रंटलाइन (इण्डिया), 17–30 जनवरी 2004, पुणे स्थित भण्डारकर संस्थान पर हमले के बारे में।
30. देखें, माइक डेविस, लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स: एल निन्यो फैमिन्स ऐण्ड द मेकिंग ऑफ द थर्ड वल्र्ड (न्यूयॉर्क: वर्सो, 2002) 'टेबल पी 1: एस्टिमेटेड फैमिन मोर्टैलिटी,' पृ. 7।
31. दूसरे स्रोतों के अलावा, देखें एडविन ब्लेक, आईबीएम ऐण्ड द होलोकॉस्ट: द स्ट्रैटिजिक अलायन्स बिटवीन नाजी जर्मनी ऐण्ड अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन (न्यूयॉर्क: थ्री रिवर्स प्रेस, 2003)।
32. 'फॉर इण्डिया इनकॉर्पोरेटेड, साइलेंस प्रोटेक्ट्स द बॉटम लाइन, टाइम्स ऑफ इण्डिया, 17 फरवरी 2003। 'सीआईआई अपोलोजाइजेज टू मोदी,' द हिन्दू, 7 मार्च 2003।
33. आडवाणी ने 25 सितम्बर 1990 को सोमनाथ से यात्रा शुरू की थी। 2005 में उन्होंने कहा कि उनकी 15 साल पहले की ऐतिहासिक राम रथ यात्रा तभी पूरी मानी जायेगी जब अयोध्या में मन्दिर बन जायेगा। देखें, विशेष सम्वाददाता, 'यात्रा कम्पलीट ओनली आफ्टर टेम्पल इज बिल्ट, सेज आडवाणी,' द हिन्दू, 26 सितम्बर 2005।
34. देखें रॉय, पावर पॉलिटिक्स, द्वितीय संस्करण, पृ. 35–86।
35. अन्य स्रोतों के साथ, देखें निर्मलांग्शु मुखर्जी, 'ट्रेल ऑफ द टेरर कॉप्स,' जेडनेट, 17 नवम्बर 2008। इण्टरनेट पर उपलब्ध http://www.zmag.org/zspace/nirmalangshumukherji (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
36. 22 दिसम्बर 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 'आतंकवाद से लड़ाई में मानवाधिकारों और आधारभूत स्वतन्त्रताओं की रक्षा' के प्रस्ताव से अपने–आप को अलग रखने वाला भारत अकेला देश था।AA/RES/58/187 (अप्रैल 2004)।
37. देखें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, इण्डियाज नक्सलाइट्स मेकिंग एफर्ट्स टू स्प्रेड टू न्यू एरियाज,' बीबीसी वर्ल्ड वाइड मॉनिटरिंग, 4 मई 2003 और 'माओइस्ट कॉल फ्रीजेज झारखण्ड, नेबर्स,' द स्टेट्समैन (इण्डिया), 15 जून 2006।
38. कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने 2004 में पोटा को रद्द कर दिया क्योंकि वह अत्यन्त क्रूर पाया गया था, और कहा कि उसका दुरुपयोग हुआ था और वह उलटे नतीजे देने वाला था, लेकिन फिर सरकार ने 'अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम में संशोधनों के रूप में और भी कड़ा आतंककारी कानून लागू कर दिया। संशोधन 15 दिसम्बर 2008 को संसद में पेश किये गये और अगले ही दिन स्वीकार कर लिये गये। लगभग कोई बहस नहीं हुई। देखें प्रशान्त भूषण, 'टेरेरिज्म: आर स्ट्रौंगर लॉज द आन्सर?' द हिन्दू, 1 जनवरी 2009।
39. देखें अरुंधति रॉय, ऐन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर में 'पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर' (नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, इण्डिया 2005)। अरुंधति रॉय, 'पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, (न्यूयॉर्क सेवन स्टोरीज प्रेस, 2004) में भी प्रकाशित।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 अप्रैल 2004 को दिये गये आई.जी. खान स्मृति व्याख्यान का सम्पूर्ण आलेख है।[1] यह पहले हिन्दी में 23–24 अप्रैल 2004 कोहिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ (अनुवाद: जितेंद्र कुमार), और फिर अंग्रेजी में 25 अप्रैल 2004 को द हिन्दू में।
हाल ही में एक नौजवान कश्मीरी दोस्त मुझसे कश्मीर की जिन्दगी के बारे में बात कर रहा था। राजनैतिक भ्रष्टाचार और अवसरवाद के दलदल, सुरक्षा–बलों के बेरहम वहशीपन और हिंसा में डूबे समाज की अधूरी संक्रमणशील सीमाओं के बारे में बता रहा था, जहाँ आतंकवादी, पुलिस, खुफिया अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी और पत्रकार भी एक–दूसरे के रू–ब–रू होते हैं और आहिस्ता–आहिस्ता एक–दूसरे में तब्दील हो जाते हैं। वह अन्तहीन खून–खराबे, लोगों के लगातार 'गायब' होने, फुसफुसाहटों, भय, अनसुलझी अफवाहों के बीच जीने के बारे में और जो सचमुच हो रहा है, जो कश्मीरी जानते हैं कि हो रहा है और जो हम बाकियों को बताया जाता है कि हो रहा है, इसकी आपसी असम्बद्धता के बीच जीने के बारे में बता रहा था। उसने कहा, 'पहले कश्मीर एक धन्धा था, अब वह पागलखाना बन चुका है।'
जितना अधिक मैं उसकी टिप्पणी के बारे में सोचती हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे यह वर्णन पूरे हिन्दुस्तान के लिए उपयुक्त जान पड़ता है। यह मानते हुए कि कश्मीर और – मणिपुर, नगालैण्ड और मिजोरम के – उत्तर-पूर्वी राज्य उस पागलखाने के दो अलग-अलग खण्ड हैं जिनमें इस पागलखाने के ज्यादा खतरनाक वार्ड हैं। लेकिन, हिन्दुस्तान के बीचोबीच भी, जानकारी और सूचना के बीच, जो हम जानते हैं और जो हमें बताया जाता है उसके बीच, जो अज्ञात है और जिसका दावा किया जाता है उसके बीच, जिस पर पर्दा डाला जाता है और जिसका उद्घाटन किया जाता है उसके बीच, तथ्य और अनुमान के बीच, 'वास्तविक' दुनिया और आभासी दुनिया के बीच जो गहरी खाई है, वह ऐसी जगह बन गयी है जहाँ अन्तहीन अटकलों और सम्भावित पागलपन का साम्राज्य फैला हुआ है। एक जहरीला घोल है जिसे हिला–हिला कर खौलाया गया है और सबसे ज्यादा घिनौने, विध्वंसक राजनैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है।
हर बार जब कोई तथाकथित आतंकवादी हमला होता है, सरकार थोड़ी–बहुत या बिना किसी छानबीन के, इसकी जिम्मेवारी किसी के सर पर मढ़ने के लिए दौड़ पड़ती है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी, संसद भवन पर 13 दिसम्बर 2001 का हमला या छत्तीसिंहपुरा (कश्मीर) में मार्च 2000 को तथाकथित आतंकवादियों द्वारा सिखों का जनसंहार इसके कुछ बड़ी–बड़ी मिसालें हैं। (वे तथाकथित आतंकवादी, जिन्हें बाद में सुरक्षा–बलों ने मार गिराया, बाद में निर्दोष साबित हुए। बाद में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि खून के फर्जी नमूने डीएनए जाँच के लिए पेश किये गये थे।[2] इनमें से हर मामले में जो साक्ष्य सामने आये, उनसे बेहद बेचैन कर देने वाले सवाल उभरे और इसलिए मामले को फौरन ताक पर धर दिया गया। गोधरा का मामला लीजिए–जैसे ही घटना घटी, गृहमंत्री ने घोषणा की कि यह आई.एस.आई. का षड्यंत्र है। विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि यह पेट्रोल बम फेंक रहे मुसलमानों की भीड़ का काम था।[3] गम्भीर सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। अटकलों का कोई अन्त नहीं है। हर आदमी जो जी चाहे मानता है, लेकिन घटना का इस्तेमाल संगठित साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए किया जाता है।
11 सितम्बर के हमले की घटना के इर्द–गिर्द बुने गये झूठ और प्रपंच का उपयोग अमरीकी सरकार ने एक नहीं, बल्कि दो देशों पर हमला करने के लिए किया–और ऊपरवाला ही जाने आगे–आगे होता है क्या? भारत सरकार इसी रणनीति का इस्तेमाल करती है–दूसरे देशों के साथ नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ।
पिछले एक दशक के अर्से में पुलिस और सुरक्षा–बलों द्वारा मारे गये लोगों की गिनती हजारों में है। हाल में मुम्बई के कई पुलिसवालों ने प्रेस के सामने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अपने ऊँचे अधिकारियों के 'आदेश' पर उन्होंने कितने 'गैंगस्टरों' का सफाया किया।[4] आन्ध्र प्रदेश में औसतन एक साल में तकरीबन दो सौ 'चरमपन्थियों' की मौत 'मुठभेड़' में होती है।[5] कश्मीर में, जहाँ हालात लगभग जंग जैसे हैं, 1989 के बाद से अनुमानतः 80 हजार लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग गायब हैं।[6] 'गुमशुदा लोगों के अभिभावक संघ' (एपीडीपी) के अनुसार अकेले 2003 में तीन हजार से अधिक लोग मारे गये हैं, जिनमें से 463 फौजी हैं।[7] 'अभिभावक संघ' के अनुसार अक्टूबर 2002 में जब से मुफ्ती मोहम्मद सरकार 'मरहम लगाने' के वादे के साथ सत्ता में आयी, तब से 54 लोगों की हिरासती मौत हुई है।[8] प्रखर राष्ट्रवाद के इस युग में जब तक मारे गये लोगों पर गैंगस्टर, आतंकवादी, राजद्रोही, या चरमपन्थी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, उनके हत्यारे राश्ट्रीय हित के धर्मयोद्धाओं के तौर पर छुट्टा घूम सकते हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। अगर यह सच भी होता (जो कि निश्चय ही नहीं है) कि हर आदमी जो मारा गया है वह सचमुच गैंगस्टर, आतंकवादी, राजद्रोही, या चरमपन्थी था–तो यह बात हमें सिर्फ यही बताती है कि इस समाज के साथ कोई भयंकर गड़बड़ी है जो इतने सारे लोगों को ऐसे हताषा–भरे कदम उठाने पर मजबूर करता है।
भारतीय राज्य–व्यवस्था में लोगों को उत्पीड़ित और आतंकित करने की तरफ जो रुझान है उसे 'आतंकवाद निरोधक अधिनियम' (पोटा) को पारित करके संस्थाबद्ध और संस्थापित कर दिया गया है, जिसे दस राज्यों ने लागू भी कर दिया है। पोटा पर सरसरी निगाह डालने से भी यह पता चल जायेगा कि वह क्रूरतापूर्ण और सर्वव्यापी है। यह ऐसा अनगिनत फंदों वाला और सर्वसमावेशी कानून है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है–विस्फोटकों के जखीरे के साथ पकड़े गये अल–कायदा का कार्यकर्ता भी और नीम के नीचे बाँसुरी बजा रहा कोई आदिवासी भी। पोटा की हुनरमन्दी की खासियत यह है कि सरकार इसे जो बनाना चाहे, यह बन सकता है। जीने के लिए हम उनके मोहताज हैं जो हम पर राज करते हैं। तमिलनाडु में राज्य सरकार इसका इस्तेमाल अपनी आलोचना का दम घोंटने के लिए करती है।[9] झारखण्ड में 3200 लोगों को, जिनमें ज्यादातर गरीब आदिवासी हैं और जिन पर माओवादी होने का आरोप लगाया गया है, पोटा के तहत अपराधी ठहराया गया है।[10] पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस कानून का उपयोग उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो अपनी जमीन और आजीविका के अधिकार के हनन का विरोध करने की जुर्रत करते हैं।[11] गुजरात और मुम्बई में इसे लगभग पूरे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता र्है।[12] गुजरात में, 2002 के राज्य प्रायोजित जनसंहार के बाद, जिसमें अनुमानतः 2000 मुसलमान मारे गये और डेढ़ लाख बेघर कर दिये गये, 287 लोगों पर पोटा लगाया गया, जिनमें 286 मुसलमान और एक सिख है।[13] पोटा में इस बात की छूट दी गयी है कि पुलिस हिरासत में हासिल बयान कानूनी सबूत के तौर पर माने जा सकते हैं। हकीकतन, पोटा निजाम के तहत, पुलिसिया छानबीन की जगह पुलिस यातना ले लेती है। यह ज्यादा त्वरित, ज्यादा सस्ता है और शर्तिया नतीजे पैदा करने वाला है। अब कीजिए बात सरकारी खर्च घटाने की।
मार्च 2004 में, मैं पोटा पर हो रही जनसुनवाई में मौजूद थी।[14] दो दिनों तक लगातार हमने अपने इस अद्भुत लोकतन्त्र में हो रही घटनाओं की लोमहर्षक गवाहियाँ सुनीं। मैं यकीनन कह सकती हूँ कि हमारे पुलिस थानों में सब कुछ होता है–लोगों को पेशाब पीने पर मजबूर करने, उन्हें नंगा करने, जलील करने, बिजली के झटके देनें, सिगरेट के जलते हुए टोटों से जलाये जाने, गुदा में लोहे की छड़ें घुसेड़ने से ले कर पीटने और ठोकरें मार–मार कर जान ले लेने तक।
देश भर में पोटा के आरोपित सैकड़ों लोग, जिनमें कुछ बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कैद करके जमानत के बिना, विशेष पोटा अदालतों में, जो जनता की छानबीन से परे हैं, सुनवाई के इन्तजार में हिरासत में रखे गये हैं। पोटा के तहत धरे गये अधिकतर लोग एक या दो अपराधों के दोषी हैं। या तो वे गरीब हैं–ज्यादातर दलित और आदिवासी। या फिर वे मुसलमान हैं। पोटा आपराधिक कानून की इस माने हुए नियम को उलट देता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। पोटा के तहत आपको तब तक जमानत नहीं मिल सकती जब तक आप साबित नहीं कर देते कि आप निर्दोष हैं और वह भी उस अपराध के सिलसिले में जिसका औपचारिक आरोप आप पर नहीं लगाया गया है। सार यह है कि आपको यह साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं भले ही आपको उस अपराध का सान–गुमान भी न हो जो फर्जिया तौर पर आपने किया है। और यह हम सब पर लागू होता है। तकनीकी तौर पर हम एक ऐसा राष्ट्र हैं, अपराधी ठहराये जाने का इन्तजार कर रहा है।
यह मानना भोलापन होगा कि पोटा का 'दुरुपयोग' हो रहा है। इसके विपरीत इसका इस्तेमाल ठीक–ठीक उन्हीं कारणों से किया जा रहा है, जिसके लिए यह बनाया गया था। असल में तो अगर मलिमथ समिति की सिफारिशों को लागू किया जाये तो पोटा जल्दी ही बेकार हो जायेगा। मलिमथ समिति ने सिफारिश की है कि किन्हीं सन्दर्भों में सामान्य आपराधिक कानून को पोटा के प्रावधानों के मुताबिक ढाला जाय।[15] इसके बाद कोई अपराधी नहीं रहेगा, सिर्फ आतंकवादी होंगे, साफ-सुथरा हल है, झंझट बचेगा।
जम्मू–कश्मीर और अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में आज 'सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम' न केवल सेना के अफसरों और कमीशन–प्राप्त जूनियर अधिकारियों को, बल्कि गैर–कमीशन–प्राप्त जूनियर अधिकारियों को भी किसी व्यक्ति पर हथियार रखने या कानून–व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाने के सन्देह में बल–प्रयोग (यहाँ तक कि मार भी डालने) की इजाजत देता है।[16] सन्देह में! किसी भी भारतवासी को इस बारे में कोई भ्रम नहीं हो सकता कि इसका क्या मतलब होता है। सुरक्षा बलों द्वारा यातना, गुमशुदगी, हिरासत में मौत, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएँ दर्ज की गयी हैं, वे आपका खून जमा देने के लिए पर्याप्त हैं। इस सब के बावजूद, अगर हिन्दुस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी और खुद अपने मध्यवर्ग के बीच एक वैध लोकतन्त्र की छवि बनाये रखने में सफल है, तो यह एक जीत ही है।
'सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम' उस अधिनियम का और भी कठोर प्रारूप है, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आन्दोलन से निपटने के लिए 15 अगस्त 1942 को पारित किया था। 1958 में इसे मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू किया गया, जिन्हें 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था। 1965 में पूरा मिजोरम, जो तब असम का हिस्सा था, 'अशांत' घोशित कर दिया गया। 1972 में इस अधिनियम के तहत त्रिपुरा भी आ गया। और 1980 के आते–आते पूरे मणिपुर को 'अशांत' घोषित कर दिया गया।[17] इससे ज्यादा और कौन–से सबूत चाहिए कि दमनकारी कदम उल्टा नतीजा देते हैं और समस्या को सुलझाने के बजाय उलझा देते हैं?
लोगों का उत्पीड़न करने और उनका सफाया कर देने की इस अशोभन उत्सुकता के साथ–साथ भारतीय राज्य–व्यवस्था में उन मामलों की छानबीन करके उन्हें अदालतों तक पहुँचाने न्याय देने की लगभग प्रकट अनिच्छा भी दिखाई देती है, जिनमें भरपूर साक्ष्य मौजूद हैं: 1984 में दिल्ली में तीन हजार सिखों का संहार, 1993 में मुम्बई में और 2002 में गुजरात में मुसलमानों का संहार (आज तक किसी को सजा नहीं), कुछ साल पहले जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रशेखर की हत्या, 12 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के शंकर गुहा नियोगी की हत्या–इसके चन्द उदाहरण हैं।[18] जब पूरी राज्य मशीनरी ही आपके खिलाफ खड़ी हो, तो चश्मदीद गवाहियाँ और ढेर सारे प्रामाणिक सबूत तक नाकाफी हो जाते हैं।
इस बीच, बड़ी पूँजी से निकलने वाले अखबारों में उल्लसित अर्थषास्त्री हमें बताते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। दुकानें सामानों से अटी पड़ी हैं। सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए हें। इस चकाचौंध से बाहर कर्ज में डूबे किसान सैकड़ों की तादाद में आत्म–हत्या कर रहे हैं।[19] देश भर से भुखमरी और कुपोषण की खबरें आ रही हैं, फिर भी सरकार ने अपने गोदामों में 6 करोड़, 30 लाख टन अनाज सड़ने दिया।[20] एक करोड़ 20 लाख टन अनाज निर्यात करके घटायी गयी दरों पर बेचा गया जिन दरों पर भारत सरकार भारत के गरीब लोगों को नहीं देना चाहती थी।[21] सुप्रसिद्ध कृषि अर्थषास्त्री उत्सा पटनायक ने सरकारी आँकड़ों के आधार पर भारत में तकरीबन सौ वर्षों की अन्न उपलब्धता और अन्न की खपत की गणना की है। उन्होंने हिसाब लगाया है कि 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों और 2001 के बीच वार्षिक अन्न उपलब्धता घट कर द्वितीय विश्वयुद्ध के वर्षों से भी कम हो गयी है, जिनमें बंगाल के अकाल वाले वर्ष शामिल हैं, जिसमें 30 लाख लोगों ने भुखमरी से जानें गँवा दी थीं।[22] जैसा कि हम प्रोफेसर अमर्त्य सेन की कृतियों से जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भूख से हुई मौतों को अच्छी नजर से नहीं देखतीं। इस पर 'स्वतंत्र समाचार माध्यमों' में नकारात्मक टीका–टिप्पणी और आलोचना होने लगती है।[23]
लिहाजा, कुपोषण और स्थायी भुखमरी के खतरनाक स्तर आजकल पसन्दीदा आदर्श हैं। तीन साल से कम उम्र के 47 फीसदी हिन्दुस्तानी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 46 फीसदी की विकास रुक गया है।[24] उत्सा पटनायक अपने अध्ययन में बतलाती है कि भारत के लगभग 40 फीसदी ग्रामवासियों की अन्न की खपज उतनी ही है जितनी कि उप–सहारा अफ्रीका के लोगों की खाते हैं।[25] आज ग्रामीण भारत में एक औसत परिवार हर साल 1990 के दशक के आरम्भिक वर्षों की तुलना में 100 किग्रा कम अनाज खाते हैं।[26]
लेकिन भारत के शहरों में, जहाँ कहीं भी आप जायें–दुकान, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जिम्नेजियम, हॉस्पिटल–हर जगह आपके सामने टीवी के पर्दे होंगे, जिनपर चुनावी वादों के पूरे हो चुके दिखेंगे। भारत चमक रहा है, 'फील गुड' कर रहा है। आपको महज किसी की पसलियों पर पुलिसवाले के बूटों की धमक पर अपने कान बन्द करने हैं, महज गन्दगी, झोपड़–पट्टियों, सड़कों पर चीथड़ों में जर्जर टूटे हुए लोगों से अपनी निगाहें हटानी हैं और उन्हें टीवी के किसी दोस्ताना पर्दे पर डालनी हैं, और आप उस दूसरी खूबसूरत दुनिया में दाखिल हो जायेंगे। बॉलीवुड की हरदम ठुमके लगाती, कमर मटकाती, नाचती–गाती दुनिया, तिरंगा फहराते और 'फील गुड' करते, स्थायी रूप से साधन–सम्पन्न और हरदम खुश हिन्दुस्तानियों की दुनिया। दिनों–दिन यह कहना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन–सी दुनिया असली है और कौन–सी दुनिया आभासी। पोटा जैसे कानून टेलीविजन स्विच के मानिन्द हैं। आप इनका प्रयोग गरीब, तंग करने वाले, अवांछित लोगों को पर्दे पर से हटाने के लिए कर सकते हैं।
***
भारत में एक नये तरह का अलगाववादी आन्दोलन चल रहा है। क्या इसे हम 'नव–अलगाववाद' कहें? यह 'पुराने अलगाववाद' का विलोम है। इसमें वे लोग जो वास्तव में एक बिलकुल दूसरी अर्थ–व्यवस्था, बिलकुल दूसरे देश, बिलकुल दूसरे ग्रह के वासी हैं, यह दिखावा करते हैं कि वे इस दुनिया का हिस्सा हैं। यह ऐसा अलगाव है जिसमें लोगों का अपेक्षाकृत छोटा तबका लोगों के एक बड़े समुदाय से सब कुछ– जमीन, नदियाँ, पानी, स्वाधीनता, सुरक्षा, गरिमा, विरोध के अधिकार समेत बुनियादी अधिकार–छीन कर अत्यन्त समृद्ध हो जाता है। यह रेखीय, क्षेत्रीय अलगाव नहीं है, बल्कि ऊपर को उन्मुख अलगाव है। असली ढाँचागत समायोजन जो 'इंडिया शाइनिंग' को, 'भारत उदय' को भारत से अलग कर देता है। यह इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सार्वजनिक उद्यम वाले भारत से अलग कर देता है।
यह ऐसा अलगाव है जिसमें सार्वजनिक तन्त्र, उत्पादक सार्वजनिक सम्पदा, पानी, बिजली, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन–वह सारी सम्पदा जिसे, यह माना जाता है कि, जनता की नुमाइन्दगी करने वाले भारतीय राज्य को धरोहर की तरह सँजो कर रखना चाहिए, वह सम्पदा जिसे दशकों के अर्से में सार्वजनिक धन से निर्मित किया और सुरक्षित रखा गया है–उसे राज्य निजी निगमों को बेच देता है। भारत में 70 प्रतिशत आबादी–70 करोड़ लोग–ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।[27] उनकी आजीविका प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इन्हें उनसे छीन लेना और थोक में निजी कम्पनियों को बेचना बर्बर पैमाने पर बेदखल करने और कंगाल बना देने की शुरुआत है।
इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कुछेक व्यापारिक घरानों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जागीर बनने की ओर बढ़ रहा है। इन कम्पनियों के प्रमुख कार्याधिकारी (सीईओ) इस देश को, इसके तन्त्र और इसके संसाधनों, इसके संचार माध्यमों और पत्रकारों के नियन्ता होंगे। लेकिन जनता के प्रति उनकी देनदारी शून्य होगी। वे पूरी तरह से–कानूनी, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक रूप से–जवाबदेही से बरी होंगे। जो लोग कहते हैं कि भारत में कुछ प्रमुख कार्याधिकारी प्रधानमन्त्री से ज्यादा ताकतवर हैं, वे जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं।
इस सब के आर्थिक आशयों से बिलकुल अलग, भले ही यह वह सब हो जिसका गुण–गान होता है (जो यह नहीं है)–चमत्कारिक, कार्यकुशल, अद्भुत–क्या इसकी राजनीति हमें स्वीकार है? अगर भारतीय राज्य अपनी जिम्मेदारियों को मुट्ठी भर निगमों के यहाँ गिरवी रखने का फैसला करता है तो क्या इसका मतलब यह है कि चुनावी लोकतन्त्र की रंगभूमि पूरी तरह अर्थहीन है? या अब भी इसकी कोई भूमिका रह गयी है?
'मुक्त बाजार' (जो दरअसल मुक्त होने से कोसों दूर है) को राज्य की जरूरत है और बेतरह जरूरत है। गरीब देशों में जैसे–जैसे अमीर और गरीब लोगों के बीच असमानता बढ़ती जाती है, राज्य का काम भी बढ़ता जाता है। अकूत मुनाफा देने वाले 'प्यारे सौदों' की गश्त पर निकली बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकासशील देशों में राज्य मशीनरी की साँठ–गाँठ के बिना इन सौदों को तय नहीं कर सकतीं, न इन परियोजनाओं को चला सकती हैं। आज कॉर्पोरेट भूमण्डलीकरण को गरीब देशों में वफादार, भ्रष्ट, सम्भव हो तो निरंकुश सरकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ की जरूरत है ताकि अलोकप्रिय सुधार लागू किये जा सकें और विद्रोह कुचले जा सकें। इसे कहा जाता है 'निवेश का अच्छा माहौल बनाना।'
जब हम वोट डालते हैं, तब हम चुनते हैं कि राज्य की उत्पीड़नकारी दमनकारी शक्तियाँ हम किस पार्टी के हवाले करना चाहेंगे।
फिलहाल भारत में हमें नव–उदारवादी पूंजीवाद और साम्प्रदायिक नव–फासीवाद की, एक–दूसरी को काटती, खतरनाक धाराओं के बीच से रास्ता बनाना है। जहाँ 'पूँजीवाद' शब्द की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी है, वहीं 'फासीवाद' शब्द का इस्तेमाल अक्सर लोगों को खिझा देता है। हमें अपने आप से पूछना होगा: क्या हम इस शब्द का सटीक प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम परिस्थिति को बढ़ा–बढ़ा कर देख रहे हैं? क्या हमारे रोजमर्रा के अनुभव फासीवाद सरीखे हैं?
जब कोई सरकार कमोबेश खुले–आम ऐसे जनसंहार का समर्थन करती है जिसमें किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के दो हजार लोग बर्बरतापूर्वक मार दिये जाते हैं, तो क्या यह फासीवाद है? जब उस समुदाय की औरतों के साथ सरे–आम बलात्कार होता है और उन्हें जिन्दा जला दिया जाता है, तो क्या यह फासीवाद है? जब सर्वोच्च सत्ता इस बात की गारण्टी करती है कि किसी को इन अपराधों की सजा न मिले, तो क्या यह फासीवाद है? जब डेढ़ लाख लोग अपने घरों से खदेड़ दिये जाते हैं, दड़बों में बन्द कर दिये जाते हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं, तो क्या यह फासीवाद है? जब देश भर में नफरत के शिविर चलाने वाला सांस्कृतिक गिरोह, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, विनिवेशमन्त्री की प्रशंसा और सम्मान का पात्र बन जाता है, तो क्या यह फासीवाद है? जब विरोध करने वाले चित्रकारों, लेखकों, विद्वानों और फिल्म–निर्माताओं को गाली दी जाती है, उन्हें धमकाया जाता है और उनकी कृतियों को जलाया, प्रतिबन्धित और नष्ट किया जाता है, तो क्या यह फासीवाद है?[28] जब सरकार एक फरमान जारी करके स्कूलों की इतिहास की पाठ्य–पुस्तकों में मनमाने परिवर्तन कराती है, तो क्या यह फासीवाद है? जब भीड़ प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अभिलेखागार पर आक्रमण करती है और उसमें आग लगा देती है, जब हर छुटभैया नेता पेशेवर मध्यकालीन इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता होने का दावा करता है, जब कष्ट साध्य विद्वत्ता को आधारहीन लोकप्रिय दावेदारी के बल पर खारिज कर दिया जाता है, तो क्या यह फासीवाद है?[29] जब हत्या, बलात्कार, आगजनी और भीड़ के न्याय को सत्ताधारी पार्टी और उससे दाना–पानी पाने वाले बौद्धिकों का गिरोह सदियों पहले की गयी वास्तविक या झूठी ऐतिहासिक गलतियों का समुचित प्रतिकार कह कर जायज ठहराता है, तो क्या यह फासीवाद है? जब मध्यवर्ग और ऊँचे तबके के लोग एक क्षण को रुक कर च्च–च्च करते हैं और मजे से फिर अपनी जिन्दगी में रम जाते हैं, तो क्या यह फासीवाद है? जब इस सबकी सरपरस्ती करनेवाले प्रधानमन्त्री को राजनीतिज्ञ और भविष्य द्रष्टा कह कर उसकी जय–जयकार की जाती है तब क्या हम भरे–पूरे फासीवाद की बुनियाद नहीं रख रहे होते?
उत्पीड़ित और पराजित लोगों का इतिहास बहुत हद तक अनलिखा रह जाता है–यह सच्चाई सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं पर लागू नहीं होती। अगर ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के राजनैतिक रास्ते पर चलना ही हमारा चुना हुआ रास्ता है तो निश्चय ही भारत के दलितों और आदिवासियों को हत्या, आगजनी और बेलगाम कहर बरपा करने का अधिकार है?
रूस में कहा जाता है कि अतीत अनुमान से परे है। भारत में, स्कूली पाठ्य–पुस्तकों के साथ हुई छेड़–छाड़ के अनुभव से हम जानते हैं कि यह बात कितनी सच है। अब सभी 'छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी' बस यही उम्मीद लगाये रखने की हालत में पहुँचा दिये गये हैं कि बाबरी मस्जिद खुदाई में पुरातत्व–विदों को राम मन्दिर का कोई अवशेष नहीं मिलेगा। अगर यह सच भी हो कि भारत की हर मस्जिद के नीचे कोई–न–कोई मन्दिर है तो फिर मन्दिर के नीचे क्या था? शायद किसी और देवी–देवता का कोई और हिन्दू मन्दिर। शायद कोई बौद्ध स्तूप। बहुत करके कोई आदिवासी समाधि। इतिहास सवर्ण हिन्दूवाद से शुरू नहीं हुआ, हुआ था क्या? कितना गहरे हम खोदेंगे? कितना उलटेंगे–पलटेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ मुसलमान जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इस देश का अटूट अंग है, बाहरी और आक्रमणकारी कहे जाते हैं और क्रूरता से निशाना बनाये जाते हैं, जबकि सरकार विकास अनुदान के लिए ठेकों और कॉर्पोरेट सौदों पर उस हुकूमत के साथ करार करने में व्यस्त है जिसने सदियों तक हमें गुलाम बनाये रखा। 1876 से 1902 के बीच, भयंकर अकालों के दौरान लाखों हिन्दुस्तानी भूख से मर गये, जबकि अंग्रेज सरकार राशन और कच्चे माल का निर्यात करके इंग्लैण्ड भेजती रही। ऐतिहासिक तथ्य मरने वालों की संख्या सवा करोड़ से तीन करोड़ के बीच बताते हैं।[30] बदला लेने की राजनीति में इस संख्या की भी तो कोई जगह होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए क्या? या फिर प्रतिशोध का मजा तभी आता है जब उसके शिकार कमजोर और अशक्त हों और आसानी से निशाना बनाये जा सकते हों?
फासीवाद को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी ही कड़ी मेहनत 'निवेश का बेहतर माहौल बनाने' के लिए करनी पड़ती है। क्या दोनों साथ–साथ बेहतर काम करते हैं? ऐतिहासिक रूप से, कॉर्पोरेशनों को फासीवाद से किसी तरह से गुरेज नहीं रहा है। सीमेन्स, आई.जी. फारबेन, बेयर, आईबीएम और फोर्ड ने नाजियों के साथ व्यापार किया था।[31] हमारे पास भी बिलकुल हाल का उदाहरण सीआईआई (कनफेडेरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, भारतीय उद्योग संघ) का है, जिसने 2002 के गुजरात जनसंहार के बाद राज्य सरकार के आगे घुटने टेक दिये थे।[32] जब तक हमारे बाजार खुले है, एक छोटा–सा घरेलू फासीवाद अच्छे सौदे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा।
यह दिलचस्प है कि जिस समय तत्कालीन वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह भारत के बाजार को नव–उदारवाद के लिए तैयार कर रहे थे, लगभग उसी समय लालकृष्ण आडवानी साम्प्रदायिक उन्माद को हवा देते हुए और हमें नव-फासीवाद के लिए तैयार करते हुए अपनी पहली रथ-यात्रा पर निकले हुए थे।[33] दिसम्बर 1992 में उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तहस–नहस कर दिया। 1993 में महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार ने एनरॉन के साथ बिजली खरीद के सौदे पर हस्ताक्षर किये। यह भारत में पहली निजी बिजली परियोजना थी। एनरॉन समझौता विध्वसंक साबित होने के बावजूद भारत में निजीकरण के युग की शुरुआत कर गया।[34] अब जब कांग्रेस चारदीवारी पर बैठ कर रिरिया रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके हाथ से मशाल छीन ली है। सरकार के दोनों हाथ मिल कर अभूतपूर्व जुगलबन्दी कर रहे हैं। एक थोक के भाव देश बेचने में व्यस्त है, जबकि दूसरा ध्यान बँटाने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कर्कश, बेसुरा राग अलाप रहा है। पहली प्रक्रिया की भयावह निर्ममता दूसरी प्रक्रिया के पागलपन में सीधे जा मिलती है।
आर्थिक रूप से भी यह जुगलबन्दी एक कारगर नमूना है। मनमाने निजीकरण से पैदा होनेवाले अकूत मुनाफों (और 'इण्डिया शाइनिंग' की कमाई) का एक हिस्सा हिन्दुत्व की विशाल सेना–आर.एस.एस., विहिप, बजरंग दल और बेशुमार दूसरी खैराती संस्थाओं और ट्रस्टों को मदद पहुँचाता है जो स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवाएँ चलाते हैं। देश भर में इन संगठनों की दसियों हजार शाखाएँ फैली हुई हैं। जिस नफरत का उपदेश ये वहाँ देते हैं, वह पूँजीवादी भूमण्डलीकरण के हाथों निरन्तर बेदखली और दरिद्रता का शिकार लोगों की अनियन्त्रित कुण्ठा से मिल कर गरीबों द्वारा गरीबों के विरुद्ध हिंसा को जन्म देती है। यह इतना कारगर पर्दा है जो सत्ता के तन्त्र को सुरक्षित और चुनौतीरहित बनाये रखता है।
बहरहाल, जनता की हताशा को हिंसा में बदल देना ही हमेशा काफी नहीं होता। 'निवेश का अच्छा माहौल' बनाने के लिए राज्य को अक्सर सीधा हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। हाल के वर्षों में, पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर, जिनमें ज्यादातर आदिवासी थे, कई बार गोलियाँ चलायी हैं। झारखण्ड में नगरनार; मध्यप्रदेश में मेंहदी खेड़ा; गुजरात में उमर गाँव; उड़ीसा में रायगढ़ और चिल्का और केरल में मुतंगा में लोग मारे गये हैं। लोग वन भूमि में अतिक्रमण करने के लिए मारे जाते हैं और उस समय भी जब वे बाँधों, खदान खोदने वालों और इस्पात के कारखानों से वनों की रक्षा कर रहे होते हैं। दमन–उत्पीड़न चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जम्बुद्वीप टापू, बंगाल; मैकंज ग्राम, उड़ीसा। पुलिस द्वारा गोली चलाने की लगभग हर घटना में जिन पर गोली चलायी गयी होती है उन्हें फौरन उग्रवादी करार दे दिया जाता है।]35]
***
जब उत्पीड़ित जन उत्पीड़ित होने से इन्कार कर देते हैं तब उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है और उनके साथ वैसा ही सलूक होता है। आतंक के विरुद्ध युद्ध के इस युग में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 181 देशों ने इस साल मतदान किया। अमरीका तक ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। भारत मतदान से बाहर रहा।[36] मानवाधिकार पर चैतरफा हमले के लिए मंच तैयार किया जा रहा है।
इस हालत में, आम लोग एक अधिकाधिक हिंसक होते राज्य के हमलों का मुकाबला कैसे करें?
अहिंसक सिविल नाफरमानी की जगह सिकुड़ गयी है। अनेक वर्षों तक संघर्ष करने के बाद कई जन प्रतिरोध आन्दोलनों की राह बन्द हो गयी है और वे अब ठीक ही महसूस कर रहे हैं कि दिशा बदलने का वक्त आ गया है। वह दिशा क्या होगी, इस पर गहरे मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हथियारबन्द संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचा है। कश्मीर और पूर्वोत्तर को छोड़ कर, जमीन की विशाल पट्टियाँ, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के पूरे–पूरे जिले उन लोगों के नियन्त्रण में हैं जो इस विचार के हामी हैं।[37] दूसरों ने अधिकाधिक मात्रा में यह मानना शुरू कर दिया है कि उन्हें चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए–व्यवस्था के भीतर घुस कर अन्दर से उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। (क्या यह कश्मीरी अवाम के सामने मौजूद विकल्पों जैसी नहीं है?) याद रखने की बात यह है कि जहाँ दोनों के तरीके मूल रूप से अलग–अलग हैं, वहीं दोनों एक बात पर सहमत हैं कि अगर इसे मोटे शब्दों में कहें तो अब बहुत हो गया। या बास्ता।
भारत में इस समय ऐसी कोई बहस नहीं हो रही, जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका नतीजा, देश के जीवन को बदल कर रख देगा–चाहे बेहतरी की तरफ बदले, चाहे बदतरी की तरफ। अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण–हरेक के लिए।
हथियारबन्द संघर्ष राज्य की ओर से की गयी हिंसा को बड़े पैमाने पर उकसा देता है। कश्मीर और समूचे पूर्वोत्तर राज्यों को इसने जिस दलदल की ओर धकेल दिया है, उसे हमने देख लिया है। तो हम क्या वहीं करें, जो प्रधानमन्त्री की सलाह है कि हमें करना चाहिए? विरोध छोड़ दें और चुनावी राजनीति के अखाड़े में दाखिल हो जायें? रोड शो में शामिल हो जायें? निरर्थक गाली–गलौज के कर्कश आदान–प्रदान में भाग लें, जिसका एकमात्र उद्देश्य उस मिली–भगत और सम्पूर्ण सहमति पर पर्दा डालना है जो तकरार में जुटे इन लोगों के बीच वैसे पहले से ही लगभग पूरी तरह मौजूद है? हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे–परमाणु बम, बड़े बाँध, बाबरी मस्जिद विवाद और निजीकरण–पर बीज कांग्रेस ने बोये और फिर भाजपा ने उसकी घिनौनी फसल काटने के लिए सत्ता सँभाली।
इसका यह मतलब नहीं है कि संसद का कोई महत्व नहीं है और चुनावों को नजरअन्दाज कर देना चाहिए। अलबत्ता, एक फासीवादी प्रवृत्ति वाली खुल्लम–खुल्ला साम्प्रदायिक पार्टी और एक अवसरवादी साम्प्रदायिक पार्टी के बीच सचमुच अन्तर है। निश्चय ही, जो राजनीति खुले तौर पर गर्व के साथ नफरत का प्रचार करती है, उसमें और काँइयेपन से लोगों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति में सचमुच अन्तर है।
लेकिन यह सही है कि एक की विरासत ने ही हमें दूसरी की भयावहता तक पहुँचाया है। इन दोनों ने मिल कर उस वास्तविक विकल्प को क्षरित कर दिया है जो संसदीय लोकतन्त्र में मिलना चाहिए। चुनावों के गिर्द रचा गया उन्माद और मेले–ठेले का माहौल संचार माध्यमों में केन्द्रीय स्थान इसलिए ले लेता है, क्योंकि हर आदमी पक्के तौर पर जानता है कि जीते चाहे जो कोई, यथास्थिति मूल रूप से कतई नहीं बदलने जा रही है। (संसद में जोरदार बहस–मुबाहसे और आवेग–भरे भाषणों के बाद भी पोटा को हटाने की प्राथमिकता किसी पार्टी के चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं बनी। वे सभी यह जानते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत है, इस रूप में या उस रूप में)।[38] चुनाव के दौरान या विपक्ष में रहते हुए वे जो भी कहें, केन्द्र या राज्य की कोई भी सरकार, कोई भी राजनैतिक दल–दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी या हाशिये का–नव–उदारवाद के अश्वमेध के घोड़े को नहीं पकड़ सका है। 'भीतर' से कोई क्रान्तिकारी बदलाव नहीं आयेगा।
व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानती कि चुनावी अखाड़े में उतरना वैकल्पिक राजनीति का रास्ता है। ऐसा किसी किस्म के मध्यवर्गीय नकचढ़ेपन के कारण नहीं–कि 'राजनीति गन्दी चीज है' या 'सभी नेता भ्रष्ट हैं'–बल्कि इसलिए कि मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ कमजोर जगहों से नहीं, बल्कि मजबूत जगहों से लड़ी जानी चाहिए।
नव–उदारवाद और साम्प्रदायिक फासीवाद के दोहरे हमले का निशाना गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय बन रहे हैं। जैसे–जैसे नव–उदारवाद गरीब और अमीर के बीच, 'इण्डिया शाइनिंग' और भारत के बीच खाई को चौड़ा करता जा रहा है, वैसे–वैसे मुख्यधारा की किसी भी राजनैतिक पार्टी के लिए गरीब और अमीर दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का नाटक करना अधिकाधिक हास्यास्पद होता जा रहा है, क्योंकि एक के हितों का प्रतिनिधित्व दूसरे की कीमत पर किया जा सकता है। सम्पन्न भारतीय के नाते मेरे 'हित' (अगर मैं साधने की सोचूँ तो) आन्ध्र प्रदेश के गरीब किसानों के हितों से मुश्किल से ही मेल खायेंगे।
गरीबों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनैतिक पार्टी गरीब पार्टी होगी। उसके पास धन की बहुत कमी होगी। आजकल बिना धन के चुनाव लड़ना सम्भव नहीं है। कुछेक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ताओं को संसद में भेज देना तो दिलचस्प है, लेकिन राजनैतिक रूप से सार्थक नहीं है। यह प्रक्रिया इस लायक नहीं है कि उसमें अपनी सारी उर्जा खपा दी जाए। व्यक्तिगत करिश्मा, व्यक्तित्व की राजनीति क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सकती।
लेकिन गरीब होना कमजोर होना नहीं हैं। गरीबों की ताकत सरकारी इमारतों या अदालती दरवाजों के भीतर नहीं है। वह तो बाहर, खेतों, पहाड़ों, घाटियों, सड़कों और इस देश के विश्वविद्यालयों के परिसरों में है। वहीं बातचीत करनी चाहिए। वहीं लड़ाई छेड़ी जानी चाहिए।
अभी तो ये जगहें दक्षिणपन्थी हिन्दू राजनीति के हवाले कर दी गयी हैं। उनकी राजनीति के बारे में आपके विचार जो भी हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वे इन जगहों पर मौजूद हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे–जैसे राज्य अपनी जिम्मेवारियों से मुँह मोड़ कर स्वास्थ्य, शिक्षा और आवष्यक सार्वजनिक सेवाओं को आर्थिक संसाधन देना बन्द करता जा रहा है, वैसे–वैसे संघ परिवार के सिपाही उन क्षेत्रों में दाखिल होते गये हैं। घातक प्रचार करती अपनी हजारों शाखाओं के साथ–साथ वे स्कूल, हस्पताल, दवाखाने, एम्बुलेंस सेवाएँ, दुर्घटना राहत निकाय भी संचालित करते हैं। वे शक्तिहीनता के बारे में जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि लोगों, खासकर शक्तिहीन लोगों की न सिर्फ रोजमर्रा की, सीधी–साधी व्यावहारिक जरूरतें होती हैं, बल्कि उनकी भावनात्मक, आध्यात्मिक, मनोरंजनपरक आवश्यकताएँ और इच्छाएँ भी होती हैं। उन्होंने ऐसी घिनौनी कुठाली बनायी है जिसमें गुस्सा, हताशा, रोजमर्रा की जिल्लत– और बेहतर भविष्य के सपने–सब एक साथ पसाये जा सकते हैं और खतरनाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इस बीच, परम्परागत मुख्यधारा का वामपन्थ अब भी 'सत्ता हथियाने' के सपने देख रहा है, लेकिन समय की पुकार को सुनने और कदम उठाने के सिलसिले में अजीब कड़ापन और अनिच्छा प्रदर्शित कर रहा है। वह अपनी ही घेरेबन्दी का शिकार हो गया है और पहुँच से बाहर ऐसे बौद्धिक स्थान में सिमट गया है जहाँ प्राचीन बहसें ऐसी आदिकालीन भाषा में चलायी जा रही हैं, जिसे नाममात्र के लोग ही समझ सकते हैं।
संघ परिवार के हमले के सामने चुनौती का थोड़ा–बहुत आभास पेश करने वाली एकमात्र ताकत वो जमीनी प्रतिरोध आन्दोलन हैं, जो छिटपुट तौर पर पूरे देश में चल रहे हैं और 'विकास' के प्रचलित नमूने के कारण हो रही बेदखली और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश आन्दोलन एक–दूसरे से अलग–थलग हैं और 'विदेशी पैसे पानेवाले एजेण्ट' होने के निरन्तर आरोप के बावजूद, उनके पास पैसे या संसाधन नहीं हैं। वे आग से जूझने वाले महान योद्धा हैं। उनकी पीठ दीवार से सटी हुई है; लेकिन उनके कान धरती की धड़कन सुनते हैं; वे जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। अगर वे इकट्ठा हो जायें, अगर उनकी मदद की जाये, तो वे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनकी लड़ाई को, जब भी वह लड़ी जायेगी, आदर्शवादी लड़ाई होना होगा, कठोर विचारधारात्मक नहीं।
ऐसे समय, जब अवसरवाद की तूती बोल रही है, जब उम्मीद दम तोड़ती लग रही है, जब हर चीज रूखी–सूखी सौदेबाजी हो गयी है, हमें सपने देखने का साहस जुटाना होगा। रोमांस पर फिर से दावेदारी करनी होगी। न्याय में, स्वतन्त्रता में और गरिमा में विश्वास का रोमांस। सबके लिए। हमें एकजुट हो कर लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए हमें समझना होगा कि यह दैत्याकार पुरानी मशीन कैसे काम करती है। कौन कीमत चुकाता है, किसे फायदा होता है।
देश भर में छिटपुट चलने वाले और अलग–अलग मुद्दों की लड़ाई अकेले लड़ने वाले अनेक प्रतिरोध आन्दोलनों ने समझ लिया है कि उनकी किस्म की विशेष हित वाली राजनीति, जिसका कभी समय और जगह थी, अब काफी नहीं है। चूँकि अब वे हाशिये पर आ गये हैं, इसलिए अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति से मुँह मोड़ लिया जाय, यह मुनासिब नहीं होगा। लेकिन यह गम्भीर आत्म–निरीक्षण करने की जरूरत की तरफ इशारा करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग जो लोकतन्त्र को फिर से हासिल करना चाहते हैं, वे अपने चाल–चलन और काम करने के तरीके में समतावादी और जनतान्त्रिक हैं। अगर हमारे संघर्ष को उन आदर्शों पर खरा उतरना है तो हमें उन अन्दरूनी नाइन्साफियों को खत्म करना होगा जो हम दूसरों पर ढाते हैं, महिलाओं पर ढाते हैं, बच्चों पर ढाते हैं। मिसाल के लिए जो साम्प्रदायिकता से लड़ रहे हैं, उन्हें आर्थिक अन्याय पर आँख नहीं बन्द करनी चाहिए। जो लोग बड़े बाँध या विकास की परियोजनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें साम्प्रदायिकता से या अपने क्षेत्र में जातीय दमन से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, भले ही तात्कालिक रूप से उन्हें अपनी फौरी मुहिम में कुछ नुकसान उठाना पड़े। अगर तदबीर के तकाजे और मौकापरस्ती हमारी आस्था के आड़े आ–जा रही है, तब हममें और मुख्यधारा के नेताओं में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। अगर हम न्याय चाहते हैं तो यह न्याय और समानता सबके लिए होनी चाहिए, न कि कुछ खास समुदायों के लोगों के लिए, जिनके पास हितों को ले कर कुछ पूर्वाग्रह है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। हमने अहिंसक प्रतिरोध को 'फील गुड' के राजनैतिक अखाड़े में सिकुड़ जाने दिया है, जिसकी सबसे बड़ी सफलता संचार माध्यमों के लिए फोटो खिंचाने के अवसर हैं और सबसे कम सफलता उपेक्षा है।
हमें प्रतिरोध की रणनीति का मूल्यांकन करके उस पर तुरन्त विचार करना होगा, वास्तविक लड़ाइयाँ छेड़नी होंगी और असली नुकसान पहुँचाना होगा। हमें याद रखना है कि दाण्डी मार्च बेहतरीन राजनैतिक नाटक ही नहीं था, वह ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक आधार में सेंध लगाना था।
हमें राजनीति के अर्थ की पुनर्व्याख्या करनी होगी। 'नागरिक समाज' की पहलकदमियों का 'एनजीओकरण' हमें विपरीत दिशा में ले जा रहा है।[39] वह हमें अराजनैतिक बना रहा है। हमें 'फण्ड' और 'चन्दे' का मोहताज बना रहा है। हमें सिविल नाफरमानी के अर्थ की पुनःकल्पना करनी होगी।
शायद हमें जरूरत है लोकसभा के बाहर एक चुनी हुई छाया–संसद की, जिसके समर्थन और अनुमोदन के बगैर संसद आसानी से नहीं चल सकती। ऐसी संसद जो एक जमींदोज नगाड़ा बजाती रहती है, जो समझ और सूचना में साझेदारी करती है (जो सब मुख्यधारा के समाचार–माध्यमों में उत्तरोत्तर अनुपलब्ध हो रहा है)। निडरता से, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हमें इस मशीन के पुर्जों को बेकार बनाना होगा, जो हमें खाये जा रही है।
हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे बोलने के दौरान भी हिंसा का घेरा कसता जा रहा है। हर हाल में बदलाव तो आना ही है। वह खून से सना हुआ भी हो सकता है या खूबसूरती में नहाया हुआ भी। यह हम पर मुनहसिर है।
संदर्भ और टिप्पणियां
1. 14 फरवरी 2003 को आई. जी. खान की हत्या पर, देखें पार्वती मेनन, 'ए मैन ऑफ कम्पैशन,' फ्रंटलाइन (इण्डिया), 29 मार्च–11 अप्रैल, 2003। इण्टरनेट पर उपलब्ध: http://www.frontlineonnet.com/fl2007/stories/20030411400.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।2. हिना कौसर आलम और पी.बालू, 'जे एण्ड के (जम्मू एण्ड कश्मीर) फजेज डीएनए सैम्पल्स टू कवर अप किलिंग्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7 मार्च 2002।
3. देखें कम्यूनलिज्म कॉम्बैट, 'गोधरा,' और वरदराजन द्वारा सम्पादित 'गुजरात' में ज्योति पुनवाणी, 'द कारनेज ऐट गोधरा।'
4. सोमित सेन, 'शूटिंग टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन एनकाउण्टर कॉप्स,' टाइम्स ऑफ इण्डिया, 23 अगस्त 2003।
5. डब्ल्यू चन्द्रकान्त, क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज ऐक्टिविस्ट्स इन दि ऑफिंग?', द हिन्दू, 4 अक्टूबर 2003, जिसमें लिखा है:
पुलिस के प्रतिशोध के डर से अनेक कार्यकर्ता गुप्तवास में चले गये हैं। उनके भय बेबुनियाद नहीं हैं, क्योंकि राज्य की पुलिस मनमाने डंग से मुठभेड़ें करती रही है। जहाँ पुलिस नक्सलवादी हिंसा के आँकड़े अक्सर जारी करती है, वह अपनी हिंसा के शिकार लोगों का जिक्र करने से गुरेज करती है। आन्ध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी ने, जो पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं का लेखा–जोखा रख रही है, 4000 से ज्यादा मौतों की फेहरिस्त पेश की है जिनमें से 2000 पिछले महज आठ वर्षों में की गयी हैं।के.टी. संगमेश्वरन, 'राइट्स ऐक्टिविस्ट्स अलेज गैंगलॉर्ड–कॉप नेक्सस,' द हिन्दू, 22 अक्टूबर 2003।
6. जम्मू कश्मीर कोअलिशन फॉर सिविल सोसाइटी के अध्ययन, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू ऐण्ड कश्मीर बीटविन 1900–2006 (श्रीनगर 2006), में अनुमान प्रकट किया गया है कि 1990 और 2004 के बीच जम्मू और कश्मीर में मरने वालों की असली तादाद 70,000 से अधिक थी, जबकि भारत सरकार ने 1990 से 2005 तक सिर्फ 47,000 मृतकों की सूचना दी। देखें, ऐजाज हुसैन, 'मुस्लिम, हिन्दू प्रोटेस्ट्स इन इण्डियन कश्मीर,' एसोसिएट प्रेस, 1 जुलाई 2008; डेविड रोहडे, 'इण्डिया ऐण्ड कश्मीर सेपेरेटिस्ट्स बिगिन टॉक ऑन एंण्डिंग स्ट्राइफ,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 23 जनवरी 2004, पृ.ए8; डोएचे–प्रेस एजेन्तुर, 'थाउजेण्ड्स मिसिंग, अनमार्क्ड ग्रेव्ज टेल कश्मीर स्टोरी,' 7 अक्टूबर 2003।
7. लापता लोगों के माता–पिता के संगठन (एपीडीपी), श्रीनगर की अप्रकाशित रिपोर्ट।
8. देखें एडवर्ड ल्यूस, 'कश्मीरीज न्यू लीडर प्रॉमिसेज ''हीलिंग टच'', फाइनैन्शियल टाइम्स (लन्दन), 28 अक्टूबर 2002, पृ. 12।
9. रं मार्सेलो, ऐण्टी–टेरेरिज्म लॉ बैक्ड बाई इण्डियाज सुप्रीम कोर्ट, फाइनैन्शियल टाइम्स (लन्दन) 17 दिसम्बर 2003, पृ. 2।
10. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), 'ए प्रिलिमिनेरी फैक्ट फाइण्डिंग ऑन पोटा केसेज इन झारखण्ड,' डेल्ही इण्डिया, 2 मई 2003। इण्टरनेट पर उपलब्ध: http://pucl.org/Topics/Law/2003/poto–jharkhand.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
11. 'पीपुल्स ट्रिब्यून हाइलाइट्स मिसयूज ऑफ पोटा', द हिन्दू, 18 मार्च 2004।
12. 'पीपुल्स ट्रिव्यूनल।' 'ह्यूमन राइट्स वॉच आस्क सेन्टर टू रिपील पोटा' द हिन्दू, 18 मार्च 2004 भी देखें।
13. देखें लीना मिश्रा, '240 पोटा केसेज, ऑल अगेंस्ट माइनॉरिटीज,' टाइम्स ऑफ इण्डिया, 15 सितम्बर 2003 और 'पीपुल्स ट्रिब्युनल हाइलाइट्स मिसयूज ऑफ पोटा,' 18 मार्च 2004। टाइम्स ऑफ इण्डिया ने पेश की गयी गवाही की गलत सूचना दी। जैसा कि प्रेस ट्रस्ट का लेख दर्ज करता है, गुजरात में, 'सूची में एकमात्र गश्ैरमुस्लिम एक सिख है, लिवरसिंह तेजसिंह सिकलीगर, जिसका उल्लेख उसमें सूरत के एक वकील हसमुख ललवाला पर जानलेवा हमला करने के लिए हुआ था और जिसने अप्रैल (2003) में सूरत की पुलिस हिरासत में कथित रूप से फाँसी लगा ली थी।' गुजरात पर देखें, रॉय, 'डेमोक्रेसीः हू इज शी ह्वेन शी इज ऐट होम?' (हिंदी में:लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है)।
14. देखें, पीपल्स ट्रिब्युनल ऑन पोटा ऐण्ड अदर सिक्यूरिटी लेजिसलेशन्ज, द टेरर ऑफ पोटा (नई दिल्ली, इण्डिया, 13–14 मार्च 2004)। इण्टरनेट पर उपलब्ध http://www.sabrang.com/pota.pdf (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
15. 'ए प्रो–पुलिस रिपोर्ट,' द हिन्दू, 20 मार्च 2004। ऐमनेस्टी इण्टरनेशनल, 'इण्डियाः रिपोर्ट ऑफ दी मलिमथ कमिटी रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम: सम कमेंट्स,' 19 सितम्बर 2003 (एएसए 20/025/2003)।
16. 'जे एण्ड के (जम्मू एण्ड कश्मीर) पैनल वॉण्ट्स ड्रेकोनियन लॉज विदड्रॉन,' द हिन्दू, 23 मार्च 2003। साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेन्टर (एसएएचआरडीसी), 'आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स ऐक्ट: ए स्टडी इन नैशनल सिक्यूरिटी टिरिनी,' नवम्बर 1995, http://www.hrdc.net/sahrdc/resources/armed_forces.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
17. 'ग्रोथ ऑफ ए डीमन: जेनिसिस ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स ऐक्ट, 1958' और सम्बन्धित दस्तावेज, मणिपुर अपडेट्स। इण्टरनेट पर उपलब्ध है, देखें, http://www.geocities.com/manipurupdate/December_features_1.htm (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
18. देखें, एडवर्ड ल्यूस, 'मास्टर ऑफ ऐम्बिग्विटी,' फाइनैन्शियल टाइम्स (लन्दन), 3–4 अप्रैल 2004, पृ. 16। 31 मार्च 2007 को चन्द्रशेखर प्रसाद की हत्या। देखें, ऐन्ड्रयू नैश, 'ऐन इलेक्शन ऐट जेएनयू,' हिमाल, दिसम्बर 2003।
19. पी. साइनाथ, 'नियो–लिबरल टेरेरिज्म इन इण्डिया: दी लार्जेस्ट वेव ऑफ सुइसाइड्स इन हिस्ट्री,' काउण्टरपंच, फरवरी 2009। इण्टरनेट पर उपलब्धः http://www.counterpunch.org/sainath02122009.html
20. एन.ए. मजूमदार, एलिमिनेट हंगर नाओ, पॉवर्टी लेटर, बिजनेस लाइन, 8 जनवरी 2003।
21. 'फूडग्रेन एक्सपोर्ट मे स्लो डाउन दिस फिष्ष्स्कल (इयर),' इण्डिया बिजनेस इनसाइट, 2 जून 2003, 'इण्डिया–ऐग्रिकल्चर सेक्टर: पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी,' बिजनेस लाइन, 26 जून 2001, रणजीत देवराज, 'फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेन्स्ट ग्लोबलाइजेशन,' इण्टर प्रेस सर्विस, 25 जनवरी 2001।
22. उत्सा पटनायक, 'फॉलिंग पर कैपिटा अवेलिबिलिटी ऑफ फूडग्रेन्स फॉर ह्यूमन कन्जंप्शन इन द रिफॉर्म्स पीरियड इन इण्डिया,' अखबार, (2 अक्टूबर 2001)। इण्टरनेट पर उपलब्धः http://indowindow.virtualstack.com/akhabar/article.php?article=44category=3&issue=12 (29 मार्च 2009 को देखा गया।) पी. साइनाथ, 'हैव टॉर्नाडो, विल ट्रैवल,' द हिन्दू मैग्जीन, 18 अगस्त 2002। सिल्विया नसर, 'प्रोफइल: द कॉन्शेन्स ऑफ द डिस्मल साइन्स,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 9 जनवरी 1994 पृ. 3-8। मारिया मिश्रा, 'हार्ट ऑफ स्मगनेस: अनलाइक बेल्ज्यिम, ब्रिटेन इज स्टील कम्प्लेसेंटली इगनोरिंग द गोरी क्रुऐलिटीज ऑफ इट्स एम्पायर,' द गार्जियन, (लन्दन) 23 जुलाई 2002, पृ. 15। उत्सा पटनायक, 'ऑन मेजरिंग, ''फैमिन'' डेथ्स: डिफ्रेंट क्राइटीरिया फॉर सोशयलिज्म ऐण्ड कैपिटलिज्म,' अखबार, 6 (नवम्बर–दिसम्बर 1999)। इण्टरनेट पर उपलब्धः http://www.indowindow.com/akhabar/article.php?article= 74&category=8&issue=9 (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
23. अमर्त्य सेन, 'डेवेलपमेन्ट ऐज फ्रीडम' (न्यूयॉर्क: अल्फ्रेड ए, नॉफ, 1999)
24. 'द वेस्टेड इण्डिया,' द स्टेट्समैन (इण्डिया), 17 फरवरी 2001। 'चाइल्डब्लेन,' द स्टेट्समैन (इण्डिया), 24 नवम्बर 2001।
25. उत्सा पटनायक, 'द रिपब्लिक ऑफ हंगर ऐण्ड अदर एसेज,' (गुड़गाँव: थ्री एसेज कलेक्टिव, 2007)।
26. प्रफुल्ल बिदवई, 'इण्डिया एडमिट्स सीरियस अग्रेरियन क्राइसिस,' सेण्ट्रल क्रॉनिकल (भोपाल), 9 अप्रैल 2004।
27. रॉय, पॉवर पोलिटिक्स, द्वितीय संस्करण, पृ. 13।
28. उदाहरण के लिए देखें, रणदीप रमेश, 'बांग्लादेशी राइटर गोज इनटू हाइडिंग', द गार्जियन (लन्दन), 27 नवम्बर 2007, पृ. 25, यह देशनिकाला प्राप्त और 2004 से कलकत्ता में रह रही लेखिका तसलीमा नसरीन के बारे में है, रणदीप रमेश, 'बैण्ड आर्टिस्ट मिसेज डेल्हीज फर्स्ट आर्ट शो,' द गार्जियन (लन्दन), 23 अगस्त 2008, पृ. 22। यह निष्कासित चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के बारे में है, और सोमिनी सेनगुप्ता, 'ऐट ए यूनिवर्सिटी इन इण्डिया, न्यू अटैक्स ऑन ऐन ओल्ड स्टाइल: इरोटिक आर्ट,' न्यूयॉर्क टाइम्स, 19 मई 2007, पृ. B7। यह महाराजा शिवाजीराव विश्वविद्यालय के छात्रों की प्रदर्शनी के बारे में। अरुंधति रॉय, 'तसलीमा नसरीन ऐण्ड ''फ्री स्पीच,''' नई दिल्ली, इण्डिया 13 फरवरी 2008 भी देखें, इण्टरनेट पर उपलब्ध http://www.zmag.org/znet/viewArticle/166646 (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
29. शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने जेम्स डब्ल्यू. लेन की पुस्तक 'शिवाजी: हिन्दू किंग इन इस्लामिक इण्डिया (ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2003) की 'सभी प्रतियों को जलाने का आह्वान' किया। देखें, 'मॉकरी ऑफ द लॉ,' द हिन्दू 3 मई 2007। प्रफुल्ल बिदवई, 'मेक्कार्थी, वेयर आर यू?' फ्रंटलाइन (इण्डिया); 10–23 मई 2003, इसमें विख्यात इतिहासकार रोमिला थापर के खिलाफ चलाये गये अभियान के बारे में लिखा गया है; और अनुपमा कटकम, ''पॉलिटिक्स ऑफ वैण्डलिज्म, फ्रंटलाइन (इण्डिया), 17–30 जनवरी 2004, पुणे स्थित भण्डारकर संस्थान पर हमले के बारे में।
30. देखें, माइक डेविस, लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स: एल निन्यो फैमिन्स ऐण्ड द मेकिंग ऑफ द थर्ड वल्र्ड (न्यूयॉर्क: वर्सो, 2002) 'टेबल पी 1: एस्टिमेटेड फैमिन मोर्टैलिटी,' पृ. 7।
31. दूसरे स्रोतों के अलावा, देखें एडविन ब्लेक, आईबीएम ऐण्ड द होलोकॉस्ट: द स्ट्रैटिजिक अलायन्स बिटवीन नाजी जर्मनी ऐण्ड अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन (न्यूयॉर्क: थ्री रिवर्स प्रेस, 2003)।
32. 'फॉर इण्डिया इनकॉर्पोरेटेड, साइलेंस प्रोटेक्ट्स द बॉटम लाइन, टाइम्स ऑफ इण्डिया, 17 फरवरी 2003। 'सीआईआई अपोलोजाइजेज टू मोदी,' द हिन्दू, 7 मार्च 2003।
33. आडवाणी ने 25 सितम्बर 1990 को सोमनाथ से यात्रा शुरू की थी। 2005 में उन्होंने कहा कि उनकी 15 साल पहले की ऐतिहासिक राम रथ यात्रा तभी पूरी मानी जायेगी जब अयोध्या में मन्दिर बन जायेगा। देखें, विशेष सम्वाददाता, 'यात्रा कम्पलीट ओनली आफ्टर टेम्पल इज बिल्ट, सेज आडवाणी,' द हिन्दू, 26 सितम्बर 2005।
34. देखें रॉय, पावर पॉलिटिक्स, द्वितीय संस्करण, पृ. 35–86।
35. अन्य स्रोतों के साथ, देखें निर्मलांग्शु मुखर्जी, 'ट्रेल ऑफ द टेरर कॉप्स,' जेडनेट, 17 नवम्बर 2008। इण्टरनेट पर उपलब्ध http://www.zmag.org/zspace/nirmalangshumukherji (29 मार्च 2009 को देखा गया)।
36. 22 दिसम्बर 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 'आतंकवाद से लड़ाई में मानवाधिकारों और आधारभूत स्वतन्त्रताओं की रक्षा' के प्रस्ताव से अपने–आप को अलग रखने वाला भारत अकेला देश था।AA/RES/58/187 (अप्रैल 2004)।
37. देखें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, इण्डियाज नक्सलाइट्स मेकिंग एफर्ट्स टू स्प्रेड टू न्यू एरियाज,' बीबीसी वर्ल्ड वाइड मॉनिटरिंग, 4 मई 2003 और 'माओइस्ट कॉल फ्रीजेज झारखण्ड, नेबर्स,' द स्टेट्समैन (इण्डिया), 15 जून 2006।
38. कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने 2004 में पोटा को रद्द कर दिया क्योंकि वह अत्यन्त क्रूर पाया गया था, और कहा कि उसका दुरुपयोग हुआ था और वह उलटे नतीजे देने वाला था, लेकिन फिर सरकार ने 'अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम में संशोधनों के रूप में और भी कड़ा आतंककारी कानून लागू कर दिया। संशोधन 15 दिसम्बर 2008 को संसद में पेश किये गये और अगले ही दिन स्वीकार कर लिये गये। लगभग कोई बहस नहीं हुई। देखें प्रशान्त भूषण, 'टेरेरिज्म: आर स्ट्रौंगर लॉज द आन्सर?' द हिन्दू, 1 जनवरी 2009।
39. देखें अरुंधति रॉय, ऐन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर में 'पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर' (नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स, इण्डिया 2005)। अरुंधति रॉय, 'पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, (न्यूयॉर्क सेवन स्टोरीज प्रेस, 2004) में भी प्रकाशित।




































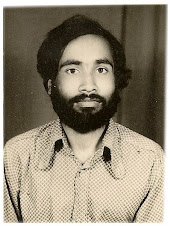

No comments:
Post a Comment