शंकर शरण
जनसत्ता 20 जनवरी, 2012: जयपुर के साहित्य समारोह में सलमान रुश्दी को आने से रोकने की दारुल उलूम की मांग पर हमारे बुद्धिजीवी मौन हैं। सबसे मुखर चुप्पी उनकी है जो हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के पाठ्यक्रम से रामायण पर एके रामानुजन का निबंध हटाए जाने पर 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का जुलूस निकाल रहे थे। वे सभी बुद्धिजीवी मानो सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जब कुछ मुसमिल कट््टरपंथी समूहों के दबाव में रुश्दी का आना रोका जा रहा है। यह दोहरापन किस बात का संकेत है?
संजय गांधी हमारे बुद्धिजीवियों के बारे में बोलते थे, 'उन्हें जितना जोर से ठोकर मारो, उतना वे तुम्हें आदर देंगे'। लगभग चार दशक पहले कही गई यह बात आज भी सच है। केवल इतना बदला है कि तब सरकारी शक्ति वाले ठोकर मारते थे। आज यह काम तरह-तरह के उग्रवादी, आतंकवादी, माओवादी और अंतरराष्ट्रीय ताकत रखने वाले संस्थान करते हैं। जिसमें जितनी ही वास्तविक शक्ति है- दंडित या उपकृत करने की- उसके प्रति हमारे बुद्धिजीवी उतने ही सदय या मौन रहते हैं।
साहित्य की भाषा में चाहें तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास 'राग दरबारी' में पुलिस थाने वाला प्रसंग याद करें। थाने के सिपाहियों को किसी वारदात की जगह पर जाना था, 'और चूंकि वहां मुठभेड़ नहीं होनी थी, इसलिए सिपाहियों ने बंदूकें ले लीं।' यही हमारे अधिकतर बुद्धिजीवियों का चरित्र है। वे केवल सुरक्षित मामलों पर बहादुरी दिखाते हैं। तब वे संजय गांधी पर मौन रहते थे, पर जयप्रकाश नारायण को 'फासिस्ट' कहते थे। आज बेचारे हिंदूवादियों को फासिस्ट कहा जाता है, जबकि हिंसक फतवे जारी करने वालों पर चुप रहने में ही भलाई समझी जाती है।
जिन महानुभावों ने हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले लेख, या हुसेन की आपत्तिजनक पेंटिंगों, दीपा मेहता की अश्लील फिल्मों, अग्निवेश की हिंदू-विरोधी टिप्पणियों आदि के पक्ष में हमेशा तत्परता से जुलूस निकाले या बयान जारी किए- वे सबके सब सलमान रुश्दी पर क्यों मौन हो गए? इस प्रकरण से एक बार फिर रहस्य खुलता है कि क्यों इस्लामी उग्रवादियों की असहिष्णुता की कभी छीछालेदर नहीं होती।
यह सोची-समझी चुप्पी पहली बार नहीं देखी गई। इससे पीछे एक सुनिश्चित पद्धति है, जिसे पहचानने में किसी परिश्रम की जरूरत नहीं। पहले भी तसलीमा नसरीन, अय्यान हिरसी अली, सलमान तासीर, सुब्रह्मण्यम स्वामी आदि की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किसी सेक्युलर-लिबरल बौद्धिक समूह की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। जबकि सलमान रुश्दी ने महज एक उपन्यास लिखा था, सेटेनिक वर्सेज, जिसे बिना पढ़े ही हमारे मुसलिम नेता सैयद शहाबुद्दीन ने प्रतिबंधित करने की मांग कर दी। पूछने पर उलटे उन्होंने ठसक से कहा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब अयातुल्ला खुमैनी ने रुश्दी को मार डालने का फतवा जारी कर दिया, तो वही काफी है। शहाबुद्दीन ने पुस्तक को देखा तक न था, पढ़ना तो दूर की बात!
इस तरह, एक मुसलिम भारतीय की मांग पर वह पुस्तक किसी मुसलिम देश से भी पहले यहां प्रतिबंधित हो गई। उसके लिए नियम-कायदों को भी ताक पर रख दिया गया। तब भी हमारे बुद्धिजीवी मौन रहे थे। एक मुशीर उल हसन ने बस इतना कहा था कि सेटेनिक वर्सेज तो बेकार-सी किताब है, मगर उसे प्रतिबंधित कर देना कोई बात नहीं हुई। बस, इतना कहने भर के कारण उन पर जानलेवा हमला हुआ, और अस्पताल ने किसी तरह उनकी जान बचाई। वैसी घटनाओं से हमारे बुद्धिजीवी अच्छे बच्चों की तरह सही सबक सीखते हैं। क्योंकि रुश्दी विरोधियों के तरीके असंदिग्ध हैं- एक ओर जिस किसी का सिर उतार लेने का बयान जारी करना, और दूसरी ओर अनजान मुसलिम समुदाय को उसे पूरा करने के लिए ललकारना।
ये ललकारने वाले प्राय: स्वयं परले दर्जे के अनपढ़ होते हैं। दिल्ली के एक इमाम साहब लंबे समय तक कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को वह 'सलमान' समझते रहे जिसने सेटेनिक वर्सेज लिखी! मगर वैसे ही नेताओं के दबदबे से हमारे बौद्धिक मुंह चुराए चुप रहते हैं और इस प्रकार उनकी ताकत बढ़ाते हैं।
तब से बाईस वर्ष बीत चुके। पक्षपाती मौन और मतलबी लफ्फाजी के मामले में स्थिति पहले से खराब हुई है। आप इस्लाम संबंधी मांगों, रूढ़ियों, परंपराओं, महानुभावों आदि की प्रशंसा मात्र कर सकते हैं, आलोचना नहीं। जबकि हिंदू विषयों के बारे में स्थिति ठीक उलट है। इनके बारे में प्रशंसा के शब्द कहना लांछित होने को आमंत्रण देना है। तुरंत आप पर 'सांप्रदायिक' या इस या उस संगठन के एजेंट होने के आरोप से मढ़ दिए जाएंगे!
हमारे सेक्युलर-लिबरल प्रवक्ता और आचार्य इस सामुदायिक अंतर को खूब समझते हैं। रुश्दी जैसे मामले में सचमुच का फासिज्म गुर्राता है। जबकि हिंदूवादियों के 'फासिज्म' का विरोध करने में त्योहार-सा आनंद रहता है। मंडी हाउस और तीन मूर्ति के वातानुकूलित सभागारों में समोसे, मिष्ठान्न और कॉफी के साथ 'अभिव्यक्ति के खतरे' उठाना और बात है! उससे रंग-बिरंगे पुरस्कार, देश-विदेश की यात्राएं, सरकारी समितियों में स्थान, ऊंची कुर्सियां और आयोगों में स्थान मिलता है। सत्ताधारियों के साथ हंसने-बतियाने के सुनहरे पल मिलते हैं। धन-कुबेर विदेशी मिशनरी एजेंसियों के निमंत्रण हासिल होते हैं। मांदेर, सीतलवाड, हाशमी, बिदवई आदि किसी से पूछ लीजिए। जबकि रुश्दी के लिए बोलने पर क्या मिलेगा, इसे सब जानते हैं।
इसलिए अभी रुश्दी पर छाई चुप्पी से हमें अपने बुद्धिजीवियों की स्थिति पहचान लेनी चाहिए कि क्यों वे इस्लामी मांगों के आगे 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' को ही हमेशा बलि चढ़ाते हैं। क्योंकि रुश्दी-विरोधी लोग हिंदूवादियों की तरह बयान-बहादुर नहीं, सचमुच के फासिस्ट हैं। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मीडिया, अपनी छवि आदि किसी की परवाह नहीं करते। बल्कि उनकी छवि ही यह है कि वे किसी भी बात पर जिस किसी की जान ले सकते हैं। कहीं भी खून-खराबा, आगजनी कर सकते हैं। इसीलिए उनके फतवों, आह्वानों को सुन कर प्रगल्भ बौद्धिक भी ऐसे निर्विकार रहते हैं, मानो कुछ सुना ही न हो! वे अभेद्य मौन साध लेते हैं। उनके सारे मूल्य खो जाते हैं। फासीवाद के विरुद्ध सारा आक्रोश हवा हो जाता है। क्योंकि रुश्दी जैसे मामलों में सचमुच मुठभेड़ हो सकती है! इसलिए वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का थाना ही छोड़ कर चले जाते हैं। पुन: किसी सुरक्षित मामले पर ही लौट कर सुविधानुसार हथियार उठा लेते हैं।
सच पूछिए, तो इसी रुश्दी विवाद का दूसरा रंग भी हो सकता था। अगर खुमैनी ने सेटेनिक वर्सेज को उपेक्षित कर दिया होता, और किसी हिंदूवादी ने रुश्दी की एक अन्य पुस्तक 'मिडनाइट चिल्ड्रन' पर बखेड़ा किया होता, तो हमारे बुद्धिजीवियों के जलवे ही कुछ और होते। इस पुस्तक में रुश्दी ने कथित रूप से राम-सीता पर कुछ कटाक्ष किए हैं। (हिंदुओं को भी रुश्दी के विरुद्ध भड़काने के लिए दिल्ली के शाही इमाम इसका हमेशा उल्लेख करते थे। तब उन्हें अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं लगती होगी। अब इसकी जरूरत नहीं रही!) अगर नाराजगी इस पुस्तक पर हुई होती, तो उसी रुश्दी का कवच बन कर हमारे सेक्युलर वामपंथ ने अखबारों के पन्ने रंग दिए होते। जैसे, उन्होंने एमएफ हुसेन के लिए धर्म-पूर्वक सदा किया।
उसी रुश्दी के लिए आज उत्साहपूर्वक टीवी चैनलों पर गर्मागर्म बहस चल रही होती, अगर विरोध 'मिडनाइट चिल्ड्रन' पर हुआ होता। पौराणिक शास्त्रों और भारतीय संविधान से लेकर गांधीजी के उद्धरणों से रुश्दी का जम कर बचाव किया जाता। यह काल्पनिक दावा नहीं है।
हम देख चुके हैं कि हुसेन द्वारा हिंदू देवी-देवताओं की भद्दी पेंटिग बनाने पर हुए लोकतांत्रिक, कानूनी विरोध की भी कितनी थोक भर्त्सना की गई। उसी तर्ज पर रुश्दी के लिए भी दोहराया जाता कि लेखकीय स्वतंत्रता कितना बड़ा मूल्य है, भिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता कैसा सामाजिक धर्म है, जिसकी समझ (हिंदू) संप्रदायवादियों को नहीं है, आदि।
इस तरह रुश्दी, तसलीमा, हुसेन, रामानुजन, सुब्रह्मण्यम आदि विविध प्रसंगों पर चुनी हुई चुप्पी और चुने हुए शोर-शराबे का एक सुनिश्चित ढर्रा पहचाना जा सकता है। हुसेन की पेंटिंगों और रामानुजन के लेख पर जैसे तर्क दिए जाते हैं, ठीक वही तर्क तसलीमा और रुश्दी के लिए अमान्य कर दिए जाते हैं। इसमें तथ्य, तर्क, जन-भावना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि किसी भी आधार पर एकसमान रुख नहीं लिया जाता। रुख लिया जाता है यह देख कर कि किस समुदाय की भावना को चोट पहुंची है या किसे रोष हुआ है? अगर किसी ने 'गलत समुदाय' के नेताओं को क्रुद्ध कर दिया हो, तो वह कितना ही बड़ा लेखक, पत्रकार क्यों न हो- हमारे बुद्धिजीवी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते!
यह रवैया स्वयं बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसे अभी रहने दें। पर इस पक्षपाती मौन से हमारे देश में सामाजिक सद्भाव बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसी मुंहदेखी चुप्पी से ही विभाजनकारी तत्त्वों को मौका मिलता है कि वे मजहब या भावना के नाम पर लोगों को बरगलाएं। क्योंकि राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग ने दोहरे पैमाने बना लिए हैं। इस दोहरेपन से किसी समुदाय में अहंकार तो किसी में भेद-भाव झेलने का घाव उभरता है।
आम जनों की दृष्टि उनसे कम पैनी नहीं होती जो सुखदायक सभागारों में अपने चुने हुए मौन या शोर-शराबे के लिए सुविधाजनक दलीलें पेश करते रहते हैं। वे दलीलें किसी को संतुष्ट नहीं करतीं। दलीलें देने वाले भी असलियत जानते हैं। फिर भी स्वार्थी, राजनीतिक कारणों से वही सब दोहरा कर एक-दूसरे को झूठी शाबासी देते हैं। मगर भेदभाव भरी बातें कभी भी सामाजिक सद्भाव नहीं बढ़ा सकतीं।
इसलिए जिन लेखकों, पत्रकारों को सचमुच सामाजिक सद्भाव और देश-हित की चिंता हो, उन्हें इस दोहरेपन का कड़ा विरोध करना चाहिए। आज सब मनुष्यों में समान अधिकार और समान व्यवहार की भावना तीव्र हुई है। अब मजहब, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि किसी भी आधार पर पक्षपात या दुराव पहले से अधिक चोट पहुंचाता है। आम जनों को चतुर दलीलों से कोई राहत नहीं मिलती। जितना अधिकार हुसेन को था, उतना ही रुश्दी को है। अगर इस पर हीला-हवाला किया जाता है तो सामुदायिक दूरी बढ़ती है। इसी प्रक्रिया में मुसलिम जनसमुदाय अपने कठमुल्ले नेताओं का स्थायी बंधक बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा दोषी यहां का सेक्युलर-वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग है। |







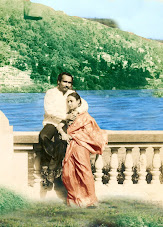












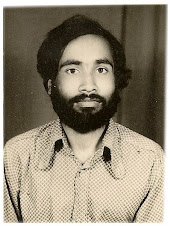

No comments:
Post a Comment