Indian Holocaust My Father`s Life and Time - Four Hundred Twenty Five
Palash Biswas
http://indianholocaustmyfatherslifeandtime.blogspot.com/
Me and Sabita have been considering ourselves as family Members of Shekhar Joshi , the Writer,Rooted in Kausani and KOSI, who Presented Details of Indian Industrial Working Conditions and Working Class! But I missed a Programme in Bharatiya Bhasha Parishad today where Shekhar Joshi recieved Chandrayan Puraskar. I am not well but I had to skip the event for my resrevations against the MARWARI Capitalist Pocket and Class which Dominates the Hindi World of Working Class well known for suffering who may well be identified with Naurangi Lal, a prominent cahracter in Joshi stories! My friend Shailendra belonging to Allahabad attended the function but we did not discuss the event as he knows my opinion. The Parishad director, Vijay Bahadur Singh also knows!
I had stayed with the family at their Home in Allahabad addressed 100, Lookerganj for weeks as I landed in the City right from the Nainital Hills as I wanted to complete my Phd under Dr Manas Mukul Das in Allahabad University .Which eevntually was not to be. Dr Batrohi and Shekahr Pathak disptched me from Nianital and originally I had to stay with Shailesh Matiyani, another Hindi Writer rooted in Almora.But there was no plae available at the home of Matiyaniji and the Joshi family admitted me imediately in their realtions. Izza, Mrs Joshi was very generous. The Chidren Pratul, Snaju and Bunti always have been close to our heart and mind.
In Nainital, we were fans of Gyan Ranjan and Muktibodh in those days. But we were also proud of Matiyani and Joshi.Kapilesh Bhoj belonged to Someshwar and we have many friends in and around Someshwar, Chanauda, Kausani, Bageshwar, Dwarahat and neighbourhood. our Guruji Tara Chandra Tripathi is also from Someshwar and he is writing beautiful memoirs of his village. Someshwar has been best presented in Shekhar Joshi`s KOSI Ke Ghatwar. While Matiyani used the folk in his writing with Kumauni diction used often, Joshi concentrated his theme around Industrial and Urban labour and I must say that he is the best in Hindi as far as I have studied.
चंद्रयान पुरस्कार कथाकार शेखर जोशी को
कोलकाता। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार शेखर जोशी को मानिक दफ्तरी ज्ञानविभा ट्रस्ट के प्रथम चंद्रयान पुरस्कार-2010 से नवाजा जायेगा। प्रबंध न्यासी धनराज दफ्तरी ने यह जानकारी देते हुए बताया की नयी कहानी में सामाजिक सरोकारों का प्रतिबद्ध स्वर जोड़ने वाले श्री शेखर जोशी को पुरस्कार स्वरुप 31,000 रुपये की राशि भेंट की जाएगी। पुरस्कार समोराह कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद् में रविवार 18 जुलाई को आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता भारतीय भाषा परिषद् के निदेशक डॉ. विजय बहादुर सिंह करेंगे जबकि प्रसिद्द विद्वान डाक्टर शिवकुमार मिश्र, अहमदाबाद मुख्य वक्ता बतौर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सञ्चालन पूर्व सांसद सरला महेश्वरी करेंगी।
को मानिक दफ्तरी ज्ञानविभा ट्रस्ट के प्रथम चंद्रयान पुरस्कार-2010 से नवाजा जायेगा। प्रबंध न्यासी धनराज दफ्तरी ने यह जानकारी देते हुए बताया की नयी कहानी में सामाजिक सरोकारों का प्रतिबद्ध स्वर जोड़ने वाले श्री शेखर जोशी को पुरस्कार स्वरुप 31,000 रुपये की राशि भेंट की जाएगी। पुरस्कार समोराह कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद् में रविवार 18 जुलाई को आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता भारतीय भाषा परिषद् के निदेशक डॉ. विजय बहादुर सिंह करेंगे जबकि प्रसिद्द विद्वान डाक्टर शिवकुमार मिश्र, अहमदाबाद मुख्य वक्ता बतौर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सञ्चालन पूर्व सांसद सरला महेश्वरी करेंगी।
इस अवसर पर शेखर जोशी की प्रचलित कहानी दाज्यू का पाठ पत्रकार प्रकाश चंडालिया करेंगे। सितम्बर 1932 में अल्मोड़ा जनपद के ओजिया गाँव में जन्मे शेखर जोशी की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुयी। कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले जोशी हिंदी के सुपरिचित कथाकार हैं। उन्हें उ.प्र. हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार-1987, साहित्य भूषण-1995 पहल सम्मान-1997 से सम्मानित किया जा चुका है।
जोशी की कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं के अलावा अँगरेज़ी, चेक, रूसी, पोलिश और जापानी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। कुछ कहानियों का मंचन और दाज्यू नमक कहानी पर बाल फ़िल्म सोसायटी द्वारा फ़िल्म का निर्माण किया गया है।
जोशी की प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं- कोशी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियाँ और एक पेड़ की याद। दाज्यू, कोशी का घटवार, बदबू, मेंटल जैसी कहानियों ने न सिर्फ़ शेखर जोशी के प्रशसकों की लम्बी ज़मात खडी की बल्कि नयी कहानी की पहचान को भी अपने तरीक़े से प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाक़ों की ग़रीबी, कठिन जीवन संघर्ष, उत्पीडन, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीद्दी से भरे औद्योगिक मज़दूरों के हालात, शहरी-कस्बाई और निम्नवर्ग के सामाजिक-नैतिक संकट, धर्म और जाती में जुडी घटक रूढ़ियाँ- ये सभी उनकी कहानियों का विषय रहे हैं।
कोलकाता से डॉ. अभिज्ञात की रपट
ये निहायत ही रचना विरोधी समय है

: कथाकार शेखर जोशी चंद्रयान पुरस्कार से सम्मानित : कोलकाता में आयोजित एक समारोह में प्रख्यात आलोचक व जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में साहित्य, कला व संस्कृति गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है।
इस दौर में आदमी की रचनाधर्मिता चुनौतियों के बीच खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये निहायत ही रचना विरोधी समय है और साहित्य अभिव्यक्ति का इतना स्खलन पहले कभी नहीं हुआ था। मिश्र ने कहा कि यदि समय का चरित्र यही रहा तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिन में आदमी कितना आदमी रह जाएगा। देखा जाए तो आज आदमी का भी क्षरण हो रहा है और बाजारतंत्र हम पर हावी है। शिवकुमार मिश्र ने ये बातें भारतीय भाषा परिषद् सभागार में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा। इस मौके पर मानिक दफ्तरी ज्ञानविभा ट्रस्ट कि ओर से हिंदी के प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी को चंद्रयान पुरस्कार - २०१० से नवाजा गया। संस्था के ट्रस्टी धनराज दफ्तरी ने पुरस्कार स्वरुप जोशी को ३१ हजार रुपये की राशि,शॉल व श्रीफल प्रदान किए।
शिवकुमार मिश्र ने इस मौके पर शेखर जोशी के सम्मान में कहा कि जोशी नई कहानी आन्दोलन के उन सदस्यों में से हैं, जिन्होंने नई कहानी को गाँव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जोशी ने औद्योगिक मजदूरों पर कहानी लिखी, जिसमे यथार्थ के सही संदर्भों को उन्होंने उभारा। यही नहीं, जोशी ने नई कहानी के तमाम दुसरे लोगों के साथ इसे व्यापक आयाम भी दिया था।
मिश्र ने कहा कि गांव को आधार बनाने के बावजूद शेखर जोशी 'मैला आँचल' के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की तरह आंचलिकता के शिकार नहीं बने। उन्होंने कहा कि जोशी की कहानी यथार्थ की व्याख्या करते हुए जरूरी व गैर -जरूरी के बीच के फर्क को स्पष्ट करती है। दूसरी ओर रेणु की त्रासदी यह रही कि आंचलिकता की रौ में उनसे जरूरी चीज़ें पीछे छूट गयी। मिश्र के मुताबिक 'मैला आँचल' में आंचलिकता के रूपवाद को मनोरंजन के रूप में पेश किया गया है। इसी संदर्भ में मिश्र ने शेखर जोशी की 'दाज्यू', 'कोसी का घटवार', 'नौरंगी बीमार है' आदि कई कहानियों का जिक्र करते हुए कहा कि जोशी कि कहानियों में यथार्थ का चित्रण हमें मिलता है।
इस मौके पर शेखर जोशी ने सम्मान के लिए आयोजक संस्था के प्रति आभार जताते हुए कहा -मैंने बहुत नहीं लिखा और यदि मैं सलीके से लिख पाया और आपकी नजर उस पर पड़ी है तो उसके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं, बल्कि उनका उन पात्रों का है जो पाठकों के मन में रच बस गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान वामपंथी राजनीति की तरफ उनका रुझान होने लगा। जोशी ने कहा -जो थोडा बहुत मैं सलीके से लिख पढ़ पाया उसका श्रेय इलाहाबाद के साहित्यिक माहौल को है। इस मौके पर नई पीढ़ी के लेखकों से निवेदन करते हुए जोशी ने कहा- जो हम लिखें, उसमे कुछ प्रकाश हो, हताशा न हो। उनके मुताबिक साहित्य से हमें कुछ ऐसा भी मिलना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय भाषा परिषद् के निदेशक विजय बहादुर सिंह ने लेखक को साहित्य का "डेंजर ज़ोन" करार देते हुए कहा कि वह (लेखक) हमें बताता है कि समाज कितने हद तक खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि संकट के समय समाज में हमेशा आता रहता है। देखा जाए तो कभी-कभी वेदना भी समाज को जागृत करती है। सिंह ने कहा कि कवि व वेदना हमें बताते है कि समाज में अभी बहुत कुछ जीवित है। उनके मुताबिक बैचैनी व उकताहट से ही साहित्य बचा रहता है।
कार्यक्रम का संचालन पत्रकार प्रकाश चंडालिया ने किया। उन्होंने शेखर जोशी की कहानी "दाज्यू" का पाठ भी किया। समारोह में डा. कृष्ण बिहारी मिश्र, आलोचक व कथाकार विमल वर्मा, श्रीहर्ष, अरुण महेश्वरी, डा. अमरनाथ, आयोजक संस्था के ट्रस्ट अध्यक्ष प्रीतम दफ्तरी व नन्दलाल टांटिया आदि भी मौजूद थे। धनराज दफ्तरी ने धन्यवाद दिया।
http://bhadas4media.com/book-story/5802-shekhar-joshi.html© गद्य कोश हिन्दी साहित्य को इंटरनैट पर एक जगह लाने का एक अव्यावसायिक और सामूहिक प्रयास है। इस वैबसाइट पर संकलित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार रचनाकार या अन्य वैध कॉपीराइट धारक के पास सुरक्षित हैं। इसलिये गद्य कोश में संकलित कोई भी रचना या अन्य सामग्री किसी भी तरह के सार्वजनिक लाइसेंस (जैसे कि GFDL) के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है।
© All the material collected in Gadya Kosh is copyrighted by their respective writers and are, therefore, not available under any public, free or general licenses including GFDL
गद्य कोश आपको कैसा लगा? इस कोश के संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी हो तो हमें अवश्य बतायें। अपनी टिप्पणी लिखने के लिये यहाँ क्लिक करें
गद्य कोश टीम से सम्पर्क करने के लिये आप gadyakosh AT gmail DOT com पर ईमेल भेज सकते हैं।
आपके विचार जान कर हमें प्रसन्नता होगी।
कहानियाँ
- नौरंगी बीमार है / शेखर जोशी
- प्रथम साक्षात्कार / शेखर जोशी
- बिरादरी / शेखर जोशी
- गाइड / शेखर जोशी
- निर्णय / शेखर जोशी
- नेकलेस / शेखर जोशी
- क़िस्सागो / शेखर जोशी
- संवादहीन / शेखर जोशी
- विडुवा / शेखर जोशी
- आशीर्वचन / शेखर जोशी
- बच्चे का सपना / शेखर जोशी
- कोसी का घटवार / शेखर जोशी
- साथ के लोग / शेखर जोशी
- दाज्यू / शेखर जोशी
- हलवाहा / शेखर जोशी
शब्दचित्र
http://gadyakosh.org/gk/index.php?title=%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%B0_%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80
Shekhar Joshi
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
| Shekhar Joshi | |
| Born | September , 1939(1939-09-00) Ojiyagaon, Almora, |
| Occupation | Novelist, Poet |
| Notable work(s) | Dajyu,Kosi Ka Ghatwar |
Shekhar Joshi (शेखरजोशी) (Born. September, 1939) is a renowned Hindi author, who is equally famous for being his hallmark insight into the culture, traditions and lifestyles of people of Uttarakhand, as late Shailesh Matiyani, together they created a composite image of ethos of Kumaon for the rest of nation. His most known works are Dajyu (Big Brother) and Kosi Ka Ghatwar (The Miller of Kosi).
Contents[hide] |
[edit] Biography
Shekhar Joshi was born in September, 1939, in village Ojiyagaon, in Almora district of Uttarakhand in a farmers family and received his early education at Dehradun and Ajmer, and thereafter while studying in Intermediate he got selected for Defense Institute of E.M.I. and went to work within the Defense establishment from 1955 to 1986, when he resigned to take up full-time writing.
His acclaimed story, Dajyu (Big Brother in Kumaoni) has also been made into a Children's film by Children Film Society of India. Kosi Ka Ghatwar (The Miller of Kosi) and many other stories have been translated into English, Russian, Czech, Polish and Japanese [1]
[edit] Bibliography
- 10 Pratinidhi Kahaniyan by Shekhar Joshi (Hindi), ISBN 04217-5286.
- Naurangi Bimar Hai by Shekhar Joshi, Rajkamal Publications.
- The Miller of Kosi by Shekhar Joshi. Modern Hindi Short Stories; translated by Jai Ratan. New Delhi, Srishti, 2003, Chapter 5. ISBN 81-88575-18-6. [2]
- Bachche Ka Sapna by Shekhar Joshi, 2004 (Hindi). ISBN 8186209441.
- Dangri Vale by Shekhar Joshi, 1998.
- Mera Pahar by Shekhar Joshi. [3]
- "Big Brother" by Shekhar Joshi (Dajyu), Andersen 1994. [4]
[edit] References
- ^ Profile www.abhivyakti-hindi.org.
- ^ Chapter 5
- ^ Shekhar Joshi Books Hindi Book Centre.
- ^ List of writers from the Indian subcontinent
[edit] External links
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Shekhar_Joshi"
Categories: 1939 births | Hindi-language writers | Indian writers | Literature of Uttarakhand | Kumaon | People from Almora | People from Uttarakhand | Living people | Literature of Kumaon
शेखर जोशी संकलित कहानियां
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सारांश: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंशबीसवीं शताब्दी के छठे दशक को आज भी हिन्दी कहानी के उर्वर दौर के रूप में याद किया जाता है। वह दौर 'नई कहानी' आन्दोलन का दौर था। शेखर जोशी (1932) उस दौर के सशक्त प्रतिनिधि हैं, जो निरन्तर अपनी कथा-रचना को ताजा और जनसंवेदी बनाए रखने में तत्पर और सावधान रहे हैं। इस तत्परता और सावधानी के क्रम में उनमें कहीं बड़बोलापन या मान्यता छीन लाने की व्याकुलता नहीं दिखी। न तो उनके आचरण में, न ही कथा-कौशल में। एकदम से धीर, थिर चित से चली जा रही कहानियां उनके यहां सरल किस्सागोई के साथ उपलब्ध हैं। उनकी कहानियों से परिचय करते हुए कथाकार का यह निर्लिप्त संकोच दिखता रहता है—कहानियों के भीतर भी और कथाकार के रूप में कहानियों के बाहर भी। उनकी कहानियों में वस्तुपरकता के स्तर पर कथाकार के सामाजिक सरोकार, और प्रस्तुति के स्तर पर पाठकों की समझ पर आस्था भरी हुई है। अपनी कहानियों को झटका देकर महत्त्वपूर्ण बनाने और पाठकों की आंखों में चमक भरने की कोशिश से कथाकार को सदा परहेज रहा है। शेखर जोशी : संकलित कहानियां उनकी ऐसी ही छब्बीस कहानियों का संकलन है। चयन कथाकार ने स्वयं किया है। भूमिकाबीती सदी का छठा दशक हिन्दी कहानी के अत्यंत उर्वर दौर के रूप में आज भी याद किया जाता है। अगर हिन्दी के दो दर्जन प्रतिनिधि कहानीकारों की फेहरिस्त बनाई जाए, तो उसमें एक तिहाई से ज्यादा नाम वही होंगे जिनकी ताजगी-भरी रचना-दृष्टि ने पचास के दशक में कहानी की विधा को साहित्य की परिधि से उठा कर केंद्र में प्रतिष्ठित कर दिया। उस उभार को अविलम्ब 'नई कहानी' की संज्ञा के साथ एक आंदोलन का दरजा हासिल हो गया था। दबे पांव चलने वाली कहानियां के सृजेता शेखर जोशी उसी उभार के एक सशक्त प्रतिनिधि हैं। उनका शुमार 'नई कहानी' में सामाजिक सरोकारों का प्रतिबद्ध स्वर जोड़ने वाले कहानीकारों में होता है। 'दाज्यू', 'कोसी का घटवार', 'बदबू', 'मेंटल' जैसी उनकी कहानियों ने न सिर्फ उनके मुरीदों और प्रशंसकों की एक बड़ी जमात तैयार की है, बल्कि 'नई कहानी' की पहचान को भी अपने तरीके से प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों की गरीबी और कठिन जीवन-संघर्ष; उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीदी से भरे औद्योगिक मजदूर वर्ग के हालात; शहरी-कस्बाई निम्न और मध्यम मध्यवर्ग के आर्थिक-सामाजिक-नैतिक संकट; धर्म और जाति से जुड़ी घातक रूढ़ियाँ; दैनन्दिन स्थितियों का वर्गीय चरित्र-ये सभी उनकी कहानियों का विषय बनते रहे हैं। 'मूड' को आधार बनाने की बजाय घटनाओं और ठोस ब्यौरों में किस्सा कहने वाले शेखर जोशी ने इन सभी विषयों को लेकर ऐसी कहानियां लिखी हैं, जो एक ओर विचार-केंद्रित कृतिम गढ़ंत से मुक्त हैं, तो दूसरी और 'अनुभव की प्रामाणिकता' और 'भोगा हुआ यथार्थ' के संकरे आशय से भी। इस लिहाज से वे अमरकांत और भीष्म साहनी की तरह घातक अतियों से कहानी का बचाव करने वाले रचनाकार हैं। शेखर जोशी हिन्दी के सबसे मितभाषी कथाकारों में से हैं। उनका कुल लेखन बमुश्किल दो स्वस्थ जिल्दों के लायक है। उपन्यास की जमीन पर उन्होंने खाता ही नहीं खोला और कहानियों की संख्या भी शतक से काफी पीछे है—संकलित और असंकलित, सब मिलाकर साठ-पैंसठ के करीब। ये तो शुक्र है कि साहित्य की दुनिया में क्रिकेट का तर्क नहीं चलता, वरना वे इस दुनिया से कब के निकाल बाहर किए जाते ! लेखन का अल्प-परिणाम शेखर जी की मितभाषित का शायद एक और गौरतलब पहलू है। वे वाचक के रूप में अपनी कहानियों के भीतर और कहानीकार के रूप में कहानियों के बाहर भी अधिक नहीं बोलते। यह संकोच उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की पहचान का महत्त्वपूर्ण घटक है...उनकी विशिष्ट पहचान बनने के रास्ते में शायद सबसे बड़ी बाधा भी। मधुरेश जैसे वरिष्ठ कथा-आलोचक को 'उनके कृतित्व में किसी किस्म की रचनात्मक छलांग का अभाव' दिखलाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि 'उनके आगे न तो रचनात्मक स्तर पर ही कभी कोई बड़ी चुनौतियां रहीं और न ही अपने सारे वैचारिक आग्रहों के बावजूद संघर्ष और विचार के ऐसे सतेज और प्रखर मुद्दे रहे जो रचनात्मकता में एक अनोखी चमक पैदा करते हैं (नयी कहानी : पुनर्विचार, प्रथम संस्करण: 1999, नेशनल पब्लिसिंग हाउस, नयी दिल्ली, पृ. 178), तो इसका एक बड़ा कारण शेखर जोशी का कम बोलनेवाला और दावेदारी के स्तर पर एक तरह का दब्बूपन बरतनेवाला कथाकार व्यक्तित्व है—ऐसा कथाकार व्यक्तित्व, जो अपने अदृश्य रहने को ही सबसे बड़ा मूल्य मानता है और इसके लिए जो कुछ जरूरी जान पड़े, करता है। मसलन—जिन स्थलों पर सामान्यतः दूसरे लेखकों को ज्यादा शब्दों, ब्यौरों, इशारों, बलाघातों की जरूरत महसूस होती है, वहां से बगैर किसी विशेष ताम-झाम के गुजर जाना; कथा-स्थितियों के अर्थगर्भत्व और स्मृद्धि को समझने/सराहने के लिए पाठक को कोई 'सर्फेस टेंशन', 'धक्का' या 'सुराग' न देना; वाचक की मुद्रा में एक सादगी और साधारणता को बज़िद बनाए रखना, इत्यादि। ऐसे में 'बदबू' 'मेंटल', 'बच्चे का सपना', 'नौरंगी बीमार है', 'समर्पण', 'निर्णायक', 'गलता लोहा', 'हलवाहा' जैसी कहानियों के होते हुए भी किसी को 'रचनात्मकता में एक अनोखी चमक पैदा' करनेवाले 'संघर्ष और विचार के सतेज और प्रखर मुद्दों' का अभाव उनमें दिखलाई दे, तो क्या हैरत !.....वस्तुतः शेखर जोशी की कहानियों का निर्वाह प्रकटतः कलात्मक होने के बजाय उनकी प्रस्तुति की मुद्रा में कोई गहरी बात करने की दावेदारी है। ये कम बोलने और आहिस्ता बोलनेवाली कहानियां हैं—ऐसी कहानियां जो अपने पाठक का सम्मान करती हैं, ज्यादा समझा कर उसकी समझ एवं संवेदनशीलता के प्रति अविश्वास प्रकट नहीं करती, साथ ही, 'दिखनेवाली' कलात्मकता से अछूती हैं, जो कि अंतर्वस्तु की गुणवत्ता के प्रति लेखक के पुख्ता आत्मविश्वास का सूचक है। शेखर जोशी की कई कहानियों को इन बातों के उदाहरण की तरह पढ़ा जा सकता है। फिलहाल इस संग्रह में संकलित एक कहानी 'समर्पण' को लें ! यहां लेखक ने प्रतीक-केन्द्रित सामाजिक संघर्ष की गतिकी को जिस तरह से चिह्नित किया है, वह असाधारण है। यज्ञोपवीत-धारण के लिए चलनेवाले अभियान की पूरी प्रक्रिया, उसकी शक्तियां और सीमाएं तथा विचारधारात्मक वर्चस्व की टिकाऊ बनावट—इन सबको एक कहानी में समेटना कोई साधारण बात नहीं ! पर शेखर जोशी का यह 'समेटना' इतना असहनीय है कि कहानी की असाधारणता उसमें छुप-सी जाती है और उसे इकहरे तरीके से पढ़ना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो जाता है कि लेखक की कथन-भंगिमा उस इकहरे पठन को कहीं से हतोत्साहित नहीं करती। पूरी कहानी प्रतीक पर केंद्रित संघर्ष (नीची जातियों द्वारा जनेऊ-धारण) के उभार और उतार का बयान है और इस सिलसिले में वह प्रतीक-केंद्रित संघर्ष की शक्तियों को विलक्षण तरीके से रेखांकित करने के साथ-साथ उसकी भयावह सीमाओं को भी सामने लाती है। एक आदर्श संतुलन के साथ वह इस बात को चिह्नित करती है कि अगर सामाजिक प्रतीकों की लड़ाई ठोस उत्पादन-संबंधों से जुड़ी लड़ाई का हमकदम या हिस्सा बन कर नहीं आती, तो अपनी पूरी नैतिक शक्ति के बावजूद वह कमोबेस ऐसे ही ट्रैजिक-कॉमिक अंत को प्राप्त होने के लिए अभिशप्त है। 'सेवक जी की अमृतवाणी मन को संतोष दे गई थी, पर तन को संतोष नहीं दे पाई।' और इसी चीज ने उस व्यापक जागृति की रीढ़ तोड़ कर रख दी, जिसे देख 'पर-पौरुख पर निर्भर दीवान वंश के कीर्तिस्तंभ की नींव' मालिक लोगों को हिलती प्रतीत होने लगी थी। कितनी बड़ी विडंबना है कि मालिक लोगों के बगैर कुछ किए उनकी यह शंका 'धीरे-धीरे स्वतः ही निर्मूल सिद्ध होने लगी !' अंततः भेदभाव के जिस प्रतीक को अपने शरीर पर धारण कर शिल्पकारों-हलवाहों ने उसका भेदभावमूलक प्रतीकार्थ नष्ट करना चाहा था, उसे अपने ही हाथों उतार फेंका। 'गलता लोहा', 'बच्चे का सपना', 'निर्णायक' आदि कहानियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। गल कर एक नया आकार लेनेवाले धातु की तरह जातिगत पहचान का स्थान वर्गीय पहचान ले रही है, इस कथ्य को बहुत महीन तरीके से सामने लाती है 'गलता लोहा ' कहानी। जातिवादी एकजुटता के छद्म का शिकार बना मेधावी ब्राह्मण कुमार अपने लोहार सहपाठी के साथ जो वर्गीय एकजुटता महसूस करता है, और उसका व्यक्तित्व-विकास जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के जिस सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है, वह कहानी के केंद्र में होने के बावजूद जरा भी मुखर नहीं है। उसे अमुखर बनाए रखने का सूक्ष्म कला-विवेक यदि शेखर जोशी में न होता, तो शायद कहानी का कथ्य ज्यादा व्यापक स्तर पर 'सुना' जाता। इसलिए यह कहना गलत न होगा कि 'गलता लोहा' अपने कला-विवेक की ही बलि चढ़ गई। वैसे शेखर जोशी की कई दूसरी कहानियों की तरह ही यह कहानी भी किसी 'दिखनेवाली' कला से प्रायः अछूती है—प्रकट रूप में लगभग कलाविहीन। पूर्वदीप्ति एक बहुप्रयुक्त तकनीक को छोड़ दें तो कलायुक्तियों का सचेत उपयोग बिल्कुल दिखलाई नहीं पड़ता। नाटकीय शैली यानी दृश्यात्मक प्रविधि बहुत कम अंशों में है; पूरी कहानी पर घटनाओं की पिछली श्रृंखला बताते जाने की शैली यानी परिदृश्यात्मक प्रविधि हावी है। मतलब यह कि कलात्मक निर्वाह के अभाव की शिकायत बड़ी आसानी से की जा सकती है, अगर आप कला को उसके दृश्यमान उपादानों से ही पहचानते हों, तो। पर यदि आप कथात्मक विधाओं के अंदर ऊंची आवाज में न बोलने को एक महत्त्वपूर्ण कला मानते हैं, तो वह 'गलता लोहा' में है। यहां स्थितियों के मध्य संबंध को रेखांकित करते हुए लेखक बहुत बारीक रेखाओं का उपयोग करता है और कहीं कमजोर निगाहों से ये रेखाएं ओझल न रह जाएं, इस डर से उनकी बारीकी के साथ कोई समझौता नहीं करता। यहां तक कि शीर्षक जिस प्रतीकार्थ को अपने में समेटे हुए है, उसकी ओर भी कोई इशारा स्पष्ट तौर पर कहानी के भीतर मौजूद नहीं है। उसे कहानी के मर्म के साथ जोड़ कर पढ़ने, या उसी की रोशनी में कहानी का मर्म निर्धारित करने का पूरा दारोमदार पाठक पर है। पाठक से मर्मज्ञता की मांग करनेवाले इस निर्वाह को अगर हम कलात्मक न मानें, तो निश्चित रूप से पच्चिकारियों को ही कला का एकमात्र नमूना मानना पड़ेगा। वस्तुतः शेखर जोशी की कहानियां बड़ी मजबूती से कला और सौंदर्य की गैररूपवादी धारणा पर टिकी हुई हैं। उनके कलात्मक सौंदर्य की सत्ता अंतर्वस्तु के ऐतिहासिक, सामाजिक और नौतिक संदर्भ से परे नहीं है। 'सिनारियो' में वृत्तचित्र बनानेवाला युवक, रवि एक पहाड़ी गांव में पहुंचा है। सूर्यास्त के समय सिंदूरी आभा से नहाया हुआ हिमालय का हिम-विस्तार देख वह मंत्र-मुग्ध हो जाता है। हिमालय की इसी शोभा को पर्दे पर जीवंत करने के लिए वह पहाड़ों में आया है। कमेंट्री, पार्श्व-संगीत, कालिदास से लेकर पंत तक की काव्य-संपदा का उपयोग—इन सब पर उसने खासा अनुसंधान और चिंतन कर रखा है। जिस घर में वह ठहरा है, वहां प्रारूपिक पहाड़ी दरिद्रता के बीच एक बूढ़ी आमां और उसकी बारह-तेरह साल की पोती रहती है। रात को सोने के बाद सुबह-सुबह पता चलता है कि चीड़ के कोयले में दबी आग चूल्हे में बची नहीं रह पाई है और माचिस रखना महंगा पड़ता है, इसलिए चाय बनाने के लिए आग का इंतजाम करने की समस्या है। थोड़ी देर बाद रवि देखता है कि आमां की पोती, सरुली एक पीतल की कलछुल लिए एक पगडंडी के रास्ते कहीं जा रही है। फिर उसी रास्ते वह कलछुल में आग लिए लौटती दिखलाई पड़ती है। घर के पास पहुंचते-पहुंचते अचानक किसी वजह से वह अपना संतुलन खो बैठती है और दूर के बड़े मकान से मांग कर लाए गए अंगारे तुषार भीगी धरती पर बिखर जाते हैं। लगभग बुझ चले अंगारों को जल्दी-जल्दी उठाकर वह कलछुल में रखती है और उन्हें फूंकती हुई घर की ओर भागती है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गुसांई का मन चिलम में भी नहीं लगा। मिहल की छाँह में उठकर वह फिर एक बार घट (पनचक्की) के अंदर गया। अभी खप्पर में एक-चौथाई से भी अधिक गेहूँ शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उलटा-पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते-आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झाँककर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी हैं, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस्स-खस्स की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेशद्वार बहुत कम ऊंचा था, खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बांहों पर आटे की एक हलकी सफेद पर्त बैठ गई थी।
खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, "जा, स्साला! सुबह से अब तक दस पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात!" बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम-निशान ही नहीं। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान-रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी-नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही हैं। छोटे नाले-गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे हैं गुसाईं का यह घट। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लू घोड़े की चाल को मात देती हैं। |
२
छप्प छप्प छप्प पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाईं पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सूराख-निकास हो, तो बंद कर दे। एक बूँद पानी भी बाहर न जाए। बूँद-बूँद की कीमत है इन दिनों। प्राय: आधा फर्लांग चलकर वह बाँध पर पहुँचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी-घास लेकर उसने बाँध में एक-दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे-किनारे चलकर घट पर आ गया।
अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहारकर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा-बहुत गेहूँ शेष था। वह उठकर बाहर आया।
दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाईं ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, "हैं हो! यहाँ लंबर देर में आएगा। दो दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेदसिंह के घट में देख लो।"
उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊँचे स्वर में पुकारकर वह बोला,"जरूरी है, जी! पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे?"
गुसाईं होंठों-ही-होठों में मुस्कराया, स्साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूँ! कुछ कम ऊँची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, "यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है, जी! तुम ऊपर चले जाओ!"
वह आदमी लौट गया।
मिहल की छाँव में बैठकर गुसाईं ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़-गुड़ करता धुआँ उड़ाता रहा
खस्सर-खस्सर चक्की का पाट चल रहा था।
किट-किट-किट-किट खप्पर से दाने गिरानेवाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी।
छिच्छर-छिच्छर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी। और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती-पाथरों के बीच में टखने-टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप! कहीं चिरैया भी नहीं बोलती। किसी प्राणी का प्रिय-अप्रिय स्वर नहीं।
सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाईं सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच्च पड़े पिसान के थैलों को देखकर। दो-चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता।
कभी-कभी गुसाईं को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी-भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही। जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते-बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का, जिसका घर-द्वार नहीं, बीबी-बच्चे नहीं, खाने-पीने का ठिकाना नहीं।
घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाईं ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था। पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते-करते गुसाईं ने हुक्के की नली से मुँह हटाया। उसके होठों में बाएँ कोने पर हलकी-सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाईं सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवालदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती।
ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवालदार धरमसिंह आया था, लॉन्ड्री की धुली, नोकदार, क्रीजवाली पैंट! वैसी ही पैंट पहनने की महत्त्वाकांक्षा लेकर गुसाईं फौज में गया था। पर फौज से लौटा, तो पैंट के साथ-साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया।
पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबद्ध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात
कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी के क्रेस्ट वाली, काली, किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर, फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल-लीव पर घर आया, तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर-उधर फैल गई थी। बच्चे-बूढ़े, सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस्स। बिस्तर की नई, एकदम साफ, जगमग, लाल-नीली धारियोंवाली दरी आँगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आँगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे-बूढ़े, सभी आए थे। सिर्फ चना-गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाईं को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाईं की आँखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थीं, वह वहाँ नहीं थी।
नाला पार के अपने गाँव से भैंस के कट्या को खोजने के बहाने दूसरे दिन लछमा आई थी। पर गुसाईं उस दिन उससे मिल न सका। गाँव के छोकरे ही गुसाईं की जान को बवाल हो गए थे। बुढ्ढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाईं को देखकर सोबनियाँ का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन-रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट-बीड़ी या गपशप के लोभ में।
एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लछमा को पात-पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गाँव की सीमा से बहुत दूर, काफल के पेड़ के नीचे गुसाईं के घुटने पर सर रखकर, लेटी-लेटी लछमा काफल खा रही थी। पके, गदराए, गहरे लाल-लाल काफल। खेल-खेल में काफलों की छीना-झपटी करते गुसाईं ने लछमा की मुठ्ठी भींच दी थी। टप-टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लछमा ने कहा था, "इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाँह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी।" वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हँस दी थी।
पुरानी बात - क्या कहा था गुसाईं ने, याद नहीं पड़ता त़ेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूँगा, मेरी सुवा! या कुछ ऐसा ही।
पर लछमा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी - पहाड़ी पार के रमुवाँ ने, जो तुरी-निसाण लेकर उसे ब्याहने आया था?
"जिसके आगे-पीछे भाई-बहिन नहीं, माई-बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखनेवाले को छोकरी कैसे दे दें हम?" लछमा के बाप ने कहा था।
उसका मन जानने के लिए गुसाईं ने टेढ़े-तिरछे बात चलवाई थी।
उसी साल मंगसिर की एक ठंडी, उदास शाम को गुसाईं की यूनिट के सिपाही किसनसिंह ने क्वार्टर-मास्टर स्टोर के सामने खड़े-खड़े उससे कहा था, "हमारे गाँव के रामसिंह ने ज़िद की, तभी छुट्टियाँ बढ़ानी पड़ीं। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है, यार! शक्ल-सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा! बड़ी हँसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गाँव के नजदीक की ही है। लछमा-लछमा कुछ ऐसा ही नाम है।"
गुसांई को याद नहीं पड़ता, कौन-सा बहाना बनाकर वह किसनसिंह के पास से चला आया था, रम-डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेनेवाला गुसाईं उस दिन पेशी करवाई थी - मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते-सोचते गुसाईं बुदबुदाया, "स्साल एडजुटेन्ट!"
गुसाईं सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से बिदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लछमा से मिला था।
"गंगनाथज्यू की कसम, जैसा तुम कहोगे, मैं वैसा ही करूँगी!" आँखों में आँसू भरकर लछमा ने कहा था।
वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लछमा से भेंट होगी, तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी-देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज़ करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ, वह कभी फल-फूल नहीं पाया। पर लछमा से कब भेंट होगी, यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी-साथी नौकरी-चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गाँव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लछमा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता।
जितने दिन नौकरी रही, वह पलटकर अपने गाँव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वालंटियरी ट्रांसफर लेनेवालों की लिस्ट में नायक गुसांईसिंह का नाम ऊपर आता रहा - लगातार पंद्रह साल तक।
पिछले बैसाख में ही वह गाँव लौटा, पंद्रह साल बाद, रिज़र्व में आने पर। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लछमा का हठ उसे अकेला बना गया।
आज इस अकेलेपन में कोई होता, जिसे गुसाईं अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता! शब्द-शब्द, अक्षर-अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने
पर नदी किनारे यह तपती रेत, पनचक्की की खटर-पटर और मिहल की छाया में ठंड़ी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाईं। और चारों ओर अन्य कोई नहीं। एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान -
एकाएक गुसाईं का ध्यान टूटा।
सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाईं ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने, काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहाँ तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला-चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुँची थी।
चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गुसाईं घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्नवाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उलटा कर दिया। किट-किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी-जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्छर-छिच्छर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ऊपरवाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का-धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाईं ने सुना अपनी पीठ के पीछे, घट के द्वार पर, इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, "कब बारी आएगी, जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है।"
सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाईं को उसका स्वर परिचित-सा लगा। चौंककर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाईं उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर-उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियाँ किट-किट बोल रही थीं और उसी गति के साथ गुसाईं को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था।
घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाईं के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध-सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना।
उसने दुबारा वे ही शब्द दुहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाईं का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उलटे पाँव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती।
३स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय-विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी।
गुसाईं झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश-सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक-दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुँह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी, जो उसका मुँह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुँच चुकी थी। गुसाईं के अंतर में तीव्र उथल-पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया, लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, "लछमा!"
घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाईं ने स्वस्थ होकर पुन: पुकारा, "लछमा!"
लछमा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे, यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था। परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्कीवाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दुबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, "मुझे पुकार रहे हैं, जी?
गुसाईं ने संयत स्वर में कहा, "हाँ, ले आ, हो जाएगा।"
लछमा क्षण-भर रूकी और फिर घट की ओर लौट आई।
अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाईं व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाँह में चला गया।
लछमा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आँचल के कोर से मुँह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुँह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर-उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाईं बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाँह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी।
गुसाईं की उदारता के कारण ऋणी-सी होकर ही जैसे उसने निकट आते-आते कहा, "तुम्हारे बाल-बच्चे जीते रहें, घटवारजी! बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने! ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता।"
अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाईं ने मन-ही-मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल-पुथल कुछ कम हो गई। लछमा उसकी ओर देखे, इससे पूर्व ही उसने कहा, "जीते रहे तेरे बाल-बच्चे लछमा! मायके कब आई?"
गुसाईं ने अंतर में घुमड़ती आँधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया, जैसे वह भी अन्य दस आदमियों की तरह लछमा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो।
दाड़िम की छाया में पात-पतेल झाड़कर बैठते लछमा ने शंकित दृष्टि से गुसाईं की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल-प्लावित होकर बहने लगती, तो भी लछमा को इतना आश्चर्य न होता, जितना अपने स्थान से केवल चार कदम की दूरी पर गुसाईं को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आँखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है, वह उसका पूर्व-परिचित गुसाईं ही है।
"तुम?" जाने लछमा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए।
"हाँ, पिछले साल पल्टन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया।" गुसाईं ने ही पूछा, "बाल-बच्चे ठीक हैं?"
आँखें जमीन पर टिकाए, गरदन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। ज़मीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लछमा उसकी पंखुड़ियों को एक-एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाईं पतली सींक लेकर आग को कुरेदता रहा।
बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाईं ने पूछा, "तू अभी और कितने दिन मायके ठहरनेवाली है?"
अब लछमा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप्-टप्-टप्, वह सर नीचा किए आँसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ-साथ उसके उठते-गिरते कंधों को गुसाईं देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे।
इतनी देर बाद सहसा गुसाईं का ध्यान लछमा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ (सुहाग-चिह्न) नहीं था। हतप्रभ-सा गुसाईं उसे देखता रहा। अपनी व्यावहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुँझलाहट हो रही थी।
आज अचानक लछमा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया, जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल-मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाईं की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लछमा आँसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी, "जिसका भगवान नहीं होता, उसका कोई नहीं होता। जेठ-जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बाँधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता।"
"यहाँ काका-काकी के साथ रह रही हो?" गुसाईं ने पूछा।
"मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता, जी! बाबा की जायदाद पर उनकी आँखें लगी हैं, सोचते हैं, कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ-साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना-देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो-ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का काँटा बनकर नहीं रहूँगी।"
गुसाईं ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की। केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता-भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकार लछमा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाईं सोचने लगा, पंद्रह-सोलह साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते, समय का यह अंतराल लछमा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा, उस छाप के नीचे वह आज भी पंद्रह वर्ष पहले की लछमा को देख रहा है।
"कितनी तेज धूप है, इस साल!" लछमा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लछमा ने यह बात जान-बूझकर कही हो।
और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया, जहाँ लछमा बैठी थी। दाड़िम की फैली-फैली अधढँकीं डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरन न जाने कब से लछमा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डूबा रही थी। गुसाईं एकटक उसे देखता रहा।
"दोपहर तो बीत चुकी होगी," लछमा ने प्रश्न किया तो गुसाईं का ध्यान टूटा, "हाँ, अब तो दो बजनेवाले होंगे," उसने कहा, "उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में।" कहता हुआ गुसाईं एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया।
"नहीं, यहीं ठीक है," कहकर लछमा ने गुसाईं की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था।
घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी-जल्दी लछमा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया।
धीरे-धीरे चलकर गुसाईं गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर-भरकर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अलमुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया।
आस-पास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते-जाते लछमा की ओर मुँह कर कह गया, "चाय का टैम भी हो रहा है। पानी उबल जाय, तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है।"
लछमा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जानेवाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही।
सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते-लौटते गुसाईं को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा, एक छ:-सात वर्ष का बच्चा लछमा की देह से सटकर बैठा हुआ है।
बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लछमा ने कहा, "इस छोकरे को घड़ी-भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। जाने कैसे पूछता-खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है।"
गुसांई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार-बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुँझलाकर लछमा ने उसे झिड़क दिया, "चुप रह! अभी लौटकर घर जाएँगे, इतनी-सी देर में क्यों मरा जा रहा है?"
चाय के पानी में दूध डालकर गुसाईं फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा-बैठा उसे गूँथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में दो-एक बर्तन और ले लिए।
लछमा ने बटलोई में दूध-चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक अलमुनियमके मैसटिन में गुसाईं ने चाय डालकर आपस में बाट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियाँ बनाने का उपक्रम करने लगा।
हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लछमा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाईं ना न कह सका। वह खड़ा-खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल-गोल डिबिया-सरीखी रोटियाँ चूल्हे में खिलने लगीं। वर्षों बाद गुसाईं ने ऐसी रोटियाँ देखी थीं, जो अनिश्चित आकार की फौज़ी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थीं। आटे की लोई बनाते समय लछमा के छोटे-छोटे हाथ बड़ी तेज़ी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते, तो खन्-खन् का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकरानेवाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाईं ने आज पहली बार अनुभव किया।
किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन-डिब्बों को उठाता-रखता रहा।
वह लौटकर आया, तो लछमा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी।
गुसाईं ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाईं को देखे जा रहा था। लछमा ने आग्रह के स्वर में कहा, "चाय के साथ खानी हों, तो खा लो। फिर ठंडी हो जाएँगी।"
"मैं तो अपने टैम से ही खाऊँगा। यह तो बच्चे के लिए" स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो।
"न-न, जी! वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियाँ बनाकर रख आई थी," अत्यंत संकोच के साथ लछमा ने आपत्ति प्रकट कर दी।
"ऐं, यों ही कहती है। कहाँ रखी थीं रोटियाँ घर में?" बच्चे ने रूआँसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढ़ीला पड़ गया था।
"चुप!" आँखें तरेरकर लछमा ने उसे डाँट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी, इस कारण लज्जा से उसका मुँह आरक्त हो उठा।
"बच्चा है, भूख लग आई होगी, डाँटने से क्या फायदा?" गुसाईं ने बच्चे का पक्ष लेकर दो रोटियाँ उसकी ओर बढ़ा दीं। परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी माँ की ओर देख लेता था।
गुसाईं के बार-बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियाँ लेने में संकोच करता रहा, तो लछमा ने उसे झिड़क दिया, "मर! अब ले क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा, वहीं अपने लच्छन दिखाएगा!"
इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दें, गुसाईं ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी-भरी आँखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा, और गुसाईं कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा।
इस छोटे-से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव-सा आ गया था, जिसे गुसाईं और लछमा दोनों ही अनुभव कर रहे थे।
स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते-खाते गुसाईं ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कराकर कहा, "लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है।"
लछमा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाईं हो-होकर खोखली हँसी हँस रहा था।
"कुछ साग-सब्ज़ी होती, तो बेचारा एक-आधी रोटी और खा लेता।" गुसाईं ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की।
"ऐसी ही खाने-पीनेवाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? दो दिन से घर में तेल-नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊँगी कुछ सौदा।"
हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाईं ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, "लछमा!"
लछमा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाईं ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, "ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनीआर्डर आया था।"
"नहीं-नहीं, जी! काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी। यह तो बात चली थी, तो मैंने कहा," कहकर लछमा ने सहायता लेने से इन्कार कर दिया।
गुसाईं को लछमा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, "दु:ख-तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया, तो बेकार है! स्साला! कितना कमाया, कितना फूँका हमने इस जिंदगी में। है कोई हिसाब! पर क्या फायदा! किसी के काम नहीं आया। इसमें अहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है स्साला! किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी!"
परन्तु गुसाईं के इस तर्क के बावजूद भी लछमा अड़ी रही, बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, "गंगनाथ दाहिने रहें, तो भले-बुरे दिन निभ ही जाते हैं, जी! पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो, कम हो जाय। अपने-पराये प्रेम से हँस-बोल दें, तो वह बहुत है दिन काटने के लिए।"
गुसाईं ने गौर से लछमा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिह्न शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बँधकर शांत हो चुका था।
रुपया लेने के लिए लछमा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। पर गहरे असंतोष के कारण बुझा-बुझा-सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लछमा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी-जल्दी अपने निजी आटे के टीन से दो-ढ़ाई सेर के करीब आटा निकालकर लछमा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक साँस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बाँध की ओर देखने लगा। ऊपर बाँध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था।
बाँध की ओर जाने से पहले वह एक बार लछमा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठककर खड़ा हो गया, मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक-अटककर वह बोला, "लछमा।"
लछमा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाईं को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है, इस बात की आशंका से उसके मुँह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाईं ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, "कभी चार पैसे जुड़ जाएँ, तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल-चूक की माफी माँग लेना। पूत-परिवारवालों को देवी-देवता के कोप से बचा रहना चाहिए।" लछमा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका।
पानी तोड़नेवाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामनेवाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लछमा अपने बच्चे के साथ धीरे-धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुँचने तक टकटकी बाँधे देखता रहा।
घट के अंदर काठ की चिड़ियाँ अब भी किट-किट आवाज कर रही थीं, चक्की का पाट खिस्सर-खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, निस्तब्ध!
Saturday, 2 February 2008
'Dajyu' by Shekhar Joshi
I'm 11 years old and I'm about to enter seventh grade. Thanks to our school's policy to not teach the regular NCERT English readers that contain rather boring lessons but to teach the text books issued by the Oxford University Press, we have very cute, small and interesting reads as our English texts. The contributing authors included big names like Hemingway, Doyle, Satyajit Ray, R.K. Narayan, Oscar Wilde and much to my delight; Isaac Asimov and Roald Dahl. Short stories by Asimov and 'Charlie and the Chocolate factory' by Dahl continue to be my favourites. However the story that impressed me most was one by an unknown Indian author, Shekhar Joshi. I rarely had emotional overflows reading a story…stories amazed me, puzzled me, made me think, made me sympathize but rarely gave me tears. And the ones that gave me those, remained etched in my memory. One by which I was deeply moved was 'Charlie and the Chocolate factory' about which I shall write someday later. The other one was from my very own English text of seventh grade, the one by Shekhar Joshi. I still have the text with me and it has travelled with me across the state and I must've read the story more than fifty times. I post it here and hope that some of you will share the same emotions that I had when I read the story as a kid of 11.Big Brother
SHEKHAR JOSHI
Jagdish Babu saw him for the first time, at the small café with the large signboard, in the market place. He had a fair complexion, sparkling eyes, golden brown hair, and an unusual smooth liveliness in his movements-like a drop water sliding along the leaf of a lotus. From the alertness in his eyes, one would guess his age at only nine or ten, and that's what it was.When Jagsish Babu, puffing on a half-lit cigarette, entered the café, the boy was removing some plates from a table. By the time Jagdish Babu had seated himself at a corner table, the boy was already standing in front of him. He looked as though he'd been waiting for hours for him-for a person to sit in that seat.
The boy said nothing. He did bow slightly, to show respect, and then just smiled. Receiving the order for a cup of tea, he smiled again, went off, and then returned with the tea in the twinkling of an eye.
Jagdish Babu had come from a distant region and was alone. In the hustle and bustle of the market place, in the clamour of the café, everything seemed unrelated to himself. Maybe after living here for a while and growing used to it, he'd start feeling some intimacy in the surroundings. But today the place seemed alien. Then he began remembering nostalgically the people of his village region, the region, the school and the college boys there, the café in the nearby town.
'Tea, Sha'b!'
Jagdish Babu flicked the ash from the cigarette. In the boy's pronunciation of 'Sahab', he seemed something which he had been missing. He started to follow up the speculation-'What's your name?'
'Madan.'
'Very well, Madan! Where are you from?'
'I'm from the hills, Babuji.'
'There are hundreds of hill places-Abu, Darjeeling, Mussorie, Simla, Almora. Which hills is your village in?'
'Almora, Sha'b,' he said with a smile, 'Almora.'
'Which village in Almora?' he persisted.
The boy hesitated. Perhaps embarrassed by the strange name of the village, he answered evasively- 'Oh it's far away, Sha'b. It must be fifteen or twenty miles from Almora.'
'But it still must have a name,' Jagdish Babu insisted.
'Dotyalgaon', he answered shyly.
The expression of loneliness vanished from Jagdish Babu's face. When he smiled and told Madan he was from a neighbouring village, the boy almost dropped his tray with delight. He stood there, speechless and dazed, as though trying to recall his past.
The past-village …. high mountains … a stream … mother …. Father ….. older sister ….. younger sister …. big brother.
Whose shadow was it that Madan saw in the form of Jagdish Babu? Mother? - No. Father? - No. Elder or younger sister? - No. Big brother? - Yes, Dajyu!
Within a few days, the gap of unfamiliarity between Madan and Jagdish Babu had disappeared. As soon as the gentleman sat down, Madan would call out-'Greetings, Dajyu!' 'Dajyu, it's very cold today.' 'Dajyu, will it snow here too?' 'Dajyu, you didn't eat much yesterday.'
Then from some direction would come a cry of 'Boy!' Madan would be there even before the echo of the call could be heard.
'Anything for you, Dajyu?' he would call out repeating the word 'Dajyu' with eagerness and affection of a mother embracing her son after a long separation.
After some time, Jagdish Babu's loneliness disappeared. Now, not only the market-place and the café, but the city itself seemed like home to him.
'Madan! Come here.'
'Coming, Dajyu!'
This repetition of the word 'Dajyu' aroused the burgeois temperament in Jagdish Babu. The thin thread of intimacy could not stand the strong pull of ego.
'Shall I bring tea, Dajyu?'
'No tea. But what's this "Dajyu, Dajyu" you keep shouting all the time? Have you no respect for a person's prestige?'
Jagdish Babu flushed with anger, had no control over his words. Nor did he stop to wonder whether Madan could know the meaning of the word 'prestige'. But Madan, even with no explanation, had understood everything. Could one who had braved an understanding of the world at such a tender age fail to understand one, unimportant word?
Having made the excuse of a head ache to the manager, Madan sat in a small room head between his knees, and sobbed. In his situation far from home, his display of intimacy towards Jagdish Babu had been perfectly natural. But now, for the first time in a foreign place, he felt as though someone had pulled him from the lap of his mother, from the arms of his father, and from the protection of his sister.
Madan returned to his work as before.
The next day, heading for the café, Jagdish Babu suddenly met a childhood friend, Hemant. Reaching the café, Jagdish Babu beckoned to Madan. But he sensed that the boy was trying to remain at a distance. On the second call, Madan finally came over.
Today that smile was not on his face, nor did he say, 'What can I bring, Dajyu?'
Jagdish Babu himself had to speak up- 'Two teas, two omlettes.'
Even then instead of replying, 'Right away, Dajyu', he said, 'Right away, Sha'b', and then left as though the man were a stranger.
'Perhaps a hill boy?' Hemant speculated.
'Yes,' muttered Jagdish Babu and changed the subject.
Madan had brought the tea.
'What's your name?' Hemant asked, trying to be friendly. For a few moments silence engulfed the table. Jagdish Babu's lowered eyes were centered on the cup of tea.
Memories swam before Madan's eyes-Jagdish Babu asking him his name like this one day … then, 'Dajyu, you didn't eat much yesterday' … and one day, 'You pay no attention to anyone's prestige …'
Jagdish Babu raised his eyes and saw that Madan seemed about to erupt like a volcano.
'What's your name?' Hemant repeated.
'Sha'b they call me "boy", he said quickly and walked away.
'A real idiot,' Hemant remarked, taking a sip of tea. 'He can't even remember his own name'.
Posted by g3Mo at 00:13
http://aeiohyou.blogspot.com/2008/02/dajyu-by-shekhar-joshi.html
एकाकी देवदारु: शेखर जोशी

विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जाना आम बात है। कभी हमने सोचा कि वह पेड़ किसी का संगी-साथी और आत्मीय भी हो सकता है। वर्षों बाद कथाकार शेखर जोशी अपने गांव गए तो बचपन के संगी देवदारु को न देखकर उनके मन में ऐसी टीस उठी, मानों कोई आत्मीय बिछड़ गया हो-
हिमालय के आंगन का वन-प्रांतर! और उस सघन हरियाली के बीच खड़ा वह अकेला देवदारु! खूब सुंदर, छरहरा और सुदीर्घ! सहस्रों लंबी-लंबी बांहें पसारे हुए। तीखी अंगुलियां और कलाइयों में काठ के कत्थई फूल पहने हुए। ऐसा था हमारा दारुवृक्ष- एकाकी देवदारु! हमारी भाषा के आत्मीय संबोधन में 'एकलु द्यार!'
वृक्ष और भी कई थे। कोई नाटे, झब्बरदार। कोई घने, सुगठित और विस्तृत। कोई दीन-हीन मरभुखे, सूखे-ठूंठ से। बांज, फयांट, चीड़, बुरांश और पांगर के असंख्य पेड़। समस्त वनप्रांतर इस वनस्पति परिवार से भरा-पुरा रहता था- वर्ष-वर्ष भर, बारहों मास, छहों ऋतुओं में।
देवदारु के वृक्ष भी कम नहीं थे। समीप ही पूरा अरण्य 'दारु-वणि' के नाम से प्रख्यात था। हजारों-हजार पेड़ पलटन के सिपाहियों की मुद्रा में खड़े हुए। कभी 'सावधान' की मुद्रा में देवमूर्ति से शांत और स्थिर तो कभी हवा-वातास चलने पर सूंसाट-भूंभाट करते साक्षात् शिव के रूप में तांडवरत। लेकिन हमारे 'एकाकी देवदारु' की बात ही और थी। वह हमारा साथी था, हमारा मार्गदर्शक था। 'दारुवणि' जहां समाप्त हो जाती, वहां से प्राय: फर्लांग भर दूर, सड़क के मोड़ पर झाड़ी-झुरमुटों के बीच वह अकेला अवधूत-सा खड़ा रहता था। जैसे, कोई साधु एक टांग पर तपस्या में मग्न हो।
सुबह-सुबह पूरब में सूर्य भटकोट की पहाड़ी के पार आकाश में एक-दो हाथ ऊपर पहुंचते तो उसका प्रकाश पर्वत शिखरों के ऊपर-ऊपर सब ओर पहुंच जाता था। एकाकी दारु के शीर्ष में प्रात: का घाम केसर के टीके से अभिषेक कर देता। रात से ही पाटी में कालिख लगा, उसे घोंट-घाट, कमेट की दावात, कलम और बस्ता तैयार कर हम लोग सुबह झटपट कलेवा कर अपने प्राइमरी स्कूल के पंडितजी के डर से निकलते। गांव भर के बच्चे जुटने में थोड़ा समय लग ही जाता था और कभी-कभार किसी अनखने-लाड़ले के रोने-धाने, मान-मनौवल में ही किंचित विलम्ब हो जाता तो मन में धुकुर-पुकुर लग जाती कि अब पंडितजी अपनी बेंत चमकाएंगे। आजकल की तरह तब घर-घर में न रेडियो था, न घड़ी। पहाड़ की चोटी के कोने-कोने में घाम उतर आया तो सुबह होने की प्रतीति हो जाती थी। ऐसे क्षणों में स्कूल के रास्ते में हमारी भेंट होती थी 'एकाकी दारु' से। वही हमको बता देता था कि अब 'हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए' प्रार्थना शुरू हो गई होगी। कि अब गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर मास्टर साहब कक्षा में आ गए होंगे।
'एकाकी दारु' के माथे पर केसर का नन्हा टीका देखकर हम निश्चिंत हो जाते थे कि अब ठीक समय पर प्रार्थना में पहुंच जाएंगे। यदि बालिश्त भर घाम की पीली पगड़ी बंध गई तो मन में धुकुर-पुकुर होने लगती थी और हम पैथल की घाटी के उतार में बेतहाश दौड़ लगा देते थे और यदि किसी दिन दुर्भाग्य से सफेद धूप का हाथ भर चौड़ा दुशाला एकाकी दारु के कंधे में लिपट जाता था तो हमारे पांव न स्कूल की ओर बढ़ पाते थे, न घर की ओर लौट पाते थे। किसी कारण घर से स्कूल की और प्रस्थान करते हुए हम मन ही मन 'एकाकी दारु' से मनौतियां मनाते कि वह केसर का टीका लगाए हमें मिले।
सांझ को स्कूल से लौटते समय चीड़ के ठीठों को ठोर मारते, हिसालू और किलमौड़े के जंगली फलों को बीनते-चखते, पेड़ों के खोखल में चिडिय़ों के घोंसलों को तलाशते, थके-मांदे 'दारुवणि' की चढ़ाई पार कर जब हम 'एकाकी दारु' की छाया में पहुंचते तो एक पड़ाव अनिवार्य हो जाता था। कोई-कोई साथी उसकी नीचे तक झुकी हुई बांहों में लेट कर झूलने लगता। कोई उसकी पत्तियों के ढेर पर फिसलने का आनंद लेता। सुबह शाम का ऐसा संगी था हमारा 'एकाकी दारु'।
वर्षा बाद मैं उसी मार्ग से गांव लौट रहा था। जंगलात की बटिया अब मोटर सड़क बन गई है। परंतु जिस समय उस मोड़ पर सड़क को चौड़ा करने के लिए निर्माण विभाग वाले एकाकी दारु को काट रहे होंगे, रस्सियां लगा कर उसकी जड़-मूल को निकालने का षडय़ंत्र रच रहे होंगे, उस समय शायद किसी ने उन्हें यह न बताया होगा कि यह स्कूली बच्चों का साथी 'एकाकी दारुÓ है, इसे मत काटो, इसे मत उखाड़ों, अपनी सड़क को चार हाथ आगे सरका लो। शायद सड़क बनवाने वाले उस साहब ने कभी बचपन में पेड़-पौधों से समय नहीं पूछा होगा, उनकी बांहों पर बैठकर झूलने का सुख नहीं लिया होगा और सुबह की धूप के उस केसरिया टीके, पीली पगड़ी और सफेद दुशाले की कल्पना भी नहीं की होगी।
अब वहां सिर्फ एक सुनसान मोड़ है और कुछ भी नहीं।
शेखर जोशी की कविताएं
कारखाना
अभी आठ की घंटी बजते
भूखा शिशु सा चीख उठा था
मिल का सायरन!
और सड़क पर उसे मनाने
नर्स सरीखी दौड़ पड़ी थी
श्रमिक जनों की पांत
यंत्रवत, यंत्रवेग से।
वहीं गेट पर बड़े रौब से
घूम रहा है फोरमैन भी
कल्लू की वह सूखी काया
शीश नवाती उसे यंत्रवत
आवश्यक है यह अभिवादन
सविनय हो या अभिनय केवल
क्योंकि यंत्रक्रम से चलता श्रम
गुरुयंत्रों की रगड़-ज्वाल से
तप जाएं न यंत्र लघुत्तम
है विनय-चाटुता तैल अत्युत्तम।
मुजफ्फरनगर 94*
जुलूस से लौटकर आई वह औरत
माचिस मांगने गई है पड़ौसन के पास।
दरवाजे पर खड़ी-खड़ी
बतिया रही हैं दोनों
नहीं सुनाई देती उनकी आवाज
नहीं स्पष्ट होता आशय
पर लगता है
चूल्हे-चौके से हटकर
कुछ और ही मुद्दा है बातों का।
फटी आंखों, रोम-रोम उद्वेलित है श्रोता
न जाने क्या-क्या कह रही हैं :
नाचती अंगुलियां
तनी हुई भंवें
जलती आंखें
और मटियाये कपड़ों की गंध
न जाने क्या कुछ कह रहे हैं
चेहरे के दाग
फड़कते नथुने
सूखे आंसुओं के निशान
आहत मर्म
और रौंदी हुई देह।
नहीं सुनाई देती उनकी आवाज
नहीं स्पष्ट होता आशय
दरवाजे पर खड़ी-खड़ी
बतियाती हैं दोनों।
माचिस लेने गई थी औरत
आग दे आई है।
(*सन्दर्भ : उत्तराखंड राज्य आंदोलन)
धानरोपाई
आज हमारे खेतों में रोपाई थी धानों की
घर में
बड़ी सुबह से हलचल मची रही काम-काज की।
खेतों में
हुड़के की थापों पर गीतों की वरषा बरसी।
मूंगे-मोती की मालाओं से सजी
कामदारिनों ने लहंगों में फेंटे मारे
आंचल से कमर कसी
नाकशीर्ष से लेकर माथे तक
रोली का टीका सजा लिया।
आषाढ़ी बादल से बैलों के जोड़े
उतरे खेतों पर
धरती की परतें खोलीं
भीगी पूंछों से हलवाहों का अभिषेक किया।
सिंचित खेतों में
विवरों से अन्नचोर चूहे निकले
मेढ़ों पर बैठे बच्चों ने किलकारी मारी
दौड़-भंूक कर झबरा पस्त हुआ।
बेहन की कालीनों से उठकर
शिशु पादप सीढ़ी-दर-सीढ़ी फैले।
विस्थापन की पीड़ा से किंचित पियराये
माटी का रस पीकर
कल ये फिर हरे-भरे झूमेंगे
मंजरित बालियां इठलाएंगी, नाचेंगी
सौंधी बयार मह-मह महकेगी।
जब घिरी सांझ
विदा की बेला आई
बचुवा की बेटी ने अंतिम जोड़ सुनाए :
धरती मां है
देगी, पालेगी, पोसेगी उनही को,
जो इसकी सेवा में जांगर धन्य करेंगे।
ऋतुएं पलटेंगी
घाम-ताप, वर्षा-बूंदी, हिम-तुषार
अपनी गति से आएंगे-जाएंगे
रहना सुख से, रहो जहां भी
होगी सबसे भेंट पुन:
जीवित यदि अगले वर्ष रही।
उन सृष्टा अंगुलियों को चूम लूं
डूबता रवि
घिर रही है सांझ
चित्रित गगन-आंगन!
किन अदीखी अंगुलियों ने वर्तुल सप्तरंगी अल्पना लिख दी?
कहां हैं वे हाथ
कितने सुघड़ होंगे?
(अल्पना के रंग साक्षी)
क्षणभर देख तो लूं
नयन-माथे से लगा लूं
उन सृष्टा अंगुलियों को चूम लूं।
मैं कि जिसका भाग्य अब तक
सूने चौक, देहरी, द्वार-आंगन से बंधा है।
शायद ये वही हों हाथ
जो धानों की हरी मखमल के किनारे
पीली गोट सरसों की बिछाते
जो धरा पर सप्तवर्णी बीज-रंगों अल्पना लिखते
जो धरा पर सप्तरंगी फूल-रंगों अल्पना लिखते
जो धरा पर सप्तगंधी अन्नरंगों अल्पना लिखते
आहï! कितने सुघड़ होंगे
पात-पल्लव-अन्न साक्षी
नयन माथे से लगा लूं
उन सृष्टा अंगुलियों को चूम लूं।
पहली वर्षा के बाद
भूरी मटमैली चादर ओढ़े
बूढ़े पुरखों से चार पहाड़
मिलजुल बैठे
ऊंघते-ऊंघते-ऊंघते।
घाटी के ओठों से कुहरा उठता
मन मारे, थके हारे बेचारे
दिन-दिन भर
चिलम फूंकते-फूंकते-फूंकते।
बर्फ
फ्रिज से निकालकर
गिलासों में ढाल लेते हैं जिसे
रंगीन पानी के साथ
चुभला भी लेते हैं कभी-कभी
खूब ठंडी-ठंडी होती है
यही शायद आप समझते हैं बर्फ है।
बर्फ जला भी देती है
गला देती है नाक, कान, अंगुलियां
पहाड़ों की बर्फ बहुत निर्मम होती है
बहुत सावधानी चाहिए बर्फ के साथ
अक्सर देखा है
बेपर्दा आंखों को अंधा कर देती है
पहाड़ों की चमकती बर्फ।
अंकित होने दो
मैं कभी कविताएं लिखता था शुभा!
और तुम अल्पना!
चांद तारे
फूल-पत्तियां
और शंखमुद्री लताएं चित्रित करते
न जाने कब
कविताओं की डायरी में
मैं हिसाब लिखने लगा।
कभी खत्म न होने वाला हिसाब
अल्ल-सुबह टूटी चप्पल से शुरू होकर
देर रात में फटी मसहरी के सर्गों तक फैला
अबूझ अंकों का महाकाव्य
और तुम
अस्पताल, रोजगार-दफ्तर
और स्कूलों की सूनी देहरी पर
मांडती रही वर्तुल अल्पना
साल दर साल!
साल दर साल!!
शुभा!
अभिशप्त हैं पीढिय़ां
लिखने को कविताएं
बुनने को सपने
और अंकित करने को सतरंगी दुनिया।
न रोको उन्हें
लिखने दो शुभा
दीवारों पर नारे ही सही
अंकित होने दो उनके सपनों का इतिहास।
द्विज
यज्ञवेदी
गीत सुस्वर
गृहजाग, समिधा-धूम
ऋचाओं की अनवरत अनुगूंज
रह-रह शंख का उद्घोष!
आज मुनुवां द्विज हो गया है।
अभी कुछ देर पहले
पिता का आदेश पाकर
'माम भिक्षाम देहिÓ कहता
वह शिखाधारी
दण्डधारी
मृगछाला लपेटे
राह गुरुकुल की चला था
लौट आया बाल-बटु फिर
कर न पाया अनसुनी मनुहार मां की!
गिन रहा अब नोट,
परखता
सूट के कपड़े, घडिय़ां
और भी कितनी अनोखी वस्तुएं
झोली में पड़ीं जो।
मुनुवां मगन है अब
आज मुनुवां द्विज हो गया है।
पर, साथ छूटा हमजोलियों का
अब बीती बात होगी:
वे ताल-पोखर
वे अमराइयां
जूठी-कच्ची कैरियां।
अब सीधे संवाद होगा
अग्नि, सविता औ वरुण से
छह पीली डोरियों से मुनुवां अब बंध गया है
आज मुनुवां द्विज हो गया है।
निराला के प्रति
शेष हुआ वह शंखनाद अब
पूजा बीती!
इन्दीवर की कथा रही
तुम तो अर्पित हुए स्वयं ही।
ओ महाप्राण!
इस कालरात्रि की गहन तमिस्रा
किन्तु न रीती!
किन्तु न रीती!!
मेरा पहाड़
हिन्दी कहानी में शिल्प और संवेदना के अन्तरसंबंधों की सुरमय रचना के साथ जीवन और समाज के सहज उन्नयन एवं परिवर्तनकारी दृष्टि के प्रति दायित्वबोध शेखर जोशी की कहानियों का प्राणतत्व है। कथात्मक ग्रन्थन में भाषा के सूक्ष्म उपयोग का उन जैसा आधुनिकबोध हिन्दी कहानी में दुर्लभ है।
शेखर जोशी सीधे-सरल, ठगे जाने को अभिशप्त, छल-छन्दहीन पहाड़ी गांवों के गरीबों की जीवन-कथा के करुण चितेरे हैं, जिनकी संघर्षशीलता ही वह शोचनीय मुद्दा है, जो कहानीकार को अवसाद और नैराश्य की भावभूमि पर धकेल देती है। लेकिन गौरतलब है कि इस अवसाद और नैराश्य को स्थिति मानकर वह रचनात्मक ईमानदारी से मुंह नहीं मोड़ लेते बल्कि क्वसिनारियों की माँ-बेटी की तरह लगभग अदृश्य, निर्धूम, चिनगारीहीन और जमीन पर बिखरे कोयलों को बटोरकर उनके बीच छिपे किसी अग्निकण से पूरी आग पैदा करने की उद्दाम आशा और धैर्य रखते हैं।
शेखर जोशी ने अपने पहाड़ को बिना किसी संवेगात्मक तरफदारी के जिस यथातथ्य भाषा में प्रस्तुत किया है, वह संवेदना को एक समृद्ध ज्ञान की कोटि में ले जाता है और संवेदना से अर्जित इस ज्ञान को पुनररचनात्मक और यथार्थपरक संवेदना में बदल देता है। यह प्रक्रिया पहाड़ को एक ऐसी काया देती है जिससे वंचित पहाड़ ऐन्द्रिक बिम्ब तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक पहाड़ नहीं हो सकता। 'मेरा पहाड़' कहानी संग्रह हिन्दी कथा साहित्य की एक उपलब्धि है।
तीसरे दिन रस्किन और शेखर पाठक ने जादू कर दिया
♦ विनीत कुमार
रस्किन बांड की बातों में हम इतनी बुरी तरह खो गये थे कि हमें पता ही नहीं चला कि आसपास बाकी क्या हरकतें हो रही हैं। ये तो जब उन्होंने रवि सिंह (पेंगुइन-इंडिया के प्रकाशक एवं मुख्य संपादक) से बातचीत पूरी की तो देखा कि हॉल पूरी तरह भरा हुआ है। एक भी कुर्सी खाली नहीं थी बल्कि कुछ लोग दीवार से सटकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि रस्किन बांड के नाम पर रातोंरात देहरादून में कुछ अतिरिक्त बुद्धिजीवी पैदा हो गये हों या फिर उन्हें सुनने के लिए शहर के बाहर से आये हों। तीन दिन की इस पेंगुइन रीडिंग्स में रस्किन बांड के सत्र को मैं जादू की तरह याद करता हूं और बिरदा के गीत को नशा के तौर पर। रस्किन बांड को सुनने के बाद हर सत्र और घटनाओं के बारे में सोचता तो आप ही कल्पना करता कि रस्किन इस बात को किस तरह से बोलते और बिरदा ऐसे मौके पर कौन सा गीत गाते?
रस्किन बांड जितना बड़ा नाम है, वो मुझे खुद उतने ही सहज इंसान लगे। चेहरे पर एक खास किस्म की चाइल्डिस इग्नोरेंस है। वो बच्चों के बीच इसी रूप में पॉपुलर हैं। शायद इसलिए उन्हें देखकर ऐसा लगा कि बच्चों के चेहरे का भोलापन रुई के फाहों की तरह उड़-उड़कर उनके चेहरे पर चिपककर एक स्थायी हिस्सा हो गया हो। ये अलग बात है कि मेरे साथ बैठी साना (दि पायनियर) ने चीट पर लिखकर बताया कि रस्किन यहां सीरियस हैं लेकिन अगर अकेले बात करो तो बहुत फनी हैं, एक समय था जब उन्हें गुस्सा बहुत आता था। रवि सिंह ने परिचय के दौरान हमें बताया कि जब वो उन्हें मसूरी लाने गये तो देखा कि बच्चे उन्हें घेरे हुए थे और सब उन्हें अंकल-अंकल पुकार रहे थे। रस्किन जब किताबों की दुकानों पर होते हैं तो ऑटोग्राफ देते नजर आते हैं। ये नजारा तो मैंने खुद सत्र खत्म होने के बाद देखा। स्टेज के चारों ओर से छिटक कर ऑडिएंस उस कोने से चिपक गयी थी जिधर रस्किन खुद बैठे थे। ऑटोग्राफ लेने वालों का तांता लगा था। कुछ लोगों ने तो किताब इसलिए खरीदी कि उन्हें फिर पता नहीं उनका ऑटोग्राफ कब मिले? कई बच्चों की मांओ ने रस्किन की स्टोरी की किताबें खरीदीं और मौका मिलते ही फोन करके बताया – बेटू, तुम्हारे लिए खुद रस्किन ने ऑटोग्राफ वाली किताब दी है।
बहरहाल, कार्यक्रम की जो रूपरेखा दी गयी थी – उसके अनुसार रस्किन अपनी रचनाओं के चुनिंदा अंशों का पाठ करते और फिर उनसे रवि सिंह की बातचीत होती। इस क्रम में उन्होंने रस्टी का पाठ किया और फिर रवि सिंह से बातचीत शुरू हुई। पूरी बताचीत में हमने जो महसूस किया कि रस्किन की दुनिया में फिक्शन और नेचर कायदे से तो मौजूद है ही, राइटिंग फॉर चाइल्ड के लिए भी वो मशहूर हैं। लेकिन शहर को समझने और उस पर बात करने की जो कला रस्किन के पास है, उसे सहेजने और विस्तार देने की जरूरत है। मौजूदा दौर में अकादमी की दुनिया में सिटी स्पेस एक नये विषय के तौर पर पॉपुलर हो रहा है। ऐसे में रस्किन की राइटिंग से शहर को समझने और व्यक्त करने की कला सीखी जा सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब वो देहरादून और मसूरी की प्रकृति पर बात करते हैं, उसके बदल जाने की बात करते हैं। बताते हैं कि तब पूरे शहर में दो ही मोटरकार हुआ करती थी। गिनती के लोगों के पास कलाई घड़ी थी। आप बॉटनी टीचर की बात करें तो लोग आपको उनके घर तक पहुंचा आते थे। शहर बनने की प्रक्रिया के साथ प्रकृति (रस्किन के लिए प्रकृति एक व्यापक शब्द है) किस तरह बदलती है, वो इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। इस तरह वो आपको प्रकृति के नाम पर सिर्फ पहाड़ों और पेड़ों के बीच खो जाने या फिर उसके नाम पर नास्टॉल्जिक हो जाने की राह नहीं थमाते बल्कि एक शहर के बनने की पूरी प्रक्रिया बारीकी तौर पर समझाते चले जाते हैं।
पूरी बातचीत में हमने पाया कि रस्किन के पास सिर्फ वर्णन करने की बेहतरीन शैली ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्वेशन की असाधारण प्रतिभा भी है। मैंने उन्हें बहुत पढ़ा नहीं है लेकिन पूरी बातचीत की बदौलत कह सकता हूं कि उनकी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इन रचनाओं में क्रिएटिविटी का हिस्सा बनकर आती है। इससे आप आर्किटेक्ट लिटरेचर की समझ हासिल कर सकते हैं जो कि लंदन शहर पर जोन्थन रेबन (1974) के लिखे उपन्यास 'सॉफ्ट सिटी' में दिखाई देता है। शहर को इस बारीक समझ के साथ महसूस करने और फिर उस पर उतनी ही बारीकी से लिखने के सवाल पर रस्किन का जबाव जितना सहज था, अमल करने के स्तर पर उतना ही बड़ा चैलेंज।
किसी भी शहर को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस शहर में पैदल चल कर चीजों को देखें। जब आप टहल रहे होते हैं, तो एक ही साथ कई चीजें आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं। आपकी समझ का दायरा बढ़ता है जो कि बिना पैदल चले संभव नहीं है। लेकिन अब लोगों ने यही करना बंद कर दिया है। बच्चे लैपटॉप की स्क्रीनों में घुस गये हैं। उसी दुनिया में खो गये हैं। यही कारण है कि वो एक ही साथ शहर से एहसास के स्तर पर कटते चले जाते हैं और प्रकृति से भी दूर होते चले जाते। ये दोनों चीजें उनके कन्सर्न में नहीं है। रस्किन के लिए प्रकृति बाकी के लेखकों से कहीं ज्यादा बड़ा शब्द है बल्कि इसे आप शब्द न कहकर एनलिटिकल टूल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा।
रवि सिंह ने जब सवाल किया कि क्या ऐसा है कि प्रकृति से जुड़ाव ने आपको ज्यादा संवेदनशील बनाया? इस सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि सिर्फ इस बात से चीजें तय नहीं होती है कि आप प्रकृति से जुड़े हैं, उस पर लिख रहे हैं, देख रहे और बात कर रहे हैं, बल्कि काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति (nature and the nature of the people) पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक तरफ वो देहरादून की नेचर के स्तर पर के बदलावों की चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की उस प्रकृति की भी विस्तार से चर्चा करते हैं, जिन्होंने कि जेनुइन और इन पहाड़ों और प्रकृति के बीच रहनेवाले लोगों को बेदखल कर दिया है। विकास के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, उसमें वो कहीं भी शामिल नहीं हैं। रस्किन के हिसाब से शहर या प्रकृति को समझने का मतलब सिर्फ चीजों की मौजूदगी को महसूस करना भर नहीं है बल्कि उनके साथ हो रहे बदलावों की पूरी प्रक्रिया को समझना है। आसपास की दुनिया को इस रूप में पहचानना ज्यादा जरूरी है।
तीसरे दिन के इस सत्र में केकी दारुवाला और आज की कहानी को यहां स्कीप करते हुए पहले हम शेखर पाठक की उत्तराखंड गाथा वाले सत्र की चर्चा करें तो बाद के कई तरह की रिपिटेशन्स से बच जाएंगे। शेखर पाठक ने उत्तराखंड के अलग-अलग पहलुओं पर प्रोजेक्टर, गिरदा और नरेंद्र नेगी के गीतों के सहारे जो बात कही, उसकी खास तौर से चर्चा की जानी चाहिए। शेखर पाठक जब उत्तराखंड पर अपनी बात रखने के लिए हमारे सामने मौजूद हुए तो इस सत्र का संचालन कर रहे पुष्पेश पंत ने हमें पूरी तरह डरा दिया। वो गाथा शब्द को पकड़कर कुछ इस तरह बैठ गये, वीरगाथाकाल से लेकर अब तक गाथा की जो भी शक्ल बनी है उसे परिभाषित करने लगे कि हमें लगा शेखर पाठक इसमें अपनी बातें ज्यादा और जमाने की बात कम करेंगे। हमारी इस दुविधा में रहा-सहा जो भी कसर था, उसे उन्होंने यह कहकर पूरा कर दिया कि शेखर पाठक सालभर पहाड़ों में घूमते हैं तो कम से कम चार घंटे तो आपके सामने बोलेंगे ही। इस शख्स से उनकी लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है लेकिन मेरी बातचीत तो कभी नहीं हो सकती। हम शेखर पाठक से कुछ सुनते – इसके पहले ही नर्वस हो गये। पुष्पेश पंत की कही सिर्फ एक बात थी जो हमें हिम्मत बंधा रही थी कि ये एक ऐसा स्कॉलर है जो दिनभर स्टडी रूम में नहीं बल्कि पहाड़ों में घूमकर अनुभव बटोरता है। यहीं पर आकर हम बेफिक्र हो गये है कि चलो, जो भी बोलेगें, किताबी नहीं बोलेंगे।
शेखर पाठक हमें उत्तराखंड की उस दुनिया में ले गये, जिसे सिर्फ उसकी पहाड़ियों, खूबसूरत वादियों और पानी की बहती धारा पर रोमैंटिक तरीके से मोहित होकर नहीं समझा जा सकता है। पुष्पेश पंत ने परिचय में ही जो सवाल खड़े कर दिये थे कि अगर शेखर पाठक गाथा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो समझ में आता है कि वो प्रकृति को लेकर एक मिथ की बात कर रहे हैं, वो यहां पूरी तरह टूटता है। शेखर पाठक इन वादियों की, ऐतिहासिक स्थलों की, हिमालय की विराटता की, नदियों के संगम की जब बात करते हैं, तो साथ ही इन वादियों में तस्करों के घुसपैठ की, पौराणिक कथाओं के बनने और उसे सहेजने की, क्षेत्रों को लेकर राजनीति और सरकारी विफलता की, विस्थापन की, बेबसी की, राजनीतिक तिकड़मों की, ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्टर के रौंदे जाने की घटना की विस्तार से चर्चा करते हैं। दस साल पुराने इस नये राज्य उत्तराखंड के विकास से ज्यादा अवसरवाद के जंजाल पैदा होने की कहानी को तल्खी से पेश करते हैं। प्रोजेक्टर पर एक-एक तस्वीरें आती है, शेखर पाठक उसकी चर्चा करते हैं। वो चर्चा प्रकृति या भौगोलिक वर्णन से कब राजनीतिक कट्टरता का बयान करने लग जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देकर सुनने की जरूरत पड़ती है – लेकिन इसके साथ ही एहसास होता है कि आप इस राज्य को सिर्फ उत्तराखंड टूरिज्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। ऊपर रस्किन बांड ने जिस तरह से शहर को देखने की बात कही, वो हमें तीन दिन में सुजीत शाक्या और शेखर पाठक के सत्र में गंभीरता के साथ देखने को मिला। शेखर पाठक हर बड़ी-छोटी घटना को एक बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़कर देखते हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि इन पहाड़ों पर बसंत अब भी उतरता है, नरेंद्र नेगी उल्लास में बसंत के गीत भी गाते हैं लेकिन गिरदा की आवाज में जैसे ही बसंत का गीत शुरू होता है, ऐसा लगता है कि किसी के पेट में बीचोंबीच तीर लगा हो और वो दूर पहाड़ पर खून को रोकने और तीर को निकालने के क्रम में कुछ गा रहा हो। शेखर पाठक इस बसंत के साथ ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करते हैं। टिहरी की चर्चा करते हैं जो कि प्रकृति से कहीं ज्यादा राजनीतिक बेहयापन का शिकार हुआ। जहां जिंदगी हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ एक जगह है। शेखर पाठक की इस पूरी चर्चा की ऑडियो रिकार्डिंग मेरे पास है। अभी सबको सहेज रहा हूं। तस्वीरों के न रहने पर भी इसे सुनकर बहुत कुछ समझा जा सकता है।
शेखर पाठक ने उत्तराखंड गाथा में जिस तरह से अपनी बात कही, वो हिंदी सेमिनारों के संस्कार में नहीं है। यहां विचार इतना हावी है कि फील्ड वर्क जीरो है। शेखर पाठक ने इस काम में हाथों को कलम से ज्यादा पैरों को चल कर थकाया है। इस पैटर्न पर अगर साहित्यिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि एक ही साथ कई विधाएं और प्रोसेस शामिल करके बात की जाने लगे तो यकीन मानिए सेमिनार में डॉक्यूमेंटरी फिल्म का असर पैदा होगा। बहरहाल शेखर पाठक की बातों में एक से एक जानकारी और रोचकता थी लेकिन हम पहले से बहुत लेट हो रहे थे। हम सबों को दिल्ली या फिर बाकी अपनी-अपनी जगहों पर जाना था इसलिए पीछे से लोगों ने ऊबना शुरू कर दिया। सवा दो बजे आते-आते लोग भूख के मारे परेशान होने लगे थे। अंत में पुष्पेश पंत को इंट्रप्ट करना पड़ा। उनका ये अंदाज बहुत सही तो नहीं था लेकिन रोकना भी जरूरी था। शेखर पाठक ने फिर दो-तीन मिनट के भीतर अपनी बात खत्म कर दी।
तीसरे दिन के सत्र में आज की हिंदी कहानी पर जो चर्चा हुई, वो अपने ढंग की अलग चर्चा रही। हम जैसे लोगों के लिए ममता कालिया को छोड़कर बाकी लोगों को सुनना पहली बार सुनने का सुख और अनुभव था। दूसरी खास बात कि जो भी जिसने और जैसा कहा, कइयों की बातों को लेकर व्यक्तिगत तौर पर मेरी असहमति है – लेकिन सबों ने बहुत ही साफगोई के साथ अपनी बात रखी। सबों का स्टैंड मेरी पकड़ में आ सका। मो हम्माद फारुकी जो कि इस सत्र का संचालन कर रहे थे, हिंदी कहानी को लेकर उनका अध्ययन बहुत ही गहरा और समझ बहुत साफ है। मैंने हिंदी के तमाम सेमिनारों में इतनी स्पष्टता के साथ बहुत ही कम लोगों को बोलते सुना है। रिसर्च में भले ही हिंदी समाज में रेफरेंस का रिवाज रहा हो लेकिन व्याख्यान में नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह और मैनेजर पांडेय जैसे कुछ गिने-चुने ही आलोचक हैं, जो इस तरीके से रेफरेंस के जरिये अपनी बात रखते हैं। फारुकी साहब को सुनना मुझे कुछ ऐसा ही लगा। आज की कहानी को लेकर पूरी बहस दो मुद्दे या खेमे में जाकर फंसी। एक तो ये कि आज की कहानी किसे कहेंगे और दूसरा कि युवा कहानीकार क्या लिख रहे हैं?
सत्र की शुरुआत करते हुए फारुकी साहब ने कहा कि आज के युवा कहानीकार बहुत लिख रहे हैं, अलग-अलग मुद्दों पर लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा तो चमकदार है लेकिन विषय को लेकर एक्सपर्टीज नहीं है। कई बार तो वो कहानी नहीं वैचारिकी होती है। ऐसे में कहानी खत्म हो जाती है। चंदन पांडे की कहानी पब्लिक स्कूल को याद करते हुए कहा कि इस कहानी को भी पढ़कर ऐसा ही लगता है और आपको कहानी पढ़ते हुए समझ आ जाएगा कि कहानीकार को पब्लिक स्कूल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। फारुकी साहब की बात को समझें तो ऐसे में अक्सर कहानीकार अपने को थीअरिस्ट जैसी धाक पैदा करने से अपने को रोक नहीं पाते। वो जिस चमकदार भाषा की बात कर रहे हैं उसका तो मैं यही अर्थ समझ पाया कि ऐसी कहानियां तुरंत असर तो करती है लेकिन स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाती है।
इस मामले में ममता कालिया युवा कहानीकारों का पक्ष लेती है और मानती हैं कि वो भी बेहतर लिख रहे हैं। लेकिन संपादक के हाथों पड़ कर कहानी बर्बाद हो रही है। आज अगर कोई कहानी को खत्म कर रहा है, तो वो है संपादक। उसने कहानी को फार्मूला बनाकर रख दिया है। वो कहानी का एजेंडा पहले से ही फिक्स कर देता है कि बेवफाई विशेषांक के लिए रचना आमंत्रित है। इस अंक में प्रेम पर कहानी भेजनी है। पत्रिका का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए चालू फार्मूला बन गया है कि स्त्री विशेषांक निकालो। उन्हें पता है कि स्त्रियों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन इस तरह से विशेषांक निकालकर कहानियां लिखना या छापना स्त्री को कोष्ठक में डाल देती है। इस फार्मूले में पढ़कर कहानी का कहानी होना खत्म हो जाता है जबकि सच बात तो ये है कि सैद्धांतकी बघारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है कहानी लिखना। जैनेंद्र ने भी प्लेटॉनिक प्रेम पर कहानियां लिखीं, लेकिन इस तरह फार्मूलाबद्ध तो नहीं किया।
मशहूर कहानीकार हिमांशु जोशी को इन दिनों लोग अगला यथार्थ की वजह से जान रहे हैं। उनका मानना है कि कहानी का सच, सच से बड़ा होता है। कहानी को सच जैसा लगना चाहिए लेकिन इतना भी सच नहीं कि वो कहानी ही न रह जाए। आज की कहानियों में, साहित्य में सिर्फ विमर्श रह गया है, साहित्य तो है ही नहीं। लोगों की छोटी-छोटी आकांक्षाएं हैं और वो उन्हीं से पारिभाषित हैं। आज निन्यानवे प्रतिशत कूड़ा लिखा जा रहा है और एक प्रतिशत सही। लोगों के छोटे-छोटे गुट बन गये हैं, लेखकों का छोटापन खुलकर सामने आता है। दो ध्रुवांत में साहित्य बंट गया है। सच के नाम पर दुनिया भर की चीजें कही जा रही हैं जबकि सच उतना ही होना चाहिए जो कि इंसान को कुछ दे सके। अगला यथार्थ के सवाल पर हिमांशु जोशी ने कहा कि ये कुछ इसी तरह का है, जैसे नेपाल से आकर हमारे यहां बहुत से लोग नौकरी करते हैं लेकिन वो खुद भी नौकर रखते हैं। नौकर भी नौकर रखने लगा है, ये नये किस्म का यथार्थ है। इसे हमें समझने की जरूरत है।
आज की कहानी के सवाल पर शेखर जोशी (कोसी का घटवार और डूब जैसी कहानियों के लेखक) ने साफ तौर पर कहा कि अगर कल की कहानी आज के संदर्भ में प्रासंगिक है तो वो आज की कहानी कही जाएगी। शेखर जोशी की मानें तो कहानी में कालक्रम से कहीं ज्यादा उसके संदर्भ महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर साबित करते हुए कहा कि पचास के दशक के बाद कहानियां इतनी केंद्र में क्यों रहीं? ऐसा इसलिए कि वो आज की कहानी है। आज इस कहानी लिखने के लिए समाज के बीच लूम्पेन ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ऐसे में मुझे अमरकांत की कहानी हत्यारे याद आ रहे हैं।
लेकिन शेखर जोशी इन सबके बावजूद युवा कहानीकारों के सवाल पर निराश नहीं होते। उनका मानना है कि आज के युवा कहानीकार बहुत बेहतर लिख रहे हैं। बहुत प्रतिभाशाली लोग कहानी लिखने में लगे हुए हैं। महिलाएं कुंठाओं से मुक्त होकर लिख रही हैं। युवाओं की कहानियों को देखकर तो कई बार दहशत होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि कहानी में सब कूड़ा ही नहीं बल्कि बेहतर भी लिखा जा रहा है।
सुभाष पंत की पहचान समांतर धारा के कहानीकारों के रूप में हैं और वो पहाड़ चोर के नाम से भी जाने जाते हैं। सुभाष पंत मौजूदा दौर में विकास और नॉलेज शेयरिंग के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसे लेकर बहुत हतोत्साहित हैं। उनका मानना है कि इंटरनेट जो कि सूचना प्रसार के दावों से लैस है, वहां सब कुछ सिर्फ सूचना और सूचना ही रह गया है, संवेदना का हिस्सा सिरे से गायब होता चला जा रहा है। सुभाष पंत जब ये बात कर रहे थे तो मेरे सहित मौजूद कई लोगों को इससे असहमति हुई। वैसे भी एक माध्यम के स्तर का नकार हम सह नहीं पाते। सुभाष पंत ने कहानी के भीतर की संवेदना के मर जाने या फिर प्रिंट की प्राथमिकता के छीजने का जो आसान फार्मूला हमलोगों को सुझाया, उससे हम कन्विंस नहीं हो पाये। लेकिन उनकी ये बात काफी हद तक सही लगी कि नॉलेज की दुनिया की एक खिड़की इंटरनेट के बाहर भी है और उसे रहना चाहिए। फारुकी साहब ने इस पूरी बातचीत को समेटते हुए नामवर सिंह के उस कथन को शामिल किया कि आज जिस तरह की कहानियां लिखी जा रही है, वो नामवर सिंह को झुठला सकेंगे कि कहानियां सिर्फ सुलाती ही नहीं जगाती भी है।
तीसरे दिन के सत्र का एक जरूरी हिस्सा केकी दारुवाला और स्टीफन ऑल्टर की रचनाओं के चुनिंदा अंशों का पाठ भी रहा। दारुवाला अंग्रेजी कविता में जाना-माना नाम हैं। उनको सुनते हुए मैंने जो महसूस किया, वो ये कि उनकी कविताओं का इंप्रेशन देशी मिजाज की अंग्रेजी भाषा के रूप में है। कविता के बीच में पूरे-पूरे वाक्य हिंदी में आते हैं और असर के तौर पर जेहन में ऐसा काम कर जाते हैं कि आप हिंदी की उस एक लाइन से ऊपर और बाद की कई अंग्रेजी लाइनों के मतलब समझ जाएं। दूसरी बात कि कविता-पाठ की शैली में भाषिक स्तर का अभिनय शामिल है।
स्टीफन ऑल्टर ने केकी के कविता पाठ के बाद चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि वो जिस तरह नॉनवेज पसंद करते हैं, उसी तरह नॉनफिक्शन। इसलिए वो नॉनफिक्शन ही लिखते हैं और उसका पाठ करेंगे। ऑल्टर ने अपने उपन्यास का अंश पाठ किया, जिसे कि हमने असर के लिहाज से नॉवेल डिस्क्रिप्शन से ज्यादा डेमोग्रेफिक स्टेटमेंट के तौर पर महसूस किया।
तीसरे दिन के कुल पांच घंटों में हमने दर्जनभर बुद्धिजीवियों और रचनाकारों के विचार सुने। लेकिन इन सारे लोगों की बातों से सहमति और असहमति के बीच गड्डमड्ड होनेवाली स्थिति कभी नहीं बनने पायी। इसकी शायद सबसे बड़ी वजह यही रही कि विश्लेषण के स्तर के फर्क और विविधता के बावजूद जो सबमें कॉमन बात थी वो ये कि विकास के घोषित पैमाने और उपलब्धियों के नाम पर ताल ठोंकने के पहले इन सबको लेकर हमें सेल्फ एसेस्मेंट और रीडिफाइन की प्रक्रिया से फिर से, बार-बार गुजरने की जरूरत है।
 (विनीत कुमार। युवा और तीक्ष्ण मीडिया विश्लेषक। ओजस्वी वक्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध। मशहूर ब्लॉग राइटर। कई राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सेदारी, राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ताना बाना और टीवी प्लस नाम के दो ब्लॉग। उनसे vineetdu@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
(विनीत कुमार। युवा और तीक्ष्ण मीडिया विश्लेषक। ओजस्वी वक्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध। मशहूर ब्लॉग राइटर। कई राष्ट्रीय सेमिनारों में हिस्सेदारी, राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ताना बाना और टीवी प्लस नाम के दो ब्लॉग। उनसे vineetdu@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
2 Comments »
Leave your response!
http://mohallalive.com/2010/04/08/third-and-last-day-reporting-of-doon-readings/ मार्कण्डेय : जीवन के बदलते यथार्थ के संवेगों का साधक |
-अरुण माहेश्वरी
 'निर्मल वर्मा की कहानियों में लेखकीय कथनों की एक कतार लगी हुई है। जहां जरा-सा गर्मी-सर्दी लगी कि कमजोर बच्चों को छींक आने लगती है। यदि और सफाई से कहें, तो जैसे रह-रह कर बैलगाड़ी के पहिये की हाल उतर जाती है, ठीक वैसे ही, पात्र जरा-सा संवेदनात्मक संकट पड़ते ही खिड़की के बाहर देखने लगते हैं – जहां कोई रेलिंग होती है और जिस पर उदास अंधेरा चुपचाप बैठा होता है। कोई बालकनी या छज्जा होता है, जहां सूखने के लिए कपड़े टंगे रहते है। और लेखक अपनी कोई उक्ति कोई काव्यात्मक प्रसंग या कोई चमत्कार-पूर्ण वाक्य डाल कर ही आगे बढ़ता है।… अपने समय के सच्चे प्रतीकों की बात करना आसान है, पर उन सच्चे प्रतीकों की ट्रू कापी (सच्ची अनुकृतियों) से अपने प्रतीकों को अलगाना जरा टेढ़ी खीर है। उन्हें प्रचारित करने वाले शक्तिशाली और समझदार लोग हैं, जो सत्य की सारी शक्ति चुरा लेने की ताकत रखते हैं। जीवन की वास्तविकताओं के बल पर ही युग के सच्चे प्रतीकों का निर्माण और उनकी मान्यता संभव है। विश्वास और रचना में मूल अंतर जीवन के साथ गहराई से लगाव न होने के कारण ही पैदा होता है और यही अंतर धीरे-धीरे एक स्थायी अन्तराल बन जाता है।'(निर्मल वर्मा: अतीत और भविष्य से मुक्त निरे वर्तमान में)
'निर्मल वर्मा की कहानियों में लेखकीय कथनों की एक कतार लगी हुई है। जहां जरा-सा गर्मी-सर्दी लगी कि कमजोर बच्चों को छींक आने लगती है। यदि और सफाई से कहें, तो जैसे रह-रह कर बैलगाड़ी के पहिये की हाल उतर जाती है, ठीक वैसे ही, पात्र जरा-सा संवेदनात्मक संकट पड़ते ही खिड़की के बाहर देखने लगते हैं – जहां कोई रेलिंग होती है और जिस पर उदास अंधेरा चुपचाप बैठा होता है। कोई बालकनी या छज्जा होता है, जहां सूखने के लिए कपड़े टंगे रहते है। और लेखक अपनी कोई उक्ति कोई काव्यात्मक प्रसंग या कोई चमत्कार-पूर्ण वाक्य डाल कर ही आगे बढ़ता है।… अपने समय के सच्चे प्रतीकों की बात करना आसान है, पर उन सच्चे प्रतीकों की ट्रू कापी (सच्ची अनुकृतियों) से अपने प्रतीकों को अलगाना जरा टेढ़ी खीर है। उन्हें प्रचारित करने वाले शक्तिशाली और समझदार लोग हैं, जो सत्य की सारी शक्ति चुरा लेने की ताकत रखते हैं। जीवन की वास्तविकताओं के बल पर ही युग के सच्चे प्रतीकों का निर्माण और उनकी मान्यता संभव है। विश्वास और रचना में मूल अंतर जीवन के साथ गहराई से लगाव न होने के कारण ही पैदा होता है और यही अंतर धीरे-धीरे एक स्थायी अन्तराल बन जाता है।'(निर्मल वर्मा: अतीत और भविष्य से मुक्त निरे वर्तमान में)
'वैसे ही जैसे कोई आदर्शों का भौतिक रूप नहीं जानता, महज कल्पना करता है या कर सकता है और यहीं नयी कहानी की एक विशेष प्रकृति सहसा अनावृत हो आती है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थ कहना एक भारी भूल होगी। वस्तुत: यह स्थिति शुद्ध रोमानी है, जिसमें ठोस वास्तविकताओं के लिए प्रतिबद्ध लोगों के मुंह से जबान गायब हो जाती है। … शेखर जोशी ने इस युगीन समस्या को अपनी संपूर्ण चेतना और अनुभूति में उतारा है, इसमें संदेह नहीं। परिवर्तन की इस तीखी प्रतिक्रिया के कारण ही वे 'दाज्यू', 'कविप्रिया', 'कोसी के घटवार' और 'बदबू' जैसी श्रेष्ठ कहानियां लिख सके हैं लेकिन अब लगता है जैसे चेतना की सहज प्रकृति रचनाकार के लिए सब कुछ नहीं होती। उसके सयाने होने का अर्थ ही यह है कि वह अपनी रचनात्मक चेतना को एक स्तर पर पहुंचा कर विश्लेषित कर ले। व्यथा और विरक्ति को सामाजिक संदर्भों में निरंतर पहचानते रहने के लिए भी यह जरूरी है।'(शेखर जोशी : विछोह या विरक्ति की कथा)
'अमरकांत विचित्र चरित्रों की रचना छोड़ कर अपनी कहानियों में समय के अंतराल को भर सकें, तो नये भाव-बोध के ग्रहण की समस्या खुद ही हल हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो समय नये सवालों के उठाने का है, न कि उन सवालों के नये उत्तर देने का जो आज की जिंदगी से पीछे छूट गये हैं।' (अमरकांत : समय नये सवालों के उठाने का)
'जानना लेखक के लिए एक आंतरिक संघर्ष है और यह संघर्ष भाषा द्वारा वास्तविकतओं के समीप पंहुचने की चुनौती के कारण निरंतर चलता रहता है। संभवत: आंतरिक संघर्ष की इस प्रक्रिया का नाम ही रचना है। जिस दिन उसे इसका बोध हो जाता है कि वह पूरा जान गया, उसी दिन उसका रचनाकार स्वर्ग सिधार जाता है और वह बहुत-सी बातें जानने वालों की कतार में एक सामान्य मनुष्य के रूप में जा खड़ा होता है अन्यथा रचनाकार एक अधूरा आदमी है, निरंतर पूरे होने की प्रक्रिया में संलग्न। …वस्तुत: मानवीय संवेदना और अनुभूतियों का सचेत परित्याग ही व्यावसायिक-लेखन की सबसे बड़ी पहचान है। …इस तरह एक ओर जहां राजेन्द्र यादव इस महाजनी युग की मूल वृत्ति के प्रभाव में नयी कहानियों की वस्तुवादी, जीवनोन्मुख धारा से किनारा कस चुके हैं, वहीं दूसरी ओर रचना-शिल्प के आन्तरिक गठन और निरंतर विकास के लिए उस छटपटाहट और बेचैनी को, जो उनकी प्रारंभिक कहानियों की सबसे बड़ी संम्भावना थी, खो चुके है।'(राजेन्द्र यादव : सूचनाधर्मी परिवेश में वास्तविकताओं की बुझौवल)
'गरज यह कि सोबती की रचना-दृष्टि में विघटन के प्रति जीवनोन्मुखी माध्यम प्रमुख नहीं हैं जो नये लेखन की खास उपलब्धि है लेकिन ऐसा भी नहीं कि वे आदर्शवादियों की तरह उड़ानें भरें और झूठ को प्रश्रय दें। तनिक रुककर देखें तो लगता है कि वे यथार्थ के आभास की लेखिका हैं। इससे तनिक और नीचे उतरने पर नुस्खों का रचनाकार बनते देर नहीं लगती। लेकिन वे वहां तक नहीं जा पायी हैं – शायद अपनी रुचियों और ईमानदारी के कारण।…चरित्रांकन की दिशा में सोबती की यह कमजोरी कुछ वैसी ही है, जैसी रोमानी लेखकों में होती है लेकिन नतीजों में वे उनसे भिन्न एक नितांत भौतिक सत्य के साथ बंधी रहती है। कभी-कभी तो उनकी निर्ममता इस हद तक पहुंच जाती है कि पाठक को उसकी स्वाभाविकता में संदेह होने लगता है।'(कृष्णा सोबती : अनोखी रीति इस देह तन की)
'रामकुमार की सीमा एकदम दूसरी है। मूलत: उनका शिल्प-बोध दृष्टि की परिसीमा में आबद्ध है। वे उतना ही दिखा पाते हैं, जितना दृष्टि-परिधि में आता है। इसलिए वह अनदेखा संसार भूलकर भी पाठक के सामने नहीं आ पाता, जो इन पात्रों की सही आधार-भूमि है। …दुनिया से इतनी दूरी का आभास देने वाला पात्र दुनिया की शर्तों की उपज कैसे हो सकता है?…आत्मनिमग्नता की इस खास लाचारी के कारण रामकुमार रूमानी लेखकों के पूर्वनियोजित चरित्रांकन की प्रणाली से छुटकारा नहीं पा सकते। …शायद ही कोई मुख्य-पात्र इन कहानियों में ऐसा मिलेगा, जो जीवन की गति में कोई परिवर्तन स्वीकार करे। इसी कारण ये सारे पात्र वास्तविकता की मर्यादा से गिर कर काल्पनिक और गढ़े हुए लगते हैं, उनकी उदासी और विकलता उनकी अपनी ही परिसीमा में संकुचित होकर छोटी हो जाती है।' (रामकुमार : हर एक की अपनी ही आवाज)
'समस्याओं के साथ वैयक्तिक हस्तक्षेप के कारण ही राकेश जहां भी जीवन के यथार्थ प्रसंग छूते हैं, समस्याएं अपने सार्वजनिक स्वरूप को छोड़ कर व्यक्तिगत बन जाती है और उनकी सीमा सिकुड़कर बहुत छोटी हो जाती है। …जीवन की परिवर्तित दिशा में जहां नये अनुभवों से कटे रह जाने के कारण पुराने लेखक अपनी सामाजिक दृष्टि में रचनात्मक परिवर्तन न लाकर स्थिर बने रहे, वहीं राकेश नये जीवनानुभवों के अनुरूप एक सहज, भौतिक-दृष्टि का विकास नहीं कर सके। इसीलिये जहां नयों के सामने 'एक और जिन्दगी' – जैसी कहानी एक निहायत भावुकतापूर्ण रोमानी कहानी बन कर रह गयी, वहीं पुराने भाव-बोध के अनुसार इसे एक असंतुलित आदमी की अस्वाभाविक काव्य-कथा का विशेषण प्राप्त हुआ। …समझ में नहीं आता कि राकेश किन अर्थों में प्रगतिशील और नये हैं जबकि उनकी कहानियां साधारण सामाजिक व्यवस्था के सामने प्रश्न-चिन्ह लगाकर भावुकता भरे काव्यमय अनुभवाभास में खो जाती है।'( मोहन राकेश : सामाजिक भाष्य के सामने प्रश्न-चि)
' भीष्म साहनी की कहानियां पढ़ते हुए बार-बार हवा में उड़ते उस दामन की याद आती है जो एक नन्हें से कांटे में फंस गया है। न वह खुलकर उड़ ही पाता है, न बदन में चिपक कर रह पाता है। हवा होने पर वह फड़फड़ाता जरूरी है लेकिन द्रष्टव्य तो यह है कि हवा न रहने पर वह कांटे में टंगकर कितना अजीब दृश्य-चित्र उपस्थित करने लगता है। यह विचारणीय है कि मिस्टर शामनाथ जैसे मध्यवर्गीय चरित्र की चीफ को खुश करने और तरक्की पाने की इतनी दयनीय मंशा है कि वह जीवन के अत्यंत मार्मिक मूल्यों तक के प्रति अमानवीय हो उठता है। लेकिन भीष्म का दामन मां के उसी परम्परागत रूप में अटका रह जाता है कि कुछ भी हो मां, मां ही है। लाख अपमानित हो, वह अपने बच्चे की तरक्की के लिए अंधी आंखों से भी फुलियारी बनायेगी ही। और भीष्म अपनी अधिकांश कहानियों में खुद मां का वही रोल अदा करते हुए देखे जाते हैं। जीवन की स्थापित मान्यताओं से टूक-टूक होकर भी उसके प्रति आन्तरिक मोह छोड़ न पाने की प्रक्रिया ही भीष्म की रचना-प्रक्रिया है। …भीष्म साहनी की कहानियां पढ़ते हुए यह बातें मन में इसलिए उठती हैं कि समूची नयी कहानी में सामाजिक चेतना के प्रति उन जैसा सहज और सम्पूर्ण लगाव शायद ही किसी का है – जैसे वे अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को अपनी रचना में नियोजित कर देते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियों में कहानी की विधा का एक सरल बहाव और सादगी है, काश वे परम्परागत बोध के पठार से आगे बढ़कर बोधहीनता की नयी सच्चाई को भी देखते।' (भीष्म साहनी : बोधहीनता एक नयी सच्चाई)
'असल में जीवन के प्रति वैयक्तिक मान्यताओं के कारण यथार्थ तक पहुंचने में जो बाधाएं उपस्थित होती है – वही बाधाएं आदर्शों की ओट लेेने पर भी होने लगती है। सही माने में भावुकता के यही दो छोर है, जहां रचनाकार किन्हीं ऐसे प्रभावों में आकर अपनी आंख पर परदा डाल लेता है और फिर ऐसे दृष्टि-प्रक्षेप करने लगता है, जिससे या तो उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं आलोकित होती है या वे आरोपित आदर्श, जिनका वह पक्षधर है और रचना का मूलाधार जीवन धीरे-धीरे उसकी दृष्टि से ओझल होने लगता है। भैरवजी की प्रारम्भिक कहानियों में हमें दृष्टि की यही ओझलता लक्षित होती है। ऊपर से सच्चाइयों की तरह दिखने पर भी रचना-प्रक्रिया के दौरान इन कहानियों का संस्पर्श यथार्थ से नहीं होता।' (भैरवप्रसाद गुप्त : आंख की पी)
'मुझे बार-बार लगता है जैसे अपने वैयक्तिक अनुभवों के लिए ही आपका रचनाकार पूर्णत: समर्पित है और अपने पर इस कदर लुभाये रहने के कारण आपकी सहानुभूति के चरित्र मशीनी हो उठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवनानुभव ही असामान्य हैं? '(उपेन्द्रनाथ अश्क : अश्क के नाम एक औरत का खत)
'यशपाल ने मान्यताएं बदल दीं। सामाजिक यथार्थ के ऊपर पड़ी परत को काटने के लिए उन्होंने ऐसे प्रतीक निर्मित किए, जिनमें अर्थवत्ता तो थी, लेकिन देह और प्राण-शक्ति पर कल्पना हावी होती गयी। पात्र और परिस्थितियां मानी हुई और नकली होने लगी, क्योंकि यशपाल की दृष्टि जीवन के बदलते हुए यथार्थ से नहीं, वरन् उस पठार से ही टकराती रही, जिसे उन्होंने मनुष्य के यथार्थवादी बोध के मार्ग में बाधक के रूप में स्वीकार कर लिया था। तनिक ध्यान से देखें, तो साफ लगेगा कि यशपाल जीवन के प्रति नहीं, उन बाधाओं के प्रति प्रतिश्रुत है, जो जीवन के विकास के मार्ग में आ पड़ी हैं।'(यशपाल : कहानी जीवन के लिए)
'पर जाने क्यों दिन-पर-दिन अज्ञेय का रचनाकार जीवन और जगत् की ओर से उदास होता चला गया और 'कलाकार की मुक्ति' तक पहुंचते-पहुंचते उसमें इतनी असमर्थता आ गई कि वह किंवदन्तियों और पौराणिक कथाओं के शिल्प पर उतर आया। संभव है, जीवन की सहज गति से रचनाकार का व्यक्तित्व किनारे पड़ गया हो, अथवा विचारों के दुरूह, अस्वाभाविक प्रतिमानों के कारण मन की वे परतें ही सूख गई हों, जिन पर सच्चाइयों के अक्स आकर नक्श होते हैं अथवा वैयक्तिक कुण्ठाओं ने अपने चारों ओर एक ऐसा खोल आढ़ लिया हो कि सब-कुछ में उसे अपने ही आरोपणों की तस्वीरें दिखने लगी हों; …हैरत की बात है कि अज्ञेय ने जहां भी एक राजनीति का विरोध किया है, वहीं एक दूसरी कमजोर राजनीति ने जन्म लेकर उनकी रचना को पंगु और प्रचारात्मक बना दिया है। '(अज्ञेय : शेखूपुरे के शरणार्थी)
'जैनेन्द्र, आत्मप्रक्षेपण द्वारा अगर बाल्टी को कुआं कहते तो भी उसके परीक्षण की गुंजाइश होती । वे तो आंख में धूल झोंकते हैं और गम्भीर मुद्रा में कहते हैं कि, 'जो आप देख रहे हैं, वह है भी, और नहीं भी है और फिर वही 'सप्तभंगी नय'! फलत: सामने आता है एक भ्रम और वह भी कल्पना के पंखों पर चढ़ा हुआ और सारी रचना-प्रक्रिया को अवास्तविक और कोरी गढ़ी हुई बनाकर कहानी को वहां की बना देता है, जहां 'शायद' है, और हम दुनिया में रहने वालों के लिए यह 'शायद' भ्रम का सगा बेटा है।'(जैनेन्द्र : कहानी वहां की)
'इन कहानियों में पात्रों के निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उग्र हमेशा बने-बनाए पात्रों की ही खोज में रहे हैं। वे जीवन की भूसी में से दाना चुनने का तकलीफदेह काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे दृष्टि को भी काम में लाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मात्र संस्कारों के सहारे वे पात्रों की चुटिया पकड़ते फिरते हैं।' (पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र : अम्मा का नाम गुलाबो)
प्रेमचंद के बाद जिन प्रमुख रचनाकारों से आधुनिक हिंदी कहानी का पूरा परिदृश्य निर्मित हुआ था, वैसे 14 कहानीकारों पर मार्कण्डेय की ये मर्म-भेदी टिप्पणियां उनके लेखों के संकलन 'कहानी की बात' के 14 लेखों से ली गयी है। कहानी या रचनाशीलता से तात्पर्य क्या है, बड़े-बड़े लेखकों में वह कहां और कैसे चुकती हुई दिखाई देती है और उनकी कलम की स्याही के सूखने का कारण बनती है, मार्कण्डेय की नजर उस पर थी। कुल मिला कर निष्कर्ष यह कि कहानी में जीवन का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जिंदगी और उसमें चल रहा प्रतिक्षण परिवर्तन ही रचना के सौन्दर्य और शक्ति का मूल स्रोत है। जो रचनाकार बदलाव के इस निरंतर प्रवाह को साधता चला जाता है, वही लिखता है – सार्थक लिखता है। अन्यथा, एक जगह आकर सिर्फ कर्मकांडी रह जाता है। जिंदगी के बनिस्बत खुद के खास-खास विचारधारात्मक या कलात्मक आग्रहों के चलते कैसे और कहां उनसे जिंदगी के यथार्थ की डोर छूट जाती है, रचनाशीलता का प्रवाह रुक जाता है, मार्कण्डेय ने इन टिप्पणियों में बड़ी बारीकी से इसे बताया है।
बात अभी से लगभग तीन दशक पहले की है। मार्कण्डेय का उपन्यास 'अग्निबीज' (1981) छप कर बाजार में आया था। हमारे घर में सबने उसे बड़े चाव से पढ़ा और यह तय हुआ कि क्यों न इस उपन्यास पर एक घरेलू गोष्ठी ही की जाएं! छुट्टी के दिन सुबह-सुबह हम बैठे। मेरे, सरला के अलावा इसराइल साहब, बाबू (रमन माहेश्वरी) और दुर्गा शामिल थे। सबने पूरा उपन्यास एक रात में, जैसे एक सांस में पढ़ा था। उपन्यास का प्रवाह ही ऐसा था। पता नहीं, वह उम्र का कारण था या कुछ और, उपन्यास पढ़ते-पढ़ते किसी के आंसू न गिरे हो, या कम से कम गला न रूंधा हो, ऐसा नहीं हो सकता था। उसी प्रभाव और आवेग की मानसिकता में हम उपन्यास पर चर्चा करने बैठे थे। जब चर्चा करनी थी, तब कोरी भावुकता से काम नहीं चल सकता था। कुछ संयत रहने और साहित्य के कुछ स्थापित, जान-माने ठोस मानदंडों की कसौटी पर उस उपन्यास को रगड़ने की जरूरत थी। इसीलिये पाठक-आस्वादक के बजाय अपने 'आलोचक' को ज्यादा ही जागृत करके मैं उस चर्चा में उतरा था और चर्चा के प्रारंभ में ही ग्रामीण जीवन के कहानीकार मार्कण्डेय से हमारी अपेक्षाओं की पूरी फेहरिस्त पेश करते हुए मांग की थी कि गांवों के परिवेश पर कोई उपन्यास लिखा जाएं और उसमें एक सिरे से जमीन का प्रश्न गायब हो, यह अस्वाभाविक, और एक हद तक अवांछित भी है। 'अग्निबीज' में भारत के गांवों का प्रमुख अंतर्विरोध, जमीन-केंद्रित अन्तर्विरोध एक सिरे से नदारद क्यों है, समझ में नहीं आता। दूसरों ने भी अपनी बात रखी, उपन्यास में जो नहीं है, उसके बजाय जो है, उसी पर बात करने के लिये भी कहा गया। लेकिन वह 80 के दशक की शुरूआत का जमाना था जब हवा में जमीन की लड़ाई का मसला छाया हुआ था। उपन्यास का काल भी आजादी के ठीक बाद का काल था, जब कांग्रेस सरकार जमींदारी उन्मुलन के कार्यक्रम को अपनाए हुए थी। इसलिये पूरी ताकत और तर्कों से मैंने उपन्यास की इस मूलभूत कमजोरी को उठाते हुए उसके प्रति अपने असंतोष को जाहिर किया। और इसीप्रकार बात खत्म होगयी। मैंने कहा कि इस पर विस्तार से लिखा जायेगा, देखें क्या होता है।
बहरहाल, अग्निबीज पर हमारी घरेलू गोष्ठी तो इसी प्रकार के तर्क-वितर्क के बाद खत्म होगयी, लेकिन हमने उपन्यास पर लिखने का जो बीड़ा उठा लिया था, वह हमारे लिये समस्या बन गया। अब उपन्यास और उसके पात्र हमारे दिमाग से उतरने के लिये तैयार नहीं थे। यह एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। क्यों और कैसे हमारे सारे 'बुनियादी' प्रश्न और शंकाएं दिमाग के एक कोने में धरे के धरे रह गये और उपन्यास को लेकर जितना सोचता गया, उसके सभी चरित्र, उनका परिवेश और लेखक के संवेदनात्मक उद्देश्य दिलो-दिमाग पर छाते चले गये। सारे पात्रों का इस प्रकार उठ खड़े होना और पूरी ताकत के साथ अपनी अस्मिता की सचाई को जाहिर करना कुछ ऐसा था, कि जिन प्रश्नों के खांचे में हम उपन्यास को उतारना चाहता था, वह समीक्षा में कहीं संदर्भ का विषय भी नहीं बन पाया। 'अग्निबीज' के पात्र न किसी संवेदनात्मक संकट की आंच पाते ही बगले झांकते दिखाई दिये, न विचित्र, काल्पनिकता से गढ़े गये वास्तविकता की मर्यादा लांघते हुए जीवन की किन्हीं व्यक्तिगत मान्यताओं या आदर्शों के वाहक या भावुकता भरे काव्यमय अनुभवाभास में खोते हुए नजर आयें। वे देह-प्राण से भरपूर, अति-संवेदनशील और साथ ही बोधहीनता के नये सामाजिक सच को उजागर करने वाले सामान्य जीवनानुभवों के अर्थवान पात्र थे।
उपन्यास के अंत में श्यामा के बेमेल विवाह और हरिजन बालिका विद्यालय में आग लगने का भावभीना और उत्तेजनापूर्ण प्रसंग है। विवाह स्थल पर पूरा गांव ही नहीं, उस क्षेत्र की सारी हस्तियां मौजूद है। हर रंग और विचारों के लोग। लेकिन गौर करने लायक बात यह थी कि श्यामा की बौद्धिक परिपक्वता के कायल, उसके व्यक्तित्व को विराट होते देखने की हार्दिक इच्छा रखने वाले वहां उपस्थित किसी भी विचारवान व्यक्ति के मन को इस बेमेल विवाह की त्रासदी से जुड़े प्रश्न बेचैन नहीं कर रहे थे। इन सबके लिये यह शादी भी हर भारतीय नारी के जीवन में सौभाग्य के उदय के महोत्सव से भिन्न और कुछ नहीं थी। अगर कोई बेचैन थे, तो सिर्फ श्यामा की मित्र-मंडली के समवयसी नौजवान सुनीत, सागर और मुराद। इस पूरे प्रकरण से गांव के एक स्थिर परिवेश में कहां और कैसे जीवन में परिवर्तन के नये सूत्र अनायास ही प्रवेश कर रहे हैं, इसे पकड़ने में कोई भी संवेदनशील पाठक नहीं चूंकेगा।
तीन खंडों में लिखे जाने वाले इस उपन्यास का दूसरा खंड कोलकाता के निकटवर्ती चटकलों के क्षेत्र पर केंद्रित होने वाला था, क्योंकि हरिजन लड़की छबिया अपने ब्राह्मण प्रेमी के साथ भाग कर इसी क्षेत्र में जा बसी थी। मार्कण्डेय इसके लिये कुछ दिन कलकत्ता रह कर चटकलों के इलाकों को देखना-जीना चाहते थे। हमलोगों से इसकी इच्छा भी जाहिर की थी। लेकिन आसानी से अपना घर छोड़ कर कहीं भी निकल जाने की मानसिकता न होने के कारण मार्कण्डेय का यह प्रकल्प सिर्फ उनकी एक इच्छा ही रह गया, कभी वास्तविकता नहीं बन पाया।
बहरहाल, 'अग्निबीज' के पात्रों की सोहबत और उपन्यास के प्रति-संसार में लगातार कई दिन और रातें गुजारते हुए एक प्रकार की आत्मलीनता से मैं बीमार भी होगया, और जो समीक्षा लिखी गयी, उस पर खुद मार्कण्डेय का पत्र आया कि उपन्यास को लिखते वक्त मैं जिस मानसिकता में रहा, तुम्हारी समीक्षा ने जैसे उसे फिर मेरे सामने जीवित कर दिया है। वह समीक्षा 'नया पथ' में छपी थी जिसका शीर्षक हमने लगाया था अग्निबीज : विगत तीन दशकों का एक अन्यतम श्रेष्ठ उपन्यास। तब चंद्रबली सिंह जलेस के महासचिव के नाते 'नया पथ' के संपादक थे। डा. नामवर सिंह ने उनकी चुटकी ली – 'अन्यतम भी, श्रेष्ठ भी'। नामवरजी के कटाक्ष ने परफेक्शनिस्ट चंद्रबली जी को बौखला दिया। तत्काल मुझे फोन करके इस गलत भाषिक प्रयोग के लिये फटकारा। उस लेख को जब मैंने अपनी पुस्तक में शामिल किया तो शीर्षक बदल दिया, लेकिन इस घटना ने आगे के लिये भाषा के मसले पर मुझे काफी सावधान किया।
मार्कण्डेय कहानी में परिवर्तनशील जीवन के यथार्थ के प्रति ईमानदारी और सूक्ष्म दृष्टि के जिस सर्वप्रमुख मानदंड को हिंदी के अन्य कहानीकारों पर लागू कर रहे थे, (जैसा कि 'कहानी की बात' से लिये गये उद्धरणों से जाहिर है) उनकी खुद की रचनाएं बताती है कि ये सारे मानदंड उनके रचनाकार व्यक्तित्व की साधना की एक स्वाभाविक उपज थे, किसी अकादमिक ज्ञान का परिणाम नहीं। साहित्य के बारे में माक्र्स का यह कथन कि लेखक के विचार जितने छुपे रहें, कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है, मार्कण्डेय की रचनाएं इसी का प्रमाण है। जब 'अग्निबीज' उपन्यास आया, उसमें हम उस समय के प्रमुख प्रश्न, जमीन के लिये संघर्ष के प्रश्न को खोज रहे थे। लेकिन जैसा कि पहले ही कह चुके है, उस उपन्यास का काल और समूचा संदर्भ ही अलग था। हमारी आत्मगत जरूरत से उपन्यास का कुछ लेना-देना नहीं था। वह विचारधारा से नहीं, अपने खुद के यथार्थ से गुंथा हुआ था, इसीलिये अपने प्रभाव और संदेश, दोनों दृष्टि से इतना सशक्त साबित हुआ। लेकिन मार्कण्डेय अपने ऐसे सुदूर अतीत में ही मूंह गड़ाये बैठे रहने वाले रचनाकार नहीं थे। अगर ऐसा होता तो वे 70 के दशक से ही हिंदी साहित्य की दुनिया में नये जनवादी उभार के इतने सशक्त व्यक्तित्व नहीं होते। आजादी के बाद के तीन दशकों में गांव का तेजी से बदल रहा परिदृश्य उनकी नजरों के सामने था। अग्निबीज के यदि और खंड लिखे गये होते तो उनमें प्रमुख तौर पर इस नये गांव के सुलगते यथार्थ का आख्यान ही होता। गांव और शहर के इस नये दौर के बदलाव को मार्कण्डेय ने अपनी कहानियों का विषय बनाया। और, कहना न होगा, 1975 में उनके कहानी संकलन 'बीच के लोग' का प्रकाशन उस समय के कथा साहित्य जगत की एक घटना थी।
'जरूरत तो ऐसी ही है। अच्छा हो कि दुनिया को जस-की-तस बनाये रहने वाले लोग अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो बीच से हट जाए, नहीं तो सबसे पहले उन्हीं को हटाना होगा, क्योंकि जिस बदलाव के लिए हम रण रोपे हुए हैं, वे उसी को रोके रहना चाहते हैं।- 'बीच के लोग' कहानी का यह अंतिम संवाद 70 के दशक के राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य को परिभाषित करने वाला संवाद था। इस समय तक उस कहानी के मुख्य पात्र 'फउदी दादा' की गांधीवादी और कानूनवादी परंपरा का पाखंड पूरी तरह तार-तार हो चुका था। शहरों में जनवादी चेतना के विस्तार तथा गांवों में भूमिहीनों और दलितों की एक नयी संघर्ष और अधिकार चेतना तथा गोलबंदी का विशेष परिदृश्य साफ तौर पर उभरने लगा था।
इसी संकलन में एक लंबी कहानी थी 'प्रिया सैनी'। शहर में नये मध्यवर्ग के उदय से जुड़ी 'स्त्री-स्वातंत्र्य' की तब यह एक बेहद चर्चित कहानी थी। कलम के संपादक-मंडल में डा.चंद्रभूषण तिवारी अपने ही प्रकार के जुझारू तेवर के व्यक्ति थे। सौन्दर्यशास्त्र में उन्होंने डाक्टरेट किया था और कभी उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी को प्रेमचंद से मुक्त करने की बात भी की थी। चंद्रभूषण जी ने ही बातों-बातों में बताया था कि प्रेमचंद के बारे में उनकी टिप्पणी को देख कर मार्कण्डेय ने उन्हें 'मानसरोवर' के सभी खंड भेंट करके उन्हें पढ़ डालने की सलाह दी थी, और इसप्रकार उनकी आंखों पर पड़े आधुनिकता के झूठे पर्दे को हटाया था। वही चंद्रभूषण जी 'प्रिया सैनी' को लेकर बेहद उत्तेजित थे। ऐसी 'लिजलिजी' रोमानी भावुकता का 'क्रांतिकारी प्रतिरोध' साहित्य में क्या काम! बार-बार 'प्रिया सैनी' कह-कह कर वे उन्हें चिढ़ाते थे। और हमने देखा था कि मार्कण्डेय, बिना किसी प्रतिवाद के, होठों पर सिर्फ एक बांक मुस्कान के साथ चुप हो जाते थे। बाद में मार्कण्डेय ने कृष्णा सोबती पर 'कलम' में जो टिप्पणी लिखी, 'अनोखी रीति इस देह तन की', जिसका एक उद्धरण यहां ऊपर दिया गया है, जीवन के नये और कठोर संदर्भों में कहानी के नये मानदंडों की मार्कण्डेय की तलाश का ही एक नतीजा है। कहना मुश्किल है कि 'कहानी की बात' की टिप्पणियों के इस समूचे उपक्रम में, जिसे उन्होंने परवर्ती दिनों में अपनी पत्रिका 'कथा' के पृष्ठों पर नीलकांत की टिप्पणियों के जरिये कुछ-कुछ जारी रखा था, उन्होंने अपनी रचनाशीलता के लिये कितनी कठिन शर्तें तैयार कर ली होगी! इसराइल की कहानियों में मजदूरों की जिन्दगी का जो धधकता हुआ यथार्थ था, मार्कण्डेय तब उसपर मुग्ध थे। 'अग्निबीज' के और खंड नहीं लिखे जा सके, इसमें इस नये और क्रांतिकारी यथार्थ को जानने और साधने के उनके इस कठिन आत्म-संघर्ष की कितनी भूमिका रही होगी, कहा नहीं जा सकता। यथार्थ के बजाय वैचारिक आग्रहों पर बल देने से बचने की जो हिदायतें उन्होंने दूसरों को दी थी, वैसे ही वैचारिक आग्रहों ने खुद उनकी रचनाशीलता के प्रवाह को कितना बाधित किया होगा, यह भी समझना कठिन है। अथवा, क्या यह सब किसी 'बीच के लोग' के दृश्य से हट जाने का एक ईमानदार निर्णय था! कुल मिला कर इतना जरूर है कि कालक्रम में वे एक बहुत उच्च-स्तरीय साहित्य संपादक के रूप में भी उभर कर सामने आयें। उनकी मौजूदगी ही कई ऊंची हांक वाले अध्यापक साहित्यकारों को असहज कर देने के लिये काफी हुआ करती थी। दोस्तों ने इस गुरुओं के गुरू के प्रति अपनी भड़ांस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
मार्कण्डेय शायद ही कभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि पार्टी के किसी भी सदस्य से वे कहीं ज्यादा निष्ठावान और अनुशासित माक्र्सवादी थे। यही वजह है कि वे सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में पार्टी के स्तर पर होने वाली सारी बहसों से पूरी तरह वाकिफ, इनके एक स्वाभाविक भागीदार हुआ करते थे। 70 के जमाने में 'स्वाधीनता' के बहुचर्चित 'सांस्कृतिक पृष्ठ' के लेखकों में एक नाम उनका भी था। 'कलम' पत्रिका के प्रकाशन और जनवादी लेखक संघ के निर्माण की पूरी प्रक्रिया में पार्टी के स्तर पर भी वे कुछ इस तरह शामिल थे कि किसी को उनके पार्टी सदस्य होने के बारे में कभी कोई संदेह नहीं हो सकता था। इन विषयों पर कामरेड बी.टी.रणदिवे के साथ कई बैठकों में वे शामिल हुए थे। वे जनवादी लेखक संघ के एक संस्थापक उपाध्यक्ष भर नहीं थे, इस संघ के निर्माताओं में उनका विशेष और बेहद महत्वपूर्ण स्थान था।
जनवादी लेखक संघ ऐसे लेखकों का संगठन है जो साहित्य की वस्तु, रूप और शैलियों के बारे में अपने दृष्टिकोणों और रुचियों की भिन्नता के बावजूद जनवाद को हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक नियति का एक अभिन्न अंग मानते हैं, जो उसे हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास की एक अनिवार्य शर्त मानते हैं, और जो उसकी रक्षा और विकास के संघर्ष को अपना एक आवश्यक लेखकीय कत्र्तव्य समझते हैं।- जलेस के घोषणापत्र में इस तरह के असीम महत्व के सूत्रीकरण में मार्कण्डेय की तरह के एक गैर-अकादमिक, मसीजीवी लेखक की उपस्थिति की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित करने की जरूरत है। 'कथा' में धर्म, उच्च शिक्षा और नवलेखन आदि विषयों पर जमाने पहले जिस प्रकार की परिचर्चाएं चलायी गयी, वे आज भी विचारों की दुनिया में वाद-विवाद-संवाद के भारी महत्व को बताने के लिये काफी है। धर्म संबंधी परिचर्चा में ईएमएस नम्बूदिरिपाद और गुरु गोलवलकर, दोनों शामिल थे, निष्कर्ष पाठकों के विवेक पर था। आज के साहित्य और विचारों की दुनिया में विवादों का अभाव उन्हें कचोटता था। रोजमर्रे की राजनीति के सभी टेढ़े-मेढ़े रास्तों और मोड़ों पर उनकी तीखी नजर थी और इसके बारे में तो जीवन के अंतिम दिनों तक हम उनसे बेधड़क चर्चाएं किया करते थे। फोन की सहूलियत ने पिछले तीस सालों में हमें कभी उनसे दूर नहीं महसूस होने दिया।
मार्कण्डेय भाई से अंतिम मुलाकात उनकी मृत्यु के दो हफ्ते पहले ही दिल्ली में हुई थी। रोहिणी में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के नजदीक ही किराये के एक फ्लैट में वे अपने इलाज के लिये टिके हुए थे। संयोग से उन्हीं दिनों हमारा दिल्ली जाना हुआ और मैं और सरला, किसी तरह रोहिणी पहुंच गये। हम सबकी आंखें छलछला रही थी। मार्कण्डेय भाई को बोलने में कष्ट हो रहा था, लेकिन चुप नहीं रह सकते थे। मानसिक तौर पर पूरी तरह जागृत थे। 'कथा' की योजना उनके दिमाग पर छायी हुई थी। हंसते हुए बोले कि नामवरजी ने कूड़े से निकाल कर अपनी जो चार नयी किताबें छपायी है, उनपर लिखवाया जायेगा। हम सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। सरला को पूरी तरह से स्वस्थ देख कर बेहद खुश थे। तमाम आशंकाओं के बावजूद, कुल मिला कर तब यही लगा था कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर इलाहाबाद लौट जायेंगे। रेडियेशन के सिर्फ पांच-छह सेशन बाकी थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन वे लौटने वाले थे, उसके एक दिन पहले ही 5 फरवरी को दिल का दौरा पड़ा और वे नहीं रहे।
मार्कण्डेय भाई ने अपने पीछे साहित्य संबंधी चिंतन की जो एक गंभीर, उत्तेजक और समृद्ध विरासत छोड़ी है, वह हर साहित्यकर्मी की एक अमूल्य धरोहर है। उनकी स्मृति को हमारा नमन।


















































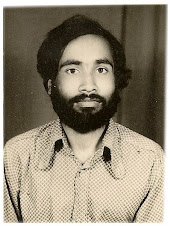

शेखर जी से पिछले महीने ही मिलना हुआ था. वह खूब यात्राएं करते हैं और मुझे लगता है पहाड़ की भाषा संस्कृति को समझने वाले गिने-चूने चेहरों में हैं और एक बात यह की उनकी संस्था का नाम भी पहाड़ ही है.
रस्किन से ना मिल पाने का अफसोस आपकी 'जिन्दा प्रस्तुति' से थोडा कम हुआ..)
लेट लतीफ़ी के नए प्रतिमान…..!
लेट लतीफ़ी के नए प्रतिमान गढ़ते हुए हम हाज़िर हैं इस रिपोर्ट पर कुछ कहने क लिए. 'Doon Readings' से तीन दिन पहले ही शेखर पाठक साहब, हम्माद फ़ारूकी साहब, जैसे लोगों से मिली थी 'उत्तराखंड महिला समाख्या' सेमिनार में. हम्माद साहब ने शाम घर पर बैठक जमाने का प्रस्ताव रखा जहाँ उन्होंने साहित्य और साहित्य से बाहर की कई ऐसी बातों का ज़िक्र किया की उन्हें डायरी में सहेजना ज़रूरी हो गया. बहुत जल्द ही सम्बंधित विषय पर उसका हवाला देनेवाली हूँ. बड़ी बात ये की हम्माद साहब ने उन्हें कितनी सहेजता से सोख़ रखा है मन में. शेखर पाठक साहब ने स्त्रीवादी सेमिनार में बड़ी ईमानदारी से पूरे पुरुष समाज की अनभिज्ञता और संवेदनशीलता पर स्वीकारोक्ति की. दुसरे दिन उन्होंने वो खूबसूरत और शायद बहोत महंगी किताब भी भेंट की, जिसमे पहाड़ और पहाड़ीपन का बेहद खूबसूरत बयां कैमरे की नज़र से है.
जहाँ तक इन्टरनेट पर सूचना और केवल सूचना का सवाल है, तो विनीत की रिपोर्ट बहुत देर तक पाठक कैसे खींचती रहती है? और भी कई लेखक-कवि-आलोचक-विश्लेषक-लिक्खाड़ हीरो हैं जो इन्टरनेट पर साहित्य के उपलब्ध होने से ही बने हैं. साहित्य अपना चोला बदल रहा है. स्वीकार कीजिये और सहर्ष कीजिये
Sheeba Aslam Fehmi