From: reyaz-ul-haque <beingred@gmail.com>
Date: 2010/7/16
Subject: पढ़िए सिनेमा की दिलचस्प कहानी
To: tahreeq@gmail.com
सिनेमा का गल्प
अच्छाई के दिन गए. जीवन में नहीं बचा तो फिर सिनेमा में क्या खाकर बचता. जो बचा है वह पैसा खाकर, या खाने के मोह में बचा है. बॉक्स ऑफिस के अच्छे दिनों की चिंता बची है, अच्छे दिनों की अच्छाई की कहां बची है, क्योंकि आदर्शों को तो बहुत पहले खाकर हजम कर लिया गया. और ऐसा नहीं है कि कुंदन शाह के 'जाने भी दो यारो' में पहली बार हुआ कि सतीश शाह केक की शक्ल में आदर्शों को खाते दीखे, तीसेक साल पहले गुरुदत्त ऑलरेडी उन आदर्शों को फुटबाल की तरह हवा में लात खाता देख गए थे. समझदार निर्माता और बेवकूफ़ दर्शक ही होता है जो मोहल्ले के लफाड़ी किसी मुन्ना भाई की झप्पियों से आश्वस्त होकर मुस्कराने लगता है, या चिरगिल्ले सरलीकरणों के इडियोटिक समाधानों का जोशीला राष्ट्रीय पर्व मनाने, ऑल इज़ वेल को राष्ट्रीय गान बनाने, बजाने लगता है.
कहने का मतलब हम सभी जानते हैं 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना' गाने का मतलब नहीं. जीवन से अच्छाई के गए दिन फिर लौट कर नहीं आते. सिनेमा के झूठ की शक्ल में भी नहीं.
प्रमोद सिंह द्वारा लिखी गई सिनेमा की यह दिलचस्प कहानी पढ़िए हाशिया पर--
Nothing is stable, except instability
Nothing is immovable, except movement. [ Engels, 1853 ]
सिनेमा का गल्प...
Posted by Reyaz-ul-haque on 7/16/2010 08:17:00 AMरामजीत के किस्सों के बाद प्रमोद सिंह (अपने वही, अजदक वाले) ने एक बार फिर इतना चकित कर देने वाला कुछ लिखा है. यह उनके ब्लॉग सिनेमा-सिलेमा पर है, जहां इसे पोस्ट करते हुए उन्होंने कुछ तसवीरें भी दी हैं. हम उनके लेख को यहां साभार पोस्ट कर रहे हैं.
क्या होता है सिनेमा? पता नहीं क्या होता है. छुटपन में सुना करते बहुत सारे घर बरबाद कर देता है. बच्चों का मन तो बरबाद करता ही है. बच्चे थे जब बाबूजी अपनी लहीम-शहीम देह सामने फैलाकर, बंदूक की तरह तर्जनी तानकर हुंकारते, 'जाओ देखने सिनेमा, बेल्ट से चाम उधेड़ देंगे!' चाम उधड़वाने का बड़ा खौफ़ होता, मगर उससे भी ज्यादा मोह खुले आसमान के नीचे 16 एमएम के प्रोजेक्शन में साधना, बबीता और आशा पारेख को ईस्टमैनकलर में देख लेने का होता. उन्हीं को नहीं जॉय मुखर्जी और शम्मी कपूर के फ़िल्मों के राजेंदर नाथ को, मुकरी, सुंदर, धुमाल, मोहन चोटी को देखने का भी होता. शंकर जयकिशन और ओपी नय्यर के गानों के पीछे सब कुछ लुटा देने का होता. मोह. जबकि उस उम्र में पास लुटाने को कुछ था नहीं. इस उम्र में भी नहीं है. तो वही. पता नहीं क्या होता है सिनेमा कि जीवन में इतने धक्के खाने के बाद अब भी 'आनन्द' के राजेश खन्ना को देखकर मन भावुक होने लगता है, जबकि बहुत संभावना है स्वयं राजेश खन्ना भी अब खुद को देखकर भावुक न होते होंगे.
सिनेमा सोचते ही 'गाइड' के पीलापन लिए उस पोस्टर का ख़याल आता जिसमें देवानंद के बंधे हाथों वहीदा रहमान का सिर गिरा हुआ है, और वह प्यार की आपसी समझदारी का चरम लगती, इतना अतिंद्रीय कि मन डूबता सा लगे. डूबकर फिर धीमे गुनगुनाने लगे, 'लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में, हाथ न ये छूटेगा, ओ मेरे जीवनसाथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं..' कितने तो रंग होते सिनेमा के. इतने कि बचपन के हाथों पकड़ में न आते. 'जुएलथीफ़' का वह सीन याद आता है? भरी महफ़िल में अशोक कुमार हल्ला मचाते कि झूठ बोलता है ये आदमी, नहीं बोल रहा तो सबके सामने दिखाए कि इसके पैर में छह उंगलियां नहीं हैं? फिर देवानंद दिखाने को धीमे-धीमे अपने जूते की तस्में खोलते, फिर मोज़े पर हाथ जाता, देवानंद का टेंस चेहरा दिखता, महफ़िल के लोगों के रियेक्शन शॉट्स, अशोक कुमार की तनी भौंहें, फिर कैमरा मोज़े पर, धीमे-धीमे नीचे को सरकता, आह, उस तनावबिंधे कसी कटिंग में लगता देवानंद के पैर में पता नहीं कितनी उंगलियां होंगी मगर हम देखनेवालों का हार्ट फेल ज़रूर हो जाएगा! जैसे 'तीसरी कसम' के क्लाइमैक्स में वहीदा के रेल पर चढ़ने और हीरामन के उस मार्मिक क्षण ऐन मौके न पहुंच पाने के खौफ़ में कलेजा लपकता मुंह को आता. एक टीस छूटी रह जाती मन में और फिर कितने-कितने दिन मन के भीतर एक गांठ खोलती और बांधती रहती. फिर 'पाक़ीज़ा' का वह दृश्य.. कौन दृश्य.. आदमी कितने दृश्यों की बात करे? और बात करने के बाद भी कह पाएगा जिसकी उसने सिनेमाघर के अंधेरों में उन क्षणों अनुभूति की? ठाड़े रहियो ओ बांके यार, कहां, चैन से ठाड़े रहने की कोई जगह बची है इस दुनिया में?
चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो.. भाग जायें? छोड़ दें सबकुछ? और उसके बाद?
पता नहीं सिनेमा क्या होता है. सचमुच.
मगर यह सब बहुत पहले के सिनेमा की बातें हैं. टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट से पहले की.
***
इटली के तवियानी भाइयों की 1977 की एक फ़िल्म है, 'पादरे पदरोने', क्रूरता और अशिक्षा की रोटी पर बड़ा हो रहा एक गड़रिया बच्चा. दरअसल किशोर. सार्दिनीया के उजाड़ मैदानों में अपने भेड़ों के पीछे, कुछ उनकी तरह ही बदहवास और अचकचाया हुआ. रास्ता भूले दो मुसाफ़िर उसी मैदान से गुजर रहे हैं. एक के हाथ में खड़खड़ाती साइकिल, दूसरा कंधे से लटकाये अपना अकॉर्डियन बजाता जा रहा है. उस बाजे के स्वर में, उस धुन में, कुछ ऐसी सम्मोहनी है कि गड़रिया किशोर तीरबींधा अपनी जगह जड़ हो जाता है. जड़ माने, जड़. कुछ पलों बाद चेतना लौटती है तो दूर सुन रहे बाजे के जादू में मंत्रमुग्ध पागलों की तरह फिर उसके पीछे भागा-भागा जाता है. अपने दर्शक को संगीत के जादू में, प्रत्यक्ष की उस इंटेंस अनुभूति में बांध लेने, बींध देने की यह अनूठी ताकत, यही है सिनेमा. जिन्होंने फ्रेंच फ़िल्मकार फ्रांसुआ त्रूफो की '400 ब्लोज़' देखी है उन्हें खूब याद होगा फ़िल्म के आखिर का वह लंबा सीक्वेंस जब बच्चा आंतुआं कैद से भागकर ज़्यां कोंस्तांतिन के कभी न भूलनेवाले संगीत की संगत में समुंदर की तरफ दौड़ता है, जीवन के सब तरह के कैदों को धता बताती मुक्ति का जो वह निर्बंध, मार्मिक, आह्लादकारी ऑर्केस्ट्रेशन है वह मन के पोर-पोर खोलकर उसे आत्मा के सब सारे उमंगों में रंग देता है! यह ताक़त है सिनेमा की. और हमेशा से रही है, चार्ली चैप्लिन के दिनों से, और जब तक लोग सिनेमाघरों के अंधेरे में बैठकर फ़िल्में देखते रहेंगे तब तक रहेगी.
मगर रहेगी? क्यों रहेगी? 'गाइड' के राजू को रोजी़ की मोहब्बत तक न बचा सकी, फिर आज की रोज़ी तो आईपीएल के अपने स्टॉक की चिंता में रहती है, किसी राजू और राहुल के मोहब्बत को बचाने की नहीं, फिर किस मोहब्बत के आसरे सिनेमा अपने सपनों को संजोये रखने की ताक़त के सपने देखेगा? देख पाएगा? दिबाकर बनर्जी के 'लव सैक्स और धोखा' में कैसा भी मोहब्बत बचता है? माथे में ऐंठता गुरुदत्त के 'प्यासा' का पुराना गाना बजता है- ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है!
अच्छाई के दिन गए. जीवन में नहीं बचा तो फिर सिनेमा में क्या खाकर बचता. जो बचा है वह पैसा खाकर, या खाने के मोह में बचा है. बॉक्स ऑफिस के अच्छे दिनों की चिंता बची है, अच्छे दिनों की अच्छाई की कहां बची है, क्योंकि आदर्शों को तो बहुत पहले खाकर हजम कर लिया गया. और ऐसा नहीं है कि कुंदन शाह के 'जाने भी दो यारो' में पहली बार हुआ कि सतीश शाह केक की शक्ल में आदर्शों को खाते दीखे, तीसेक साल पहले गुरुदत्त ऑलरेडी उन आदर्शों को फुटबाल की तरह हवा में लात खाता देख गए थे. समझदार निर्माता और बेवकूफ़ दर्शक ही होता है जो मोहल्ले के लफाड़ी किसी मुन्ना भाई की झप्पियों से आश्वस्त होकर मुस्कराने लगता है, या चिरगिल्ले सरलीकरणों के इडियोटिक समाधानों का जोशीला राष्ट्रीय पर्व मनाने, ऑल इज़ वेल को राष्ट्रीय गान बनाने, बजाने लगता है.
कहने का मतलब हम सभी जानते हैं 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना' गाने का मतलब नहीं. जीवन से अच्छाई के गए दिन फिर लौट कर नहीं आते. सिनेमा के झूठ की शक्ल में भी नहीं.
***
झूठ कह रहा हूं. बुरे दिनों की कहानियां अच्छे अंत के नोट पर खत्म होती ही हैं. अच्छे दिन सिनेमा की झूठ की शक्ल में लौटते ही हैं. बार-बार लौटते हैं. न लौटें तो मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा के लौटने की फिर कोई जगह न बचे. श्री 420 से शुरू होकर मिस्टर 840 तक हीरो का अच्छाई पर अंत लौटाये लिये लाना ही हिंदी फ़िल्म में समाज को संदेश है. अच्छे रुमानी भले लोगों का इंटरवल तक किसी बुरे वक़्त के दलदल में उलझ जाना, मगर फिर अंत तक अच्छे कमल-दल की तरह कीचड़ से बाहर निकल आना के झूठे सपने बेचने की ही हिंदी सिनेमा खाता है. एक लातखाये मुल्क में दर्शकों के लिए भी सहूलियत की पुरानी आदत हो गई है. कि लातखाये जीवन में शाहरुख और आमिर के न्यूयॉर्क या मुंबई की जीत को वह बिलासपुर और वैशाली के अपने मनहारे जीवन पर सुपरइंपोज़ करके किसी खोखली खुशहाली के सपनों की उम्मीद में सोये रहें. जीवन में कैसे अच्छा होगा से मुंह चुराते, सिनेमा में अच्छा हो जाएगा को गुनगुनाते सिनेमा में जागे और जीवन में उनींदे रहें.
जबकि सिनेमा, सिनेमा में सोया रहेगा. वह बुरे दिनों के इकहरे, सस्ते अंत के सपने खोज लाएगा, बुरे दिनों की समझदार पड़ताल में उतरने की कोशिश से बचेगा. उसके लिए कितने रास्तों का आख्यान बुनना, कैसी भी जटिलता में पसरना, मुश्किल होगा. क्योंकि अपनी लोकोपकारी (पढ़ें पॉपुलिस्ट) प्रकृति में वह राज खोसला के 'दो रास्ते' के बने-बनाये पिटे रास्ते पर चलना ज़्यादा प्रीफर करेगा, जिसमें लोग, लोग नहीं, कंस और कृष्ण के अतिवादी रंगत में होंगे. अच्छे (बलराज साहनी) और बुरे (प्रेम चोपड़ा) की दो धुरियां होंगी और नायक जो है, हमेशा अच्छे के पक्ष में खड़ा दीखेगा और फ़िल्म का अंत हमेशा 'बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी' के खुशहाल ठुमकों के पीछे अपने को दीप्ति दे लेगी. मतलब राय के बांग्ला 'अरेण्येर दिन रात्री' से परिवेश व जीवन के अंतर्संबंधों की व्याख्या तो वह नहीं ही सीखेगा, गुरुदत्त के 'प्यासा' की पारिवारिक और प्रेम (माला सिन्हा) की भावपूर्ण समीक्षा को भी अपनी अपनी समझ की परम्परा में जोड़ने से बचा ले जाएगा. 'सारा आकाश' और 'पिया का घर' की टीसभरी सफ़र पर निकलनेवाले बासु चटर्जी को चित चुराने और कुछ खट्टा कुछ मीठा बनानेवाले लाइट एंटरटेनर में बदल देगा. मतलब हिंदी सिनेमा में बुरे दिनों का एंटरटेनमेंट बना रहेगा, अच्छे दिनों को पहचानने की समझदारी की उसमें जगह नहीं बनेगी.
***
एक कैमरामैन मित्र मुझसे कहता है इतने वर्षों बाद भी हम वही रामायण वाली कहानी ही कह रहे हैं. रावण को धूल चटाकर रामबाबू सीताबाई के संग अयोध्या लौटे टाइप. मैं खीझकर कहता हूं कुछ महाभारत वाला तत्व भी होगा. मित्र कहता है होगा ही, लेकिन महाभारत की जटिलता हम सीधे मन के टेढ़ों लोगों के लिए अपच पैदा करती है, तो वहां से भी उठाई चीज़ भी भाई लोग रामायण के सांचे में ढालकर ही सुनायेंगे!
एक बड़ा तबका है, बुद्धिभरा तबका भी है, जो हिंदी सिनेमा के हमारी अति विशिष्ट भारतीय शैली के कसीदे गाता है. माने हमें दुनिया से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, हम दुनिया को सीखा देंगे वाला गाना. पिटे हुए मुल्कों में ऐसा अहंकारी राग गानेवाले हमेशा ऐंठे हुए कुछ कैरिकेचर टाइप होते हैं. वे यह तक नहीं मानते कि पिटे हुए हैं. बिना बात रहते-रहते हम तब से लगे हैं जब दुनिया कहीं नहीं थी जैसा डायलॉग बोलने लगते हैं. दम भर सांस लेकर फिर हमीं ने दुनिया को सबसे पहले चेतना, विमान, म्यूजिकल और सपना देखने के अरमान दिये, फिर आप भूलो मत! टाइप चुनौती. ऐसे अति विशिष्टी अहम को फिर कहां कुछ सीखने की ज़रूरत है? भले सिनेमा में अगले हफ़्ते 'मस्ती: पार्ट टू' और 'गोलमाल: पार्ट थ्री' चढ़ रही हो!
सही भी है दुनिया हमसे सीखे, इरान ने आखिर हिंदी फ़िल्में देख-देखकर ही अपने यहां सिनेमा की नींव डाली, और नब्बे के बाद से घूम-घूमकर दुनिया भर के फ़िल्म समारोहों में इनाम पर इनाम बटोर रही है, तो इरान को फ़िल्म बनाना हमने सीखाया नहीं? अच्छा है इनाम बटोर रही है लेकिन हम भी तो पैसा बटोर रहे हैं. और ईनाम भी बटोरा है. डैनी बॉयल का बटोरना और हमारा एक ही बात है. आशुकृपा और कृपादृष्टि तो अंतत: हमारी ही है. जो लंबी यात्रायें की हैं हिंदी सिनेमा ने वह तुम्हारा मलिन मन कहां से देखेगा? कितना बटोरा है इसका कोई अंदाज़ है? शक्ति सामंत और मनमोहन देसाई के ज़माने में रुपल्लियों में बटोरते थे, अब करण जौहर और चोपड़ाओं के दौर में डॉलर और यूरो में बटोर रहे हैं. समूची दुनिया का भट्टा बैठ जाएगा मगर आप सुन लो, हमारा बॉलीवुड फिर भी बैठेगा नहीं, राज करेगा, यू गेट ईट? वी आर लाइक दिस ऑनली!
पश्चिम में भी कुछ तिलकुट इंटैलेक्चुअल टाइप हैं, पीछे कोरस में स्माइल देकर गाते हैं, नथिंग गोन्ना चेंज द वर्ल्ड, दे आर लाइक दिस ऑनली!
***
ये मैं कहां किन ओझाइयों, ओछाइयों में उलझता, गिरता गया हूं? सिनेमा को इतने ओछे स्तर तक उतारते लाने की कोई वज़ह है? जो सलीका और तमीज़ सिनेमा से पाया, उसे इस बेमतलब, पैसातलब नज़रिये के सियाह धुंओं में बिसरा दें? इसी दिन के लिए देखा था व्ही शांताराम की 'माणुस' और महबूब ख़ान की 'रोटी', 'अंदाज़', 'अमर' ? केदार शर्मा की 'जोगन'? उलझी दुनिया को पढ़ने की वह सुलझी नज़र भूल गया? यही दिन देखने के लिए दिलीप साहब ने 'गंगा जमुना' लिखी, पैसे लगाये, नितिन बाबू ने जान झोंककर फ़िल्म खड़ी की? 'बसंत क्या कहेगा' की कहानियां लिखनेवाले बलराज साहनी ने सलीम मिर्जा़ का सबकुछ एक लंबी सांस खींचकर बरदाश्त करते जाने वाला ज़िन्दा किरदार निभाया ('गर्म हवा')?
जीवन में प्रेम हमेशा ज़रूरी नहीं मिले, एक शादी मिल जाती है और उसे निभाना पड़ता है. खुद मैं कितने वर्षों निभाता रहा, चार साल की उम्र रही होगी जब से देखता रहा हिंदी फ़िल्में. 'हरे कांच की चूड़ियां', 'काजल', 'दिल दिया दर्द लिया', 'बीस साल बाद', 'प्यार का मौसम', 'सावन की घटा', 'जब प्यार किसी से होता है', 'दस लाख', 'साथी', 'शागिर्द', 'एक सपेरा एक लुटेरा', 'तुम हसीं मैं जवां'. कुमकुम की 'गंगा की लहरें' और आईएस जौहर की फ़िल्में और राजेश खन्ना का 'बंडलबाज' तक देखी. छुटपन के आवारा भटकन के जो भी हाथ चढ़ता, सब बराबर के श्रद्धाभाव से देखता. परदे पर हरकत करती, घूमती तस्वीरों को फटी आंखों तकने में कोई अपूर्व रोमांच, कोई जादुई अनुभूति मिलती होगी जभी स्कूली पढ़ाई के दौरान एक दौर था पड़ोस की तमिल सोसायटी के माहवारी सोशल ड्रामा और कॉमेडी फ़िल्मों की स्क्रिनिंग में भी भागा पहुंच जाता. मतलब तमिल का बिना एक शब्द समझे नागेश, जेमिनी, शिवाजी गणेशन की करीब सौ फ़िल्में तो उस बचपन में ज़रूर ही देखी होंगी. कहां जानता था कुछ वर्षों बाद विश्वविद्यालय की फ़िल्म सोसायटी की चार सालों की संगत में समांतर सिनेमा की भी सीमायें और बोझिलता गिनाने लगूंगा? हॉलीवुड के जॉन फोर्ड और इलिया कज़ान और फ्रांकेनहाइमर ही नहीं, यूरोप से बाहर, अर्जेंटिना, जापान, कोरिया कहां-कहां तक नज़रें फैलाने लगूंगा?
***
जीवन में जिस तरह के लोगों की संगत बनती है कोई वज़ह होती है कि क्यों बनती है. इनमें मन रमता है तो वह दूसरा क्यों फूटी आंखों नहीं जमता. मुमताज़ को, बबीता और साधना को चाहती होगी पूरी एक दुनिया, लेकिन कोई एक दीवाना मन किसी एक रेहाना सुल्तान में जाकर अटक जाता होगा. करनेवाले संजय, शशी कपूर की चिकनाइयों का ज़िक्र करते होंगे, न करनेवाला शेख़ मुख़्तार को अच्छा बताता होगा. राजेंदर और प्रदीप कुमार की दुनिया में जयंत, मोतीलाल, बलराज साहनी का होना गिनाता होगा. कोई वज़ह होती है दुनिया का हर एक्टर ऑस्कर पाने में अपने पूरे जीवन की कमाई, काम की गिनाई देखता है, हमारी हिंदी इंडस्ट्री के भी ऐसे अमीर हैं जो ऑस्कर की हल्की गुहार पर सब काम छोड़े भागे-भागे हॉलीवुड जाते हैं, मगर फिर कोई मारलन ब्रांडो भी होता है जो ऑस्कर पुरस्कारों को आलू का बोरा बताता है, गोद में आई को बेपरवाही से ठुकराता है. कोई वज़ह होती है लोग जो होते हैं वैसा क्यों होते हैं.
कोई वज़ह होती होगी अपने यहां हीरोगिरी की हवा छोड़ने वाले ढेरों एक्टर मिलते हैं, कोई जॉर्ज क्लूनी या शान पेन नहीं होता जो सिर्फ़ अपने स्टारडम की ही नहीं खाता, समय और अपने समाज के बारे में साफ़ नज़रिया भी बनाता हो. इव्स मोंतों जैसी कोई शख्सीयत नहीं मिलती जिसके चेहरे की हर लकीर, हर भाव बताते कि बंदे ने सख्त, एक समूची ज़िंदगी जी है. दुनिया में डिज़ाइनर कपड़ा पहनने आए थे और टीवी के लिए सजीली मुस्की मुस्कराने की अदाकारियां मिलती हैं, परदा अभिनय की भव्यता और मन जीवन की उस समझ के आगे नत हो जाए, एक्टिंग की जेरार् देपारर्द्यू वाली वह ऊंचाई नहीं मिलती. मारचेल्लो मास्त्रोयान्नी की तरह मन लुभाना ढेरों जानते हैं, मगर विस्कोंती की 'सफ़ेद रातें' और फ़ेल्लीनी की 'आठ और आधे' की महीन वल्नेरिबिलिटी में रुपहले परदे को जीवन से भर सकें का ककहरा अभी तलक नहीं पहचानते. बहुत सारी लड़कियां होंगी कमाल का नाचती हैं, लेकिन जुलियेट बिनोश की तरह कुर्सी पर बैठे-बैठे संवाद बोलना नहीं जानतीं, एडिथ पियाफ़ को परदे पर मारियों कोतियार की तरह भरपूर आत्मा से गा सकें ('ल वियों रोज़'), अभिनय और जीवन के उस विहंगम संसार को दूर-दूर तक नहीं पहचानतीं. कोई तो वज़ह होती है कि सबकुछ वैसा क्यों होता है जैसा वह होता है.
अपने यहां एक्टर चार पैसे कमाकर एक दुबई में और दूसरा अमरीका में फ्लैट खरीदने के पैसे जोड़ता है, दूसरी ओर चिरगिल्ली भूमिकाओं की ज़रा सी कमाई को जॉन कसेवेट्स ऐसी अज़ीज़ फ़िल्मों को बनाने, बुनने में झोंकता है जो फ़िल्म नहीं, लगता है हमसे जीवन की अंतरतम, अंतरंग गुफ़्तगू कर रही हों. तुर्की का स्टार अभिनेता यीलमाज़ गुने अपने विचारों के लिए जेल जाता है, जेल में रहकर फ़िल्में बनाता है, हमारे यहां स्टार होते हैं, राजनीति में वह भी जाते हैं, कभी दूर तो कभी अमर सिंह को पास बुलाते हैं. कोई वज़ह होती होगी कि अपने यहां फ़िल्मों से जुड़े लोगों को हम जो इज़्ज़त देते हैं, क्यों देते हैं.
रोज़ इतने डायरेक्टर पैदा होते रहते हैं, एक सच्चा दिबाकर बनर्जी पैदा होता है, बाकी के कच्चे दरज़ी जाने क्या सिलाई सीलते रहते हैं, क्या वज़ह होती है?
***
आख़िर क्या वज़ह है हिंदी सिनेमा के अरमान इतने फिसड्डी, इतने दो कौड़ी के हैं? ऐसा क्यों होता है कि 'रंग दे बसंती' के कलरफुल फ्लाइट के ठीक अगले कदम वह 'दिल्ली 6' के दिशाहारे मैदान में जाकर ढेर हो जाता है? सिनेमा की अपनी आंतरिक है या यह हिंदी संसार के सपना देख पाने की कूवत के भयावह दलिद्दर की दास्तान है? क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा कि पूरी आधी सदी में एक 'परती परिकथा', एक 'आधा गांव' के साहित्य और आधे 'राग दरबारी' के एंटरटेनमेंट के दम पर एक पूरा समाज अपनी ठकुर सुहाती गाता, ऐंठ के गुमान में इतराता होगा? उसकी अपनी ज़बान में अंतर्राष्ट्रीय तो क्या राष्ट्रीय ख्याति का भी कोई अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री क्यों नहीं की सोचता वह कभी नहीं लजाता? इसलिए कि लोगों को वही सरकार मिलती है जितना पाने के वह काबिल होते हैं? हिंदी का साहित्यकार भी हमें उतना ही साहित्य देता है जितने की राजा राममोहन राय लाइब्रेरी खरीदी कर सके? सौ लोग लेखक को लेखक मानकर पहचानने लगें, साहित्य अकादमी रचना-पाठ के लिए उसे बुला सके, शिमला या बीकानेर की कोई कृशकाय कन्या एक भटके, आह्लादकारी क्षणों में लेखक की तारीफ़ में तीन पत्र लिख मारे कि फिर लेखक उसे पटा सके, आगे का अपना चिरकुट जीवन खुशी-खुशी चला सके?
चंद तिलकुट पुरस्कार और इससे ज़्यादा हिंदी का लेखक यूं भी कहां कुछ चाहता है? प्रूस्त और बोदेलेयर बनने के तो उसके अरमान नहीं ही होते, वॉल्टर बेन्यामिन बनने का तो वह अपने दु:स्वप्न में भी नहीं सोचता, फिर हिंदी सिनेमा ही ऐसी क्यों बौड़म हो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे?
साहित्य को तो साहित्यकार के यार लोग ही हैं जो अपने सिर लिए रहते हैं, हिंदी सिनेमा की दिलदारी का तो व्यापक विस्तार भी है, देश में ही नहीं, समुंदरों पार भी है. बिना कुछ किये, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का हलकान गा-गाकर ही वह सफल बनी हुई है, तो ख्वामख्वाह अपनी सफलता का फॉर्मूला वह क्यों बिगाड़े? चौदह सौ लोगों के बीच के हिंदी साहित्य तक ने जब रिस्क नहीं लिया तो चालीस करोड़ों के बीच घूमनेवाला हिंदी सिनेमा किस सामाजिकता की गरज में अपना बना-बनाया धंधा खराब करे? कोई तुक है? नहीं है.
***
सवाल पूछनेवाले अलबत्ता पूछ सकते हैं इतना किस बात का रोना? क्या ऐसा नहीं है कि हाल के वर्षों में हिंदी सिनेमा ने अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज जैसे फ़िल्मकार दिए हैं? सही है अनुराग की फ़िल्में हताशाओं व जुगुप्साओं के मेलों में भटकती फिरती हैं मगर उतना ही यह भी सही है कि 'देव डी' का अभय देओल इकहरा काठ का पुतला नहीं लगता, कमरे की अराजकता के बीच लाल अंडरवेयर में हम उसे सिर खुजाता देखते हैं, निस्संग, जीवन की नाउम्मीदी से वह किस कदर पका हुआ है के भाव हमेशा उसकी उपस्थिति को रेसोनेट करते हैं. वैसे ही उतना यह भी सही है कि विशाल बंबइया स्टारों के फेर में भले पड़े रहें, मिज़ों सेन सजाना जानते हैं, कहानी अपने को ठीक से भले न कह पाये, फ़िल्म की पैकेजिंग की कला है उनके पास, असमंजस के धुएं में फ़िल्म गहरे अर्थ दे रहा है की गलतफ़हमी भी बनी रहती है, मगर इससे ज़्यादा फिर कोई एक हिंदी फ़िल्मकार से फिर क्या चाहता है?
बहुत पहले की बात है, कुछ वर्षों के लिए मुझे इटली में रहने का सुअवसर मिला था. रफ़्ता-रफ़्ता इतालवी ज़बान पकड़ में आ गई थी, मगर लोग तब भी पकड़ में आने से रह जाते. समाज जो नज़रों के आगे रोज़ दीखता, वह समझ नहीं आता, गो फ़ेल्लीनी साहब की फ़िल्में खूब समझ आतीं, उनके ही रास्ते फिर समाज को समझने और उससे स्नेहिल संबंध बनाने की कुंजी भी मिलती रहती. अपने हिंदी सिनेमा की संगत में जबकि मामला ठीक इसके उल्टा होता है. देश और लोग बाज मर्तबा, लगता है बहुत सारे स्तरों पर, परतों में समझ आते हैं, लेकिन बचपन की पुरानी दीवानगी के बावजूद अब भी हिंदी फ़िल्म में उतरते ही लगता है यहां जाने किस दुनिया की बात हो रही है. और जिस भी दुनिया की हो रही है उसका हमारे रोज़-बरोज़ की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं. समय और समाज को समझने की कुंजी तो वह किसी सूरत में नहीं बनती. यहीं यह सवाल भी निकलता है कि फ़िल्मों से, इन जनरल, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं? जीवन से, सिनेमा के रागात्मक, कलात्मक अनुभव से हम उम्मीदें क्या पालते हैं.
सिनेमा यथार्थ नहीं. फ़ेल्लीनी की फ़िल्में यथार्थ नहीं, सिनेमा के अंधेरों में हमारे अवचेतन से खेलता वह कोई सपनीला जादू है जिसके भीतर उतरकर, कुछ घंटों के लिए हम अपने यथार्थ से एक नए तरह के संवाद में जाते हैं, और उस यथार्थ को समृद्ध करने की एक नयी ताक़त लिए सिनेमाघर से बाहर आते हैं, ऐसा कुछ?
स्पेन के होसे लुईस गेरीन की 2007 की अपेक्षाकृत गुमनाम सी फ़िल्म है, 'इन द सिटी ऑफ़ सिल्वी', चौरासी मिनट की फ़िल्म में कुल जमा पांच-सात मिनट के संवाद होंगे, बाकी जो है नौजवान पर्यटक नायक की नज़रों- कुछ वर्षों पहले घटित किसी मीठी मुलाक़ात की महीन याद की दुबारा 'खोज' के बहाने अजाने शहर में भटकने, 'देखने' का अंतरंग भावलोक है. कैमरे की आंख से जगह विशेष में लोगों का यह उनकी आन्तरिकता में 'दिखना'; कामनाओं, अनुभूति, जुगुप्साओं की यह दबी-छुपी ताकझांक खास सिनेमाई रसानुभव है और वह किसी अन्य कला-माध्यम से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता था.
अमरीकी निर्देशक रॉबर्ट ऑल्टमैन की एक म्यूज़िकल है, 1975 में बनी थी, 'नैशविल'. राष्ट्रपति के चुनाव अभियान वाला मौसम है, नैशविल के छोटे शहर में राजनीतिक गहमा-गहमी के दिन हैं. कंट्री और गॉस्पल संगीत से जुड़़े लोगों की दुनिया में ज़रा समय को घूमती (159 मिनट की अवधि) इस फ़िल्म में तकरीबन 24 मुख्य किरदार हैं, चूंकि गवैयों की दुनिया है सो घंटे भर का वक़्र्त उनके परफ़ॉरमेंस व गाने का है, जाने कितनी सारी स्टोरीलाइन है. ऑवरलैपिंग संवादों का साउंडट्रैक है और फ़िल्म इतने सारे स्तरों पर चलती है कि कभी भरम होता है आप फ़िल्म नहीं देख रहे, बाल्जाक का उपन्यास पढ़ रहे हैं.
अर्थशून्य जीवन में प्रेम चला आये तो वह ऐसी ही सघन नाटकीय अपेक्षाओं की लड़ी बुनने लगता है. फिर सरल सिनेमा के देश में तरल वाचन की प्रत्याशाएं जीवन को खामख्वाह मुश्किल बनाने लगती हैं.
***
सवाल फिर वही है सिनेमा से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं? क्या चाहते हैं? स्वयं सिनेमा हमसे क्या चाहता है? महज़ क्या 'कूल' हैं की एक बार और आश्वस्ति चाहते हैं? या ज़रा और उदार, महात्वाकांक्षी होकर इच्छाओं, कामनाओं के एक सघन ऐंद्रिक अनुभव से गुज़रना भर चाहते हैं? और सिनेमा? अपने अंधेरों-उजालों के जादू में बांधकर जीवन जैसा ही कुछ दीखते किस यथार्थ के पीछे अवचेतन की कैसी यात्राओं पर हमें वह लिए जाना चाहती है? सिनेमाघर से बाहर के जटिल यथार्थ को समझने में वह किसी भी तरह से हमारी मदद करती है? लेकिन हम 'प्यार बांटते चलो' गाना चाहते हैं, किसने कहा जटिल यथार्थ का बाजा सुनना चाहते हैं?
1974 की जॉन कैसेवेट्स की अमरीकी फ़िल्म है, 'ए वुमन अंडर द इन्फ्लुयेंस'. बिना किसी भावुकता के प्रेम और परिवार की ही अंतर्कथा ही है, और बहुत धीमे-धीमे बहुत गहरे धंसती चलती है. बहुत सारे तारे हैं और सब ज़मीन पर ही गिरे हैं मगर फ़िल्मकार उसका रंगीन पोस्टर सजाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता, जीवन की ज़रा और मार्मिक समझदारी हम आपस में शेयर कर सकें, जैसे कभी कोई मार्मिक नाट्य-मंचन कर ले जाता है, फ़िल्म वैसी ही कुछ हमसे अपेक्षा करती है, और प्रेम व परिवार की अपनी समझ में हम थोड़ा और अमीर होकर फ़िल्म से बाहर आते हैं.
कुछ वैसी ही अर्जेंटिना के पाब्लो त्रापेरो की फ़िल्म है, 'फमिलिया रोदांते' (रोलिंग फैमिली, 2004), सुदूर देहात में किसी बिसराये रिश्तेदार के यहां शादी का न्यौता है जहां पहुंचने के लिए एक बुढ़िया अपने सब बेटी, बेटा इकट्ठा करती है, और एक खड़खड़िया खस्ताहाल वैन में पूरा कुनबा सुदूर देहात के सफ़र पर निकलता है. हमारे लिए वह सफ़र अपने समय और पारिवारी बुनावट को समझने की मार्मिक कथा बनती है.
अर्जेंटिना की ही एक अन्य महिला निर्देशक, लुक्रेसिया मारतेल की 2001 की फ़िल्म है, 'ला सियेनागा', या जापान के मिवा निशिकावा की 2009 की फ़िल्म, 'डियर डॉक्टर', जो ऊपरी तौर पर नितांत साधारण सी दिखती- परिवार, परिवेश और उस समाज की कथा भर लगे, मगर फिर बड़े धीरज और करीने से हमारे आगे उसके भीतरी गांठों को एक-एक करके खोलती चले. आपस में बांटी गई संगत की यह समझ भी सिनेमा की अपनी विशिष्ट ताक़त है, खेद कि हिंदी सिनेमा के पास नहीं है.
***
पांचवे दशक के आखिर तक (और कुछ-कुछ छठवें दशक के शुरुआती दौर में भी खिंचे जाते हुए) रही थी हिंदी फ़िल्मों की अपनी एक सामाजिकता, सौद्देश्यता. उसके बाद लगता है, शनै-शनै देश ने जैसे जान लिया कि आज़ादी का ठीक मतलब जो भी है, जीवन की खुशहाली के लिए बहुत नहीं है, और आदर्शवादी सपनों की जैसे-जैसे हवा निकलती गई, वैसे-वैसे हिंदी सिनेमा कैमरे से अपने परिवेश की पड़ताल करने की बजाय शंकर जयकिशन व ओपी नय्यर के संगीत पर सवार पहाड़ोन्मुखी होता गया. नितिन बोस, केदार शर्मा, व्ही शांताराम, बाबू महबूब ख़ान, बिमल रॉय पीछे छूटते गए. शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत का पहाड़ी वादियों में जीप पर घूमना और स्की पर फिसलना चालू हो गया. पीछे-पीछे बाबू राजेशजी खन्ना आए तो उन्हें 'मेरे सपनों की रानी' गवाने के लिए शक्ति सामंत श्रीनगर की बजाय दार्जिलिंग लिवाये गए. गनीमत है अमिताभ तक ड्रामा फिर पहाड़ से हटकर वापस बंबई और नज़दीक के मैदानों में लौटा, लेकिन वह ज़मीन पर लौटी है के नाटकीय सलीम-जावेद वाले डायलॉगबाजी में भले लौटी, कायदे से ज़मीन पर कहां लौटती? सुपरहीरो और सुपर ड्रामा की दुनिया थी, अंतत: 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है' ही गाती, समाज को अपने साथ कहां, किधर लेकर जाती? कहीं नहीं गई. नब्बे के दशक में, 'हम आपके हैं कौन' के बाद से बड़ी तसल्ली से शादी के वीडियो छापने लगी. दुनिया आंख फाड़-फाड़ कर देखती रही हिंदुस्तानी शादियां क्या अनूठी चीज़ हैं, हिंदुस्तानी परिवार कैसी लाजवाब संस्था है. फिर जैसे इतना प्रहसन काफ़ी न हो, आगे शादियां और अनूठे पारिवारिक प्रसंग भी सीधे लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्ट कर दिये गए. दलिद्दर देश के कंगले रुपल्ली से हाथ झाड़कर सीधे डॉलर और स्टर्लिंग से हाथ जोड़ लिया गया.
भावुकता के उद्रेक में मैंने अतिशयता की थोड़ी ज़्यादा भोंडी तस्वीर खींच दी होगी, मगर कमोबेश आजा़दी के बाद के पांच दशक हिंदी सिनेमा जिन रास्तों चली कुछ इसी तरह का उसका स्थूल वनलाइनर समअप है. अब इस समअप में समाज को देखने की सचमुच कहां गुंजाइश निकलती है? काफी नहीं है कि अभी भी बीच-बीच में ऐसी फ़िल्में बन जा रही हैं जिसकी शूटिंग जोहानसबर्ग और ज्युरिख़ की बजाय हिंदुस्तान में ही कहीं हो जाती है?
सच्चाई है हिंदी सिनेमा का दरअसल अपना कोई समाज है नहीं. पंजाबी, राजस्थानी, बंबई सबकी मिलाजुली पॉटपूरी है, कोई एक ऐसा भूगोल नहीं जिसे केंद्र में करके कहानी घूम रही है. अब चूंकि जब केंद्र ही नहीं है तो फ़िल्म फ़ोकस कहां होगी? बेचारी नहीं हो पाती और यहां और उसके बाद वहां फुदकती रहती है. बीच में जब असमंजस बढ़ जाता है और बात भूल जाती है कि फ़िल्म की कहानी दरअसल थी किसके बारे में तो एक गाना और कॉमेडी का सीन डल जाता है. उसके बाद भी बना रहे, असमंजस, तो पूरी यूनिट घबराकर विदेश चली जाती है, कि शायद विदेशी लोकेल फ़िल्म में अर्थवत्ता फूंक सकें!
***
कोई वज़ह होगी, मगर जो भी है सोचनेवालों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि अमरीकी फ़िल्मों की नकल से थके हुए हमारी हिंदी सिनेमा के दरजी नयेपन की गरज में, फिर चोरी के लिए फ्रांस तो कभी हॉंगकांग और ताइवान की तरफ़ नज़र दौड़ाते हैं, क्यों दौड़ाते हैं? इरान, कोरिया, चीन ही नहीं, बांग्लादेश और वियतनाम तक अपने परिवेश की कथा बुनकर मार्मिक फ़िल्में खड़ी कर लेते हैं, बस यह हिंदी सिनेमा का ही निर्देशक है जो लगातार अपनी जी हुई सच्चाइयों से मुंह चुराता, दिल्ली का होकर गुजरात और मुंबई का बंगाली बच्चा फिर राजस्थान अपनी शूटिंग सजाने जाता है. ऐसा क्यों है कि लोग वही कहानी कहते जो जीवन में उन्होंने जीया है? इसलिए कि उनके पास ज़िंदगी है लेकिन उसके जीये की कहानी नहीं? मम्मीजी की गोद में वे अमिताभ और रेखा का नाचना और श्रीदेवी का फुदकना देखते हुए बड़े हुए? फ़िल्म बनाना चाहते हैं और बनाते रहेंगे इसलिए नहीं कि कहानियां कहने को हैं, बल्कि इसलिए कि एक पिटे हुए समाज में ऐश और स्टारडम के नशे में जीने की वही एक इकलौती जगह दिखती है?
हिंदी का हर निर्देशक दो फ़िल्में बनाने के बाद तीसरी बड़े स्टार के साथ बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है, भई? इसलिए कि फ़िल्म को एक्सपोज़र मिल जाता है, बाज़ार बनाने में आसानी हो जाती है. तो वही बात है. बाद में बाज़ार और निर्देशक के निजी जीवन की बेहतरी ही बनती रहती है, फ़िल्म की बेहतरी का सवाल पीछे कहीं पृष्ठभूमि में छूट जाता है. दिक़्क़त वही है, अपने यहां लोगों के मन में चिंता फ़िल्मों की बेहतरी से ज़्यादा जीवन को सेट कर लेने की है. जैसे हिंदी साहित्यकार की चिंता अपने साहित्य से ज़्यादा साहित्य अकादमी से अपने संबंधों की है.
***
जून्हो बॉंग की 2003 की एक कोरियन फ़िल्म है 'मेमरीज़ ऑफ़ मर्डर'. जो दर्शक रामगोपाल वर्मा की 'सत्या', 'कंपनी' और 'सरकार' देखकर दांत में हाथ डालते रहे हैं, उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए. एक कस्बाई शहर में एक के बाद एक हत्यायें हुई हैं और स्थानीय पुलिस हत्यारे की पहचान में माथा फोड़ रही है. मगर उसमें कोई हिरोइकपना या नाटकीयता नहीं. पुलिस की नौकरी में लगे किरदारों की अपने जीवन के टंटे हैं, केस की जटिलता में थकते अधिकारी एक कमज़ोर, अर्द्ध-विक्षिप्त को फांसकर उसे हत्यारे की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं, मगर मामला फिर और उलझता जाता है. राजधानी सेओल से मामले की तफ़तीश को आया अपेक्षाकृत ज़्यादा शिक्षित एक दूसरा अफ़सर अचानक समझता है उसकी खोज रंग लाई, असल हत्यारे की उसने पहचान कर ली है, मगर वहां जीवन का एक अन्य घाव खुलता है, असल हत्यारे की पहचान नहीं होती. असल हत्यारे की पहचान फ़िल्म के आखिर तक नहीं होती, और हमारे मन में कड़वा सा कोई स्वाद छूटा रह जाता है, जैसा बहुधा जीवन में होता है, मसले सॉल्व नहीं होते, हमेशा कथार्सिस की मुक्ति नहीं होती.
एक दूसरी फ़िल्म है, हिंदी में है, अभी तक अनरिलीज़्ड, बेला नेगी की उनकी पहली, 'दायें या बायें'. उत्तराखंड की दुनिया में खुलती है. नायक मुंबई से अपने गांव लौटा है. मगर वह औसत नायकों की तरह का नायक नहीं, उसके जिज्ञासु बेटा है, शहराती अरमानों वाली बीवी है, टीवी देख-देखकर अपना सपना बुनती साली है, कंधे के झोले में कलेजा लिये घूमता बचपन का यार है, गांव का पूरा उबड़-खाबड़ जाने कितने परतों में खुल रहा, बदलता संसार है, और फ़िल्म नायक के बहाने इन सबकी कहानियों में उतरती है. इकहरी कथा कहने की जगह मल्टीपल लेवल पर नैरेटिव खोलती चलती है. वह सब आसानी से करती लिये जाती है जो कांख-कांखकर भी कोई बड़ा बंबइया फ़िल्म निर्देशक नहीं कर पाता, और ठहरकर सोचिए तो सोचते हुए यह बात भी सन्न करती है कि समझदारी भरा यह काम एक लड़की की पहली फ़िल्म है.
***
कहने का मतलब अपने परिवेश को केंद्र में रखकर फ़िल्में बन सकती हैं. और कलात्मक फ़िल्मों का दुखड़ा रोती, बिना देह पर उनका जामा डाले बन सकती हैं. दिबाकर बनर्जी की अब तक की बनाई तीनों फ़िल्में इसका अच्छा उदाहरण हैं कि धौंस और धमक में बन सकती हैं. एक के बाद एक क्रियेटिव उछालें ले सकती हैं. समाज की सच्चाइयों को सांड़ के सींग पर उठाकर चौतरफ़ा चक्कर घुमवा सकती हैं. हां, उसके लिए अपने समाज के प्रति वैसी ही करुणा, समझ और दिल की उछाल चाहिए. जिगरा. चाहिए. दिबाकर ने दिखा दिया है कि यह सब हो तो समाज में अच्छे सिनेमा की जगह है. इस पतित समय में भी. हिंदी सिनेमा के गिरे संसार में भी!
'खोसला का घोंसला' में ही कहीं-कहीं प्रियदर्शन टाइप फिल्मी तत्व हैं, मगर पहली फ़िल्म के नर्वस असमंजस के लिए उन्हें नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए, दूसरी, 'ओये लकी, लकी ओये' से दिबाकर जैसे अपना सुर साधने लगते हैं. अपने बचपन की जानी-पहचानी दिल्लीवाली दुनिया के पोर-पोर की उनको पहचान है, उसके चिथड़े वह सिरे से सजाते चलते हैं. सब घर में ठेल लेने की कामनाओं में, भूख की बदहाली और आत्मा की तंगहाली एक चोर की नहीं, समूचे समाज की कहानी होने लगती है. उस चोरमन समाज के बीच घूमते हुए दिखता है कि चोरी पर जी रहा फ़िल्म का नायक ही इकलौता रिडेम्प्टिव कैरेक्टर है. बाकी जो तथाकथित शरीफ़, धुले हुए हैं वह इस मूल्यहीन, पतित संसार के सबसे बड़े अधम हैं. वह दुनिया उदास करती है, मगर अपने समय और समाज की समझ में हमें ज़रा बड़ा भी कर जाती है. समांतर सिनेमा की तरह सिनेमाघर से हम डिप्रैस हुए बाहर नहीं निकलते.
दिबाकर की तीसरी फ़िल्म, 'लव, सैक्स और धोखा' में कहीं और ज़्यादा क्रियेटिव छलांग है, अबकी वह अपेक्षाकृत पहचाने अभय देओल जैसे किसी स्टार चेहरे के फेर में भी नहीं पड़ती. दरअसल पारंपरिक तरीके से किसी को नायकत्व देती भी नहीं. समाज के नंगे हमाम में कैमरा लेकर उतरती है, जहां पारंपरिक कैमरावर्क की पॉलिशिंग और कंफर्ट तक नहीं है, और मनोरंजक तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि आंखों के आगे जिस समाज के दृश्य खुलते हैं, वह सिर से पैर तक बीमारियों में रंगी है, अपने दो कौड़ी के फौरी स्वार्थों से अलग उसकी आत्मा खाली है. खोखली. कहीं कोई वह सामाजिकता की करुणा, आपसी बंधाव नहीं है जो इस पिटी दुनिया का किसी तरह बेड़ा पार लगायेगा, मालूम नहीं इस हालत में भीतर से पूरी तरह जर्जर यह समाज फिर कहां जाएगा? एक बार फिर, इतनी उदास दुनिया है, मगर मन डिप्रैस नहीं होता. अपने घटियापे में लोग विलेन नहीं लगते, विलेन वह समाज दीखता है जिसमें अपने फ़ायदे के होड़ ने सबकी यह दुर्गति, परिणति की है. और जिस तरह से अभिनेताओं का इस्तेमाल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गहरे जुड़े संवादों का, और सबके बावज़ूद (फ़िल्म के टाइटल से अलग) कहीं कोई नाटकीयता नहीं, आप फ़िल्म देखकर सोचते हैं और आपका मन लाज़वाब हुआ जाता है.
हिंदी सिनेमा अब भी संभावना है. शाबास दिबाकर!
***
दिसम्बर 1995 में तब फ़ैशन पत्रिका, फ्रेंच 'एल' के ज़्यां दोमीनीक बोबी एडिटर इन चीफ़ थे, जब एक मैसिव स्ट्रोक के बाद पूरी तरह पैरालाईज़्ड हो गए. सारे अंग बेमतलब हुए, सिर्फ़ उनकी आंख, एक आंख, अपना काम करती रही. अस्पताल के बिस्तरे से लगे, उस आंख के सहारे ही उन्होंने अपने संस्मरण डिक्टेट कराये, उसकी किताब तैयार हुई. 'द डाईविंग बेल ऐन्ड द बटरफ्लाई' उसी किताब पर आधारित जुलियेन श्नाबेल की 2007 की फ़िल्म है. डाईविंग बेल, माने पानी की अतल गहराई में ऐसे डूबना जिससे बाहर सिर्फ आंख से दिखते उजाले की चौंध भर ही हो. और बटरफ्लाई? मन की ऐसी उड़ान जो शरीर के कैद से किसी पंछी के गहरे आसमान में निकल पड़ना हो जैसे, अंतहीन विस्तार. एक आंख से देखी दुनिया की यादों के उमंगों की, हृदयविदारक कहानी है फ़िल्म. एक ही समय में मार्मिक और अदम्य जिजीविषा की कहानी जो अपने तरल क्राफ्ट में लगभग एक विज़ुअल कविता सी बहती रहती है, या कहें कि निर्देशक जुलियन श्नाबेल की पेंटिंग जैसी..
एक पैरालाईज़्ड लेखक के बायोपिक को इतना जीवंत, कोमल और जिजीविषा के स्वप्निल रंगों में पेंट करते जाना आसान नहीं रहा होगा. जैसा कि ज़्यां दो ने अपनी किताब में कहा है कि अब मैं खदबदाती स्मृतियों की कला सीख रहा हूं, श्नाबेल की फ़िल्म उस खदबदाहट को एक अलौकिक आश्चर्यलोक में बदलता-सा चलती है. इतने सारे तक़लीफ़ों के नीचे दबा जीवन भी कैसी उमंग और दीप्तिमय कविता होती रह सकती है 'द डाईविंग बेल ऐन्ड द बटरफ्लाई' लगातार हमें उन ऊंचाइयों तक लिये जाता है.
कविता की ऊंचाइयां, समझ की गहराइयों तक, उड़ने, उड़ाये जाने का काम बखूबी करती है सिनेमा, सवाल है फ़िल्म बनानेवाला निर्देशक जीवन से, व अपने माध्यम से ऐसे गहरे संबंध रखता हो, फ़िल्म देखनेवाले दर्शक सिनेमा में जीवन को मार्मिकता से उतरता देखने का मान, ऐसे अरमान रखते हों..
***
किसी सपनीले लोक में, गाढ़े अंधेरों की गहिन दुनिया में चमकते जुगनुओं सी चमकीली, एकदम पास-पास, फिर भी हाथ न आती रौशनी.. दिलफ़रेब ख़्वाब कोई.. मनहारे अंधेरों में छुपी किसी रौशन दुनिया का अव्यक्त अहसास बना रहे.. नमी, एक ताप कोई बना रहे.. अजाने वाद्य के किसी अनूठे संगीतबंध सा जीवन की उलझी परतें एक-एक करके खुलती रहें.. और यह खुलना किसी जादू से कम न हो.. वैसे ही जैसे मर्मस्पर्शी नितांत अंतरंग क्षणों में जीवन का साक्षात् करना.. जीवन को उसके समूचे ताप में, आत्मा के गहिन माप में जीना, और सृजनशीलता को.. कितना सुंदर हो सकेगा सिनेमा.. हो सकेगा, ज़रूर.. बशर्ते उसे बनानेवाला जानता हो मन के धन, बिछे धूल के मणि-कण.. अपनी ज़मीन को पहचानता हो, उसकी अंतरंग विद्युत तरंगों को.. और इन सब को जोड़ने वाले उस तार को और ये कि जो जितना सरल है उतना ही गूढ़ है और इसी के बीच न दिखने वाली कोई बहती नदी की धार है जो सिर्फ अपने होने भर से उस सरल दुरूह में कोई ऐसा मायने भर जाती है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, कोई नाटक नहीं होता.. और ये कि उस सिनेमा को देखने वाला दर्शक भी किसी अबूझ प्रक्रिया से उस कहानी की गहराईयों और ऊंचाइयों में ठीक उसी सुर में डूबे जैसे कोई अदृश्य सूत्र से सब बंधे हों. सिनेमा फिर जीवन को उसकी पूरी सच्चाई में, उसके समूचेपन में खोल देने का ज़रिया हो.. कि लो देखो यही जीवन है अपने समस्त जीवंत रंगों में, अपनी समूची मार्मिकता में. यही जीवन है यही तो इसलिये सिनेमा भी है.. या होना चाहिये..
अप्रैल, 2010
(ज़रा अनजान, नई पहचान के एक नौजवान की चिरौरी पर यह लेखनुमा जो भी चीज़ है, लिखी थी. कुछ गल्प जैसा बंधता चले का आग्रह था, मगर लिखे को पाकर नौजवान मित्र खुश होने की जगह कातर होते रहे, कि लय नहीं है, लुत्फ़ नहीं है, आदि. उन्हें पसन्द न आया, उनके पास वजह होगी. कुछ समय तक लेख मेरे पास पड़ा रहा, फिर किन्हीं दूसरे मित्र की कृपा से लख़नऊ से छपनेवाली एक पत्रिका 'लमही' के पास पहुंचा, उनकी कृपा हुई, लेख वहां जुलाई-सितम्बर के अंक में छपा जैसा सुन रहा हूं, स्वयं पत्रिका अभी मैंने देखी नहीं है. जो बंधुवर धीरज से आखिर तक लेख निकाल जायेंगे, उनकी हिम्मत की दाद दिये देता हूं)
महंगाईः व्यवस्था का झूठ और जनता का यथार्थ
Posted by Reyaz-ul-haque on 7/15/2010 07:45:00 PMरविभूषण
प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी एक कविता 'महंगाई' में महंगाई घटाने में 'राजतंत्र' के असमर्थ होने की बात कही है. 70 के दशक के आरंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार थी. उस समय केंद्र में कांग्रेस की अकेली सत्ता थी. आज केंद्र में संप्रग की सरकार है. कांग्रेस के साथ उसके अन्य सहयोगी दल हैं. राजनीति में अब स्थितियां बदल चुकी हैं. उस समय केदारनाथ अग्रवाल ने 'लोकतंत्र' नहीं 'राजतंत्र' का प्रयोग किया था. वास्तविक लोकतंत्र और छद्म या दिखावटी लोकतंत्र में अंतर है. महंगाई आज कहीं अधिक ज्यादा है और प्रायः सभी राजनीतिक दल कांग्रेसी संस्कृति से प्रभावित हैं. प्रेरित-संचालित भले न हों. एक सप्ताह पहले (5 जुलाई) का भारत बंद एक लंबे समय के बाद संपन्न-सफल हुआ. इस बंद में दो-चार विपक्षी दलों को छोड कर सभी विपक्षी दल एक साथ थे. भाजपा व वामदलों के साथ के कारण वामदलों की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल भी उठाये गये. अब वामदलों ने भाजपा से अपने को अलग कर लिया है. पेट्रोलियम की मूल्य-वृद्धि और महंगाई के मुद्दे पर दो अलग विचारधाराओं के दल कुछ समय के लिए ही एक साथ हुए. सांप्रदायिकता के प्रश्न को बार-बार उठाना सही है क्योंकि भाजपा की विचारधारा उससे जुडी है, पर सबसे बडा प्रश्न जीवनयापन का है. एक समय था, जब समाजवादी 'दाम बांधो आंदोलन' चलाते थे. अब तो कहीं 'काम दो आंदोलन' भी नहीं है. 'बंद' और 'आंदोलन' में अंतर है. बंद ज्यादा नहीं खिंच सकता, जबकि आंदोलन लंबे समय तक चलता है. आंदोलन में व्यापक जन-समुदाय की भागीदारी होती है. बंद में ऐसा नहीं होता. स्वतः स्फूर्त बंद के अब कम उदाहरण हैं. बंद से शहरी जीवन प्रभावित होता है, न कि ग्रामीण जीवन. बंद का संबंध भय से भी हैं. बंद में उपद्रवी तत्व भी होते हैं, जिनका उपद्रवी राजनीति से किसी-न-किसी रूप में संबंध होता है. बंद में तोड-फोड की घटनाएं भी होती हैं. बंद होता कम है, कराया अधिक जाता है. आंदोलन सरकार के अतिरिक्त तंत्र को भी प्रभावित करता है. बंद का अपना तर्क और समाजशास्त्र भी है. जेपी आंदोलन के बाद कोई आंदोलन व्यापक स्तर पर नहीं हुआ. भारत बंद की घटनाएं भी विगत दो दशकों में नगण्य हैं. 5 जुलाई 2010 के भारत बंद की सफलता के बाद भी क्या पेट्रोल, डीजल आदि की मूल्य-वृद्धि घटेगी? संसद के मानसून सत्र के आरंभ केपूर्व का यह बंद प्रतीकात्मक है. 12 घंटे के भारत बंद से क्या सरकार सचमुच महंगाई पर पुनर्विचार करेगी?
विपक्षी दलों के कई नेताओं ने यह कहा था कि यह बंद बहरी सरकार को सुनाने के लिए है. बहरी सरकार को सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था. ब्रिटिश सरकार बहरी थी, पर स्वतंत्र भारत की सरकार भी क्या सचमुच बहरी नहीं है? हकीकत यह है कि हमारे देश की सरकार शहरी होने के कारण बहरी है. भारत की कुल एक अरब 16 करोड़ की जनसंख्या में से आज भी शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? भारत की अधिसंख्य आबादी आज भी गांवों में रहती है. शहरों में भी साधारण जनों व दैनिक मजदूरों की एक संख्या है. महंगाई का सीधा संबंध सामान्य जन से है. भारतीय नागरिकों की आज कई कोटियां हैं. भ्रष्टाचारी-सदाचारी, पूंजीपति-किसान-श्रमिक, संपन्न-विपन्न, शिक्षित-अशिक्षित सभी भारतीय हैं. भारत बंद में विपक्ष की एकता मात्र 12 घंटे की थी. क्या ऐसी एकता से सत्ताधारी वर्ग और शासक पर कोई प्रभाव पडता है? सरकार बहरी ही नहीं, अंधी भी है. वह न सामान्य जन को देखना चाहती है, न उसकी आवाज सुनना चाहती है. विपक्षी दल महंगाईको सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखता है. क्या विपक्षी दलों की आर्थिक नीतियां सचमुच सरकारी आर्थिक नीतियों से भिन्न है? क्या सचमुच विपक्षी दल महंगाई के खिलाफ सडक से संसद तक केवल आवाज उठाने में नहीं, सार्थक ढंग से उसे सही मुकाम तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहेगा? क्या सचमुच वह चार-पांच गुना वेतन-भत्तादि की वृद्धि को नामंजूर करेगा?
समाज का एक तबका, जिसमें अब मीडिया भी शामिल है, बंद के दुष्प्रभावों की बात करता है- विशेषतः बंद होने से होनेवाला आर्थिक नुकसान. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद से 13 हजार करोड़ के आर्थिक नुकसान की बात कही है. संख्या में थोडा-बहुत जो भी फर्क हो, पर आर्थिक नुकसान की बात करनेवालों के साथ मीडिया भी है. इन सबके अनुसार बंद बंद होना चाहिए. इनकी बात करनेवाले सामान्य जनों की बातें कम करते हैं. एक दिन का बंद किसे परेशान करता है? क्या गांवों और सामान्य कस्बों में भी बंद का असर होता है. सरकारें अब सामान्य भाषा नहीं सुनतीं वे दबाव की भाषा से, जिसके कई रूप हैं, प्रभावित होती हैं. अभी अर्थशास्त्री विवेकओबेराय ने अपने एक लेख 'प्राइस ऑफ ए बंद' (इंडियन एक्सप्रेस, 9 जुलाई 2010) में 2009-10 के सकल घरेलू उत्पाद का वर्तमान मूल्य 57,91,268 करोड़ बताया है. उनके अनुसार 2010-11 का सकल घरेलू उत्पाद 65,15,177 करोड़ होगा. इस हिसाब से एक दिन का सकल घरेलू उत्पादन 17,849 करोड़ रुपये होगा. यह माना जा सकता है कि एक दिन के बंद से इतनी राशि का नुकसान हुआ. विवेक ओबेराय ने अपने देश में वर्ष भर के अवकाश दिवस की चर्चा की है. सामान्य तौर पर 50 अवकाश-दिवस हैं. वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार यह संख्या 11 होनी चाहिए. अर्थात 39 अवकाश दिवस अधिक हैं. इसका नुकसान एक वर्ष में 696111 करोड़ रुपये है, जो सप्ताह के अंतिम दो दिवसों को छोडने के बाद है. विवेक देवराय के इस कथन से सबकी सहमति होगी कि बंद शहरी फेनोमेना है. उनके अनुसार भारत में दैनिक मजदूरों की संख्या एक करोड़ 40 लाख है और स्वयं नियुक्त दो करोड़ 10 लाख हैं. पहली श्रेणी के लोगों की दैनिक आय प्रतिदिन सौ रुपये है. बंद से इनके 140 करोड़ रुपये और दूसरी श्रेणी के लोगों की 420 करोड़ रुपये अर्थात कुल 560 करोड़ रुपये कीहानि होती है. उनके अनुसार बंद से किसी भी तरह 250 करोड़ से अधिक का नुकसान नहीं होता.
प्रश्न बंद के समर्थन व विरोध का नहीं है. इससे शायद ही किसी को असहमति होगी कि बंद से शहरी जीवन प्रभावित होता है. अब किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता गांवों से कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता है. राजनीतिक दलों के आयोजन शहर केंद्रित हो गये हैं. नेताओं की जीवन शैलियां बदल चुकी हैं. उनका जन प्रतिनिधि रहना एक बडा झूठ है. सरकार को केवल चुनाव के समय जनता से मतलब होता है. वे जनोन्मुखी नहीं, बाजारोन्मुखी हैं. लोकसभा में तीन सौ से अधिक सांसद करोड़पति हैं. किस तर्क से उन्हें गरीबों और बेरोजगारों का प्रतिनिधि कहा जायेगा? बंद एक अभिव्यक्ति है, दबाव है, प्रतीक है, जिसका संबंध व्यापक जन समूह से नहीं है. वेतन-वृद्धि का भी मूल्य वृद्धि से संबंध है. 80-90 करोड़ की जनता के लिए महंगाई का जो अर्थ है, वही अर्थ 10-20 करोड़ लोगों के लिए नहीं है. नौकरी करनेवालों का वेतन पांच-10 वर्ष बाद बढता है. वर्ष में दो-चार बार महंगाई भत्ता बढता चलता है. यह वर्ग सरकार और व्यवस्था के साथ है. भारतीय मध्यवर्ग अपनी सकारात्मक-विधेयात्मक भूमिका त्याग चुका है. वह महंगाई से प्रभावित नहीं है. सरकार भयावह भारतीय यथार्थ को देखना नहीं चाहती. एक दिन का भारत बंद उसे परेशान करता है. जबकि इसका कोई बडा प्रभाव नहीं पडता. बंद कई कारणों से होते हैं. धार्मिक कारणों से होनेवाले बंद और सामाजार्थिक कारणों से होनेवाले 'बंदों' में अंतर है. राजनीतिक दल वास्तविक विपक्ष की भूमिका में नहीं हैं. संसद में वे अपनी वास्तविक भूमिका का कम निर्वाह करते हैं. संसद और सडक, दोनों ही जगहों में विरोध जरूरी है.
कैसे मिले मानसिक हिंसा से छुटकारा?
Posted by Reyaz-ul-haque on 7/14/2010 07:12:00 PMबीते सप्ताह फ्रांस की संसद ने परिवार के भीतर, मानसिक हिंसा रोकने के लिए विधेयक पारित किया। आज दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में तनाव, हिंसा और युद्ध की चीख़ें गूंज रही हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी का वादा अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए पल भर के लिए भी सुकूनदेह साबित नहीं हो रहा है। ईरान पर आक्रमण करने की अमरीकी मुहिम में इसरायल अपनी निर्णायक सहमति दे चुका है और क्षेत्रीय हथकंडे की भूमिका में उतरने को तैयार है। और इराक़ में भूख से मरने वाले बच्चों की तादाद में कमी होने के आसार कम ही दिख रहे हैं। कई विश्लेषकों की राय है कि पश्चिमी यूरोप में रूस और अमरीकी टकराव ज़ोर पकड़ रहा है। उज़्बेकिस्तान में महीने भर पहले दो समुदायों के बीच हुए खूंनी टकराव आगामी युद्धमोर्चे के पार्श्व सूचक हैं।
इसे हम 'सभ्यताओं के' अनिवार्य 'टकराव' की आक्रमणकारी संज्ञा नहीं दे सकते। आर्थिक मोर्चे पर ज़ारी संकट दुनिया के लिए रोज़ नई विपदाएं लेकर हाज़िर हो रहे हैं। पखवाड़े भर पहले ज़ारी हुई संयुक्त राष्ट्र की 'सहस्त्राब्दी विकास परियोजना' की सालाना समीक्षा साफ़ कहती है कि पूरी दुनिया में भूख और बेरोज़गारी का मारक स्तर बढ़ रहा है। ख़ासतौर से, दक्षिण एशिया में भूख का वर्तमान स्तर १९९० के दशक के सूचकांक के क़रीब पहुंच गया है। इस रपट के सार के अनुसार, 'विकसित' देश, आर्थिक भहराव से तभी उबर सकते हैं जब 'कम विकसित' और 'विकासशील' देशों की व्यापक आबादी के रहन सहन में उन्नति के अवसरों की गांठें खुलेंगी। यह रिपोर्ट २०१५ तक दुनिया की एक तिहाई आबादी को भूख और वंचना से मुक्त करने की दिशा में सरकारों की अक्षम कार्ययोजना की ओर भी ध्यान दिलाती है।
हमारे अपने देश में मंहगाई का तक़लीफ़देह बुख़ार रोज़ी रोटी पर तेज़ी से अपना असर दिखा रहा है। आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए अब नमक-रोटी जुटा पाने के मौसमी ठिकानों की खोज मुश्किल और टेढ़ा मेढ़ा अभियान साबित होने जा रहा है। निर्धन और निर्धनतम जिस नाउम्मीदी के अनचाहे और आसान शिकार बन रहे हैं वह उन्हें सामूहिक तौर पर ऐतिहासिक त्रासदियों की ओर ले जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी से पहले ही दैनंदिन ज़रुरतों की चीज़ों की सर्वसुलभता की डोर खींची जा चुकी है। वंचित और निर्धनतम आबादी के राजनीतिक अधिकारों को टिकाऊ बनाने के लिए 'मुख्यधारा' की पार्टियों में न्यूनतम रचनात्मक दिलचस्पी का सुखाड़, फैलती आग में गाढ़े घी का काम कर रहा है।
ऐसे में, गांधी, रस्किन, क्रोपटिकन जैसे चिंतकों और जे सी कुमारप्पा जैसे अर्थशास्त्री, भविष्य के वादों को गढ़ने के उपक्रमों के लिए एक बार फिर बेहद प्रासंगिक हो चले हैं। जॉन रस्किन की भविष्यदृष्टा किताब 'अन टू द लास्ट' के परिचय में वालजी गोविंदजी देसाई लिखते हैं, 'नैतिकता, दुनिया की सभी आस्थाओं में अति-आवश्यक ऊपादान होती है, लेकिन हमारी सहज बुद्धि, धर्म के दायरे के बाहर, हमें सुझाती है कि नैतिकता के क़ानून के निरीक्षण की ज़रूरत है। हालांकि, ख़ुद को धर्म की परंपरागत व्याख्या से परे मानने वाले चिंतक क्रोपटिकन को 'नैतिक संत' की संज्ञा दी गई है।
आज, जबकि सारी दुनिया की विशाल आबादी कुपोषण, भूख, बेरोज़गारी और तीखे होते सामुदायिक टकरावों की समुद्र-चक्की में फंसी हुई है तो मानसिक हिंसा के बारीक़ चक्रों को समझने की कोशिश, दिन में आकाशगंगा की लकीरें खोजने जैसी है। फ्रांस के निरंतर गतिशील समाज में मानसिक हिंसा की व्याख्या और क़ानून को संसदीय मान्यता शायद इसलिए मिल रही है क्योंकि वहां चिंतन के क्षितिज में नित नए आयाम उद्घाटित होते रहे हैं। १९वीं और २०वीं सदी में इन धारणाओं की प्रामाणिक पुष्टि के उत्पादक बीज मिलते हैं।
हमारे अपने देश में, कश्मीर, उत्तरपूर्व सहित मध्य भारत के कई इलाकों में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कहीं हिंसा की मरूभूमि दिखती है तो कहीं लोग टोही शिकार की तरह मारे जा रहे हैं। समाज के ज़रुरी शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संक्रमण के विचार-स्वप्न का अभाव भविष्य की भरोसेमंद पगडंडी को जगह जगह छील रहा है।
विभिन्न राजनीतिक धाराओं की वैचारिक आस्थाओं में नैतिकता के क़ानून, चिल्लर पैसों की तरह चलन से बाहर होते जा रहे हैं। पेशेवर ईमानदारी के पैमाने जिस मायूसी और अनिच्छा से लागू होते हैं, उनसे बेहतर भविष्य बुनने में धीमी आंच महसूसना ख़याली पुलाव ज़्यादा है। बढ़ती शहरी आबादी को रेलम-भाग ज़िंदगी के जिस अजूबे और अजनबीपन से साना जा रहा है, उसके किरचन की आवाज़ के लिए कोई सूकूनदेह और खुली जगह कम ही बन पा रही है और आमफ़हम-सी दिखने वाली ज़िंदगियों की तहों में व्याप्त गोरखधंधे, आकंठ भ्रष्टाचार से लथपथ व्यवस्था के लिए सहज ग्राह्य हैं।
सामुदायिक संस्कृति को उन्नत और अधिक मानवीय बनाने के हमारे अधिकतर राजनीतिक दलों के उपकरण घिस-पिट चुके हैं। 'वोट प्रबंधन' की अंतहीन गणित अब आम जन जल्दी समझने लगे हैं। निर्धनतम और वंचित समुदायों को १०० दिवसीय रोज़ी रोटी की गारंटी के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन सौंपना ही होगा। फिर, इस प्रक्रिया को अधिकतम किस अवधि तक हवा में लटकाया जा सकता है? वरना, देश में गृहयुद्ध की आग तो पहले ही कम नहीं धधक रही है।
ऐसे में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के पहले उद्घोषक देश फ्रांस की संसद में पारिवारिक रिश्तों और आपसी संबंधों में समानता के धरातल-निर्माण की यह कोशिश मामूली ही सही लेकिन एक उत्साहजनक मिसाल है।
लेखक हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में मीडिया के शोधार्थी हैं।
--
Palash Biswas
Pl Read:
http://nandigramunited-banga.blogspot.com/


 | Posted in »
| Posted in » 

































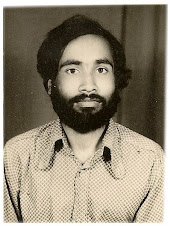

No comments:
Post a Comment