लेखक वस्तुत: अपनी भाषा का आदिवासी होता है
♦ उदय प्रकाश
15 फरवरी 2011 को यह वक्तव्य मैंने लिखा था। तकनीकी असुविधाओं के बावजूद इसे आज अपने गांव में लगा रहा हूं। साहित्य अकादमी पुरस्कार का यह औपचारिक 'स्वीकार-वक्तव्य' था: उदय प्रकाश
मुझसे कहा गया है कि मुझे साहित्य अकादेमी द्वारा 'मोहन दास' को दिये गये पुरस्कार को स्वीकार करते हुए, इस संदर्भ में अपनी ओर से कुछ कहना है। यह एक परंपरा रही है। मेरे असमंजस और दुविधा की शुरूआत ही यहीं से होती है। मैं क्या कहूं?
˜मुझे लिखते-पढ़ते हुए कई दशक हो चुके हैं। लिखने की शुरूआत बचपन से ही कर दी थी, जब खड़ी हिंदी बोली ठीक ढंग से आती भी नहीं थी। तब कभी यह सोचा नहीं था कि इसी भाषा में एक दिन सिर्फ लेखक बनना है। ऐसा लेखक, जिसकी सामाजिक अस्मिता और जीवन का आधार किसी एक भाषा में लिखने तक ही सीमित होकर रहता है। रोलां बाथ जिसे 'पेपर बीइंग' कहते थे। तरह-तरह के कागजों़ पर स्याही में लिखे या छपे अक्षरों-शब्दों में, उन्ही के जरिये किसी तरह अपना अस्तित्व बनाता हुआ प्राणी। आज के समय में वे होते तो कहते आधिभौतिक आभासी व्योम में द्युतिमान अक्षर या शब्द के द्वारा अपने होने को प्रमाणित करता कोई अस्तित्व। यानी 'कहीं नहीं' में 'कहीं होता' कोई अ-प्राणी। 'ए वर्चुअल नॉनबीइंग।' यानी 'ए सोशल नथिंग।' किसी अप्रकाशित को महाशून्य में प्रकाशित करने की माया रचता भासमान अनागरिक। आकाशचारी 'नेटजन'।
˜बचपन जैसा असुरक्षित और भटकावों से भरा रहा, उसे देखते हुए, आकांक्षा यही थी कि आगे चलकर एक सुरक्षित और अपेक्षाकृत स्थिर वास्तविक जीवन मिले। इसके लिए वास्तविक कोशिश भी की। परिश्रम किया। परीक्षाओं में अंक अच्छे लाए। यह सारा प्रयत्न उसी भाषा में किया, जिसमें लेखक के रूप में उपस्थित और जीवित रहता था। सोचा कोई नौकरी मिल जाएगी तो वास्तविक जीवन गुज़र जाएगा। समाज-परिवार की जिम्मेदारी निभ जाएगी। किसी मध्यवर्गीय नागरिक की तरह। फिर एक समय, जब युवा होने की दहलीज़ पर ही था, यह लगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। इतना आत्मकेंद्रित क्या होना? जो किताबें पढ़ता था, उनसे भी यही प्रेरणा मिलती थी कि अपने समय को अधिक न्यायपूर्ण, सुंदर, मानवीय और उत्तरदायी बनाना चाहिए। इतिहास ऐसे प्रयत्नों के बारे में, उन प्रयत्नों की सफलताओं-असफलताओं के बारे में बताता था। उपन्यास, कविताएं, दर्शन, विज्ञान और मानविकी की तमाम पुस्तकों में ऐसे संकेत और विवरण थे। कलाएं भी इसका उदाहरण बनती थीं। नितांत अकेलेपन और एकांतिक पलों में उपजने वाली भाषिक-वाचिक अभिव्यक्तियों या अन्य कलाओं में भी यह प्रयत्न दिखाई देता था। लेकिन इन सबमें सबसे प्रगट और शायद अधिक ठोस, साफ और आसान-सा उपक्रम जहां दिखता था, उसे राजनीति या सामाजिक कर्म कहते हैं। तो मैं उधर भी गया। इस सबके पीछे ऐसा लगता है कि कोई महान मानवीय-सामाजिक कार्य करने, बड़ा परिवर्तन लाने का कोई आत्मबलिदानी आदर्श या क्रांतिकारी लक्ष्य किसी समय रहा होगा। जिस पीढ़ी का मैं था, वह पीढ़ी ही कुछ-कुछ ऐसी थी।
˜आज इस उम्र में, इतनी दूर आकर कह सकता हूं, कि शायद वह सारा प्रयत्न भी मेरी अपनी ही सुरक्षा और अस्तित्व की चिंता से जुड़ा हुआ था। एक स्तर पर वह कहीं गहराई से व्यक्तिगत भी था। शायद हम किसी भी परिवर्तन की कोशिश में तभी सम्मिलित होते हैं, जब हम उसमें स्वयं अपनी मुक्ति और अपनी स्थितियों में बदलाव देखते-पाते हैं। मेरे पास भाषा और अपने शरीर के अलावा कोई दूसरा साधन और ऐसा माध्यम नहीं था, जिससे मैं दूसरों, और इस तरह अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा सामाजिक प्रयत्न कर सकता। तो एक दीर्घ समय तक, बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े हिस्से को, मैंने वहीं खर्च किया। यही सोचते हुए कि एक ऐसे समाज और समय में, जिसमें मेरे जैसे अन्य सभी सुरक्षित और स्वतंत्र होंगे, उसमें मैं भी स्वतंत्रता और नागरिक वैयक्तिक गरिमा के साथ रह सकूंगा।
˜आज इतने वर्षों के बाद भी मुझे लगता है कि मैं इस भाषा, जो कि हिंदी है, के भीतर, रहते-लिखते हुए, वही काम अब भी निरंतर कर रहा हूं। जब कि जिन्हें इस काम को भाषेतर या व्यावहारिक सामाजिक धरातल पर संगठित और सामूहिक तरीके से करना था, उसे उन्होंने तज दिया है। इसके लिए दोषी किसी को ठहराना सही नहीं होगा। वह समूची सभ्यता का आकस्मिक स्तब्धकारी बदलाव था। मनुष्यता के प्रति प्रतिज्ञाओं से विचलन की यह परिघटना संभवतः पूंजी और तकनीक की ताकत से अनुचर बना डाली गई सभ्यता का छल था। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में कई-कई बार ऐसा हुआ है कि सबसे आखीर में, जब सारा शोर, नाट्य और प्रपंच अपना अर्थ और अपनी विश्वसनीयता खो देता है, तब हमेशा इस सबसे दूर खड़ा, अपने निर्वासन, दंड, अवमानना और असुरक्षा में घिरा वह अकेला कोई लेखक ही होता है, जो करुणा, नैतिकता और न्याय के पक्ष में किसी एकालाप या स्वगत में बोलता रहता है। या कागज़ पर कुछ लिखता रहता है। किसी परित्यक्त अनागरिक होते जाते बूढ़े की अनंत बुदबुदाहट, कभी किसी पुरानी स्मृतियों के कोहरे और अंधंरे से निकलती और कभी किसी स्वप्न के बारे में संभाव्य-सा कुछ इशारा करती। इसे 'सॉलीलाक्वीस' कहते हैं। मैं ज़रा-सा भाग्यशाली इसलिए हूं कि इस स्वगत को सुनने वाले बहुत से लोग मुझे अपनी ही नहीं, दूसरी अन्य भाषाओं में भी मिल गये हैं। इसमें हमारे अपने देश की भी भाषाएं हैं और दूसरे कुछ देशों की भी।
˜एक प्रश्न हमेशा मेरे सामने आ खड़ा होता है। वह यह कि जिस धरती पर मैं भौतिक रूप से रहता हूं, जिस शहर, समाज या राज्य में, उसका मालिक आखिर कौन है? किसका आधिपत्य उस पर है? किसी नागरिक, प्रजा या मनुष्य के रूप में उस मालिक ने मुझे कितनी स्वतंत्रता दे रखी है? उसकी हदबंदियां और ज़ंजीरें कहां-कहां हैं? और ठीक इसी से जुड़ा हुआ, इसी प्रश्न के साथ, इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा भी सामने आ जाता है कि जिस भाषा में मैं लिखता हूं, उस भाषा का मालिक कौन है? वह कौन सी सत्ता है, जिसके अधीन यह भाषा है? जैसा मैंने अभी कहा, लेखक और कुछ नहीं, भाषा में ही अपना अस्तित्व हासिल करता कोई प्राणी होता है। भाषा ही उसका कार्यक्षेत्र, उसका देश , उसका घर और उसका अंतरिक्ष होती है। उसकी संपूर्ण सत्ता भाषा में ही अंतर्निहित होती हैं। लेकिन मैंने अक्सर पाया है कि भाषा और भूगोल, या शब्द और राज्य, दोनों को अपने अधीन बनाने वाली सत्ता एक ही होती है। कई तरह के प्रतिपक्षी और प्रतिभिन्न पाठों में प्रकट होते शब्दाडंबरों या डेमॉगागी के आर-पार वर्चस्व की वही संरचनाएं रहती हैं, जो किसी धरती के नागरिक या किसी भाषा के लेखक की स्वतंत्रता को नियंत्रित, अनुकूलित या अधीन करती हैं। हर तरह की ऐसी सत्ता, मुझे अनिवार्य रूप से लगता है कि अपने मूल चरित्र में सर्वसत्तावादी होती है। इतिहास ने और मेरे अपने ही जीवन की स्मृतियों और अनुभवों ने इस धारणा को पुष्ट ही किया है। यह सत्ता राज्य-व्यवस्था ही नहीं, किसी भी भाषा में विनिर्मित उन विचार-सरणियों को भी अधिगृहीत कर लेती हैं, जिनमें सबकी मुक्ति की कोई संभावना होती है। पिछले दो-ढाई दशकों के मेरे अनुभवों और संज्ञान ने यह बोध मुझे दिया है। इसीलिए, जिस भाषा में मैं लिखता और रहता हूं, वह मेरे लिए, सिर्फ 'हिंदी' नहीं रह जाती। वह जीवन और यथार्थ का एक ऐसा जटिल प्रश्न बन कर उपस्थित होती है, जिसे किसी कथा या कविता या अपने किसी बयान में कहता हुआ मैं सत्ताओं के संदेह के घेरे में अक्सर आता रहता हूं।
इसके बाद इस जगह मैं चुप रहूंगा।
˜मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पिछली सदी के ठीक बीतते ही, जब सब नयी सहस्राब्दी के स्वागत की मुद्रा में थे, मैंने एक लंबी प्रेमकथा लिखी थी -'पीली छतरी वाली लड़की'। आप अगर ध्यान दें, तो लोकरंजक सरलता के उस सहज पाठ में भाषा और मनुष्य का गहरा अनुचिंतन और विखंडन एक साथ विन्यस्त था। अपने नये कविता संग्रह-'एक भाषा हुआ करती है' का भी ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हो जाने की अस्मिता हासिल होने के बाद उसकी स्वतंत्रता किसी भी जातीय, सांप्रदायिक, धार्मिक, लैंगिक या राजनीतिक या डेमॉगागिक वर्चस्व से नियंत्रित होती ही है। हर लेखक को, अगर उसने अन्य अस्मिताओं के सारे आवरण और कवच उतार दिये हैं और उसके पास अपने जीवन और अपने आत्म की रक्षा के लिए भाषा के अतिरिक्त कोई दूसरा उपकरण नहीं बचा है, तो उसे हमेशा अपनी इस पराधीनता या औपनिवेशीकरण से मुक्ति का प्रयत्न करना ही पड़ता है।
˜मेरा यह भी मानना है और इसे मैं पिछले लंबे अर्से से कहता आ रहा हूं कि लेखक वस्तुतः अपनी भाषा का मूलनिवासी या आदिवासी होता है। उसकी भाषा ही उसका जल, जंगल, ज़मीन और जीवन हुआ करता है। किसी लालच या अन्य उन्माद में सभ्यताएं हमेशा किन्हीं आदिवासियों को उसके स्थान से विस्थापित करती आयी हैं। यह सिर्फ किसी कोलंबस का ऐतिहासिक वृत्तांत भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सर्वव्यापी सच है, जो आज तक देखी-जानी गई हर तरह की सत्ता-संरचना को शर्मशार कर सकती है। आज जब मैं यहां आपके सामने अपना यह वक्तव्य पढ़ रहा हूं, उस समय आप सब देख रहे हैं कि पूंजी और तकनीक की ताकतों के साथ जुड़ी लोभ की सत्ता ने किस व्यापक पैमाने पर हिंसा और संवेदनहीनता के साथ निरस्त्र मूलनिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ना शुरू किया है। यह एक तरह का सभ्यता का उन्माद है। एक ऐसा मनोरोग जो किसी खास जगह नहीं, बल्कि संसार के सभी वंचित, वध्य, सत्ताहीन और शांत-अहिंसक मूलनिवासियों के जीवन में 'होलोकास्ट' पैदा कर रहा है। कई साल पहले मिशेल फूको की किताब -'सभ्यता और उन्माद' पढ़ी थी, उसे इस डरावने ढंग से प्रमाणित होते आज हम अपने सामने देख रहे हैं।
भाषा भी पूंजी और तकनीक के साथ जुड़ी लोभी सत्ता-संरचनाओं की चपेट में है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। उतना समय भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि भाषा भी अब एक जिंस और एक उत्पाद भर मान ली गई है और इससे जुड़े जितने भी अकादेमिक, व्यापारिक और राजकीय उद्यम हैं, किसी सचमुच स्वतन्त्र नागरिक लेखक की उसमें कहीं कोई जगह नहीं है। वह विस्थापन के ठीक उसी बिंदु पर है, जिसमें हमारे समय की वंचित मूलनिवासी मनुष्यता है।
˜मैं साहित्य अकादेमी को धन्यवाद देता हूं और उस निर्णायक मंडल के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिसने मेरी लंबी कहानी या आख्यान 'मोहन दास' को यह सम्मान दिया। जाहिर है, कोई भी पुरस्कार किसी भाषा और भूमि में किसी मनुष्य का पुनर्वास तो नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी खुशी यहां प्रकट करता हूं।
यह खुशी इसलिए अर्थ रखती है कि इस राज्य के एक नागरिक के रूप में मैं कुछ अपेक्षाकृत सुरक्षित-सा अनुभव कर रहा हूं।
आप सबका हृदय से आभार।
(उदय प्रकाश। मशहूर कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार। कई कृतियों के अंग्रेजी, जर्मन, जापानी एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध। लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में रचनाएं अनूदित। 'उपरांत' और 'मोहन दास' के नाम से इनकी कहानियों पर फीचर फिल्में भी बन चुकी हैं। उनसे udayprakash05@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
http://mohallalive.com/2013/04/25/uday-prakash-speech-on-the-occasion-of-sahitya-academy-award/






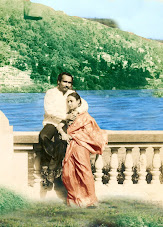












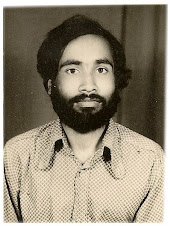

No comments:
Post a Comment