कुछ तो ख़ता, कुछ ख़ब्त भी है
लोकतंत्र है। अर्थतंत्र है। भेंड़तंत्र है। भीड़तंत्र है। लूटतंत्र है। सर्वत्र फैला ढोंगतंत्र है। यंत्रवाद है। बौद्धिक साम्राज्यवाद है। सियासी वितंडावाद है। भोगवाद है। विकासवाद है। समाजवाद है। पूंजीवाद है। संचार युग है। मीडिया है। बाज़ार है। सराय है। यानी जो कुछ है- प्रचुर है। कोई खुशी तो कोई गम में चूर है। जिसके पास नहीं है, वह मजबूर है। जिसके पास है, वह मग़रूर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नहीं है। यंत्र-तंत्र, व्यवस्था, पैरोकार, बिचौलिए, सरदार, सरकार, नेता, सत्ता, कुर्सी, मंत्री, संतरी, चोर, पहरेदार…
यानी सबकुछ तो उपलब्ध है। अपनी सुविधा से चुनिए, गुनिए या फिर सिर धुनिए। कहीं कोई छवि धूमिल है, कहीं कोई चमकदार है। अव्यवस्था है। आतंकवाद है। राष्ट्रभक्त हैं, गद्दार हैं। पुलिस है, सेना है। नक्सली हैं, मुठभेड़ है। कहीं कोई शहीद तो कहीं कोई ढेर है। न्याय है, अन्याय है। हत्या है, बलात्कार है। कहीं रौब है तो कहीं अत्याचार है। शहर है, सभ्य है। गांव है, गंवार है। अच्छी है, बुरी है, लूली है, लंगड़ी है, कमज़ोर है, मज़बूत है, जैसी भी है लोकतांत्रिक सरकार है। कहीं वाहवाही है, कहीं किरकिरी है। यानी हींग है, हर्रे है, फिटकिरी है।
कहने को तो सबकुछ है। लेकिन पता नहीं क्यों, अक्सर कमी ही महसूस होती रही है। दोस्तों का आरोप कि बात-बात में मीन-मेख निकालने वाले पेशे का आदमी, भला अच्छाई देखे तो देखे कैसे! सोहबत भी रही तो शब्दों से, संवेदनाओं से और रही-सही कसर विचारधारा ने पूरी कर दी। बाज़ार फैलने लगा तो सांस्कृतिक विचलन का ख़ौफ़। औद्योगीकरण की बात उठी तो ज़मीन छिन जाने का भय। आबादी बढ़ी तो रोजगार का संकट। स्कूलों की खस्ता हालत। बच्चों में कुपोषण। महिलाओं में एनीमिया। पुरुषों में हाईपर टेंशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत। कल-कारखाने खुलने लगे। गाड़ियां बढ़ने लगीं। सड़कें चौड़ी होने लगीं तो प्रदूषण का डर, बिचौलियों की धमक, सरकारी खजाने की लूट-खसोट, कमीशन, रिश्वत, रोटी, रोना और न जाने क्या-क्या…। मानो ज़िन्दगी, ज़िन्दगी न रही, ख़बर हो गई।
देश बढ़ने लगा, बाज़ार खुलने लगे तो परंपरागत पेशों पर संकट मंडराया, झंडा बुलंद। सड़क नहीं थी, मरीज़ अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया, झंडा बुलंद। सड़क बनने लगी, लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण और झंडा बुलंद। यानी कहीं, कोई भी ऐसा काम या कदम नहीं, जहां झंडा बुलंद करने की ज़रूरत नहीं हो। देश ने मीडिया क्रांति देखी। इसकी अच्छाइयां देखीं। इसकी ताक़त देखी। ओछी हरकतें भी देखीं और दोरंगी नीति भी देख ली। सोझो दिख्यो, ओछो दिख्यो। कोई बात नहीं। कल का इज्ज़तदार पत्रकार, आज का ज़लील-कमीन पत्रकार। बदलता ही रहा है, जीवन से लेकर जगत तक, बारी-बारी एक-एक मुहावरा लगातार।
बातें अटपटी लग रही होंगी। लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां कुछ भी संभव है और अगर आपको अटपटी लगती है तो ये आपके पिछड़ेपन की निशानी है। हम शब्दों के मूल अर्थ का क़त्ल करने में माहिर हैं। आपको याद होगा, कभी एकाध आतंकवादी पकड़ाते थे। लोग सुनकर भौंचक रह जाते थे। हमने इस शब्द को इतना घिस दिया है कि अब आतंकवाद मामूली लगने लगा है। वैसे ख़ौफ़ को पैदा तो हमने इसलिए किया था कि आप डरें और हमारी बकवास सुनें। लेकिन हमने इतना डराया कि अब आप चौंकते नहीं, बदन में झुरझुरी नहीं आती। हमने शुरू में ही आपको इतना डरा दिया था कि अब आपके जहन-ओ-दिल से डर ही निकल गया। पुलिस ने भी कुछ कम कमाल नहीं किए, हमारे इस नेक काम में उसने भी पूरा साथ निभाया है और हर दूसरा टुटपुंजिया आज के दौर में आतंकवादी करार दे दिया जाता है।
हम देशभक्त हैं। भ्रष्टाचार में लिथड़े नेता की चापलूसी कर सकते हैं। नफ़रत के बीज बो सकते हैं। लूट सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। ये नया मुहावरा है। मीडिया ने गढ़ा है। जैसे राष्ट्रवाद का एक मुहावरा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गढ़ रखा है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं रहे। शब्दों का जो स्टॉक हमारे पास है, वो बहुत कम है। ख़बरों का दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने उसे भी संकुचित कर दिया है। ख़बर वही है, जिसके बहाने आप स्टूडियो में खड़े एंकर नाम के प्राणी को चीखने पर मजबूर कर सकें। एंकर वही बेहतर है, जिसमें छोटी-छोटी घटनाओं पर भी बेवजह चीखने की क्षमता हो। वो क्या बोलता है, क्या पूछता है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है? ये सब बेकार के सवाल हैं। चीख़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको ठिठकने पर मजबूर करती है। ऐसी धारणा अब आम हो चली है कि तेज़ और शानदार चीख़ को टीआरपी की भीख मिलती है।
मीडिया समाजसेवा का सशक्त माध्यम है। पता नहीं ये अवधारणा किसकी है, लेकिन जिसकी भी है, उसका वास्तविक जीवन-जगत से कोई संबंध नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य तो यही कि मीडिया का गहरा नाता बाज़ार से रहा है। 1929 में जब विश्व महान आर्थिक मंदी का शिकार था। उस वक्त बाज़ार को हिम्मत-ढाढ़स बंधाने का पुनीत कार्य रेडियो ने किया था। जबकि बाज़ार की चमक और रौनक द्वितीय विश्व युद्ध से लौटी थी। इतिहासकारों ने इन चीज़ों को बड़ी गहराई से देखा, जांचा, परखा और लिखा है। लिहाजा इस पर कुछ ज्यादा लिखने-कहने की ज़रूरत नहीं है।
हमारा बुद्धिजीवी तबका अक्सर ये शिकायत करता है कि मीडिया में साहित्य को जगह नहीं मिलती। पहले जहां अख़बारों का संपादन साहित्यिक हस्तियों के हाथ हुआ करता था। अब वहां मार्केट फ्रेंडली लोगों को बिठाया जाता है। साहित्य, समाज और सियासी समझ से संपादन कौशल का अब कुछ ज्यादा लेना-देना नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक की तो ख़ैर बात ही छोड़ दें, अब प्रिंट में भी साहित्य के लिए बमुश्किल ही जगह निकल पाती है। लेकिन ये शिकायत कितनी जायज़ है? सभी जानते हैं, बाजारीकरण और दिखने-बिकने की नयी संस्कृति ने बहुत सी अहम चीज़ों को जबरन नेपथ्य में धकेल दिया है। साहित्य भी उन्हीं में से एक है। वैसे भी लिखने वाले में छपने की भूख होनी चाहिए, दिखने की नहीं।
अख़बारों ने बेरुख़ी अख्तियार कर ली है। सच है, लेकिन लघु पत्रिकाओं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ब्लॉग्स ने इस कमी को भलिभांति दूर करने की कोशिश की है और ये बात बिल्कुल सच है कि साहित्य को प्रचार-प्रसार के लिए पहले से ज्यादा सशक्त माध्यम आज उपलब्ध हैं। साहित्य का पाठक और टीवी का दर्शक, चारित्रिक स्तर पर बिल्कुल अलग-अलग है। फिर भी टीवी से शिकायत! जिन्हें ये शिकायत है, वह ये भूल जाते हैं कि टीवी देखने-दिखाने की चीज़ है। टीवी तस्वीरों का जंगल है। साहित्य शब्दों का बाग़ीचा। कहीं कोई मेल ही नहीं है। फिर भी शिकायत!!
शिकायतें कितनी जायज़ हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जवाब ढूंढने की फुर्सत किसे है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम दिखाना है। दिखाया वही जाएगा जो दिखने लायक़ होगा, जो बिकने लायक़ होगा। लेकिन पता नहीं क्यों जो लोग लिखने वाले हैं, वह भी दिखना चाहते हैं। ये बड़े ही अजीब किस्म की भूख है। लिखने वाले को छपने की भूख होती थी। लेकिन अब वक्त के साथ सोच बदली है और वो दिखना चाहते हैं। दिखाओ तो अच्छे हो, नहीं दिखाओ तो पता नहीं क्या-क्या दिखाते रहते हैं! टीवी एक से डेढ़ मिनट का पैकेज डिमांड करती है। मुद्दों की बात करती है। कहानी पढ़ने के लिए है, सुनाने के लिए है। दिखाने के लिए नहीं। गंभीर कहानी या कविता का पाठक तो हो सकता है, दर्शक नहीं होता। साहित्य को टेलीविज़न की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी ख़बरों में ही साहित्य को जगह की दरकार क्यों है? सवाल वाजिब है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। जवाब देंगे नहीं।
कटरीना का ठुमका। करीना की नज़ाकत। जेनेलिया की शरारत। लता की आवाज़। ए आर रहमान का म्यूज़िक। दिखाने-सुनाने के लिए ये सब क्या कम हैं जो टीवी वाले बुड्ढे साहित्यकारों, आलोचकों से स्क्रीन को भरने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करें? मीडिया ने थोड़ी न समाजसेवा या कि साहित्य सेवा का ठेका ले रखा है! मीडिया ने तो अरसा पहले चीखना शुरू कर दिया था और चीख़-चीख़ कर ये कह दिया था कि हमारे यहां वही चलेगा जो लोग देखेंगे। मसलन नेताओं के बीच लाईव थुक्कम-फजीहत, तू-तू, मैं-मैं, राखी का स्वयंवर, गोविंदा का थप्पड़ और नेताओं पर लोगों की चप्पल। इससे फुर्सत मिली तो बलात्कार, अवैध सम्बंधों की वजह से हत्या या फिर प्रेमी-प्रेमिका का घर परित्याग या फिर मजनूं की सरे-राह पिटाई। कुछ भी तो अघोषित नहीं है। फिर हाय-तौबा क्यों?
टीवी की भाषा को लेकर चकल्लस क्यों..? शब्दों पर आप जाते ही क्यों हैं..? क्या मालिकों ने चैनल की बागडोर भाषाविदों को सौंप रखी है? जी, नहीं आप मुग़ालते में न रहें। टीवी दृश्य माध्यम है। यहां दृश्य ही शब्द हैं। दृश्य ही भाव हैं। एंकर तो बस गूंगापन दूर करने के लिए है, चीखने के लिए है। अगर आप किसी एंकर से विषय की गहराई या ख़बर की बारीकी की उम्मीद रखते हैं तो इसमें बेचारे एंकर का क्या कसूर?
मीडिया अपनी राह से भटका नहीं है। वह वही कर रहा है, जो करने की जिम्मेदारी उस पर है, जो वह करना चाहता है। लक्स कोज़ी, नैपकीन, टॉयलेट सोप, कंघी, नेकलेस से लेकर चड्डी-बनियान और अब तो नेल पॉलिश तक दिख-बिक रहा है। सरकार को झुकाने के लिए, मास को जगाने के लिए, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट के हित साधन के लिए.., मीडिया जो कर सकता है, कर तो रहा है। टीवी को देखने-समझने के लिए नज़र से ज्यादा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। माध्यम कोई भी ग़लत नहीं होता, चुनाव सही-ग़लत हो सकता है। लिहाजा चुनने में सावधानी बरतें। रिमोट तो आप ही के हाथ में है। कंटेट पर नाक-भौं मत सिकोड़िए, चैनल बदलिए।
अकबर रिजवी, लेखक युवा पत्रकार हैं, ई टी वी और दूरदर्शन न्यूज़ में कार्य कर चुके हैं, बकौल उनके -"मामूली सा इन्सान, जिसे आजकल आम आदमी कहने का चलन है। नंगी सच्चाइयों से वाकिफ़ हूं। अंदर तिलमिलाहट है। चाहता हूं, झूठ पर पड़े गाढ़े पर्दे को तार-तार कर दूं। इधर-उधर कर दूं। लेकिन …"






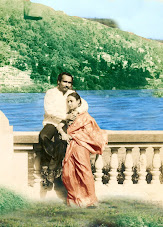












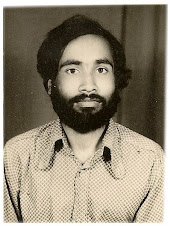

No comments:
Post a Comment