अपूर्वानंद
जनसत्ता 14 जनवरी, 2012 : पटना में प्रेमचंद रंगशाला का जनता के लिए खोला जाना राष्ट्रीय महत्त्व की घटना नहीं मालूम पडेगी। अगर यह कहा जाए कि इसके फिर से खोले जाने की कहानी का प्रेस की आजादी के संघर्ष से गहरा रिश्ता है तो शायद पाठकों को ताज्जुब होगा। लेकिन इसके बनने, बंद होने, सैन्यबल की पनाहगाह में तब्दील होने और सामाजिक स्मृति के तलघर में दीर्घ अंतराल तक पडेÞ रहने, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आकांक्षा की आभा में जनचेतना में इसके उभर उठने और फिर इसे सैन्यबल के कब्जे से मुक्त कर रंगशाला के रूप में वापस बहाल करने की गाथा के अभिप्राय एक प्रदेश तक सीमित नहीं, उनकी एक सार्वभौमिक व्यापकता है।
पिछली सदी के छठे दशक में प्रेमचंद रंगशाला का बनना एक नई राष्ट्रीय सांस्कृतिक सांस्थानिक गतिविधि का परिणाम कहा जा सकता है। इसकी परिकल्पना प्रख्यात नाटककार और बिहार सरकार में उच्च पदाधिकारी जगदीश चंद्र माथुर की बताई जाती है। वह दौर नई सांस्थानिक कल्पना का था। इसलिए आश्चर्य नहीं कि यह रंगशाला बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के ठीक बगल में बनाई गई। परिषद की योजना से भी माथुर साहब का जुड़ाव रहा था। इन दोनों के बीच बिहार ग्रंथ अकादमी दिखाई पड़ जाती थी। रंगशाला का नाम प्रेमचंद पर होने का कोई कारण नहीं था, सिवाय इसके कि इसके करीब चौराहे पर प्रेमचंद की एक प्रतिमा लगाई गई और उसके अनावरण के समय अमृत राय और महादेवी वर्मा की उपस्थिति में ही राजकीय रंगशाला को प्रेमचंद राजकीय रंगशाला घोषित करने का निर्णय लिया गया।
लेकिन रंगशाला बनने के फौरन बाद यानी 1971-72 में इसके पहले कार्यक्रम में ही किसी अव्यवस्था के चलते भड़क उठे लोगों ने इसमें आग लगा दी। कायदे से इसे दुबारा ठीक करके नाट्य-प्रदर्शन के लिए उपलब्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। छठे दशक की समाप्ति को भारतीय नव राष्ट्रीय रोमांटिक दौर की समाप्ति का समय भी कहा जा सकता है। संस्थाओं के स्थापित होने और जनता के साथ उनके रिश्ते बनने के पहले ही उनके प्रति अविश्वास जड़ जमाने लगा था और सामान्य जन का किसी भी राजकीय सांस्थानिक प्रयास के साथ एक प्रकार का उपयोगितावादी और सिनिक, संदेह से भरा संबंध बन गया था। यह बात शिक्षा से लेकर संस्कृति के क्षेत्र तक देखी जा सकती है।
छठे दशक में राजकीय संस्था-तंत्र को ही ध्वस्त कर देने के विचार ने युवाओं के बीच बौद्धिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। राज्य भी जल्दी ही असली राजनीति में व्यस्त होने वाला था । साथ ही नव-निर्माण के लिए जो जीवट चाहिए था उसकी कमी के कारण उस परियोजना से ही उदासीन होते चला जाना उसके लिए स्वाभाविक था। नाटक यों भी समाज के लिए हाशिये की चीज है और जब तक किसी राष्ट्रीय हित-पूर्ति के साधन के रूप में उसकी उपयोगिता स्पष्ट न हो, राज्य के लिए वह महत्त्वपूर्ण नहीं।
प्रेमचंद रंगशाला के जन्म के साथ ही उसके साथ हुई यह दुर्घटना एक रूपक के तौर पर देखी जा सकती है। 1974 बिहार के छात्र आंदोलन के लिए याद किया जाता है। इसका सामना करने के लिए बिहार सरकार ने जो अर्ध-सैन्यबल (सीआरपीएफ) बुलाया था, उसे रखने के लिए इस बेकार पड़ी रंगशाला से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। इस पर आपत्ति करने का वह समय भी नहीं था। आपातकाल लगाया गया, हटा भी, चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को जनता ने सत्ता से बेदखल भी कर दिया। जो जनता पार्टी सत्ता में आई, उसकी सरकार के लिए भी रंगशाला में सीआरपीएफ का होना सांस्कृतिक विसंगति न थी। इस तरह एक नई संस्था बनने के तुरंत बाद अवचेतन का अंग बन गई। समाज ने उसे फिर आंख उठा कर देखना जरूरी नहीं समझा।
मार्क्सवाद की सरल समझ के मुताबिक भौतिक अवस्था से चेतना का स्तर निर्धारित होता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि चेतना या कल्पना नई भौतिक परिस्थिति को जन्म देती है। ऐसा ही कुछ प्रेमचंद रंगशाला के साथ हुआ। कौन जानता था कि प्रेस की आजादी का मसला इस रंगशाला को सामूहिक स्मृति के तलघर से निकाल कर सतह पर ले आएगा। 1982 में बिहार में जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार ने प्रेस विधेयक लागू करने की घोषणा की। यह एक विडंबनापूर्ण संयोग था कि प्रेमचंद के जन्मदिवस, 31 जुलाई (1982) को बिहार विधानसभा ने सिर्फ पांच मिनट में एक ऐसा अधिनियम पारित कर दिया जो प्रेस को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दे सकता था।
इसके अनुसार 'अशोभन और अश्लील और ईश-निंदा करने वाले या ब्लैकमेल के इरादे से' किए गए किसी भी प्रकाशन पर कार्रवाई की जा सकती थी। इसे एक गैर-जमानती अपराध बना दिया गया था और इस पर कार्रवाई करने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट की जगह अधिशासी मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था। फौरन ही बिहार समेत पूरे देश में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ट्रेड यूनियन, छात्र और युवा संगठन और गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दल इसके विरुद्ध संगठित हो गए और तीन सितंबर, 1982 को देशव्यापी हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
प्रेस विधेयक ऊपरी तौर पर प्रेस का मामला था। लेकिन आपातकाल अभी बहुत पीछे नहीं छूटा था और जनता किसी भी तरह अपनी नई हासिल की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंवाने के मूड में न थी। इसलिए पत्रकारों के साथ हर तबका इसके खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। ठीक इसी राजनीतिक क्षण में पटना के कुछ तरुण रंगकर्मियों ने यह तय किया कि अगर प्रेमचंद रंगशाला को व्यापक दिलचस्पी का मुद्दा बनाना है तो इसे अभिव्यक्ति की सिकुड़ती जगह के एक प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। 1982 के अंतिम महीनों में राजकीय युवा महोत्सव को ऐसे अवसर के रूप में देखा गया जहां इस बात को जोरदार ढंग से उठाया जा सकता था।
पहली कार्रवाई इस तरह प्रेस विधेयक के विरोध और प्रेमचंद रंगशाला से सीआरपीएफ को हटाने की मांगों को साथ-साथ रख कर की गई। पहली बार युवा महोत्सव के पारितोषिक वितरण के बहिष्कार की इस कार्रवाई में तरुणों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें रिहा करने के लिए पटना के मुख्य अशोक राजपथ को देर रात तक जाम भी किया गया। आज तीस साल बाद यह सोच कर जरा हैरानी होती है कि कैसे बिना किसी सैद्धांतिक और राजनीतिक प्रशिक्षण के एक राजनीतिक रूप से परिपक्व आंदोलनात्मक रणनीति कुछ तरुण बना पा रहे थे।
प्रेस विधेयक तो वापस ले लिया गया। इस तरह प्रेमचंद रंगशाला का मुद्दा, जो कलाकारों के आंदोलन में दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर आप-ही आप आ गया। 1982 से यह संघर्ष काफी लंबा चलने वाला था। शहर में सभा-गृहों का न होना या रंगशाला का बंद रहना क्यों महत्त्व का मुद्दा होना चाहिए, यह समझाना बड़ा कठिन था।
राजनीतिक दलों की इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। प्रेस निहायत ही उदासीन था। उस समय बिहार में आर्यावर्त, प्रदीप, सर्चलाइट और इंडियन नेशन का राज था; आंदोलनकारी खबर लिए डोलते रहते थे और कृपापूर्वक भीतर के पृष्ठों पर कभी तीन तो कभी चार पंक्तियों की जरा सी जगह दे दी जाती थी। यह तो हिंदुस्तान टाइम्स था जिसने पहली बार इसे पहले पेज पर प्रकाशित किया।
वर्ष 1982 से प्रेमचंद रंगशाला को सीआरपीएफ के कब्जे से मुक्त कराने का यह कलाकारों का आंदोलन कई मायनों में दिलचस्प था। एक तो इसी कारण कि इसके नेतृत्व की औसत उम्र कोई बीस-इक्कीस साल की थी। दूसरे कि अलग-अलग काम करने वाले रंग-समूहों का किसी एक मसले पर भी साथ काम करना इतना आसान नहीं था। इसके नेतृत्व में इप्टा के लोग थे, लेकिन उनमें इतनी समझदारी थी कि वे खुद को ही आगे न रखें। उस समय पटना में सक्रिय संस्थाओं में सर्जना, नवजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा, जनवादी कला-विचार मंच आदि ने इस आंदोलन की शुरुआत की और जल्दी ही पैंतीस से ऊपर रंगकर्मियों और लेखकों-कलाकारों की संस्थाएं इस मंच पर इकट््ठा हो गर्इं। इसके साथ छात्र संगठन भी शरीक हो गए।
आंदोलन ने कई उतार-चढ़ाव देखे। ऐसा लगा कि इसका चलना ही मुश्किल है, क्योंकि कोई अंत नजर नहीं आता था। 1985 में राज्य द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के बहिष्कार और उसके समांतर प्रेमचंद युवा महोत्सव के आयोजन का आह्वान भी अनेक लोगों को दुस्साहस लगा। लेकिन इसे अपूर्व सफलता मिली। इसके बावजूद प्रेमचंद रंगशाला एक प्रादेशिक और क्षेत्रीय मुद्दा ही था। आंदोलनकारी भी पहले से अधिक वयस्क हो गए थे। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि उनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर पर आदर के साथ देखे जाने लगे थे, अपनी रंग-प्रतिभा के कारण। इसने बिहार तक सीमित इस मसले को राष्ट्रीय फलक प्रदान करने में मदद की। 1985 में गुवाहाटी के संगीत नाटक अकादेमी के नाट्य-उत्सव के मंच पर इसे उठाया गया और ब. व. कारंत ने खुल कर इस कब्जे की भर्त्सना की।
वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादेमी ने पटना में पूर्व-क्षेत्रीय नाट्योत्सव आयोजित किया। इसमें नेमिचंद्र जैन, ब. व. कारंत, रतन थियम, कुमार राय, देवाशीष मजुमदार जैसी शख्सियतें एकत्र हुर्इं। आंदोलनकारियों ने उद््घाटन के मंच पर कब्जा करके संपूर्ण भारतीय रंग-संसार से प्रेमचंद रंगशाला के उद्धार में हाथ बढ़ाने की अपील की। अगले दिन नेमिजी, कारंत, कुमार राय, देवाशीष मजुमदार के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ और फिर ये सब तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे से मिलने गए। महोत्सव खत्म होने के दिन ही मुख्यमंत्री ने रंगशाला से सीआरपीएफ को हटा लेने की घोषणा की।
इस घोषणा के कोई चौथाई सदी गुजर जाने के बाद अब जाकर इस रंगशाला को फिर से इस लायक बनाया जा सका है कि इसमें नाटक हो सकें। इस मौके पर बिहार सरकार की विज्ञप्ति ने कलाकारों के संघर्ष को याद किया है। लेकिन रंगकर्मियों की आशंका कुछ और है। अभी पटना में कोई ऐसा प्रेक्षागृह नहीं जहां शौकिया रंग-समूह अपने सीमित साधनों में नाटक कर सकें। पचीस हजार से पचास हजार रुपए किराए पर हॉल लेकर नाटक करने की क्षमता किसी में नहीं।
फिर बडेÞ भव्य ढंग से तैयार की गई इस प्रेमचंद रंगशाला को भी क्या इसी तरह रंग-कर्म के लिए इतना महंगा कर दिया जाएगा कि उसमें नाटक हो ही न सकें। या जो सलूक इस सरकर ने हिंदी भवन के साथ किया, क्या वही इसके साथ भी होगा। एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए गए हिंदी भवन को प्रबंधन संस्थान के हवाले कर देने में सरकार को संकोच नहीं हुआ। लेखकों की गुहार को उसने बिल्कुल अनसुना कर दिया। क्या यह रंगशाला भी उसी राह जाएगी? फिर अभिव्यक्ति की जिस जगह के सिकुड़ने के खिलाफ यह रंगशाला एक प्रतीक बन गई थी, वह क्या दूसरे तरीके से उतनी ही संकुचित रह जाएगी? |







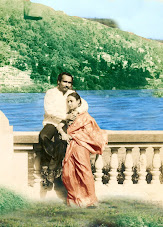












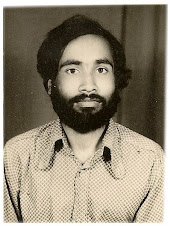

No comments:
Post a Comment